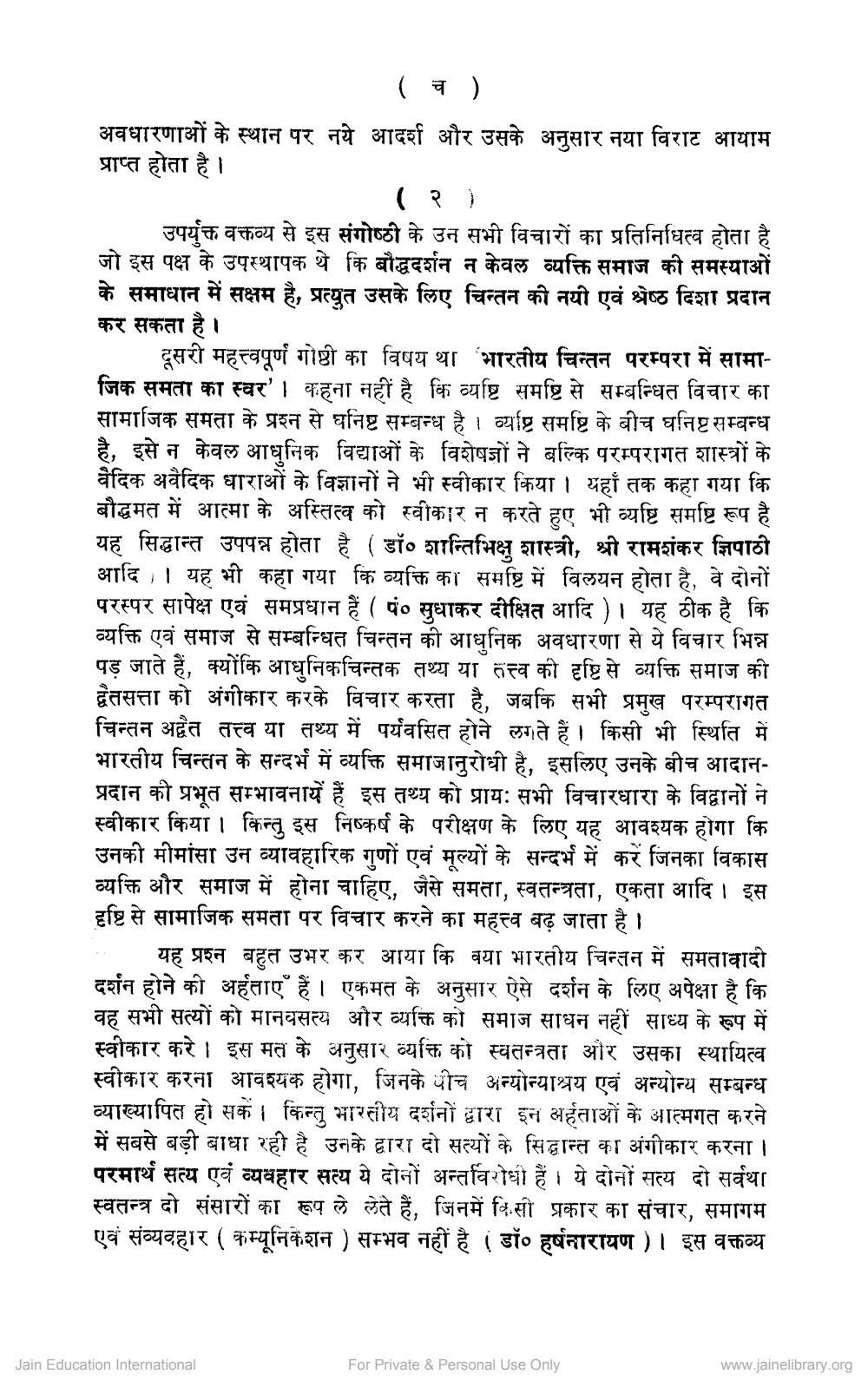________________
( च ) अवधारणाओं के स्थान पर नये आदर्श और उसके अनुसार नया विराट आयाम प्राप्त होता है।
उपर्युक्त वक्तव्य से इस संगोष्ठी के उन सभी विचारों का प्रतिनिधित्व होता है जो इस पक्ष के उपस्थापक थे कि बौद्धदर्शन न केवल व्यक्ति समाज की समस्याओं के समाधान में सक्षम है, प्रत्युत उसके लिए चिन्तन की नयी एवं श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकता है।
दूसरी महत्त्वपूर्ण गोष्ठी का विषय था भारतीय चिन्तन परम्परा में सामाजिक समता का स्वर'। कहना नहीं है कि व्यष्टि समष्टि से सम्बन्धित विचार का सामाजिक समता के प्रश्न से घनिष्ट सम्बन्ध है। व्यष्टि समष्टि के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है, इसे न केवल आधुनिक विद्याओं के विशेषज्ञों ने बल्कि परम्परागत शास्त्रों के वैदिक अवैदिक धाराओं के विज्ञानों ने भी स्वीकार किया। यहाँ तक कहा गया कि बौद्धमत में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए भी व्यष्टि समष्टि रूप है यह सिद्धान्त उपपन्न होता है ( डॉ० शान्तिभिक्षु शास्त्री, श्री रामशंकर ज्ञिपाठी आदि । यह भी कहा गया कि व्यक्ति का समष्टि में विलयन होता है, वे दोनों परस्पर सापेक्ष एवं समप्रधान हैं ( पं० सुधाकर दीक्षित आदि )। यह ठीक है कि व्यक्ति एवं समाज से सम्बन्धित चिन्तन की आधुनिक अवधारणा से ये विचार भिन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि आधुनिकचिन्तक तथ्य या तत्त्व की दृष्टि से व्यक्ति समाज की द्वैतसत्ता को अंगीकार करके विचार करता है, जबकि सभी प्रमुख परम्परागत चिन्तन अद्वैत तत्त्व या तथ्य में पर्यवसित होने लगते हैं। किसी भी स्थिति में भारतीय चिन्तन के सन्दर्भ में व्यक्ति समाजानुरोधी है, इसलिए उनके बीच आदानप्रदान की प्रभूत सम्भावनायें हैं इस तथ्य को प्रायः सभी विचारधारा के विद्वानों ने स्वीकार किया। किन्तु इस निष्कर्ष के परीक्षण के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी मीमांसा उन व्यावहारिक गुणों एवं मूल्यों के सन्दर्भ में करें जिनका विकास व्यक्ति और समाज में होना चाहिए, जैसे समता, स्वतन्त्रता, एकता आदि। इस दृष्टि से सामाजिक समता पर विचार करने का महत्त्व बढ़ जाता है।
___यह प्रश्न बहुत उभर कर आया कि क्या भारतीय चिन्तन में समतावादी दर्शन होने की अर्हताएं हैं। एकमत के अनुसार ऐसे दर्शन के लिए अपेक्षा है कि वह सभी सत्यों को मानवसत्य और व्यक्ति को समाज साधन नहीं साध्य के रूप में स्वीकार करे। इस मत के अनुसार व्यक्ति को स्वतन्त्रता और उसका स्थायित्व स्वीकार करना आवश्यक होगा, जिनके पीच अन्योन्याश्रय एवं अन्योन्य सम्बन्ध व्याख्यापित हो सके। किन्तु भारतीय दर्शनों द्वारा इन अर्हताओं के आत्मगत करने में सबसे बड़ी बाधा रही है उनके द्वारा दो सत्यों के सिद्धान्त का अंगीकार करना । परमार्थ सत्य एवं व्यवहार सत्य ये दोनों अन्तविरोधी हैं। ये दोनों सत्य दो सर्वथा स्वतन्त्र दो संसारों का रूप ले लेते हैं, जिनमें किसी प्रकार का संचार, समागम एवं संव्यवहार ( कम्यूनिकेशन ) सम्भव नहीं है ( डॉ० हर्षनारायण )। इस वक्तव्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org