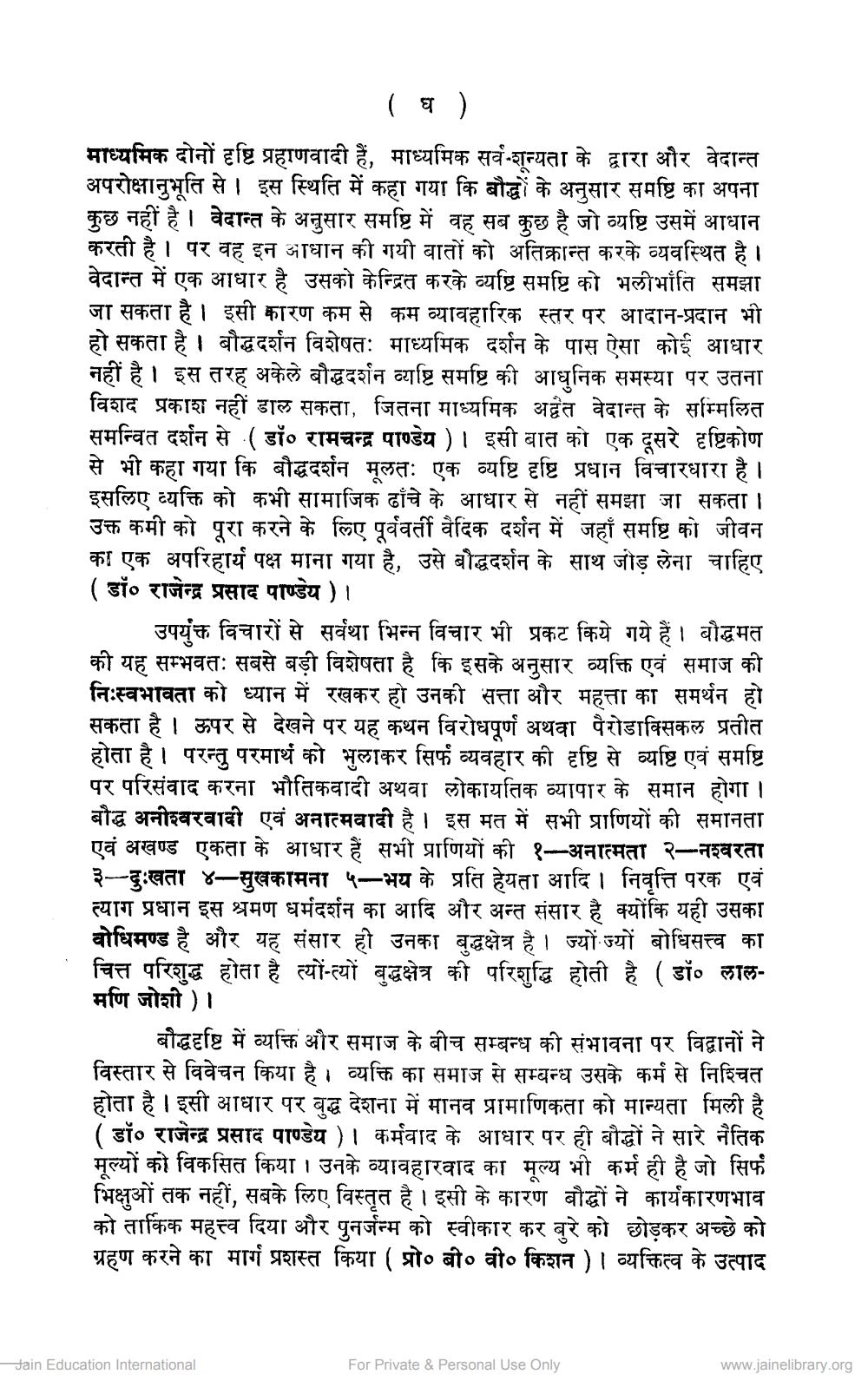________________
( घ ) माध्यमिक दोनों दृष्टि प्रहाणवादी हैं, माध्यमिक सर्व-शून्यता के द्वारा और वेदान्त अपरोक्षानुभूति से । इस स्थिति में कहा गया कि बौद्धों के अनुसार समष्टि का अपना कुछ नहीं है । वेदान्त के अनुसार समष्टि में वह सब कुछ है जो व्यष्टि उसमें आधान करती है। पर वह इन आधान की गयी बातों को अतिक्रान्त करके व्यवस्थित है। वेदान्त में एक आधार है उसको केन्द्रित करके व्यष्टि समष्टि को भलीभांति समझा जा सकता है। इसी कारण कम से कम व्यावहारिक स्तर पर आदान-प्रदान भी हो सकता है। बौद्ध दर्शन विशेषतः माध्यमिक दर्शन के पास ऐसा कोई आधार नहीं है। इस तरह अकेले बौद्धदर्शन व्यष्टि समष्टि की आधुनिक समस्या पर उतना विशद प्रकाश नहीं डाल सकता, जितना माध्यमिक अद्वैत वेदान्त के सम्मिलित समन्वित दर्शन से ( डॉ० रामचन्द्र पाण्डेय )। इसी बात को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी कहा गया कि बौद्धदर्शन मूलतः एक व्यष्टि दृष्टि प्रधान विचारधारा है । इसलिए व्यक्ति को कभी सामाजिक ढाँचे के आधार से नहीं समझा जा सकता। उक्त कमी को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती वैदिक दर्शन में जहाँ समष्टि को जीवन का एक अपरिहार्य पक्ष माना गया है, उसे बौद्धदर्शन के साथ जोड़ लेना चाहिए (डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय )।
उपर्यक्त विचारों से सर्वथा भिन्न विचार भी प्रकट किये गये हैं। बौद्धमत की यह सम्भवतः सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अनुसार व्यक्ति एवं समाज की निःस्वभावता को ध्यान में रखकर हो उनकी सत्ता और महत्ता का समर्थन हो सकता है । ऊपर से देखने पर यह कथन विरोधपूर्ण अथवा पैरोडाक्सिकल प्रतीत होता है। परन्तु परमार्थ को भुलाकर सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से व्यष्टि एवं समष्टि पर परिसंवाद करना भौतिकवादी अथवा लोकायतिक व्यापार के समान होगा। बौद्ध अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। इस मत में सभी प्राणियों की समानता एवं अखण्ड एकता के आधार हैं सभी प्राणियों की १-अनात्मता २-नश्वरता ३-दुःखता ४-सुखकामना ५-भय के प्रति हेयता आदि । निवृत्ति परक एवं त्याग प्रधान इस श्रमण धर्मदर्शन का आदि और अन्त संसार है क्योंकि यही उसका वोधिमण्ड है और यह संसार ही उनका बुद्धक्षेत्र है। ज्यों ज्यों बोधिसत्त्व का चित्त परिशुद्ध होता है त्यों-त्यों बुद्धक्षेत्र की परिशुद्धि होती है ( डॉ० लालमणि जोशी )।
बौद्धदृष्टि में व्यक्ति और समाज के बीच सम्बन्ध की संभावना पर विद्वानों ने विस्तार से विवेचन किया है। व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध उसके कर्म से निश्चित होता है । इसी आधार पर बुद्ध देशना में मानव प्रामाणिकता को मान्यता मिली है (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय )। कर्मवाद के आधार पर ही बौद्धों ने सारे नैतिक मूल्यों को विकसित किया। उनके व्यावहारवाद का मूल्य भी कर्म ही है जो सिर्फ भिक्षुओं तक नहीं, सबके लिए विस्तृत है । इसी के कारण बौद्धों ने कार्यकारणभाव को तार्किक महत्त्व दिया और पुनर्जन्म को स्वीकार कर बुरे को छोड़कर अच्छे को ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया (प्रो० बी० वी० किशन )। व्यक्तित्व के उत्पाद
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org