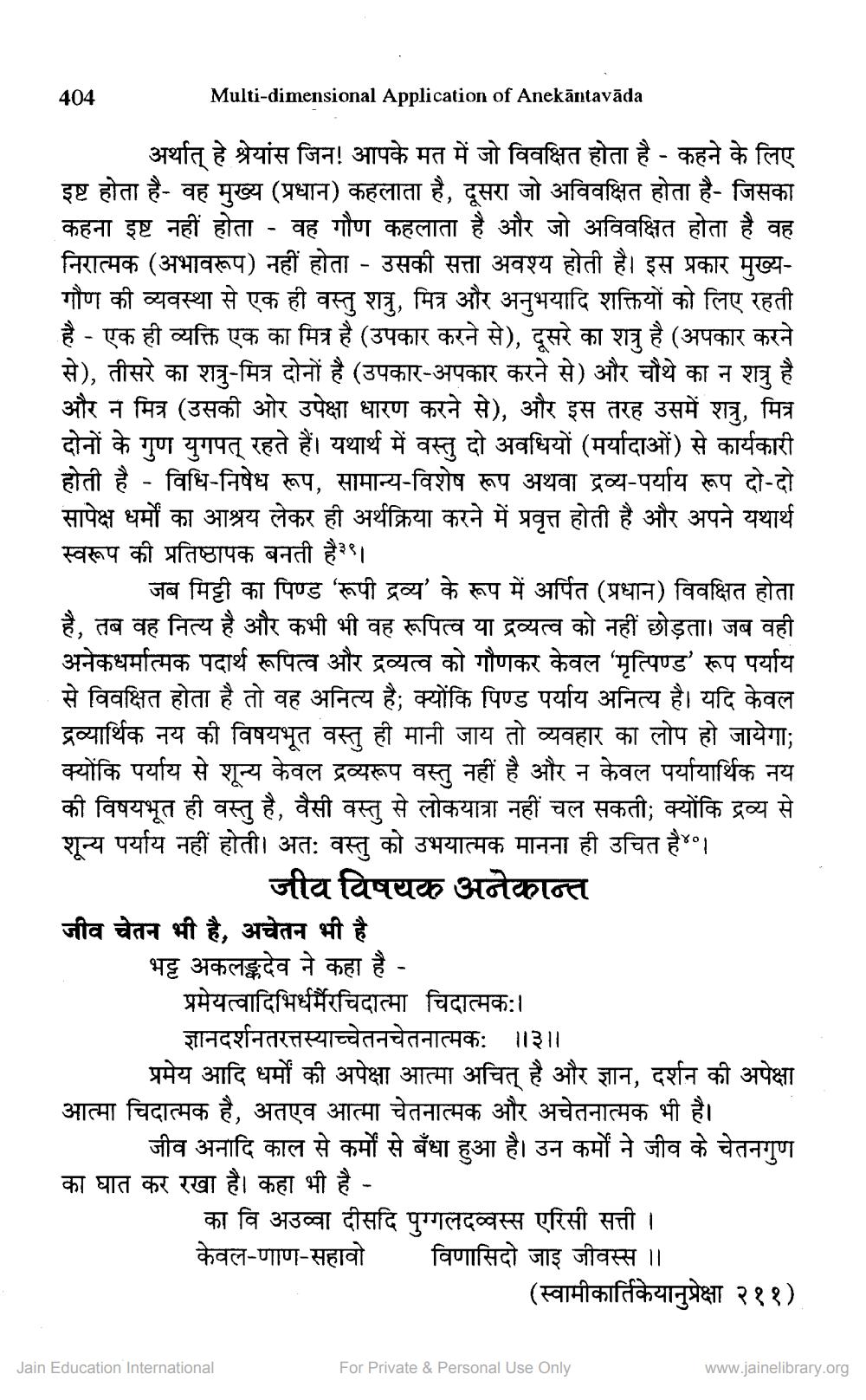________________
Multi-dimensional Application of Anekāntavāda
अर्थात् हे श्रेयांस जिन! आपके मत में जो विवक्षित होता है - कहने के लिए इष्ट होता है - वह मुख्य (प्रधान) कहलाता है, दूसरा जो अविवक्षित होता है - जिसका कहना इष्ट नहीं होता वह गौण कहलाता है और जो अविवक्षित होता है वह निरात्मक (अभावरूप) नहीं होता उसकी सत्ता अवश्य होती है। इस प्रकार मुख्यगौण की व्यवस्था से एक ही वस्तु शत्रु, मित्र और अनुभयादि शक्तियों को लिए रहती है - एक ही व्यक्ति एक का मित्र है (उपकार करने से ), दूसरे का शत्रु है (अपकार करने से), तीसरे का शत्रु-मित्र दोनों है (उपकार - अपकार करने से ) और चौथे का न शत्रु है और न मित्र (उसकी ओर उपेक्षा धारण करने से ), और इस तरह उसमें शत्रु, मित्र दोनों के गुण युगपत् रहते हैं। यथार्थ में वस्तु दो अवधियों (मर्यादाओं) से कार्यकारी होती है - विधि - निषेध रूप, सामान्य- विशेष रूप अथवा द्रव्य-पर्याय रूप दो-दो सापेक्ष धर्मों का आश्रय लेकर ही अर्थक्रिया करने में प्रवृत्त होती है और अपने यथार्थ स्वरूप की प्रतिष्ठापक बनती है ३९ ।
404
जब मिट्टी का पिण्ड 'रूपी द्रव्य' के रूप में अर्पित (प्रधान) विवक्षित होता है, तब वह नित्य है और कभी भी वह रूपित्व या द्रव्यत्व को नहीं छोड़ता। जब वही अनेकधर्मात्मक पदार्थ रूपित्व और द्रव्यत्व को गौणकर केवल 'मृत्पिण्ड' रूप पर्याय से विवक्षित होता है तो वह अनित्य है; क्योंकि पिण्ड पर्याय अनित्य है। यदि केवल द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत वस्तु ही मानी जाय तो व्यवहार का लोप हो जायेगा; क्योंकि पर्याय से शून्य केवल द्रव्यरूप वस्तु नहीं है और न केवल पर्यायार्थिक नय की विषयभूत ही वस्तु है, वैसी वस्तु से लोकयात्रा नहीं चल सकती; क्योंकि द्रव्य से शून्य पर्याय नहीं होती । अतः वस्तु को उभयात्मक मानना ही उचित है ४ । जीव विषयक अनेकान्त
जीव चेतन भी है, अचेतन भी है
भट्ट अकलङ्कदेव ने कहा है
प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः । ज्ञानदर्शनतरत्तस्याच्चेतनचेतनात्मकः ॥३॥
प्रमेय आदि धर्मों की अपेक्षा आत्मा अचित् है और ज्ञान, दर्शन की अपेक्षा आत्मा चिदात्मक है, अतएव आत्मा चेतनात्मक और अचेतनात्मक भी है। जीव अनादि काल से कर्मों से बँधा हुआ है। उन कर्मों ने जीव के चेतनगुण का घात कर रखा है। कहा भी है -
का वि अउव्वा दीसदि पुग्गलदव्वस्स एरिसी सत्ती केवल - णाण-सहावो विणासिदो जाइ जीवस्स ||
Jain Education International
( स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा २११ )
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org