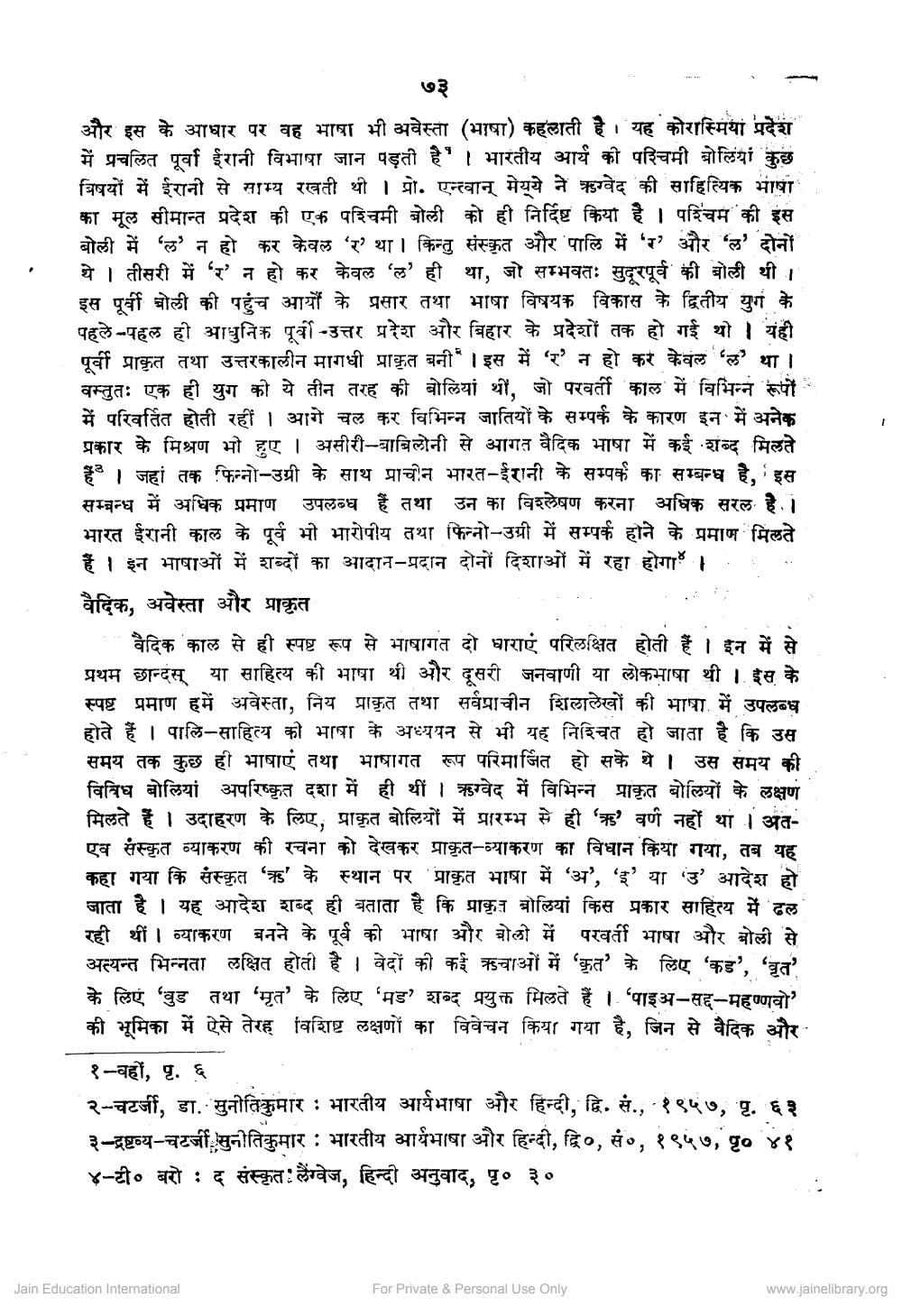________________
और इस के आधार पर वह भाषा भी अवेस्ता (भाषा) कहलाती है। यह कोरास्मिया प्रदेश में प्रचलित पूर्वा ईरानी विभाषा जान पड़ती है । भारतीय आर्य की पश्चिमी बोलियां कुछ विषयों में ईरानी से साम्य रखती थी । प्रो. एन्त्वान् मेयये ने ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा का मूल सीमान्त प्रदेश की एक पश्चिमी बोली को ही निर्दिष्ट किया है । पश्चिम की इस बोली में 'ल' न हो कर केवल 'र' था। किन्तु संस्कृत और पालि में 'र' और 'ल' दोनों थे । तीसरी में 'र' न हो कर केवल 'ल' ही था, जो सम्भवतः सुदूरपूर्व की बोली थी। इस पूर्वी बोली की पहुंच आर्यों के प्रसार तथा भाषा विषयक विकास के द्वितीय युग के पहले-पहल ही आधुनिक पूर्वी - उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रदेशों तक हो गई थी। यही पूर्वी प्राकृत तथा उत्तरकालीन मागधी प्राकृत बनी । इस में 'र' न हो कर केवल 'ल' था। वस्तुतः एक ही युग की ये तीन तरह की बोलियां थीं, जो परवर्ती काल में विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहीं । आगे चल कर विभिन्न जातियों के सम्पर्क के कारण इन में अनेक प्रकार के मिश्रण भो हुए । असीरी-बाबिलोनी से आगत वैदिक भाषा में कई शब्द मिलते हैं । जहां तक फिन्नो-उग्री के साथ प्राचीन भारत-ईरानी के सम्पर्क का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं तथा उन का विश्लेषण करना अधिक सरल है । भारत ईरानी काल के पूर्व भी भारोपीय तथा फिन्नो-उग्री में सम्पर्क होने के प्रमाण मिलते हैं । इन भाषाओं में शब्दों का आदान-प्रदान दोनों दिशाओं में रहा होगा । . .. वैदिक, अवेस्ता और प्राकृत
वैदिक काल से ही स्पष्ट रूप से भाषागत दो धाराएं परिलक्षित होती हैं । इन में से प्रथम छान्दस् या साहित्य की भाषा थी और दूसरी जनवाणी या लोकभाषा थी । इस के स्पष्ट प्रमाण हमें अवेस्ता, निय प्राकृत तथा सर्वप्राचीन शिलालेखों की भाषा में उपलब्ध होते हैं । पालि-साहित्य को भाषा के अध्ययन से भी यह निश्चित हो जाता है कि उस समय तक कुछ ही भाषाएं तथा भाषागत रूप परिमार्जित हो सके थे। उस समय की विविध बोलियां अपरिष्कृत दशा में ही थीं । ऋग्वेद में विभिन्न प्राकृत बोलियों के लक्षण मिलते हैं । उदाहरण के लिए, प्राकृत बोलियों में प्रारम्भ से ही 'ऋ' वर्ण नहीं था । अतएव संस्कृत व्याकरण की रचना को देखकर प्राकृत-व्याकरण का विधान किया गया, तब यह कहा गया कि संस्कृत 'ऋ' के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'अ', 'इ' या 'उ' आदेश हो जाता है । यह आदेश शब्द ही बताता है कि प्राकृत बोलियां किस प्रकार साहित्य में ढल रही थीं। व्याकरण बनने के पूर्व की भाषा और बोलो में परवर्ती भाषा और बोली से अत्यन्त भिन्नता लक्षित होती है । वेदों की कई ऋचाओं में 'कृत' के लिए 'कड', 'वृत' के लिए 'वुड तथा 'मृत' के लिए 'मड' शब्द प्रयुक्त मिलते हैं । 'पाइअ-सद्द-महण्णवो' की भूमिका में ऐसे तेरह विशिष्ट लक्षणों का विवेचन किया गया है, जिन से वैदिक और १-वहों, पृ. ६ २-चटर्जी, डा. सुनोतिकुमार : भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, द्वि. सं., १९५७, पृ. ६३ ३-द्रष्टव्य-चटर्जी सुनीतिकुमार : भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, द्वि०, सं०, १९५७, पृ० ४१ ४-टी० बरो : द संस्कृत : लैंग्वेज, हिन्दी अनुवाद, पृ० ३०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org