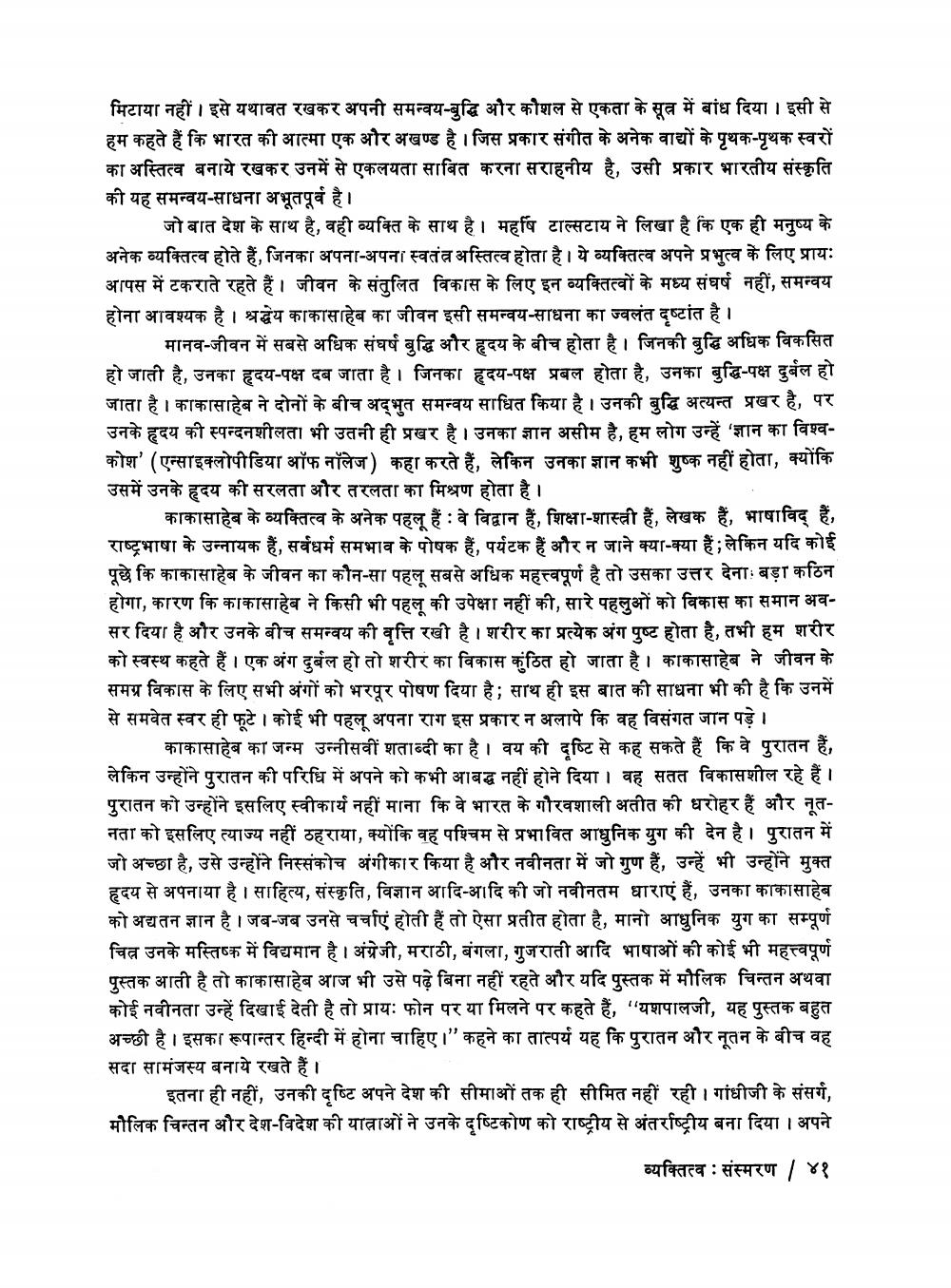________________
मिटाया नहीं। इसे यथावत रखकर अपनी समन्वय-बुद्धि और कौशल से एकता के सूत्र में बांध दिया। इसी से हम कहते हैं कि भारत की आत्मा एक और अखण्ड है। जिस प्रकार संगीत के अनेक वाद्यों के पृथक-पृथक स्वरों का अस्तित्व बनाये रखकर उनमें से एकलयता साबित करना सराहनीय है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की यह समन्वय-साधना अभूतपूर्व है।
जो बात देश के साथ है, वही व्यक्ति के साथ है। महर्षि टाल्सटाय ने लिखा है कि एक ही मनुष्य के अनेक व्यक्तित्व होते हैं, जिनका अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये व्यक्तित्व अपने प्रभुत्व के लिए प्रायः आपस में टकराते रहते हैं। जीवन के संतुलित विकास के लिए इन व्यक्तित्वों के मध्य संघर्ष नहीं, समन्वय होना आवश्यक है। श्रद्धेय काकासाहेब का जीवन इसी समन्वय-साधना का ज्वलंत दृष्टांत है।
मानव-जीवन में सबसे अधिक संघर्ष बुद्धि और हृदय के बीच होता है। जिनकी बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है, उनका हृदय-पक्ष दब जाता है। जिनका हृदय-पक्ष प्रबल होता है, उनका बुद्धि-पक्ष दुर्बल हो जाता है। काकासाहेब ने दोनों के बीच अद्भुत समन्वय साधित किया है। उनकी बुद्धि अत्यन्त प्रखर है, पर उनके हृदय की स्पन्दनशीलता भी उतनी ही प्रखर है। उनका ज्ञान असीम है, हम लोग उन्हें 'ज्ञान का विश्वकोश' (एन्साइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज) कहा करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान कभी शुष्क नहीं होता, क्योंकि उसमें उनके हृदय की सरलता और तरलता का मिश्रण होता है।
काकासाहेब के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं : वे विद्वान हैं, शिक्षा-शास्त्री हैं, लेखक हैं, भाषाविद् हैं, राष्ट्रभाषा के उन्नायक हैं, सर्वधर्म समभाव के पोषक हैं, पर्यटक हैं और न जाने क्या-क्या हैं लेकिन यदि कोई पूछे कि काकासाहेब के जीवन का कौन-सा पहलू सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है तो उसका उत्तर देनाः बड़ा कठिन होगा, कारण कि काकासाहेब ने किसी भी पहलू की उपेक्षा नहीं की, सारे पहलुओं को विकास का समान अवसर दिया है और उनके बीच समन्वय की वृत्ति रखी है। शरीर का प्रत्येक अंग पुष्ट होता है, तभी हम शरीर को स्वस्थ कहते हैं। एक अंग दुर्बल हो तो शरीर का विकास कंठित हो जाता है। काकासाहेब ने जीवन के समग्र विकास के लिए सभी अंगों को भरपूर पोषण दिया है। साथ ही इस बात की साधना भी की है कि उनमें से समवेत स्वर ही फूटे । कोई भी पहलू अपना राग इस प्रकार न अलापे कि वह विसंगत जान पड़े।
काकासाहेब का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी का है। वय की दृष्टि से कह सकते हैं कि वे पुरातन हैं, लेकिन उन्होंने पुरातन की परिधि में अपने को कभी आबद्ध नहीं होने दिया। वह सतत विकासशील रहे हैं। पुरातन को उन्होंने इसलिए स्वीकार्य नहीं माना कि वे भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर हैं और नूतनता को इसलिए त्याज्य नहीं ठहराया, क्योंकि वह पश्चिम से प्रभावित आधुनिक युग की देन है। पुरातन में जो अच्छा है, उसे उन्होंने निस्संकोच अंगीकार किया है और नवीनता में जो गुण हैं, उन्हें भी उन्होंने मुक्त हृदय से अपनाया है । साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि-आदि की जो नवीनतम धाराएं हैं, उनका काकासाहेब को अद्यतन ज्ञान है । जब-जब उनसे चर्चाएं होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो आधुनिक युग का सम्पूर्ण चित्र उनके मस्तिष्क में विद्यमान है। अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की कोई भी महत्त्वपूर्ण पुस्तक आती है तो काकासाहेब आज भी उसे पढ़े बिना नहीं रहते और यदि पुस्तक में मौलिक चिन्तन अथवा कोई नवीनता उन्हें दिखाई देती है तो प्रायः फोन पर या मिलने पर कहते हैं, "यशपालजी, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। इसका रूपान्तर हिन्दी में होना चाहिए।" कहने का तात्पर्य यह कि पुरातन और नूतन के बीच वह सदा सामंजस्य बनाये रखते हैं।
इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। गांधीजी के संसर्ग, मौलिक चिन्तन और देश-विदेश की यात्राओं ने उनके दृष्टिकोण को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय बना दिया । अपने
व्यक्तित्व : संस्मरण | ४१