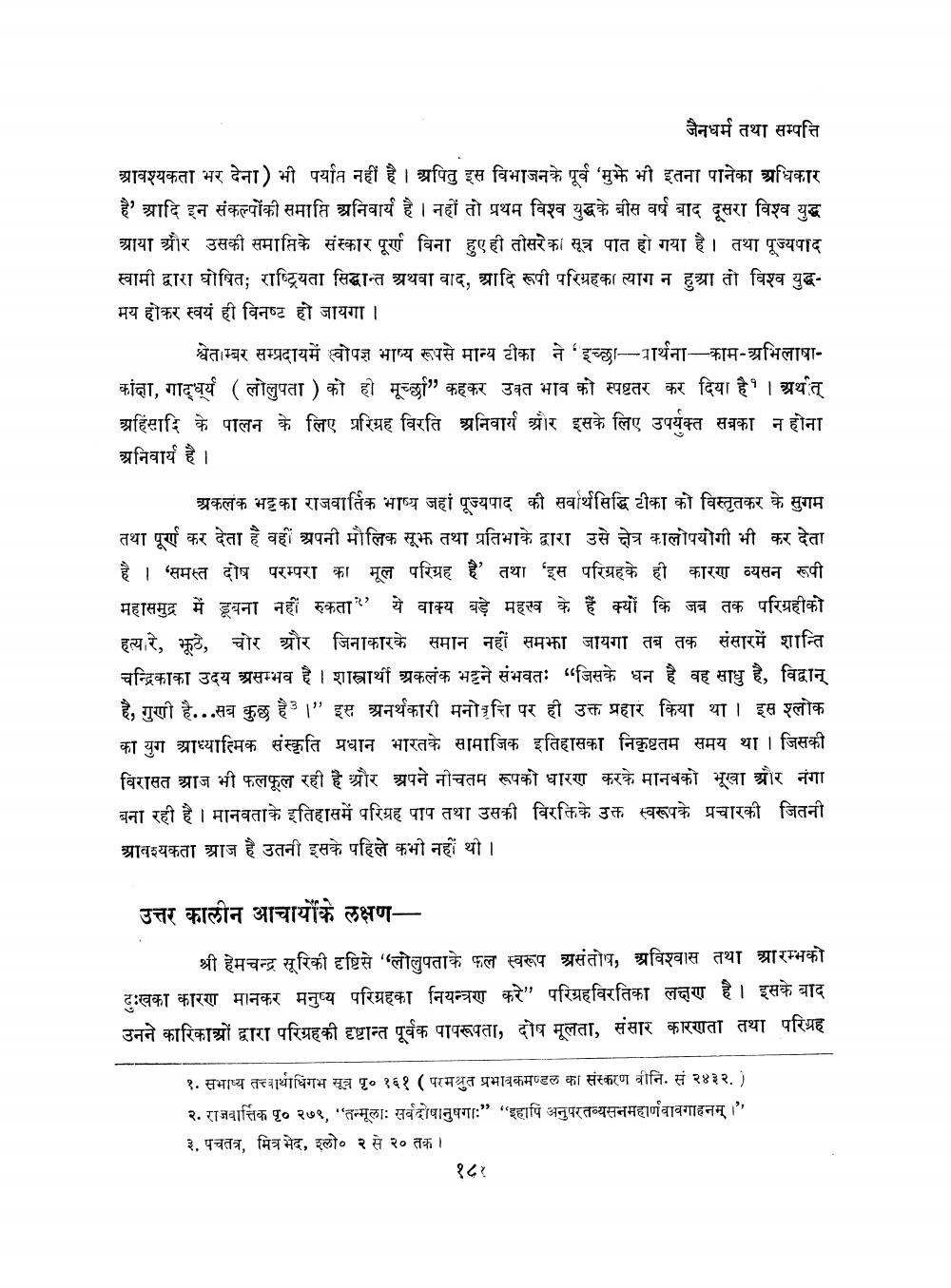________________
जैनधर्म तथा सम्पत्ति आवश्यकता भर देना ) भी पर्यात नहीं है । अपितु इस विभाजन के पूर्व 'मुझे भी इतना पानेका अधिकार है' आदि इन संकल्पोंकी समाप्ति अनिवार्य है । नहीं तो प्रथम विश्व युद्ध के बीस वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध
या और उसकी समाप्तिके संस्कार पूर्ण विना हुए ही तीसरेका सूत्र पात हो गया है । तथा पूज्यपाद स्वामी द्वारा घोषित; राष्ट्रियता सिद्धान्त अथवा वाद, यादि रूपी परिग्रहका त्याग न हुआ तो विश्व युद्धमय होकर स्वयं ही विनष्ट हो जायगा ।
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें त्वोपज्ञ भाग्य रूपसे मान्य टीका ने 'इच्छार्थना काम - अभिलाषाकांदा, गा (लोलुपता ) को ही मूर्च्छा" कहकर उक्त भाव को स्पष्टतर कर दिया है । अर्थात् अहिंसादि के पालन के लिए प्ररिग्रह विरति अनिवार्य और इसके लिए उपर्युक्त सत्रका न होना अनिवार्य है ।
कलंक भट्टका राजवार्तिक भाष्य जहां पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि टीका को विस्तृतकर के सुगम तथा पूर्ण कर देता है वहीं अपनी मौलिक सूझ तथा प्रतिभा के द्वारा उसे क्षेत्र कालोपयोगी भी कर देता है । 'समस्त दोष परम्परा का मूल परिग्रह है' तथा 'इस परिग्रहके ही कारण व्यसन रूपी महासमुद्र में डूबना नहीं रुकता " ये वाक्य बड़े महस्व के हैं क्यों कि जब तक परिग्रहीको हत्यारे, झूठे, चोर और जिनाकारके समान नहीं समझा जायगा तब तक संसारमें शान्ति चन्द्रिकाका उदय असम्भव है । शास्त्रार्थी कलंक भट्टने संभवतः "जिसके धन है वह साधु है, विद्वान् है, गुणी है... सब कुछ है ।" इस अनर्थकारी मनोवृत्ति पर ही उक्त प्रहार किया था। इस श्लोक का युग प्राध्यात्मिक संस्कृति प्रधान भारतके सामाजिक इतिहासका निकृष्टतम समय था । जिसकी विरासत आज भी फलफूल रही है और अपने नीचतम रूपको धारण करके मानवको भूखा और नंगा बना रही है । मानवता के इतिहास में परिग्रह पाप तथा उसकी विरक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी श्रावश्यकता श्राज है उतनी इसके पहिले कभी नहीं थी ।
उत्तर कालीन आचार्यों के लक्षण
श्री हेमचन्द्र सूरिकी दृष्टि से " लोलुपता के फल स्वरूप असंतोष, अविश्वास तथा आरम्भको दुःखका कारण मानकर मनुष्य परिग्रहका नियन्त्रण करे" परिग्रहविरतिका लक्षण है । इसके बाद उने कारिका द्वारा परिग्रह की दृष्टान्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, संसार कारणता तथा परिग्रह
१. सभाप्य तच्चार्थाधिगभ सूत्र पृ० १६१ ( परमश्रुत प्रभावकमण्डल का संस्करण वीनि. सं २४३२. ) २. राजवार्तिक पृ० २७९, " तन्मूला: सर्वदोषानुषगाः " " इहापि अनुपरतव्यसन महार्णवावगाहनम् ।" ३. पंचतंत्र, मित्रभेद, श्लो० २ से २० तक ।
१८९