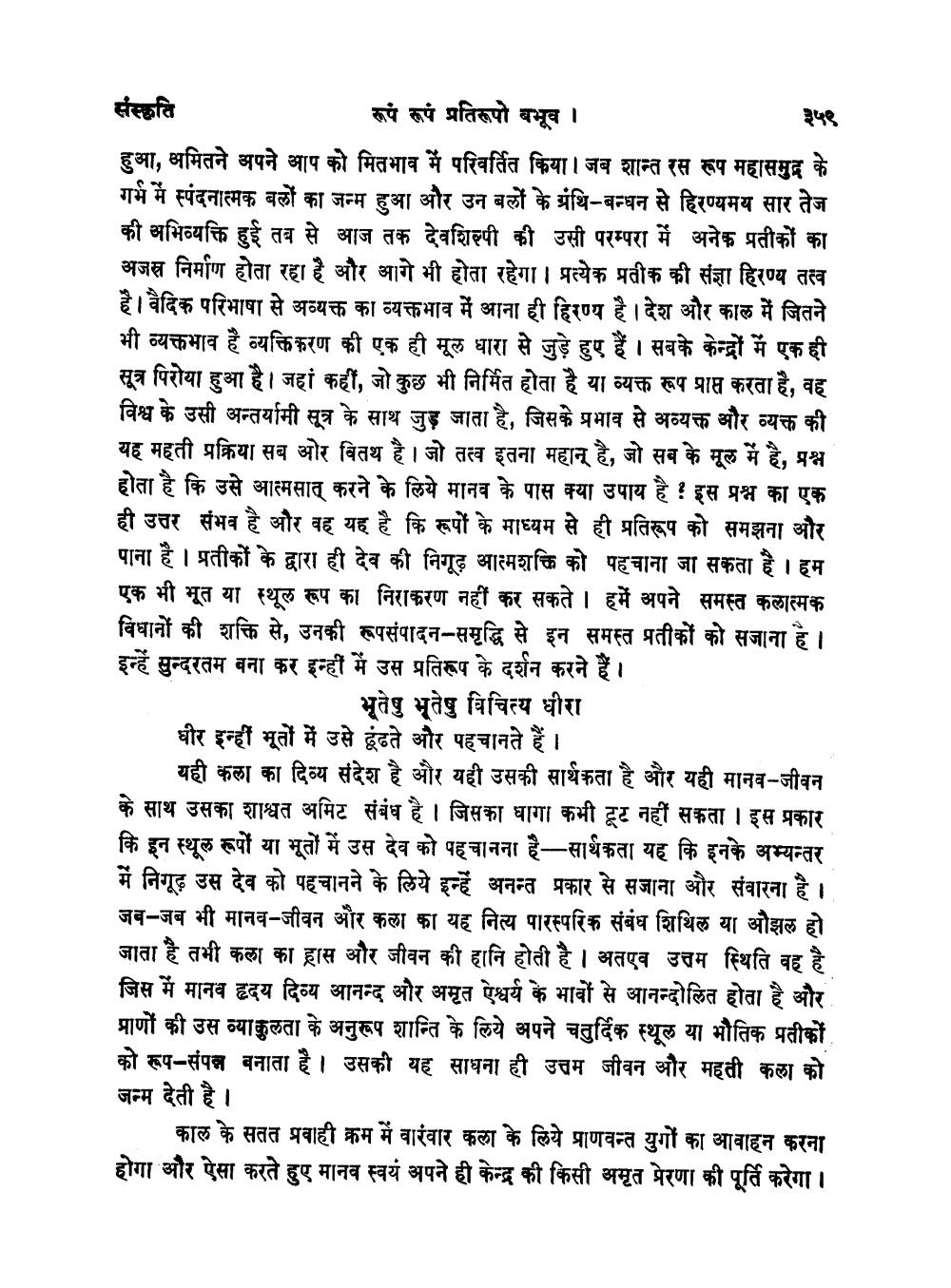________________
संस्कृति
३५९
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । हुआ, अमितने अपने आप को मितभाव में परिवर्तित किया। जब शान्त रस रूप महासमुद्र के गर्म में स्पंदनात्मक बलों का जन्म हुआ और उन बलों के ग्रंथि-बन्धन से हिरण्यमय सार तेज की अभिव्यक्ति हुई तब से आज तक देवशिल्पी की उसी परम्परा में अनेक प्रतीकों का अजस्र निर्माण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। प्रत्येक प्रतीक की संज्ञा हिरण्य तत्व है। वैदिक परिभाषा से अव्यक्त का व्यक्तभाव में आना ही हिरण्य है । देश और काल में जितने भी व्यक्तभाव है व्यक्तिकरण की एक ही मूल धारा से जुड़े हुए हैं। सबके केन्द्रों में एक ही सूत्र पिरोया हुआ है। जहां कहीं, जो कुछ भी निर्मित होता है या व्यक्त रूप प्राप्त करता है, वह विश्व के उसी अन्तर्यामी सूत्र के साथ जुड़ जाता है, जिसके प्रभाव से अव्यक्त और व्यक्त की यह महती प्रक्रिया सब ओर वितथ है । जो तत्व इतना महान् है, जो सव के मूल में है, प्रश्न होता है कि उसे आत्मसात् करने के लिये मानव के पास क्या उपाय है ! इस प्रश्न का एक ही उत्तर संभव है और वह यह है कि रूपों के माध्यम से ही प्रतिरूप को समझना और पाना है । प्रतीकों के द्वारा ही देव की निगूढ़ आत्मशक्ति को पहचाना जा सकता है । हम एक भी भूत या स्थूल रूप का निराकरण नहीं कर सकते । हमें अपने समस्त कलात्मक विधानों की शक्ति से, उनकी रूपसंपादन-समृद्धि से इन समस्त प्रतीकों को सजाना है। इन्हें सुन्दरतम बना कर इन्हीं में उस प्रतिरूप के दर्शन करने हैं।
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा धीर इन्हीं भूतों में उसे ढूंढते और पहचानते हैं।
यही कला का दिव्य संदेश है और यही उसकी सार्थकता है और यही मानव-जीवन के साथ उसका शाश्वत अमिट संबंध है । जिसका धागा कभी टूट नहीं सकता । इस प्रकार कि इन स्थूल रूपों या भूतों में उस देव को पहचानना है—सार्थकता यह कि इनके अभ्यन्तर में निगूढ़ उस देव को पहचानने के लिये इन्हें अनन्त प्रकार से सजाना और संवारना है । जब-जब भी मानव-जीवन और कला का यह नित्य पारस्परिक संबंध शिथिल या औझल हो जाता है तभी कला का हास और जीवन की हानि होती है । अतएव उत्तम स्थिति वह है जिस में मानव हृदय दिव्य आनन्द और अमृत ऐश्वर्य के भावों से आनन्दोलित होता है और प्राणों की उस व्याकुलता के अनुरूप शान्ति के लिये अपने चतुर्दिक स्थूल या भौतिक प्रतीकों को रूप-संपन्न बनाता है। उसकी यह साधना ही उत्तम जीवन और महती कला को जन्म देती है।
काल के सतत प्रवाही क्रम में वारंवार कला के लिये प्राणवन्त युगों का आवाहन करना होगा और ऐसा करते हुए मानव स्वयं अपने ही केन्द्र की किसी अमृत प्रेरणा की पूर्ति करेगा।