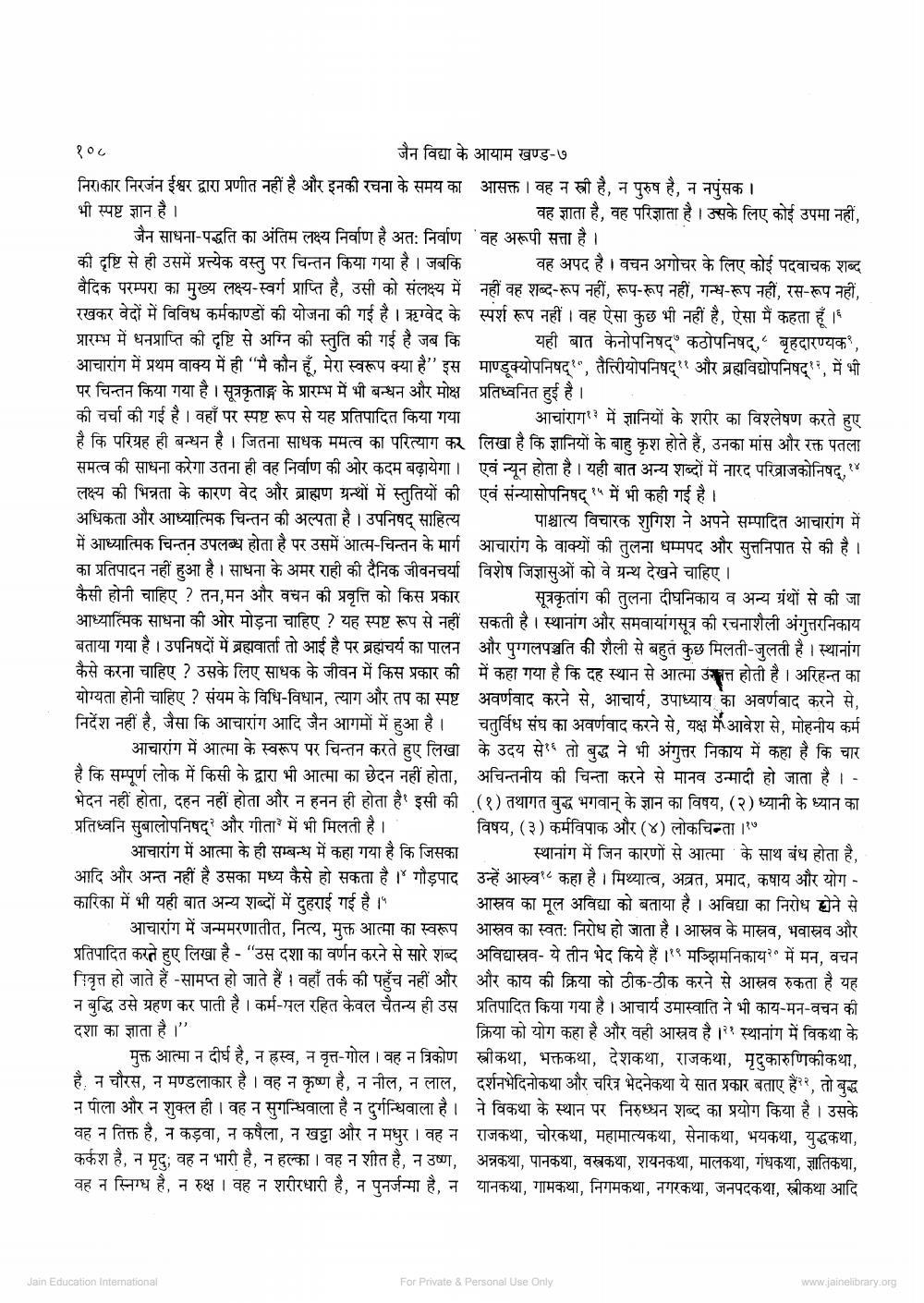________________
१०८
जैन विद्या के आयाम खण्ड-७ निराकार निरजंन ईश्वर द्वारा प्रणीत नहीं है और इनकी रचना के समय का आसक्त । वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक । भी स्पष्ट ज्ञान है।
वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है। उसके लिए कोई उपमा नहीं, जैन साधना-पद्धति का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है अत: निर्वाण वह अरूपी सत्ता है। की दृष्टि से ही उसमें प्रत्येक वस्तु पर चिन्तन किया गया है। जबकि वह अपद है। वचन अगोचर के लिए कोई पदवाचक शब्द वैदिक परम्परा का मुख्य लक्ष्य-स्वर्ग प्राप्ति है, उसी को संलक्ष्य में नहीं वह शब्द-रूप नहीं, रूप-रूप नहीं, गन्ध-रूप नहीं, रस-रूप नहीं, रखकर वेदों में विविध कर्मकाण्डों की योजना की गई है। ऋग्वेद के स्पर्श रूप नहीं। वह ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ।६ प्रारम्भ में धनप्राप्ति की दृष्टि से अग्नि की स्तुति की गई है जब कि यही बात केनोपनिषद् कठोपनिषद्, बृहदारण्यक, आचारांग में प्रथम वाक्य में ही “मै कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है" इस माण्डूक्योपनिषद्, तैत्तिरीयोपनिषद् ११ और ब्रह्मविद्योपनिषद्१२, में भी पर चिन्तन किया गया है। सूत्रकृताङ्ग के प्रारम्भ में भी बन्धन और मोक्ष प्रतिध्वनित हुई है। की चर्चा की गई है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया आचांराग१३ में ज्ञानियों के शरीर का विश्लेषण करते हए है कि परिग्रह ही बन्धन है । जितना साधक ममत्व का परित्याग कर लिखा है कि ज्ञानियों के बाह कृश होते हैं, उनका मांस और रक्त पतला समत्व की साधना करेगा उतना ही वह निर्वाण की ओर कदम बढ़ायेगा। एवं न्यून होता है। यही बात अन्य शब्दों में नारद परिव्राजकोनिषद्,१४ लक्ष्य की भिन्नता के कारण वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में स्तुतियों की एवं संन्यासोपनिषद् १५ में भी कही गई है। अधिकता और आध्यात्मिक चिन्तन की अल्पता है। उपनिषद् साहित्य पाश्चात्य विचारक शुगिश ने अपने सम्पादित आचारांग में में आध्यात्मिक चिन्तन उपलब्ध होता है पर उसमें आत्म-चिन्तन के मार्ग आचारांग के वाक्यों की तुलना धम्मपद और सूत्तनिपात से की है। का प्रतिपादन नहीं हुआ है । साधना के अमर राही की दैनिक जीवनचर्या विशेष जिज्ञासुओं को वे ग्रन्थ देखने चाहिए। कैसी होनी चाहिए ? तन,मन और वचन की प्रवृत्ति को किस प्रकार सूत्रकृतांग की तुलना दीघनिकाय व अन्य ग्रंथों से की जा आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना चाहिए? यह स्पष्ट रूप से नहीं सकती है। स्थानांग और समवायांगसूत्र की रचनाशैली अंगुत्तरनिकाय बताया गया है । उपनिषदों में ब्रह्मवार्ता तो आई है पर ब्रह्मचर्य का पालन और पुग्गलपञ्चति की शैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । स्थानांग कैसे करना चाहिए ? उसके लिए साधक के जीवन में किस प्रकार की में कहा गया है कि दह स्थान से आत्मा उम्मत्त होती है। अरिहन्त का योग्यता होनी चाहिए ? संयम के विधि-विधान, त्याग और तप का स्पष्ट अवर्णवाद करने से, आचार्य, उपाध्याय का अवर्णवाद करने से, निर्देश नहीं है, जैसा कि आचारांग आदि जैन आगमों में हुआ है। चतुर्विध संघ का अवर्णवाद करने से, यक्ष में आवेश से, मोहनीय कर्म
आचारांग में आत्मा के स्वरूप पर चिन्तन करते हुए लिखा के उदय से१६ तो बुद्ध ने भी अंगुत्तर निकाय में कहा है कि चार है कि सम्पूर्ण लोक में किसी के द्वारा भी आत्मा का छेदन नहीं होता, अचिन्तनीय की चिन्ता करने से मानव उन्मादी हो जाता है। - भेदन नहीं होता, दहन नहीं होता और न हनन ही होता है। इसी की (१) तथागत बुद्ध भगवान के ज्ञान का विषय, (२) ध्यानी के ध्यान का प्रतिध्वनि सुबालोपनिषद्और गीता में भी मिलती है। विषय, (३) कर्मविपाक और (४) लोकचिन्ता ।१७
आचारांग में आत्मा के ही सम्बन्ध में कहा गया है कि जिसका स्थानांग में जिन कारणों से आत्मा के साथ बंध होता है, आदि और अन्त नहीं है उसका मध्य कैसे हो सकता है। गौड़पाद उन्हें आस्व८ कहा है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग - कारिका में भी यही बात अन्य शब्दों में दुहराई गई है।
आस्रव का मूल अविद्या को बताया है । अविद्या का निरोध होने से आचारांग में जन्ममरणातीत, नित्य, मुक्त आत्मा का स्वरूप आस्रव का स्वत: निरोध हो जाता है । आस्रव के मास्रव, भवास्रव और प्रतिपादित करते हुए लिखा है - "उस दशा का वर्णन करने से सारे शब्द अविद्यास्रव- ये तीन भेद किये हैं ।१९ मञ्झिमनिकायरे में मन, वचन प्रिवृत्त हो जाते हैं -सामप्त हो जाते हैं । वहाँ तर्क की पहुँच नहीं और और काय की क्रिया को ठीक-ठीक करने से आस्रव रुकता है यह न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है । कर्म-सल रहित केवल चैतन्य ही उस प्रतिपादित किया गया है। आचार्य उमास्वाति ने भी काय-मन-वचन की दशा का ज्ञाता है।"
क्रिया को योग कहा है और वही आस्रव है ।२१ स्थानांग में विकथा के मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व, न वृत्त-गोल । वह न त्रिकोण स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा, राजकथा, मृदुकारुणिकीकथा, है, न चौरस, न मण्डलाकार है । वह न कृष्ण है, न नील, न लाल, दर्शनभेदिनोकथा और चरित्र भेदनेकथा ये सात प्रकार बताए हैं२२, तो बुद्ध न पीला और न शुक्ल ही । वह न सुगन्धिवाला है न दुर्गन्धिवाला है। ने विकथा के स्थान पर निरुध्धन शब्द का प्रयोग किया है। उसके वह न तिक्त है, न कड़वा, न कषैला, न खट्टा और न मधुर । वह न राजकथा, चोरकथा, महामात्यकथा, सेनाकथा, भयकथा, युद्धकथा, कर्कश है, न मृदु; वह न भारी है, न हल्का । वह न शीत है, न उष्ण, अन्नकथा, पानकथा, वस्त्रकथा, शयनकथा, मालकथा, गंधकथा, ज्ञातिकथा, वह न स्निग्ध है, न रुक्ष । वह न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा है, न यानकथा, गामकथा, निगमकथा, नगरकथा, जनपदकथा, स्त्रीकथा आदि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org