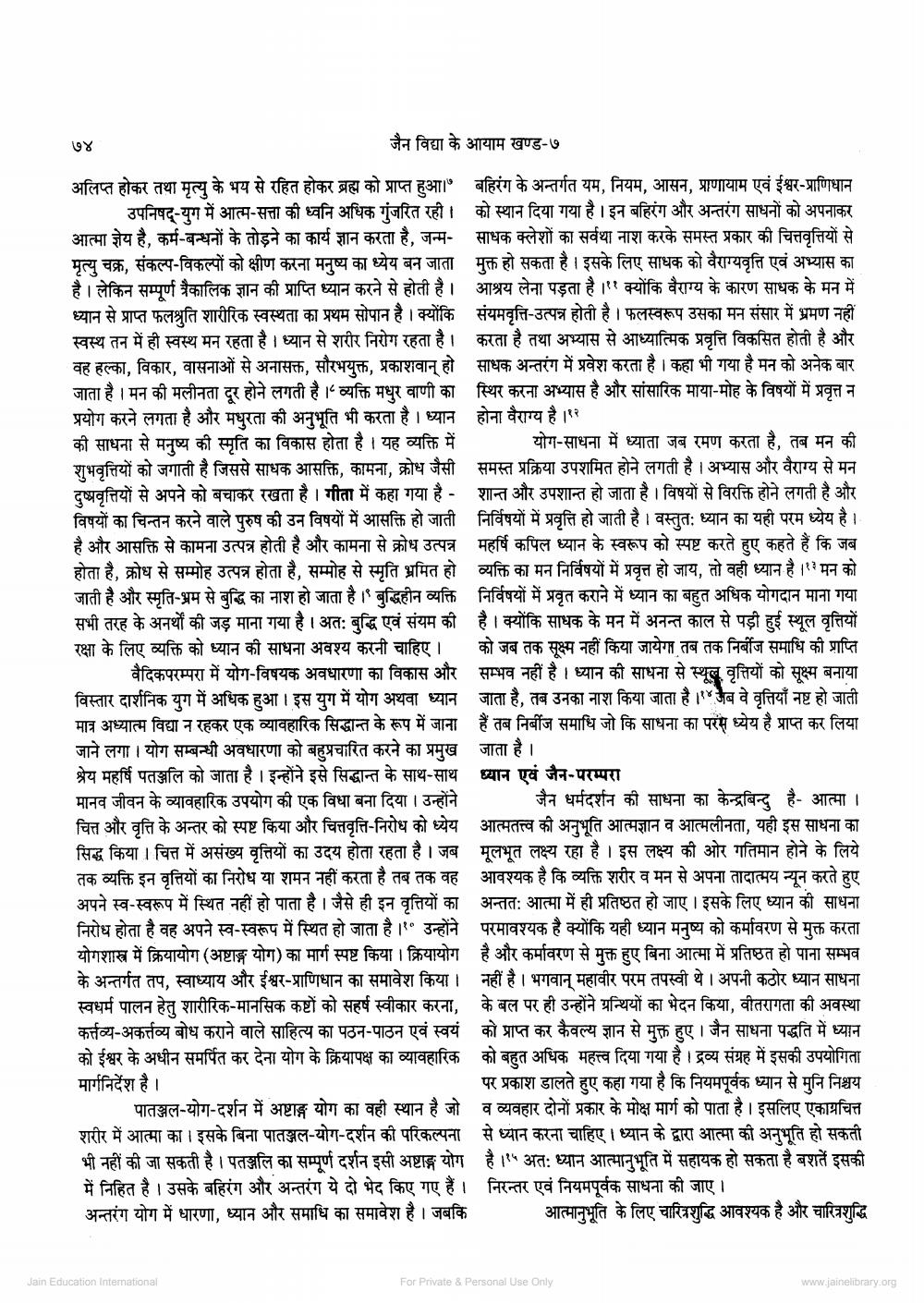________________
७४
जैन विद्या के आयाम खण्ड-७
अलिप्त होकर तथा मृत्यु के भय से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हुआ। बहिरंग के अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं ईश्वर-प्राणिधान
उपनिषद्-युग में आत्म-सत्ता की ध्वनि अधिक गुंजरित रही। को स्थान दिया गया है । इन बहिरंग और अन्तरंग साधनों को अपनाकर आत्मा ज्ञेय है, कर्म-बन्धनों के तोड़ने का कार्य ज्ञान करता है, जन्म- साधक क्लेशों का सर्वथा नाश करके समस्त प्रकार की चित्तवृत्तियों से मृत्यु चक्र, संकल्प-विकल्पों को क्षीण करना मनुष्य का ध्येय बन जाता मुक्त हो सकता है । इसके लिए साधक को वैराग्यवृत्ति एवं अभ्यास का है। लेकिन सम्पूर्ण कालिक ज्ञान की प्राप्ति ध्यान करने से होती है। आश्रय लेना पड़ता है ।११ क्योंकि वैराग्य के कारण साधक के मन में ध्यान से प्राप्त फलश्रुति शारीरिक स्वस्थता का प्रथम सोपान है । क्योंकि संयमवृत्ति-उत्पन्न होती है । फलस्वरूप उसका मन संसार में भ्रमण नहीं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। ध्यान से शरीर निरोग रहता है। करता है तथा अभ्यास से आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित होती है और वह हल्का, विकार, वासनाओं से अनासक्त, सौरभयुक्त, प्रकाशवान् हो साधक अन्तरंग में प्रवेश करता है । कहा भी गया है मन को अनेक बार जाता है । मन की मलीनता दूर होने लगती है। व्यक्ति मधुर वाणी का स्थिर करना अभ्यास है और सांसारिक माया-मोह के विषयों में प्रवृत्त न प्रयोग करने लगता है और मधुरता की अनुभूति भी करता है। ध्यान होना वैराग्य है ।१२ की साधना से मनुष्य की स्मृति का विकास होता है । यह व्यक्ति में योग-साधना में ध्याता जब रमण करता है, तब मन की शुभवृत्तियों को जगाती है जिससे साधक आसक्ति, कामना, क्रोध जैसी समस्त प्रक्रिया उपशमित होने लगती है। अभ्यास और वैराग्य से मन दुष्प्रवृत्तियों से अपने को बचाकर रखता है । गीता में कहा गया है - शान्त और उपशान्त हो जाता है। विषयों से विरक्ति होने लगती है और विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती निर्विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है । वस्तुत: ध्यान का यही परम ध्येय है। है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न महर्षि कपिल ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब होता है, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो व्यक्ति का मन निर्विषयों में प्रवृत्त हो जाय, तो वही ध्यान है ।१३ मन को जाती है और स्मृति-भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति निर्विषयों में प्रवृत कराने में ध्यान का बहुत अधिक योगदान माना गया सभी तरह के अनर्थों की जड़ माना गया है । अत: बुद्धि एवं संयम की है। क्योंकि साधक के मन में अनन्त काल से पड़ी हुई स्थूल वृत्तियों रक्षा के लिए व्यक्ति को ध्यान की साधना अवश्य करनी चाहिए। को जब तक सूक्ष्म नहीं किया जायेगा तब तक निर्बीज समाधि की प्राप्ति
वैदिकपरम्परा में योग-विषयक अवधारणा का विकास और सम्भव नहीं है। ध्यान की साधना से स्थूल वृत्तियों को सूक्ष्म बनाया विस्तार दार्शनिक युग में अधिक हुआ। इस युग में योग अथवा ध्यान जाता है, तब उनका नाश किया जाता है। १४ अब वे वृत्तियाँ नष्ट हो जाती मात्र अध्यात्म विद्या न रहकर एक व्यावहारिक सिद्धान्त के रूप में जाना हैं तब निर्बीज समाधि जो कि साधना का परम ध्येय है प्राप्त कर लिया जाने लगा । योग सम्बन्धी अवधारणा को बहुप्रचारित करने का प्रमुख जाता है । श्रेय महर्षि पतञ्जलि को जाता है। इन्होंने इसे सिद्धान्त के साथ-साथ ध्यान एवं जैन-परम्परा मानव जीवन के व्यावहारिक उपयोग की एक विधा बना दिया। उन्होंने जैन धर्मदर्शन की साधना का केन्द्रबिन्दु है- आत्मा । चित्त और वृत्ति के अन्तर को स्पष्ट किया और चित्तवृत्ति-निरोध को ध्येय आत्मतत्त्व की अनुभूति आत्मज्ञान व आत्मलीनता, यही इस साधना का सिद्ध किया । चित्त में असंख्य वृत्तियों का उदय होता रहता है । जब मूलभूत लक्ष्य रहा है । इस लक्ष्य की ओर गतिमान होने के लिये तक व्यक्ति इन वृत्तियों का निरोध या शमन नहीं करता है तब तक वह आवश्यक है कि व्यक्ति शरीर व मन से अपना तादात्मय न्यून करते हुए अपने स्व-स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता है। जैसे ही इन वृत्तियों का अन्तत: आत्मा में ही प्रतिष्ठत हो जाए। इसके लि निरोध होता है वह अपने स्व-स्वरूप में स्थित हो जाता है। उन्होंने परमावश्यक है क्योंकि यही ध्यान मनुष्य को कर्मावरण से मुक्त करता योगशास्त्र में क्रियायोग (अष्टाङ्ग योग) का मार्ग स्पष्ट किया। क्रियायोग है और कर्मावरण से मुक्त हुए बिना आत्मा में प्रतिष्ठत हो पाना सम्भव के अन्तर्गत तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान का समावेश किया। नहीं है । भगवान् महावीर परम तपस्वी थे। अपनी कठोर ध्यान साधना स्वधर्म पालन हेतु शारीरिक-मानसिक कष्टों को सहर्ष स्वीकार करना, के बल पर ही उन्होंने ग्रन्थियों का भेदन किया, वीतरागता की अवस्था कर्तव्य-अकर्तव्य बोध कराने वाले साहित्य का पठन-पाठन एवं स्वयं को प्राप्त कर कैवल्य ज्ञान से मुक्त हुए । जैन साधना पद्धति में ध्यान को ईश्वर के अधीन समर्पित कर देना योग के क्रियापक्ष का व्यावहारिक को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। द्रव्य संग्रह में इसकी उपयोगिता मार्गनिर्देश है।
पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि नियमपूर्वक ध्यान से मुनि निश्चय पातञ्जल-योग-दर्शन में अष्टाङ्ग योग का वही स्थान है जो व व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को पाता है। इसलिए एकाग्रचित्त शरीर में आत्मा का। इसके बिना पातञ्जल-योग-दर्शन की परिकल्पना से ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा आत्मा की अनुभूति हो सकती भी नहीं की जा सकती है। पतञ्जलि का सम्पूर्ण दर्शन इसी अष्टाङ्ग योग है ।१५ अत: ध्यान आत्मानुभूति में सहायक हो सकता है बशर्ते इसकी में निहित है। उसके बहिरंग और अन्तरंग ये दो भेद किए गए हैं। निरन्तर एवं नियमपूर्वक साधना की जाए। अन्तरंग योग में धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश है। जबकि आत्मानुभूति के लिए चारित्रशुद्धि आवश्यक है और चारित्रशुद्धि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org