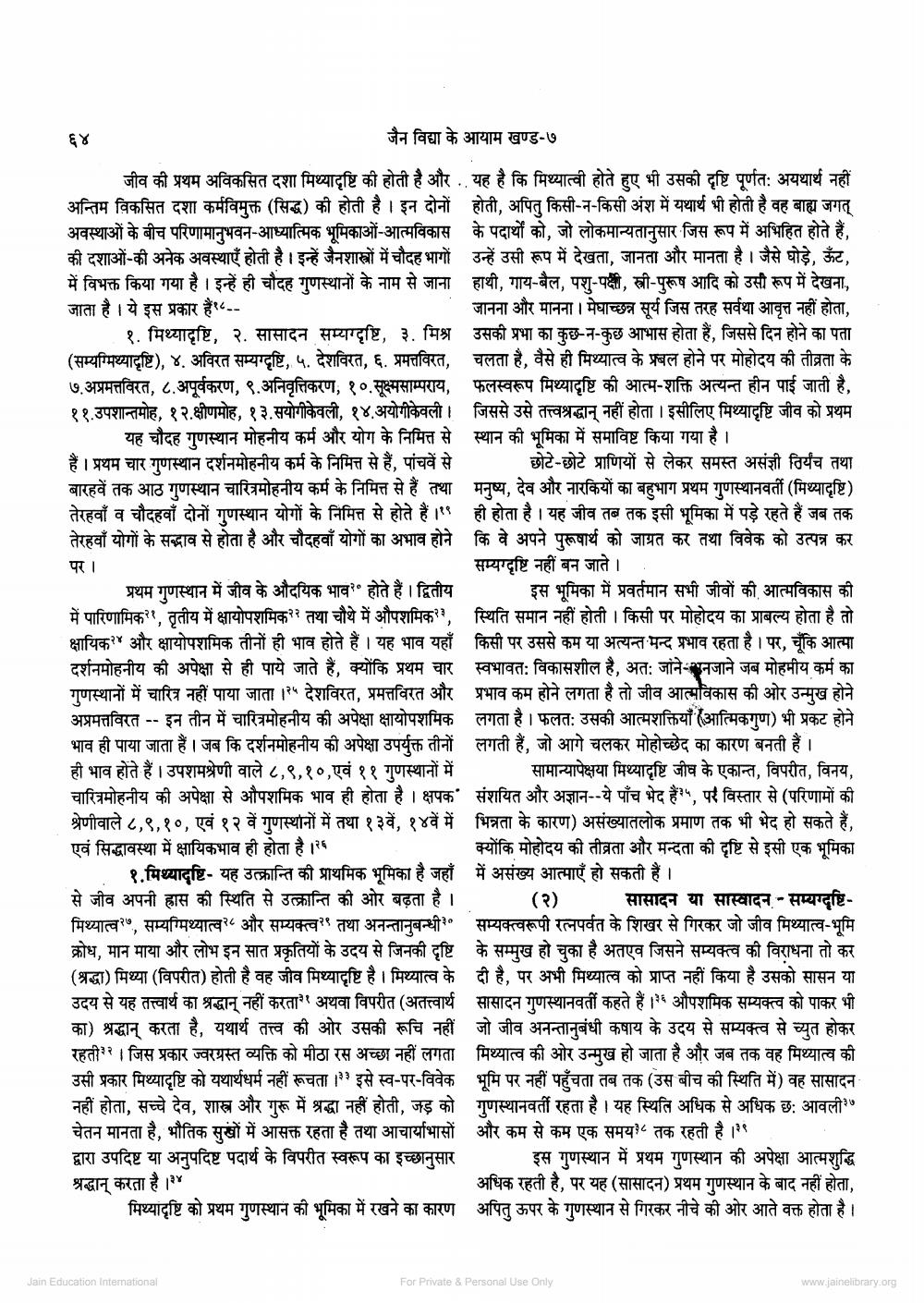________________
६४
जीव की प्रथम अविकसित दशा मिथ्यादृष्टि की होती है और अन्तिम विकसित दशा कर्मविमुक्त (सिद्ध) की होती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परिणामानुभवन- आध्यात्मिक भूमिकाओं आत्मविकास की दशाओं की अनेक अवस्थाएं होती है। इन्हें जैनशास्त्रों में चौदह भागों में विभक्त किया गया है । इन्हें ही चौदह गुणस्थानों के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार है-
जैन विद्या के आयाम खण्ड- ७
१. मिथ्यादृष्टि, २. सासादन सम्यग्दृष्टि, ३. मिश्र (सम्यग्मिथ्यादृष्टि), ४. अविरत सम्यग्दृष्टि, ५. देशविरत, ६. प्रमत्तविरत ७. अप्रमत्तविरत, ८. अपूर्वकरण, ९. अनिवृत्तिकरण, १०. सूक्ष्मसाम्पराय, ११. उपशान्तमोह, १२. क्षीणमोह, १३. सयोगीकेवली, १४. अयोगीकेवली ।
यह चौदह गुणस्थान मोहनीय कर्म और योग के निमित्त से है। प्रथम चार गुणस्थान दर्शनमोहनीय कर्म के निमित्त से हैं, पांचवें से बारहवें तक आठ गुणस्थान चारित्रमोहनीय कर्म के निमित्त से हैं तथा तेरहवाँ व चौदहवाँ दोनों गुणस्थान योगों के निमित्त से होते हैं ।१९ तेरहवाँ योगों के सद्भाव से होता है और चौदहवाँ योगों का अभाव होने
पर ।
प्रथम गुणस्थान में जीव के औदयिक भाव होते हैं। द्वितीय में पारिणामिक’१, तृतीय में क्षायोपशमिक तथा चौथे में औपशमिक ३, क्षायिक" और क्षायोपशमिक तीनों ही भाव होते हैं। यह भाव यहाँ दर्शनमोहनीय की अपेक्षा से ही पाये जाते हैं, क्योंकि प्रथम चार गुणस्थानों में चारित्र नहीं पाया जाता।" देशविरत, प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत इन तीन में चारित्रमोहनीय की अपेक्षा क्षायोपशमिक
। पाया जाता है। जब कि दर्शनमोहनीय की अपेक्षा उपर्युक्त तीनों ही भाव होते हैं। उपशमश्रेणी वाले ८, ९,१०, एवं ११ गुणस्थानों में चारित्रमोहनीय की अपेक्षा से औपशमिक भाव ही होता है। क्षपक श्रेणीवाले ८,९,१०, एवं १२ वें गुणस्थानों में तथा १३ वें, १४वें में एवं सिद्धावस्था में क्षायिकभाव ही होता है।
--
१. मिथ्यादृष्टि- यह उत्क्रान्ति की प्राथमिक भूमिका है जहाँ से जीव अपनी ह्रास की स्थिति से उत्क्रान्ति की ओर बढ़ता है। मिथ्यात्व २७, सम्यग्मिथ्यात्व २८ और सम्यक्त्व २९ तथा अनन्तानुबन्धी" क्रोध, मान माया और लोभ इन सात प्रकृतियों के उदय से जिनकी दृष्टि (श्रद्धा) मिथ्या (विपरीत) होती है वह जीव मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यात्व के उदय से यह तत्वार्थ का श्रद्धान् नहीं करता अथवा विपरीत (अतत्त्वार्थ का) श्रद्धान् करता है, यथार्थ तत्त्व की ओर उसकी रूचि नहीं रहती १२। जिस प्रकार ज्वरप्रस्त व्यक्ति को मीठा रस अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार मिध्यादृष्टि को यथार्थधर्म नहीं रूचता ।" इसे स्व-पर-विवेक नहीं होता, सच्चे देव, शास्त्र और गुरू में श्रद्धा नहीं होती, जड़ को चेतन मानता है, भौतिक सुखों में आसक्त रहता है तथा आचार्याभासों द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट पदार्थ के विपरीत स्वरूप का इच्छानुसार श्रद्धान् करता है । ३४
Jain Education International
10
यह है कि मिथ्यात्वी होते हुए भी उसकी दृष्टि पूर्णतः अयथार्थ नहीं होती, अपितु किसी-न-किसी अंश में यथार्थ भी होती है वह बाह्य जगत् के पदार्थों को, जो लोकमान्यतानुसार जिस रूप में अभिहित होते हैं, उन्हें उसी रूप में देखता, जानता और मानता है। जैसे घोड़े, ऊँट, हाथी, गाय-बैल, पशु-पक्षी, स्त्री-पुरूष आदि को उसी रूप में देखना, जानना और मानना । मेघाच्छन सूर्य जिस तरह सर्वथा आवृत नहीं होता, उसकी प्रभा का कुछ-न-कुछ आभास होता हैं, जिससे दिन होने का पता चलता है, वैसे ही मिथ्यात्व के प्रबल होने पर मोहोदय की तीव्रता के फलस्वरूप मिथ्यादृष्टि की आत्म-शक्ति अत्यन्त हीन पाई जाती है, जिससे उसे तत्त्वश्रद्धान् नहीं होता । इसीलिए मिथ्यादृष्टि जीव को प्रथम स्थान की भूमिका में समाविष्ट किया गया है ।
छोटे-छोटे प्राणियों से लेकर समस्त असंज्ञी तियंच तथा मनुष्य, देव और नारकियों का बहुभाग प्रथम गुणस्थानवर्ती (मिध्यादृष्टि ) ही होता है। यह जीव तब तक इसी भूमिका में पड़े रहते हैं जब तक कि वे अपने पुरूषार्थ को जाग्रत कर तथा विवेक को उत्पन्न कर सम्यग्दृष्टि नहीं बन जाते ।
इस भूमिका में प्रवर्तमान सभी जीवों की आत्मविकास की स्थिति समान नहीं होती । किसी पर मोहोदय का प्राबल्य होता है तो किसी पर उससे कम या अत्यन्त मन्द प्रभाव रहता है। पर, चूंकि आत्मा स्वभावत: विकासशील है, अतः जाने-अनजाने जब मोहमीय कर्म का प्रभाव कम होने लगता है तो जीव आत्मविकास की ओर उन्मुख लोने लगता है। फलतः उसकी आत्मशक्तियाँ (आत्मिकगुण) भी प्रकट होने लगती हैं, जो आगे चलकर मोहोच्छेद का कारण बनती हैं।
--
सामान्यापेक्षया मिथ्यादृष्टि जीव के एकान्त, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान ये पांच भेद हैं, पर विस्तार से (परिणामों की भिन्नता के कारण ) असंख्यातलोक प्रमाण तक भी भेद हो सकते हैं, क्योंकि मोहोदय की तीव्रता और मन्दता की दृष्टि से इसी एक भूमिका में असंख्य आत्माएँ हो सकती हैं ।
(२) सासादन या सास्वादन सम्यग्दृष्टिसम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व भूमि के सम्मुख हो चुका है अतएव जिसने सम्यक्त्व की विराधना तो कर दी है, पर अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है उसको सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं।" औपशमिक सम्यक्त्व को पाकर भी जो जीव अनन्तानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व की ओर उन्मुख हो जाता है और जब तक वह मिथ्यात्व की भूमि पर नहीं पहुँचता तब तक उस बीच की स्थिति में वह सासादन गुणस्थानवर्ती रहता है। यह स्थिति अधिक से अधिक छ आवली " । और कम से कम एक समय तक रहती है।"
इस गुणस्थान में प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा आत्मशुद्धि अधिक रहती है, पर यह (सासादन) प्रथम गुणस्थान के बाद नहीं होता, मिथ्यादृष्टि को प्रथम गुणस्थान की भूमिका में रखने का कारण अपितु ऊपर के गुणस्थान से गिरकर नीचे की ओर आते वक्त होता है।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org