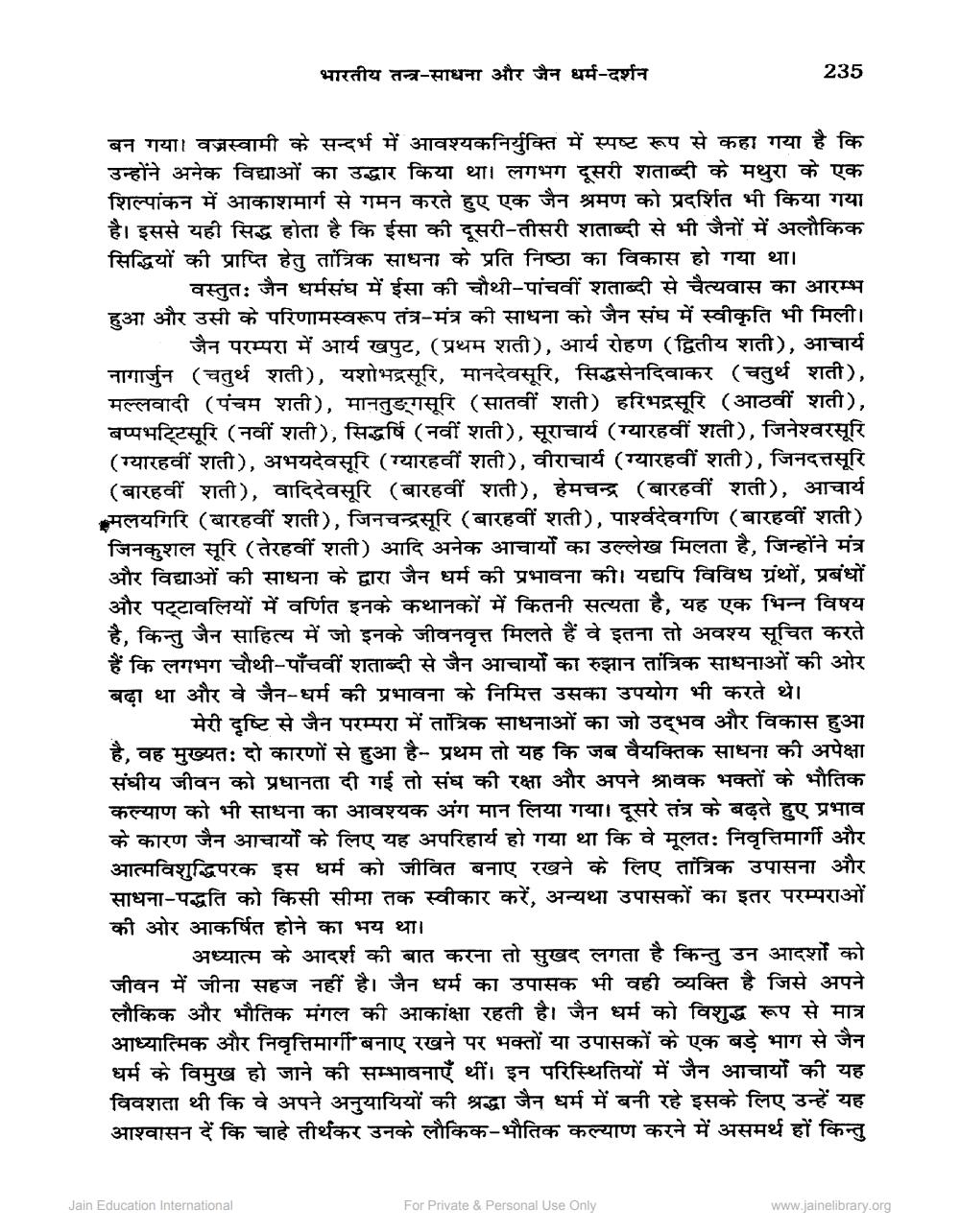________________
भारतीय तन्त्र-साधना और जैन धर्म-दर्शन
बन गया। वज्रस्वामी के सन्दर्भ में आवश्यकनियुक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने अनेक विद्याओं का उद्धार किया था। लगभग दूसरी शताब्दी के मथुरा के एक शिल्पांकन में आकाशमार्ग से गमन करते हुए एक जैन श्रमण को प्रदर्शित भी किया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी से भी जैनों में अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हेतु तांत्रिक साधना के प्रति निष्ठा का विकास हो गया था।
वस्तुत: जैन धर्मसंघ में ईसा की चौथी पांचवीं शताब्दी से चैत्यवास का आरम्भ हुआ और उसी के परिणामस्वरूप तंत्र-मंत्र की साधना को जैन संघ में स्वीकृति भी मिली। जैन परम्परा में आर्य खपुट, (प्रथम शती), आर्य रोहण (द्वितीय शती), आचार्य नागार्जुन (चतुर्थ शती), यशोभद्रसूरि, मानदेवसूरि, सिद्धसेनदिवाकर (चतुर्थ शती), मल्लवादी (पंचम शती), मानतुङ्गसूरि (सातवीं शती) हरिभद्रसूरि ( आठवीं शती), बप्पभट्टिसूरि (नवीं शती), सिद्धर्षि (नवीं शती), सूराचार्य ( ग्यारहवीं शती), जिनेश्वरसूरि (ग्यारहवीं शती), अभयदेवसूरि (ग्यारहवीं शती), वीराचार्य ( ग्यारहवीं शती), जिनदत्तसूरि (बारहवीं शती), वादिदेवसूरि (बारहवीं शती), हेमचन्द्र (बारहवीं शती), आचार्य *मलयगिरि (बारहवीं शती), जिनचन्द्रसूरि (बारहवीं शती), पार्श्वदेवगण (बारहवीं शती) जिनकुशल सूरि (तेरहवीं शती) आदि अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंत्र और विद्याओं की साधना के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना की । यद्यपि विविध ग्रंथों, प्रबंधों और पट्टावलियों में वर्णित इनके कथानकों में कितनी सत्यता है, यह एक भिन्न विषय है, किन्तु जैन साहित्य में जो इनके जीवनवृत्त मिलते हैं वे इतना तो अवश्य सूचित करते हैं कि लगभग चौथी-पाँचवीं शताब्दी से जैन आचार्यों का रुझान तांत्रिक साधनाओं की ओर बढ़ा था और वे जैन धर्म की प्रभावना के निमित्त उसका उपयोग भी करते थे।
मेरी दृष्टि से जैन परम्परा में तांत्रिक साधनाओं का जो उद्भव और विकास हुआ है, वह मुख्यतः दो कारणों से हुआ है- प्रथम तो यह कि जब वैयक्तिक साधना की अपेक्षा संघीय जीवन को प्रधानता दी गई तो संघ की रक्षा और अपने श्रावक भक्तों के भौतिक कल्याण को भी साधना का आवश्यक अंग मान लिया गया। दूसरे तंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जैन आचार्यों के लिए यह अपरिहार्य हो गया था कि वे मूलतः निवृत्तिमार्गी और आत्मविशुद्धिपरक इस धर्म को जीवित बनाए रखने के लिए तांत्रिक उपासना और साधना-पद्धति को किसी सीमा तक स्वीकार करें, अन्यथा उपासकों का इतर परम्पराओं की ओर आकर्षित होने का भय था।
Jain Education International
235
अध्यात्म के आदर्श की बात करना तो सुखद लगता है किन्तु उन आदर्शों को जीवन में जीना सहज नहीं है। जैन धर्म का उपासक भी वही व्यक्ति है जिसे अपने लौकिक और भौतिक मंगल की आकांक्षा रहती है। जैन धर्म को विशुद्ध रूप से मात्र आध्यात्मिक और निवृत्तिमार्गी बनाए रखने पर भक्तों या उपासकों के एक बड़े भाग से जैन धर्म के विमुख हो जाने की सम्भावनाएँ थीं। इन परिस्थितियों में जैन आचार्यों की यह विवशता थी कि वे अपने अनुयायियों की श्रद्धा जैन धर्म में बनी रहे इसके लिए उन्हें यह आश्वासन दें कि चाहे तीर्थंकर उनके लौकिक-भौतिक कल्याण करने में असमर्थ हों किन्तु
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org