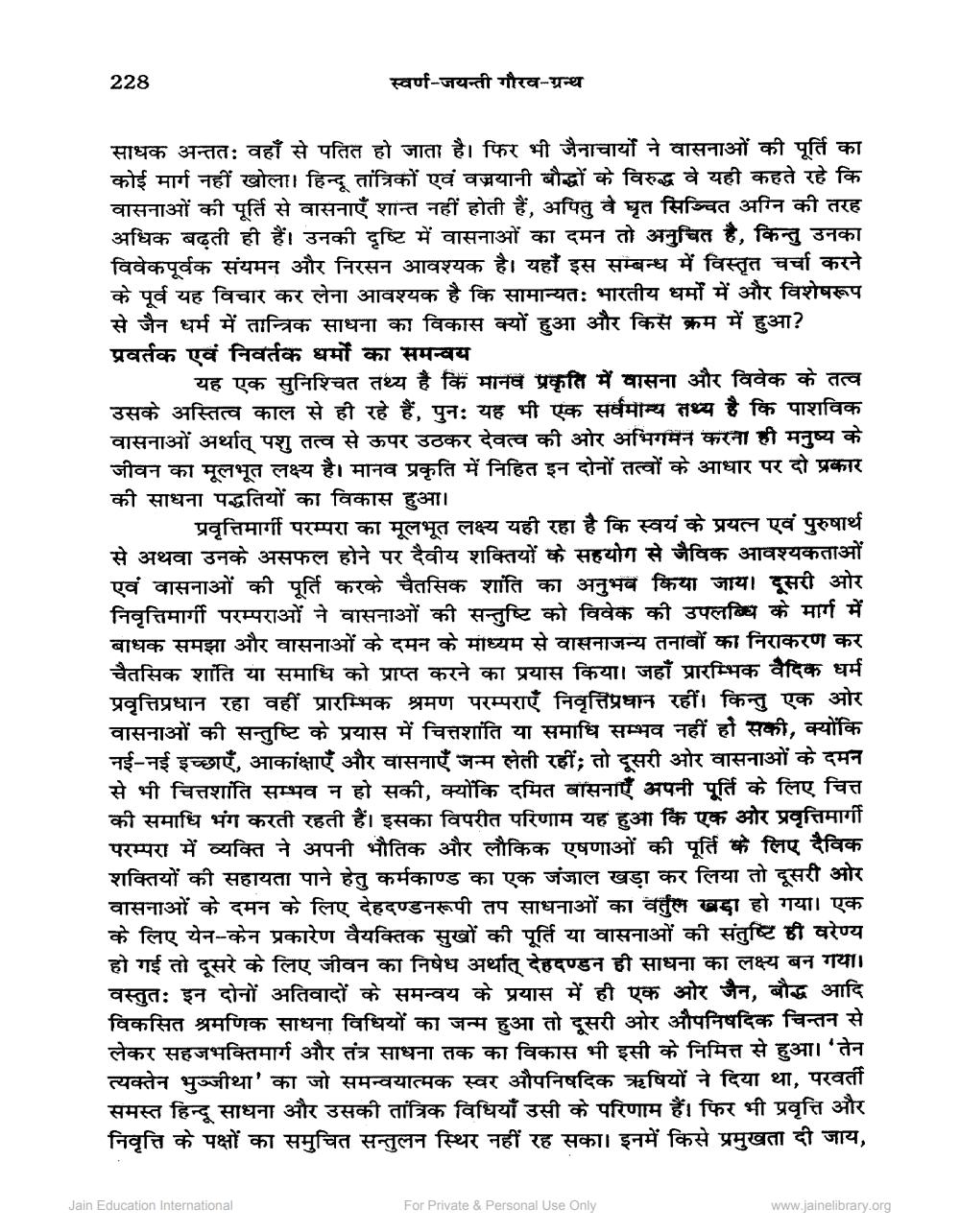________________
228
स्वर्ण जयन्ती गौरव-ग्रन्थ
साधक अन्ततः वहाँ से पतित हो जाता है। फिर भी जैनाचार्यों ने वासनाओं की पूर्ति का कोई मार्ग नहीं खोला। हिन्दू तांत्रिकों एवं वज्रयानी बौद्धों के विरुद्ध वे यही कहते रहे कि वासनाओं की पूर्ति से वासनाएँ शान्त नहीं होती हैं, अपितु वे घृत सिञ्चित अग्नि की तरह अधिक बढ़ती ही हैं। उनकी दृष्टि में वासनाओं का दमन तो अनुचित है, किन्तु उनका विवेकपूर्वक संयमन और निरसन आवश्यक है। यहाँ इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने के पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है कि सामान्यतः भारतीय धर्मों में और विशेषरूप से जैन धर्म में तान्त्रिक साधना का विकास क्यों हुआ और किस क्रम में हुआ? प्रवर्तक एवं निवर्तक धर्मों का समन्वय
यह एक सुनिश्चित तथ्य हैं कि मानव प्रकृति में वासना और विवेक के तत्व उसके अस्तित्व काल से ही रहे हैं, पुनः यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि पाशविक वासनाओं अर्थात् पशु तत्व से ऊपर उठकर देवत्व की ओर अभिगमन करना ही मनुष्य के जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। मानव प्रकृति में निहित इन दोनों तत्वों के आधार पर दो प्रकार की साधना पद्धतियों का विकास हुआ।
प्रवृत्तिमार्गी परम्परा का मूलभूत लक्ष्य यही रहा है कि स्वयं के प्रयत्न एवं पुरुषार्थ से अथवा उनके असफल होने पर दैवीय शक्तियों के सहयोग से जैविक आवश्यकताओं एवं वासनाओं की पूर्ति करके चैतसिक शांति का अनुभव किया जाय। दूसरी ओर निवृत्तिमार्गी परम्पराओं ने वासनाओं की सन्तुष्टि को विवेक की उपलब्धि के मार्ग में बाधक समझा और वासनाओं के दमन के माध्यम से वासनाजन्य तनावों का निराकरण कर चैतसिक शांति या समाधि को प्राप्त करने का प्रयास किया। जहाँ प्रारम्भिक वैदिक धर्म प्रवृत्तिप्रधान रहा वहीं प्रारम्भिक श्रमण परम्पराएँ निवृत्तिप्रधान रहीं। किन्तु एक ओर वासनाओं की सन्तुष्टि के प्रयास में चित्तशांति या समाधि सम्भव नहीं हो सकी, क्योंकि नई-नई इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और वासनाएँ जन्म लेती रहीं; तो दूसरी ओर वासनाओं के दमन से भी चित्तशांति सम्भव न हो सकी, क्योंकि दमित वासनाएँ अपनी पूर्ति के लिए चित्त की समाधि भंग करती रहती हैं। इसका विपरीत परिणाम यह हुआ कि एक ओर प्रवृत्तिमार्गी परम्परा में व्यक्ति ने अपनी भौतिक और लौकिक एषणाओं की पूर्ति के लिए दैविक शक्तियों की सहायता पाने हेतु कर्मकाण्ड का एक जंजाल खड़ा कर लिया तो दूसरी ओर वासनाओं के दमन के लिए देहदण्डनरूपी तप साधनाओं का वर्तुल खड़ा हो गया। एक के लिए येन-केन प्रकारेण वैयक्तिक सुखों की पूर्ति या वासनाओं की संतुष्टि ही वरेण्य हो गई तो दूसरे के लिए जीवन का निषेध अर्थात् देहदण्डन ही साधना का लक्ष्य बन गया। वस्तुतः इन दोनों अतिवादों के समन्वय के प्रयास में ही एक ओर जैन, बौद्ध आदि विकसित श्रमणिक साधना विधियों का जन्म हुआ तो दूसरी ओर औपनिषदिक चिन्तन से लेकर सहजभक्तिमार्ग और तंत्र साधना तक का विकास भी इसी के निमित्त से हुआ। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' का जो समन्वयात्मक स्वर औपनिषदिक ऋषियों ने दिया था, परवर्ती समस्त हिन्दू साधना और उसकी तांत्रिक विधियाँ उसी के परिणाम हैं। फिर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति के पक्षों का समुचित सन्तुलन स्थिर नहीं रह सका। इनमें किसे प्रमुखता दी जाय,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org