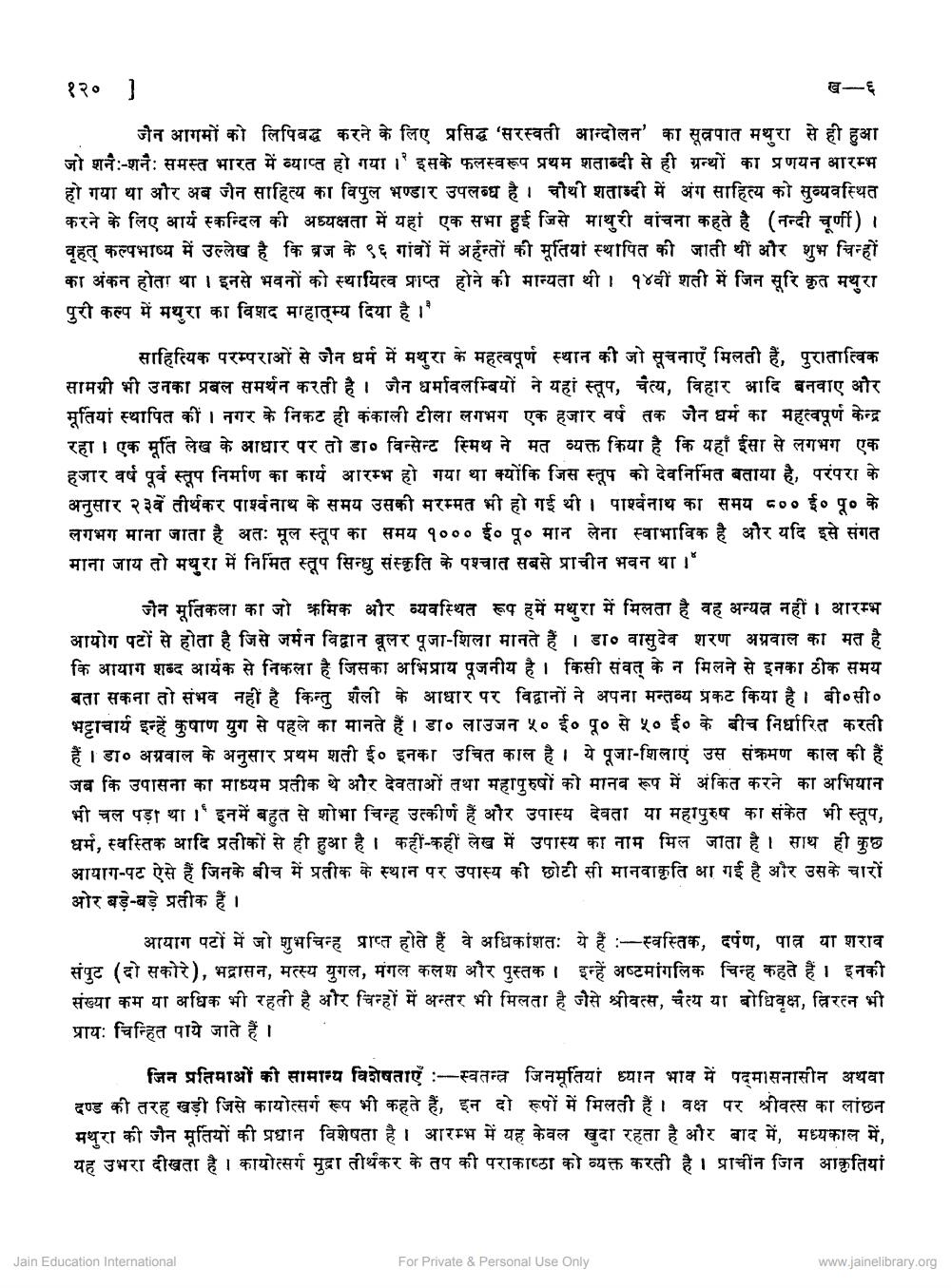________________
१२० ]
जैन आगमों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रसिद्ध 'सरस्वती आन्दोलन' का सूत्रपात मथुरा से ही हुआ जो शनैः-शनैः समस्त भारत में व्याप्त हो गया। इसके फलस्वरूप प्रथम शताब्दी से ही ग्रन्थों का प्रणयन आरम्भ हो गया था और अब जैन साहित्य का विपुल भण्डार उपलब्ध है । चौथी शताब्दी में अंग साहित्य को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्य स्कन्दिल की अध्यक्षता में यहां एक सभा हुई जिसे माथुरी वांचना कहते है ( नन्दी चूर्णी ) । वृहत् कल्पभाष्य में उल्लेख है कि ब्रज के ९६ गांवों में अर्हन्तों की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और शुभ चिन्हों का अंकन होता था । इनसे भवनों को स्थायित्व प्राप्त होने की मान्यता थी । १४वीं शती में जिन सूरि कृत मथुरा पुरी कल्प में मथुरा का विशद माहात्म्य दिया है।'
साहित्यिक परम्पराओं से जैन धर्म में मथुरा के महत्वपूर्ण स्थान की जो सूचनाएं मिलती है, पुरातात्विक सामग्री भी उनका प्रबल समर्थन करती है। जैन धर्मावलम्बियों ने यहां स्तूप, चैत्य, विहार आदि बनवाए और मूर्तियां स्थापित की। नगर के निकट ही कंकाली टीला लगभग एक हजार वर्ष तक जैन धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। एक मूर्ति लेख के आधार पर तो डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने मत व्यक्त किया है कि यहाँ ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व स्तूप निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया था क्योंकि जिस स्तूप को देवनिर्मित बताया है, परंपरा के अनुसार २३ वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के समय उसकी मरम्मत भी हो गई थी । पार्श्वनाथ का समय ८०० ई० पू० के लगभग माना जाता है अतः मूल स्तूप का समय १००० ई० पू० मान लेना स्वाभाविक है और यदि इसे संगत माना जाय तो मथुरा में निर्मित स्तूप सिन्धु संस्कृति के पश्चात सबसे प्राचीन भवन था।
ख.
जैन मूर्तिकला का जो ऋमिक और व्यवस्थित रूप हमें मथुरा में मिलता है वह अन्यत्र नहीं । आरम्भ आयोग पटों से होता है जिसे जर्मन विद्वान बूलर पूजा- शिला मानते हैं। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि आयाग शब्द आर्यक से निकला है जिसका अभिप्राय पूजनीय है। किसी संवत् के न मिलने से इनका ठीक समय बता सकना तो संभव नहीं है किन्तु शैली के आधार पर विद्वानों ने अपना मन्तव्य प्रकट किया है। बी०सी० भट्टाचार्य इन्हें कुषाण युग से पहले का मानते हैं। डा० लाउजन ५० ई० पू० से ५० ई० के बीच निर्धारित करती हैं । डा० अग्रवाल के अनुसार प्रथम शती ई० इनका उचित काल है । जब कि उपासना का माध्यम प्रतीक थे और देवताओं तथा महापुरुषों को मानव रूप में अंकित करने का अभियान भी चल पड़ा था। इनमें बहुत से शोभा चिन्ह उत्कीर्ण हैं और उपास्य देवता या महापुरुष का संकेत भी स्तूप, उपास्य का नाम मिल जाता है । साथ ही कुछ छोटी सी मानवाकृति आ गई है और उसके चारों
ये पूजा- शिलाएं उस संक्रमण काल की हैं।
धर्म, स्वस्तिक आदि प्रतीकों से ही हुआ है । कहीं-कहीं लेख में आयाग-पट ऐसे हैं जिनके बीच में प्रतीक के स्थान पर उपास्य की ओर बड़े-बड़े प्रतीक हैं।
आयाग पटों में जो शुभचिन्ह प्राप्त होते हैं वे अधिकांशतः ये हैं :- स्वस्तिक, दर्पण, पात्र या शराव संपुट (दो सकोरे ), भद्रासन, मत्स्य युगल, मंगल कलश और पुस्तक इन्हें अष्टमांगलिक चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या कम या अधिक भी रहती है और चिन्हों में अन्तर भी मिलता है जैसे श्रीवत्स, वैश्य या बोधिवृक्ष, विरत्न भी प्रायः चिन्हित पाये जाते हैं ।
जिन प्रतिमाओं की सामान्य विशेषताएँ : स्वतन्त्र जिनमूर्तियां ध्यान भाव में पद्मासनासीन अथवा दण्ड की तरह खड़ी जिसे कायोत्सर्ग रूप भी कहते हैं, इन दो रूपों में मिलती हैं । वक्ष पर श्रीवत्स का लांछन मथुरा 'की जैन मूर्तियों की प्रधान विशेषता है । आरम्भ में यह केवल खुदा रहता है और बाद में, मध्यकाल में, यह उभरा दीखता है। कायोत्सर्ग मुद्रा तीर्थकर के तप की पराकाष्ठा को व्यक्त करती है। प्राचीन जिन आकृतियां
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org