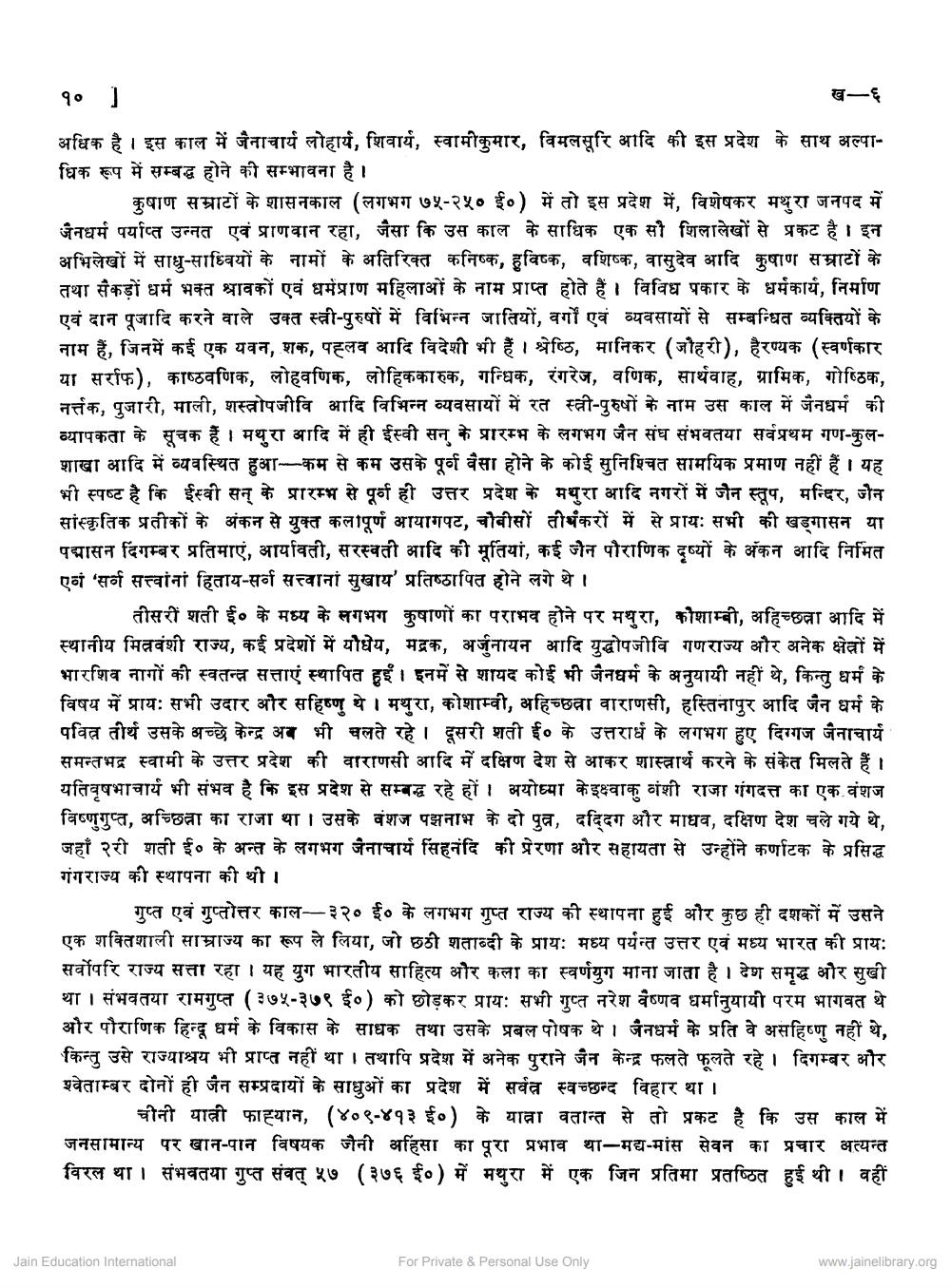________________
१०
]
अधिक है । इस काल में जैनाचार्य लोहार्य, शिवार्य, स्वामीकुमार, विमलसूरि आदि की इस प्रदेश के साथ अल्पाधिक रूप में सम्बद्ध होने की सम्भावना है।
कुषाण सम्राटों के शासनकाल (लगभग ७५-२५० ई०) में तो इस प्रदेश में, विशेषकर मथुरा जनपद में जैनधर्म पर्याप्त उन्नत एवं प्राणवान रहा, जैसा कि उस काल के साधिक एक सौ शिलालेखों से प्रकट है। इन अभिलेखों में साधु-साध्वियों के नामों के अतिरिक्त कनिष्क, हविष्क, वशिष्क, वासुदेव आदि कुषाण सम्राटों के तथा सैकड़ों धर्म भक्त श्रावकों एवं धर्मप्राण महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। विविध प्रकार के धर्मकार्य, निर्माण एवं दान पूजादि करने वाले उक्त स्त्री-पुरुषों में विभिन्न जातियों, वर्गों एवं व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें कई एक यवन, शक, पलव आदि विदेशी भी हैं । श्रेष्ठि, मानिकर (जौहरी), हैरण्यक (स्वर्णकार या सर्राफ), काष्ठवणिक, लोहवणिक, लोहिककारुक, गन्धिक, रंगरेज, वणिक, सार्थवाह, ग्रामिक, गोष्ठिक, नर्तक, पूजारी, माली, शस्त्रोपजीवि आदि विभिन्न व्यवसायों में रत स्त्री-पुरुषों के नाम उस काल में जैनधर्म की व्यापकता के सूचक हैं । मथुरा आदि में ही ईस्वी सन के प्रारम्भ के लगभग जैन संघ संभवतया सर्वप्रथम गण-कुलशाखा आदि में व्यवस्थित हआ-कम से कम उसके पूर्व वैसा होने के कोई सुनिश्चित सामयिक प्रमाण नहीं हैं। यह भी स्पष्ट है कि ईस्वी सन के प्रारम्भ से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मथुरा आदि नगरों में जैन स्तूप, मन्दिर, जैन सांस्कृतिक प्रतीकों के अंकन से युक्त कलापूर्ण आयागपट, चौबीसों तीथंकरों में से प्रायः सभी की खड़गासन या पद्मासन दिगम्बर प्रतिमाएं, आर्यावती, सरस्वती आदि की मूर्तियां, कई जैन पौराणिक दृष्यों के अंकन आदि निर्मित एवं 'सर्ग सत्त्वांनां हिताय-सन सत्त्वानां सुखाय' प्रतिष्ठापित होने लगे थे।
तीसरी शती ई० के मध्य के लगभग कुषाणों का पराभव होने पर मथुरा, कौशाम्बी, अहिच्छना आदि में स्थानीय मित्रवंशी राज्य, कई प्रदेशों में यौधेय, मद्रक, अर्जुनायन आदि युद्धोपजीवि गणराज्य और अनेक क्षेत्रों में भारशिव नागों की स्वतन्त्र सत्ताएं स्थापित हुई। इनमें से शायद कोई भी जैनधर्म के अनुयायी नहीं थे, किन्तु धर्म के विषय में प्रायः सभी उदार और सहिष्णु थे। मथुरा, कोशाम्वी, अहिच्छत्रा वाराणसी, हस्तिनापुर आदि जैन धर्म के पवित्र तीर्थ उसके अच्छे केन्द्र अब भी चलते रहे । दूसरी शती ई० के उत्तरार्ध के लगभग हुए दिग्गज जैनाचार्य समन्तभद्र स्वामी के उत्तर प्रदेश की वाराणसी आदि में दक्षिण देश से आकर शास्त्रार्थ करने के संकेत मिलते हैं। यतिवृषभाचार्य भी संभव है कि इस प्रदेश से सम्बद्ध रहे हों। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा गंगदत्त का एक वंशज विष्णुगुप्त, अच्छिना का राजा था। उसके वंशज पझनाभ के दो पुत्र, ददिदग और माधव, दक्षिण देश चले गये थे, जहाँ २री शती ई० के अन्त के लगभग जैनाचार्य सिंहनंदि की प्रेरणा और सहायता से उन्होंने कर्णाटक के प्रसिद्ध गंगराज्य की स्थापना की थी।
गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल-३२० ई. के लगभग गुप्त राज्य की स्थापना हुई और कुछ ही दशकों में उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य का रूप ले लिया, जो छठी शताब्दी के प्रायः मध्य पर्यन्त उत्तर एवं मध्य भारत की प्रायः सर्वोपरि राज्य सत्ता रहा । यह युग भारतीय साहित्य और कला का स्वर्णयुग माना जाता है। देश समृद्ध और सुखी था। संभवतया रामगुप्त (३७५-३७९ ई०) को छोड़कर प्रायः सभी गुप्त नरेश वैष्णव धर्मानुयायी परम भागवत थे और पौराणिक हिन्दू धर्म के विकास के साधक तथा उसके प्रबल पोषक थे। जैनधर्म के प्रति वे असहिष्णु नहीं थे, किन्तु उसे राज्याश्रय भी प्राप्त नहीं था। तथापि प्रदेश में अनेक पुराने जैन केन्द्र फलते फलते रहे। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही जैन सम्प्रदायों के साधुओं का प्रदेश में सर्वत्र स्वच्छन्द विहार था।
___ चीनी यात्री फाह्यान, (४०९-४१३ ई.) के यात्रा वतान्त से तो प्रकट है कि उस काल में जनसामान्य पर खान-पान विषयक जैनी अहिंसा का पूरा प्रभाव था-मद्य-मांस सेवन का प्रचार अत्यन्त विरल था। संभवतया गुप्त संवत् ५७ (३७६ ई०) में मथुरा में एक जिन प्रतिमा प्रतष्ठित हुई थी। वहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org