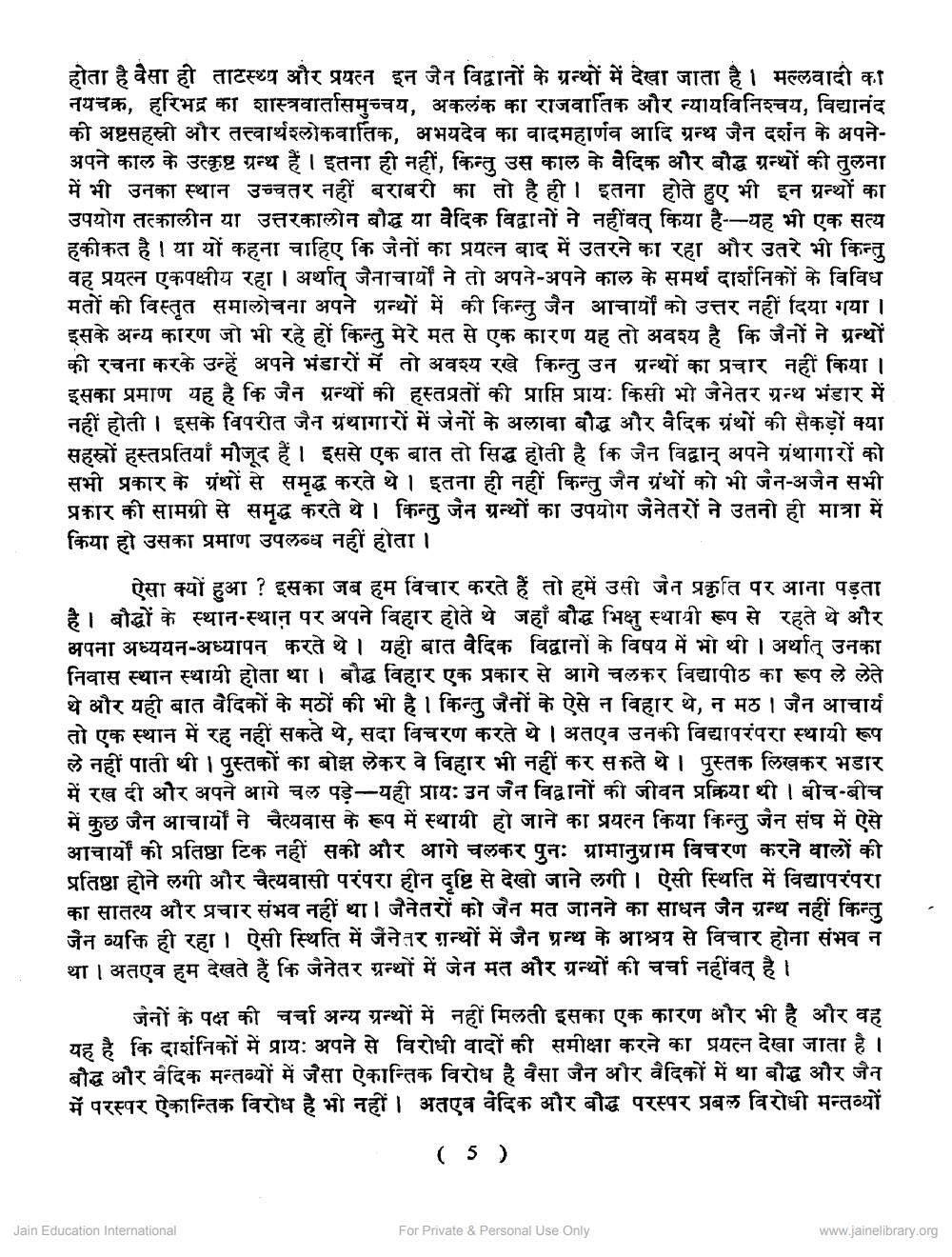________________
होता है वैसा ही ताटस्थ्य और प्रयत्न इन जैन विद्वानों के ग्रन्थों में देखा जाता है। मल्लवादी का नयचक्र, हरिभद्र का शास्त्रवार्तासमुच्चय, अकलंक का राजवार्तिक और न्यायविनिश्चय, विद्यानंद की अष्टसहस्री और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अभयदेव का वादमहार्णव आदि ग्रन्थ जैन दर्शन के अपनेअपने काल के उत्कृष्ट ग्रन्थ हैं । इतना ही नहीं, किन्तु उस काल के वैदिक और बौद्ध ग्रन्थों की तुलना में भी उनका स्थान उच्चतर नहीं बराबरी का तो है ही। इतना होते हुए भी इन ग्रन्थों का उपयोग तत्कालीन या उत्तरकालोन बौद्ध या वैदिक विद्वानों ने नहींवत् किया है. यह भी एक सत्य हकीकत है । या यों कहना चाहिए कि जैनों का प्रयत्न बाद में उतरने का रहा और उतरे भी किन्तु वह प्रयत्न एकपक्षीय रहा । अर्थात् जैनाचार्यों ने तो अपने-अपने काल के समर्थ दार्शनिकों के विविध मतों की विस्तृत समालोचना अपने ग्रन्थों में की किन्तु जैन आचार्यों को उत्तर नहीं दिया गया । इसके अन्य कारण जो भी रहे हों किन्तु मेरे मत से एक कारण यह तो अवश्य है कि जैनों ने ग्रन्थों की रचना करके उन्हें अपने भंडारों में तो अवश्य रखे किन्तु उन ग्रन्थों का प्रचार नहीं किया। इसका प्रमाण यह है कि जैन ग्रन्थों की हस्तप्रतों की प्राप्ति प्रायः किसी भी जैनेतर ग्रन्थ भंडार में नहीं होती। इसके विपरीत जैन ग्रंथागारों में जेनों के अलावा बौद्ध और वैदिक ग्रंथों की सैकड़ों क्या सहस्रों हस्तप्रतियाँ मौजूद हैं। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि जैन विद्वान् अपने ग्रंथागारों को सभी प्रकार के ग्रंथों से समृद्ध करते थे। इतना ही नहीं किन्तु जैन ग्रंथों को भी जैन-अजैन सभी प्रकार की सामग्री से समृद्ध करते थे। किन्तु जैन ग्रन्थों का उपयोग जैनेतरों ने उतनी ही मात्रा में किया हो उसका प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।
ऐसा क्यों हुआ? इसका जब हम विचार करते हैं तो हमें उसो जैन प्रकृति पर आना पड़ता है। बौद्धों के स्थान-स्थान पर अपने विहार होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षु स्थायी रूप से रहते थे और अपना अध्ययन-अध्यापन करते थे। यही बात वैदिक विद्वानों के विषय में भो थी । अर्थात उनका निवास स्थान स्थायी होता था। बौद्ध विहार एक प्रकार से आगे चलकर विद्यापीठ का रूप ले लेते थे और यही बात वैदिकों के मठों की भी है। किन्तु जैनों के ऐसे न विहार थे, न मठ । जैन आचार्य तो एक स्थान में रह नहीं सकते थे, सदा विचरण करते थे । अतएव उनकी विद्यापरंपरा स्थायी रूप ले नहीं पाती थी। पुस्तकों का बोझ लेकर वे विहार भी नहीं कर सकते थे। पुस्तक लिखकर भडार में रख दी और अपने आगे चल पड़े-यही प्रायः उन जैन विद्वानों की जीवन प्रक्रिया थी । बीच-बीच में कुछ जैन आचार्यों ने चैत्यवास के रूप में स्थायी हो जाने का प्रयत्न किया किन्तु जैन संघ में ऐसे आचार्यों की प्रतिष्ठा टिक नहीं सकी और आगे चलकर पुनः ग्रामानुग्राम विचरण करने वालों की प्रतिष्ठा होने लगी और चैत्यवासी परंपरा हीन दृष्टि से देखो जाने लगी। ऐसी स्थिति में विद्यापरंपरा का सातत्य और प्रचार संभव नहीं था। जैनेतरों को जैन मत जानने का साधन जैन ग्रन्थ नहीं किन्तु जैन व्यक्ति ही रहा। ऐसी स्थिति में जैनेतर ग्रन्थों में जैन ग्रन्थ के आश्रय से विचार होना संभव न था । अतएव हम देखते हैं कि जैनेतर ग्रन्थों में जेन मत और ग्रन्थों की चर्चा नहींवत् है।
जैनों के पक्ष की चर्चा अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलती इसका एक कारण और भी है और वह यह है कि दार्शनिकों में प्रायः अपने से विरोधी वादों की समीक्षा करने का प्रयत्न देखा जाता है । बौद्ध और वैदिक मन्तव्यों में जैसा ऐकान्तिक विरोध है वैसा जैन और वैदिकों में था बौद्ध और जैन में परस्पर ऐकान्तिक विरोध है भी नहीं। अतएव वैदिक और बौद्ध परस्पर प्रबल विरोधी मन्तव्यों
( 5 )
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org