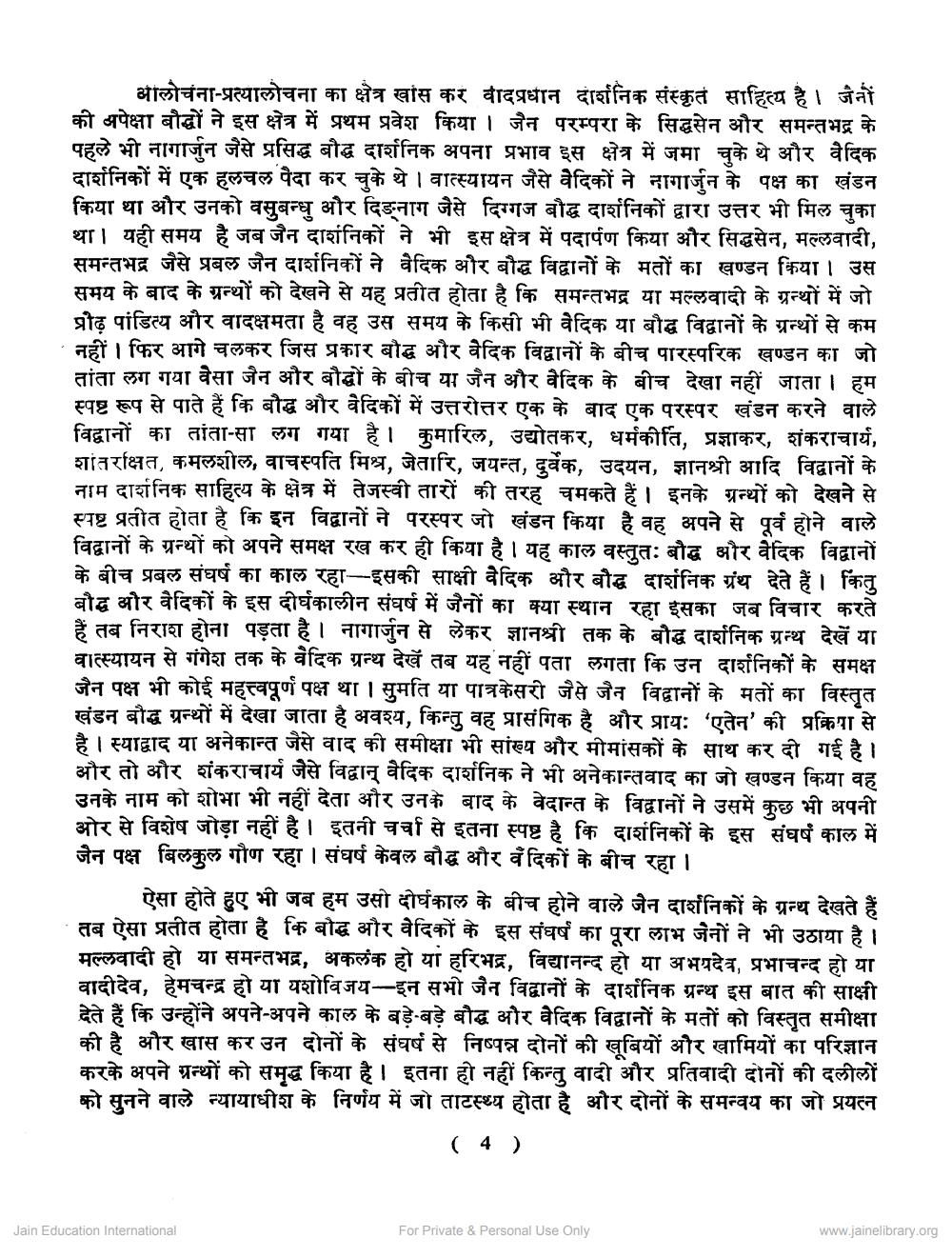________________
आलोचना-प्रत्यालोचना का क्षेत्र खास कर वादप्रधान दार्शनिक संस्कृत साहित्य है। जैनों की अपेक्षा बौद्धों ने इस क्षेत्र में प्रथम प्रवेश किया । जैन परम्परा के सिद्धसेन और समन्तभद्र के पहले भी नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अपना प्रभाव इस क्षेत्र में जमा चुके थे और वैदिक दार्शनिकों में एक हलचल पैदा कर चुके थे । वात्स्यायन जैसे वैदिकों ने नागार्जुन के पक्ष का खंडन किया था और उनको वसुबन्धु और दिङ्नाग जैसे दिग्गज बौद्ध दार्शनिकों द्वारा उत्तर भी मिल चुका था। यही समय है जब जैन दार्शनिकों ने भी इस क्षेत्र में पदार्पण किया और सिद्धसेन, मल्लवादी, समन्तभद्र जैसे प्रबल जैन दार्शनिकों ने वैदिक और बौद्ध विद्वानों के मतों का खण्डन किया। उस समय के बाद के ग्रन्थों को देखने से यह प्रतीत होता है कि समन्तभद्र या मल्लवादी के ग्रन्थों में जो प्रौढ पांडित्य और वादक्षमता है वह उस समय के किसी भी वैदिक या बौद्ध विद्वानों के ग्रन्थों से कम नहीं। फिर आगे चलकर जिस प्रकार बौद्ध और वैदिक विद्वानों के बीच पारस्परिक खण्डन का जो तांता लग गया वैसा जैन और बौद्धों के बीच या जैन और वैदिक के बीच देखा नहीं जाता। हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि बौद्ध और वैदिकों में उत्तरोत्तर एक के बाद एक परस्पर खंडन करने वाले विद्वानों का तांता-सा लग गया है। कुमारिल, उद्योतकर, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर, शंकराचार्य,
कमलशील, वाचस्पति मिश्र, जेतारि, जयन्त, दुर्वेक, उदयन, ज्ञानश्री आदि विद्वानों के नाम दार्शनिक साहित्य के क्षेत्र में तेजस्वी तारों की तरह चमकते हैं। इनके ग्रन्थों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन विद्वानों ने परस्पर जो खंडन किया है वह अपने से पूर्व होने वाले विद्वानों के ग्रन्थों को अपने समक्ष रख कर ही किया है । यह काल वस्तुतः बौद्ध और वैदिक विद्वानों के बीच प्रबल संघर्ष का काल रहा-इसकी साक्षी वैदिक और बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ देते हैं। किंतु बौद्ध और वैदिकों के इस दीर्घकालीन संघर्ष में जैनों का क्या स्थान रहा इसका जब विचार करते हैं तब निराश होना पड़ता है। नागार्जुन से लेकर ज्ञानश्री तक के बौद्ध दार्शनिक ग्रन्थ देखें या वात्स्यायन से गंगेश तक के वैदिक ग्रन्थ देखें तब यह नहीं पता लगता कि उन दार्शनिकों के समक्ष जैन पक्ष भी कोई महत्त्वपूर्ण पक्ष था । सुमति या पात्रकेसरी जैसे जैन विद्वानों के मतों का विस्तृत खंडन बौद्ध ग्रन्थों में देखा जाता है अवश्य, किन्तु वह प्रासंगिक है और प्रायः ‘एतेन' की प्रक्रिया से है। स्याद्वाद या अनेकान्त जैसे वाद की समीक्षा भी सांख्य और मीमांसकों के साथ कर दी गई है। और तो और शंकराचार्य जैसे विद्वान् वैदिक दार्शनिक ने भी अनेकान्तवाद का जो खण्डन किया वह उनके नाम को शोभा भी नहीं देता और उनके बाद के वेदान्त के विद्वानों ने उसमें कुछ भी अपनी ओर से विशेष जोड़ा नहीं है। इतनी चर्चा से इतना स्पष्ट है कि दार्शनिकों के इस संघर्ष काल में जैन पक्ष बिलकुल गौण रहा । संघर्ष केवल बौद्ध और वैदिकों के बीच रहा ।
ऐसा होते हुए भी जब हम उसो दीर्घकाल के बीच होने वाले जैन दार्शनिकों के ग्रन्थ देखते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध और वैदिकों के इस संघर्ष का पूरा लाभ जैनों ने भी उठाया है । मल्लवादी हो या समन्तभद्र, अकलंक हो या हरिभद्र, विद्यानन्द हो या अभयदेव, प्रभाचन्द हो या वादीदेव, हेमचन्द्र हो या यशोविजय-इन सभी जैन विद्वानों के दार्शनिक ग्रन्थ इस बात की साक्षी देते हैं कि उन्होंने अपने-अपने काल के बड़े-बड़े बौद्ध और वैदिक विद्वानों के मतों को विस्तृत समीक्षा की है और खास कर उन दोनों के संघर्ष से निष्पन्न दोनों की खूबियों और खामियों का परिज्ञान करके अपने ग्रन्थों को समृद्ध किया है। इतना ही नहीं किन्तु वादी और प्रतिवादी दोनों की दलीलों को सुनने वाले न्यायाधीश के निर्णय में जो ताटस्थ्य होता है और दोनों के समन्वय का जो प्रयत्न
(
4
)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org