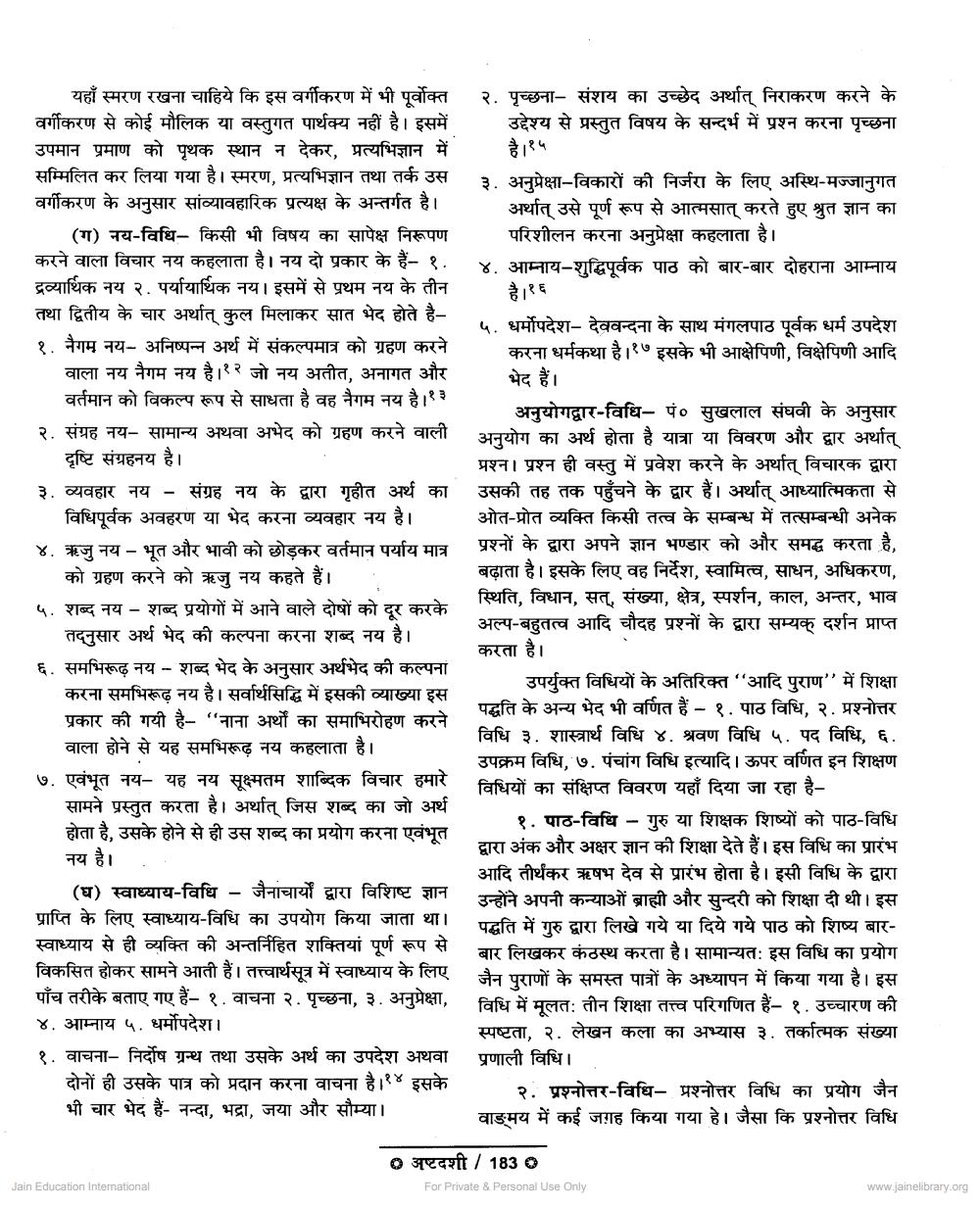________________
यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि इस वर्गीकरण में भी पूर्वोक्त २. पृच्छना- संशय का उच्छेद अर्थात् निराकरण करने के वर्गीकरण से कोई मौलिक या वस्तुगत पार्थक्य नहीं है। इसमें उद्देश्य से प्रस्तुत विषय के सन्दर्भ में प्रश्न करना पृच्छना उपमान प्रमाण को पृथक स्थान न देकर, प्रत्यभिज्ञान में है।१५ सम्मिलित कर लिया गया है। स्मरण, प्रत्यभिज्ञान तथा तर्क उस ३. अनप्रेक्षा-विकारों की निर्जरा के लिए अस्थि-मज्जानुगत वर्गीकरण के अनुसार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत है।
अर्थात् उसे पूर्ण रूप से आत्मसात् करते हुए श्रुत ज्ञान का (ग) नय-विधि- किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण परिशीलन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। करने वाला विचार नय कहलाता है। नय दो प्रकार के हैं- १. ४. आम्नाय-शद्धिपूर्वक पाठ को बार-बार दोहराना आम्नाय द्रव्यार्थिक नय २. पर्यायार्थिक नय। इसमें से प्रथम नय के तीन तथा द्वितीय के चार अर्थात् कुल मिलाकर सात भेद होते है
५. धर्मोपदेश- देववन्दना के साथ मंगलपाठ पूर्वक धर्म उपदेश १. नैगम नय- अनिष्पन्न अर्थ में संकल्पमात्र को ग्रहण करने
करना धर्मकथा है।१७ इसके भी आक्षेपिणी, विक्षेपिणी आदि वाला नय नैगम नय है।१२ जो नय अतीत, अनागत और
भेद हैं। वर्तमान को विकल्प रूप से साधता है वह नैगम नय है।१३
अनुयोगद्वार-विधि- पं० सुखलाल संघवी के अनुसार २. संग्रह नय- सामान्य अथवा अभेद को ग्रहण करने वाली
अनुयोग का अर्थ होता है यात्रा या विवरण और द्वार अर्थात् दृष्टि संग्रहनय है।
प्रश्न। प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात् विचारक द्वारा ३. व्यवहार नय - संग्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ का उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं। अर्थात् आध्यात्मिकता से
विधिपूर्वक अवहरण या भेद करना व्यवहार नय है। ओत-प्रोत व्यक्ति किसी तत्व के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी अनेक ४. ऋजु नय - भूत और भावी को छोड़कर वर्तमान पर्याय मात्र ।
प्रश्नों के द्वारा अपने ज्ञान भण्डार को और समद्ध करता है, को ग्रहण करने को ऋजु नय कहते हैं।
बढ़ाता है। इसके लिए वह निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण,
स्थिति, विधान, सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव ५. शब्द नय - शब्द प्रयोगों में आने वाले दोषों को दूर करके
अल्प-बहुतत्व आदि चौदह प्रश्नों के द्वारा सम्यक् दर्शन प्राप्त तद्नुसार अर्थ भेद की कल्पना करना शब्द नय है।
करता है। ६. समभिरूढ़ नय - शब्द भेद के अनुसार अर्थभेद की कल्पना
उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त “आदि पुराण' में शिक्षा करना समभिरूढ़ नय है। सर्वार्थसिद्धि में इसकी व्याख्या इस
पद्धति के अन्य भेद भी वर्णित हैं - १. पाठ विधि, २. प्रश्नोत्तर प्रकार की गयी है- "नाना अर्थों का समाभिरोहण करने
विधि ३. शास्त्रार्थ विधि ४. श्रवण विधि ५. पद विधि, ६. वाला होने से यह समभिरूढ़ नय कहलाता है।
उपक्रम विधि, ७. पंचांग विधि इत्यादि। ऊपर वर्णित इन शिक्षण ७. एवंभूत नय- यह नय सूक्ष्मतम शाब्दिक विचार हमारे
विधियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा हैसामने प्रस्तुत करता है। अर्थात् जिस शब्द का जो अर्थ
१. पाठ-विधि - गुरु या शिक्षक शिष्यों को पाठ-विधि होता है, उसके होने से ही उस शब्द का प्रयोग करना एवंभूत
द्वारा अंक और अक्षर ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इस विधि का प्रारंभ नय है।
आदि तीर्थंकर ऋषभ देव से प्रारंभ होता है। इसी विधि के द्वारा (घ) स्वाध्याय-विधि - जैनाचार्यों द्वारा विशिष्ट ज्ञान
उन्होंने अपनी कन्याओं ब्राह्मी और सुन्दरी को शिक्षा दी थी। इस प्राप्ति के लिए स्वाध्याय-विधि का उपयोग किया जाता था।
पद्धति में गुरु द्वारा लिखे गये या दिये गये पाठ को शिष्य बारस्वाध्याय से ही व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियां पूर्ण रूप से
बार लिखकर कंठस्थ करता है। सामान्यत: इस विधि का प्रयोग विकसित होकर सामने आती हैं। तत्त्वार्थसूत्र में स्वाध्याय के लिए
जैन पुराणों के समस्त पात्रों के अध्यापन में किया गया है। इस पाँच तरीके बताए गए हैं-१. वाचना २. पृच्छना, ३. अनुप्रेक्षा, विधि में मलतः तीन शिक्षा तत्त्व परिगणित हैं- १. उच्चारण की ४. आम्नाय ५. धर्मोपदेश।
स्पष्टता, २. लेखन कला का अभ्यास ३. तर्कात्मक संख्या १. वाचना- निर्दोष ग्रन्थ तथा उसके अर्थ का उपदेश अथवा प्रणाली विधि। दोनों ही उसके पात्र को प्रदान करना वाचना है।१४ इसके
२. प्रश्नोत्तर-विधि- प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग जैन भी चार भेद हैं- नन्दा, भद्रा, जया और सौम्या।
वाङ्मय में कई जगह किया गया है। जैसा कि प्रश्नोत्तर विधि
० अष्टदशी / 1830
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org