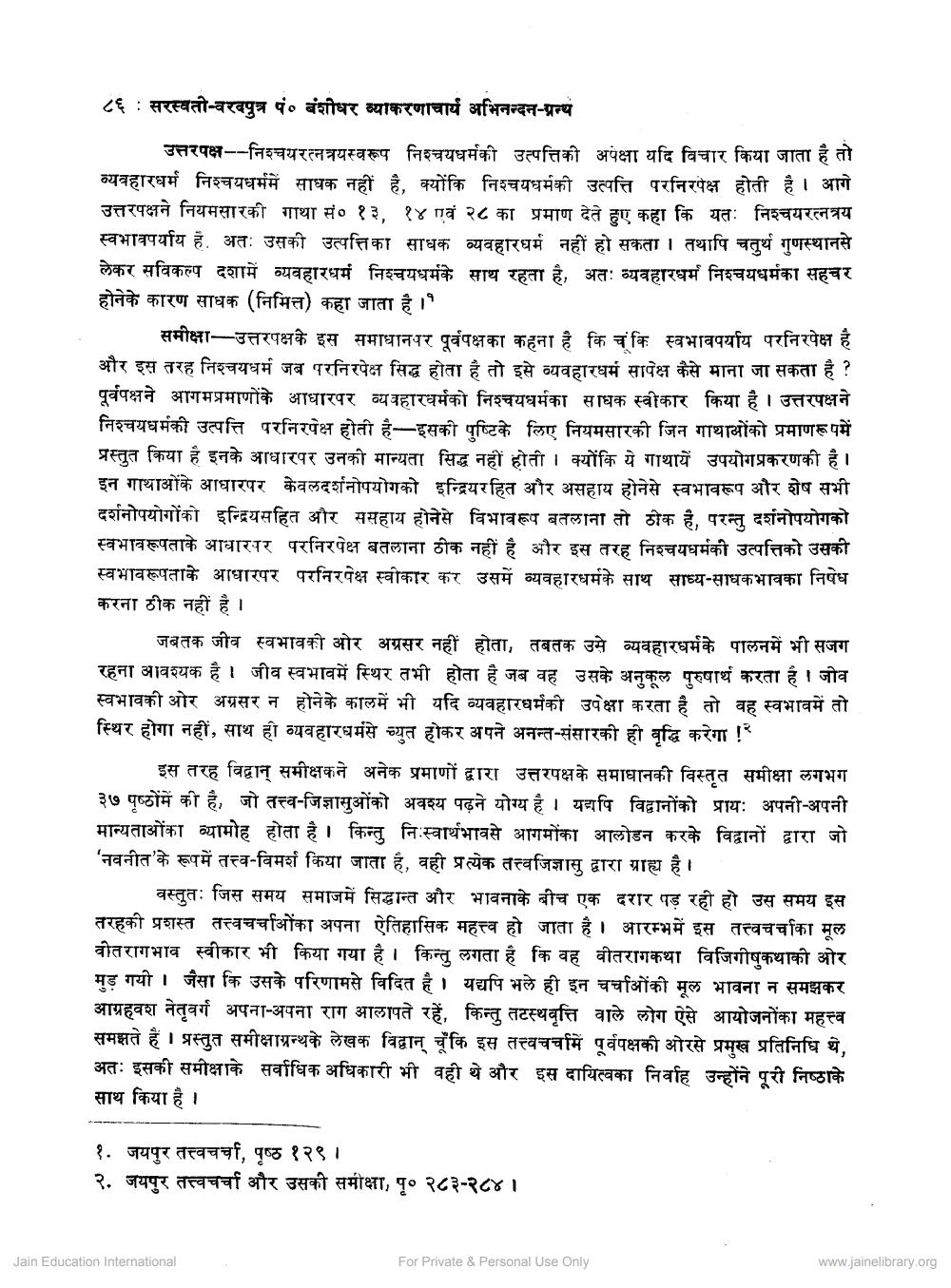________________
८६ : सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-प्रन्य
उत्तरपक्ष--निश्चयरत्नत्रयस्वरूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिकी अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक नहीं है, क्योंकि निश्चयधर्मकी उत्पत्ति परनिरपेक्ष होती है। आगे उत्तरपक्षने नियमसारकी गाथा सं० १३, १४ एवं २८ का प्रमाण देते हुए कहा कि यतः निश्चयरत्नत्रय स्वभावपर्याय है. अतः उसकी उत्पत्तिका साधक व्यवहारधर्म नहीं हो सकता । तथापि चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सविकल्प दशामें व्यवहारधर्म निश्चयधर्मके साथ रहता है, अतः व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सहचर होनेके कारण साधक (निमित्त) कहा जाता है।'
समीक्षा-उत्तरपक्षके इस समाधानपर पूर्वपक्षका कहना है कि चंकि स्वभावपर्याय परनिरपेक्ष है और इस तरह निश्चयधर्म जब परनिरपेक्ष सिद्ध होता है तो इसे व्यवहारधर्म सापेक्ष कैसे माना जा सकता है ? पूर्वपक्षने आगमप्रमाणोंके आधारपर व्यवहारधर्मको निश्चयधर्मका साधक स्वीकार किया है । उत्तरपक्षने निश्चयधर्मकी उत्पत्ति परनिरपेक्ष होती है-इसकी पुष्टिके लिए नियमसारकी जिन गाथाओंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है इनके आधारपर उनकी मान्यता सिद्ध नहीं होती। क्योंकि ये गाथायें उपयोगप्रकरणकी है। इन गाथाओंके आधारपर केवलदर्शनोपयोगको इन्द्रियरहित और असहाय होनेसे स्वभावरूप और शेष सभी दर्शनोपयोगोंको इन्द्रियसहित और ससहाय होनेसे विभावरूप बतलाना तो ठीक है, परन्तु दर्शनोपयोगको स्वभावरूपताके आधारसर परनिरपेक्ष बतलाना ठीक नहीं है और इस तरह निश्चयधर्मकी उत्पत्तिको उसकी स्वभावरूपताके आधारपर परनिरपेक्ष स्वीकार कर उसमें व्यवहारधर्मके साथ साध्य-साधकभावका निषेध करना ठीक नहीं है।
जबतक जीव स्वभावकी ओर अग्रसर नहीं होता, तबतक उसे व्यवहारधर्मके पालन में भी सजग रहना आवश्यक है। जीव स्वभावमें स्थिर तभी होता है जब वह उसके अनुकूल पुरुषार्थ करता है । जीव स्वभावकी ओर अग्रसर न होनेके कालमें भी यदि व्यवहारधर्मकी उपेक्षा करता है तो वह स्वभावमें तो स्थिर होगा नहीं, साथ ही व्यवहारधर्मसे च्युत होकर अपने अनन्त-संसारकी ही वृद्धि करेगा !
इस तरह विद्वान् समीक्षकने अनेक प्रमाणों द्वारा उत्तरपक्षके समाधानकी विस्तृत समीक्षा लगभग ३७ पृष्ठोंमें की है, जो तत्त्व-जिज्ञासुओंको अवश्य पढ़ने योग्य है । यद्यपि विद्वानोंको प्रायः अपनी-अपनी मान्यताओंका व्यामोह होता है। किन्तु निःस्वार्थभावसे आगमोंका आलोडन करके विद्वानों द्वारा जो 'नवनीत'के रूप में तत्त्व-विमर्श किया जाता है, वही प्रत्येक तत्त्वजिज्ञासु द्वारा ग्राह्य है।
वस्तुतः जिस समय समाजमें सिद्धान्त और भावनाके बीच एक दरार पड़ रही हो उस समय इस तरहकी प्रशस्त तत्त्वचर्चाओंका अपना ऐतिहासिक महत्त्व हो जाता है। आरम्भमें इस तत्त्वचर्चाका मूल वीतरागभाव स्वीकार भी किया गया है। किन्तु लगता है कि वह वीतरागकथा विजिगीषुकथाकी ओर मड गयी। जैसा कि उसके परिणामसे विदित है। यद्यपि भले ही इन चर्चाओंकी मूल भावना न समझकर आग्रहवश नेतृवर्ग अपना-अपना राग आलापते रहें, किन्तु तटस्थवृत्ति वाले लोग ऐसे आयोजनोंका महत्त्व समझते हैं । प्रस्तुत समीक्षाग्रन्थके लेखक विद्वान् चूँकि इस तत्त्वचर्चामें पूर्वपक्षकी ओरसे प्रमुख प्रतिनिधि थे, अतः इसकी समीक्षाके सर्वाधिक अधिकारी भी वही थे और इस दायित्वका निर्वाह उन्होंने पूरी निष्ठाके साथ किया है।
१. जयपुर तत्त्वचर्चा, पृष्ठ १२९ । २. जयपुर तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा, पृ० २८३-२८४ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org