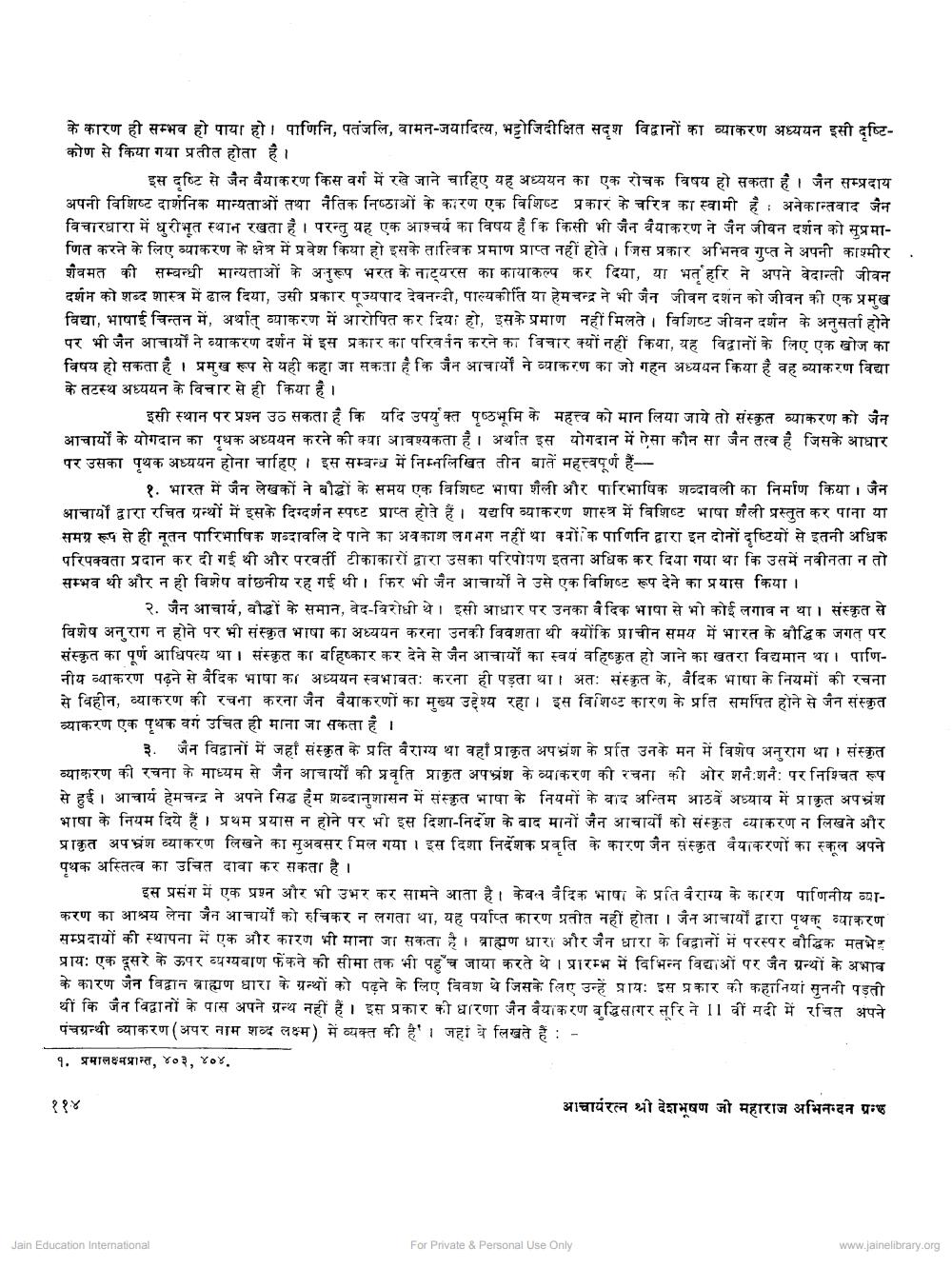________________
के कारण ही सम्भव हो पाया हो। पाणिनि, पतंजलि, वामन-जयादित्य, भट्टोजिदीक्षित सदृश विद्वानों का व्याकरण अध्ययन इसी दृष्टिकोण से किया गया प्रतीत होता है।
इस दृष्टि से जैन वैयाकरण किस वर्ग में रखे जाने चाहिए यह अध्ययन का एक रोचक विषय हो सकता है। जैन सम्प्रदाय अपनी विशिष्ट दार्शनिक मान्यताओं तथा नैतिक निष्ठाओं के कारण एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का स्वामी है। अनेकान्तवाद जैन विचारधारा में धुरीभूत स्थान रखता है। परन्तु यह एक आश्चर्य का विषय है कि किसी भी जैन वैयाकरण ने जैन जीवन दर्शन को सुप्रमाणित करने के लिए व्याकरण के क्षेत्र में प्रवेश किया हो इसके तात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार अभिनव गुप्त ने अपनी काश्मीर शैवमत की सम्बन्धी मान्यताओं के अनुरूप भरत के नाट्यरस का कायाकल्प कर दिया, या भत हरि ने अपने वेदान्ती जीवन दर्शन को शब्द शास्त्र में ढाल दिया, उसी प्रकार पूज्यपाद देवनन्दी, पाल्यकीर्ति या हेमचन्द्र ने भी जैन जीवन दर्शन को जीवन की एक प्रमुख विद्या, भाषाई चिन्तन में, अर्थात् व्याकरण में आरोपित कर दिया हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते। विशिष्ट जीवन दर्शन के अनुसा होने पर भी जैन आचार्यों ने व्याकरण दर्शन में इस प्रकार का परिवर्तन करने का विचार क्यों नहीं किया, यह विद्वानों के लिए एक खोज का विषय हो सकता है । प्रमुख रूप से यही कहा जा सकता है कि जैन आचार्यों ने व्याकरण का जो गहन अध्ययन किया है वह व्याकरण विद्या के तटस्थ अध्ययन के विचार से ही किया है।
इसी स्थान पर प्रश्न उ सकता है कि यदि उपर्युक्त पृष्ठभूमि के महत्त्व को मान लिया जाये तो संस्कृत व्याकरण को जैन आचार्यों के योगदान का पृथक अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। अर्थात इस योगदान में ऐसा कौन सा जैन तत्व है जिसके आधार पर उसका पृथक अध्ययन होना चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं
१. भारत में जैन लेखकों ने बौद्धों के समय एक विशिष्ट भाषा शैली और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया। जैन आचार्यों द्वारा रचित ग्रन्थों में इसके दिग्दर्शन स्पष्ट प्राप्त होते हैं। यद्यपि व्याकरण शास्त्र में विशिष्ट भाषा शैली प्रस्तुत कर पाना या समग्र रूप से ही नूतन पारिभाषिक शब्दावलि दे पाने का अवकाश लगभग नहीं था क्यों क पाणिनि द्वारा इन दोनों दृष्टियों से इतनी अधिक परिपक्वता प्रदान कर दी गई थी और परवर्ती टीकाकारों द्वारा उसका परिपोषण इतना अधिक कर दिया गया था कि उसमें नवीनता न तो सम्भव थी और न ही विशेष वांछनीय रह गई थी। फिर भी जैन आचार्यों ने उसे एक विशिष्ट रूप देने का प्रयास किया ।
२. जैन आचार्य, बौद्धों के समान, वेद-विरोधी थे। इसी आधार पर उनका वैदिक भाषा से भी कोई लगाव न था। संस्कृत से विशेष अनुराग न होने पर भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करना उनकी विवशता थी क्योंकि प्राचीन समय में भारत के बौद्धिक जगत पर संस्कृत का पूर्ण आधिपत्य था। संस्कृत का बहिष्कार कर देने से जैन आचार्यों का स्वयं वहिष्कृत हो जाने का खतरा विद्यमान था। पाणिनीय व्याकरण पढ़ने से वैदिक भाषा का अध्ययन स्वभावतः करना ही पड़ता था। अत: संस्कृत के, वैदिक भाषा के नियमों की रचना से विहीन, व्याकरण की रचना करना जैन वैयाकरणों का मुख्य उद्देश्य रहा। इस विशिष्ट कारण के प्रति समर्पित होने से जन संस्कृत व्याकरण एक पृथक वर्ग उचित ही माना जा सकता है ।
३. जैन विद्वानों में जहाँ संस्कृत के प्रति वैराग्य था वहाँ प्राकृत अपभ्रंश के प्रति उनके मन में विशेष अनुराग था। संस्कृत व्याकरण की रचना के माध्यम से जैन आचार्यों की प्रवृति प्राकृत अपभ्रंश के व्याकरण की रचना की ओर शनैःशनै: पर निश्चित रूप से हुई। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने सिद्ध हैम शब्दानुशासन में संस्कृत भाषा के नियमों के बाद अन्तिम आठवें अध्याय में प्राकृत अपभ्रंश भाषा के नियम दिये हैं। प्रथम प्रयास न होने पर भी इस दिशा-निर्देश के बाद मानों जैन आचार्यों को संस्कृत व्याकरण न लिखने और प्राकृत अपभ्रंश व्याकरण लिखने का सुअवसर मिल गया। इस दिशा निर्देशक प्रवृति के कारण जैन संस्कृत वैयाकरणों का स्कूल अपने पृथक अस्तित्व का उचित दावा कर सकता है।
इस प्रसंग में एक प्रश्न और भी उभर कर सामने आता है। केवल वैदिक भाषा के प्रति वैराग्य के कारण पाणिनीय व्याकरण का आश्रय लेना जैन आचार्यों को रुचिकर न लगता था, यह पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता । जैन आचार्यों द्वारा पृथक् व्याकरण सम्प्रदायों की स्थापना में एक और कारण भी माना जा सकता है। ब्राह्मण धारा और जैन धारा के विद्वानों में परस्पर बौद्धिक मतभेट प्राय: एक दूसरे के ऊपर व्यग्यबाण फेंकने की सीमा तक भी पहच जाया करते थे। प्रारम्भ में विभिन्न विद्याओं पर जैन ग्रन्थों के अभाव के कारण जैन विद्वान ब्राह्मण धारा के ग्रन्थों को पढ़ने के लिए विवश थे जिसके लिए उन्हें प्रायः इस प्रकार की कहानियां सुननी पड़ती थीं कि जैन विद्वानों के पास अपने ग्रन्थ नहीं हैं। इस प्रकार की धारणा जैन वैयाकरण बुद्धिसागर सूरि ने 11 वीं मदी में रचित अपने पंचग्रन्थी व्याकरण (अपर नाम शब्द लक्ष्म) में व्यक्त की है। जहां वे लिखते हैं : - १. प्रमालक्ष्मप्रान्त, ४०३, ४०४.
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रन्छ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org