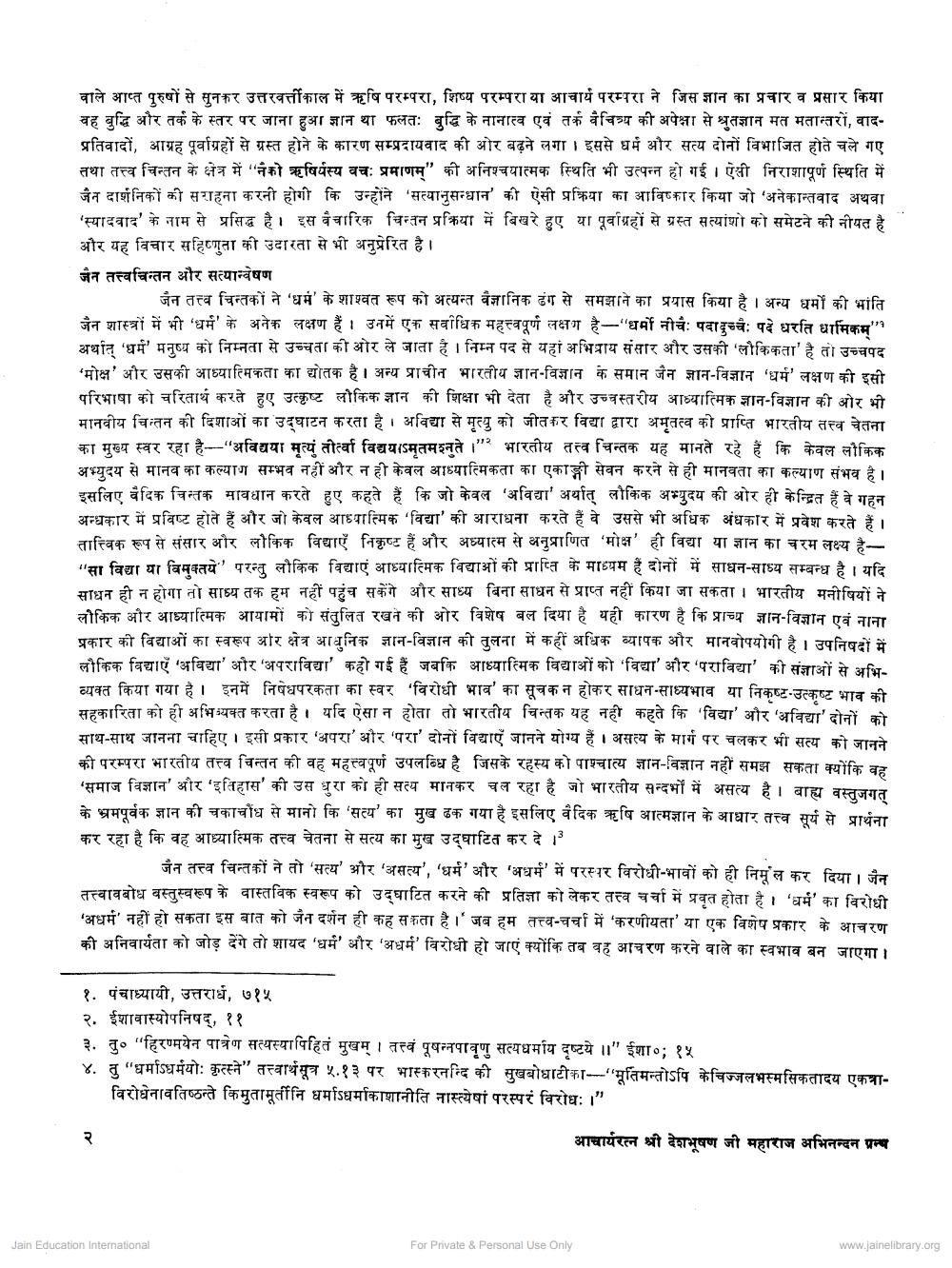________________
वाले आप्त पुरुषों से सुनकर उत्तरवर्त्तीकाल में ऋषि परम्परा, शिष्य परम्परा या आचार्य परम्परा ने जिस ज्ञान का प्रचार व प्रसार किया वह बुद्धि और तर्क के स्तर पर जाना हुआ ज्ञान था फलतः बुद्धि के नानात्व एवं तर्क वैचित्र्य की अपेक्षा से श्रुतज्ञान मत मतान्तरों, वादप्रतिवादों, आग्रह पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने के कारण सम्प्रदायवाद की ओर बढ़ने लगा। इससे धर्म और सत्य दोनों विभाजित होते चले गए तथा तत्त्व चिन्तन के क्षेत्र में "नेको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम्" की अनिश्चयात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो गई। ऐसी निराशापूर्ण स्थिति में जैन दार्शनिकों की सराहना करनी होगी कि उन्होंने 'सत्यानुसन्धान' की ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया जो 'अनेकान्तवाद अथवा 'स्यादवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। इस वैचारिक चिन्तन प्रक्रिया में बिखरे हुए या पूर्वाग्रहों से ग्रस्त सत्यांशो को समेटने की नीयत है और यह विचार सहिष्णुता की उदारता से भी अनुप्रेरित है ।
जैन तत्वचिन्तन और सत्यान्वेषण
जैन तत्त्व चिन्तकों ने 'धर्म' के शाश्वत रूप को अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अन्य धर्मों की भांति जैन शास्त्रों में भी 'धर्म' के अनेक लक्षण है उनमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है-धर्मो नी पापदे धरति धार्मिकम्"" अर्थात् 'धर्म' मनुष्य को निम्नता से उच्चता की ओर ले जाता है । निम्न पद से यहां अभिप्राय संसार और उसकी 'लौकिकता' है तो उच्चपद 'मोक्ष' और उसकी आध्यात्मिकता का द्योतक है। अन्य प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान के समान जैन ज्ञान-विज्ञान 'धर्म' लक्षण की इसी परिभाषा को चरितार्थ करते हुए उत्कृष्ट लौकिक ज्ञान की शिक्षा भी देता है और उच्चस्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान की ओर भी मानवीय चिन्तन की दिशाओं का उद्घाटन करता है। अविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति भारतीय तत्त्व चेतना का मुख्य स्वर रहा है- "अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।" भारतीय तत्व चिन्तक यह मानते रहे हैं कि केवल लौकिक अभ्युदय से मानव का कल्याण सम्भव नहीं और न ही केवल आध्यात्मिकता का एकाङ्गी सेवन करने से ही मानवता का कल्याण संभव है । इसलिए वैदिक चितक सावधान करते हुए कहते हैं कि जो केवल 'अविद्या' अर्थात् लौकिक अभ्युदय की ओर ही केन्द्रित हैं वे गहन अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं और जो केवल आध्यात्मिक 'विद्या' की आराधना करते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं । तात्विक रूप से संसार और लौकिक विद्याएँ निकृष्ट हैं और अध्यात्म से अनुप्राणित 'मोक्ष' ही विद्या या ज्ञान का चरम लक्ष्य है"सा विद्या या विमुक्तये' परन्तु लौकिक विद्याएं आध्यात्मिक विद्याओं की प्राप्ति के माध्यम हैं दोनों में साधन - साध्य सम्बन्ध है । साधन ही न होगा तो साध्य तक हम नहीं पहुंच सकेंगे और साध्य बिना साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता । भारतीय मनीषियों ने लौकिक और आध्यात्मिक आयामों को संतुलित रखने की ओर विशेष बल दिया है यही कारण है कि प्राच्य ज्ञान-विज्ञान एवं नाना प्रकार की विद्याओं का स्वरूप और क्षेत्र आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और मानवोपयोगी है। उपनिषदों में लौकिक विद्याएँ 'अविद्या' और 'अपराविद्या' कहो गई हैं जबकि आध्यात्मिक विद्याओं को 'विद्या' और 'पराविद्या' की संज्ञाओं से अभिव्यक्त किया गया है । इनमें निषेधपरकता का स्वर 'विरोधी भाव' का सूचक न होकर साधन-साध्यभाव या निकृष्ट उत्कृष्ट भाव की सहकारिता को ही अभिव्यक्त करता है। यदि ऐसा न होता तो भारतीय चिन्तक यह नहीं कहते कि 'विद्या' और 'अविद्या' दोनों को साथ-साथ जानना चाहिए। इसी प्रकार 'अपरा' और 'परा' दोनों विद्याएँ जानने योग्य हैं। असत्य के मार्ग पर चलकर भी सत्य को जानने की परम्परा भारतीय तत्त्व चिन्तन की वह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके रहस्य को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान नहीं समझ सकता क्योंकि वह 'समाज विज्ञान' और 'इतिहास' की उस धुरा को ही सत्य मानकर चल रहा है जो भारतीय सन्दर्भों में असत्य है । बाह्य वस्तुजगत् के भ्रमपूर्वक ज्ञान की चकाचौंध से मानो कि 'सत्य' का मुख ढक गया है इसलिए वैदिक ऋषि आत्मज्ञान के आधार तत्त्व सूर्य से प्रार्थना कर रहा है कि वह आध्यात्मिक तत्त्व चेतना से सत्य का मुख उद्घाटित कर दे 13
जैन तत्त्व चिन्तकों ने तो 'सत्य' और 'असत्य', 'धर्म' और 'अधर्म' में परस्पर विरोधी भावों को ही निर्मूल कर दिया। जैन तत्त्वावबोध वस्तुस्वरूप के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने की प्रतिज्ञा को लेकर तत्व पर्या में प्रवृत होता है 'धर्म' का विरोधी 'अधर्म' नहीं हो सकता इस बात को जैन दर्शन ही कह सकता है।' जब हम तत्त्व-चर्चा में 'करणीयता' या एक विशेष प्रकार के आचरण की अनिवार्यता को जोड़ देंगे तो शायद 'धर्म' और 'अधर्म' विरोधी हो जाएं क्योंकि तब वह आचरण करने वाले का स्वभाव बन जाएगा ।
१. पंचाध्यायी उत्तरार्ध ७१५
1
२. ईशावास्योपनिषद् ११
३. तु० "हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। " ईशा ०; १५
४. तु " धर्माधर्मयोः कृत्स्ने" तत्त्वार्थ सूत्र ५.१३ पर भास्करनन्दि की सुखबोधाटीका ---" मूर्तिमन्तोऽपि केचिज्जलभस्मसिकतादय एकत्राविरोधेनावतिष्ठन्ते किमुतामूर्ती धर्माधर्माकाशानीति नास्त्येषां परस्परं विरोधः ।"
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन प्रत्य
२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org