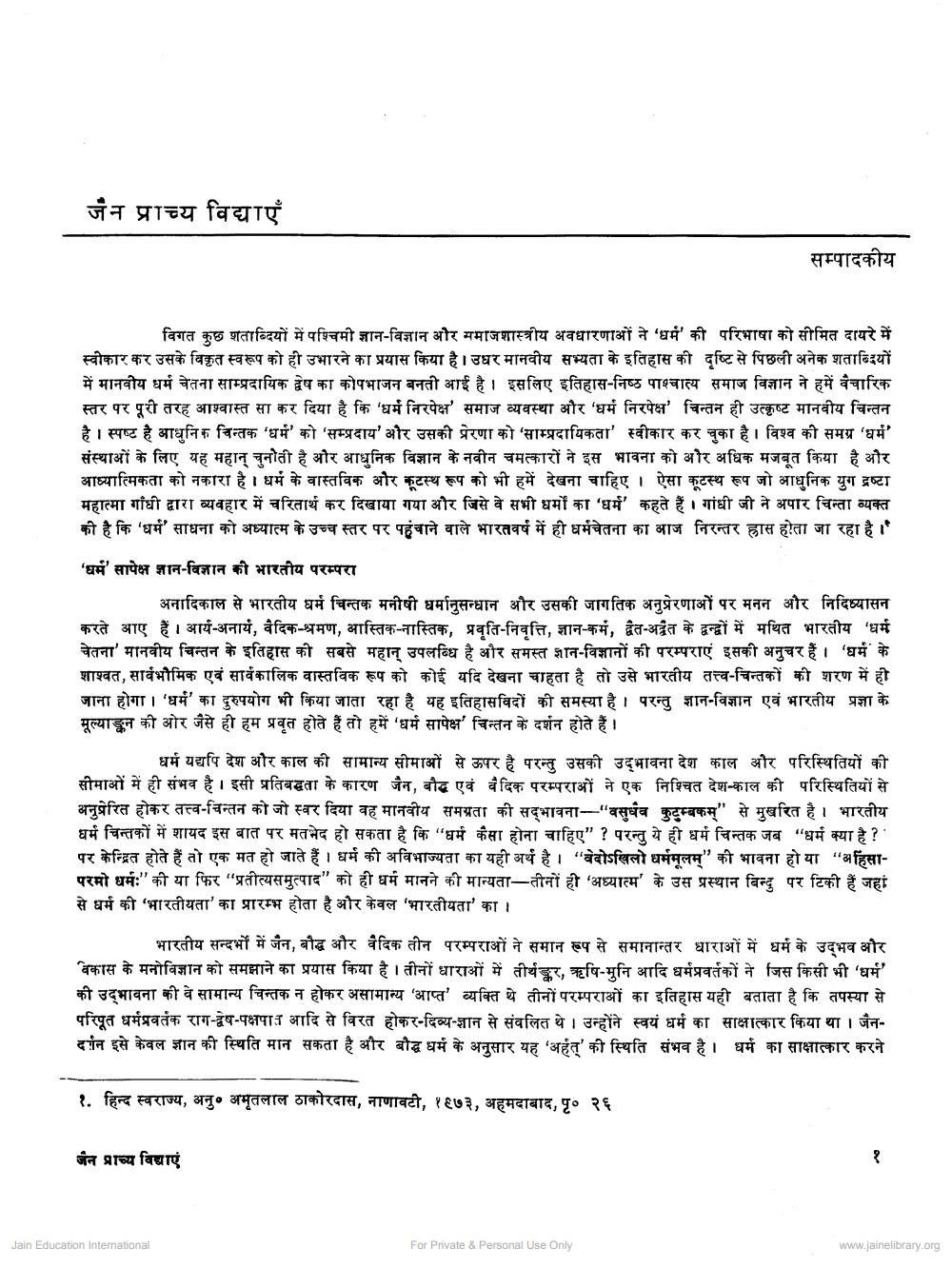________________
जन प्राच्य विद्याएँ
सम्पादकीय
विगत कुछ शताब्दियों में पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान और ममाजशास्त्रीय अवधारणाओं ने 'धर्म' की परिभाषा को सीमित दायरे में स्वीकार कर उसके विकृत स्वरूप को ही उभारने का प्रयास किया है। उधर मानवीय सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से पिछली अनेक शताब्दियों में मानवीय धर्म चेतना साम्प्रदायिक द्वेष का कोपभाजन बनती आई है। इसलिए इतिहास-निष्ठ पाश्चात्य समाज विज्ञान ने हमें वैचारिक स्तर पर पूरी तरह आश्वास्त सा कर दिया है कि 'धर्म निरपेक्ष' समाज व्यवस्था और 'धर्म निरपेक्ष' चिन्तन ही उत्कृष्ट मानवीय चिन्तन है । स्पष्ट है आधुनिक चिन्तक 'धर्म' को 'सम्प्रदाय' और उसकी प्रेरणा को 'साम्प्रदायिकता' स्वीकार कर चुका है। विश्व की समग्र 'धर्म' संस्थाओं के लिए यह महान् चुनोती है और आधुनिक विज्ञान के नवीन चमत्कारों ने इस भावना को और अधिक मजबूत किया है और आध्यात्मिकता को नकारा है। धर्म के वास्तविक और कूटस्थ रूप को भी हमें देखना चाहिए। ऐसा कूटस्थ रूप जो आधुनिक युग द्रष्टा महात्मा गांधी द्वारा व्यवहार में चरितार्थ कर दिखाया गया और जिसे वे सभी धर्मों का 'धर्म' कहते हैं। गांधी जी ने अपार चिन्ता व्यक्त की है कि 'धर्म' साधना को अध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले भारतवर्ष में ही धर्मचेतना का आज निरन्तर ह्रास होता जा रहा है।'
'धर्म' सापेक्ष ज्ञान-विज्ञान की भारतीय परम्परा
अनादिकाल से भारतीय धर्म चिन्तक मनीषी धर्मानुसन्धान और उसकी जागतिक अनुप्रेरणाओं पर मनन और निदिध्यासन करते आए हैं। आर्य-अनार्य, वैदिक-श्रमण, आस्तिक-नास्तिक, प्रवृति-निवृत्ति, ज्ञान-कर्म, द्वैत-अद्वैत के द्वन्द्वों में मथित भारतीय 'धर्म चेतना' मानवीय चिन्तन के इतिहास की सबसे महान् उपलब्धि है और समस्त ज्ञान-विज्ञानों की परम्पराएं इसकी अनुचर हैं। 'धर्म के शाश्वत, सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक वास्तविक रूप को कोई यदि देखना चाहता है तो उसे भारतीय तत्त्व-चिन्तकों की शरण में ही जाना होगा। 'धर्म' का दुरुपयोग भी किया जाता रहा है यह इतिहासविदों की समस्या है। परन्तु ज्ञान-विज्ञान एवं भारतीय प्रज्ञा के मूल्याङ्कन की ओर जैसे ही हम प्रवृत होते हैं तो हमें 'धर्म सापेक्ष चिन्तन के दर्शन होते हैं।
धर्म यद्यपि देश और काल की सामान्य सीमाओं से ऊपर है परन्तु उसकी उद्भावना देश काल और परिस्थितियों की सीमाओं में ही संभव है। इसी प्रतिबद्धता के कारण जैन, बौद्ध एवं वैदिक परम्पराओं ने एक निश्चित देश-काल की परिस्थितियों से अनुप्रेरित होकर तत्त्व-चिन्तन को जो स्वर दिया वह मानवीय समग्रता की सद्भावना-"वसुधव कुटुम्बकम्" से मुखरित है। भारतीय धर्म चिन्तकों में शायद इस बात पर मतभेद हो सकता है कि "धर्म कैसा होना चाहिए" ? परन्तु ये ही धर्म चिन्तक जब "धर्म क्या है ? ' पर केन्द्रित होते हैं तो एक मत हो जाते हैं । धर्म की अविभाज्यता का यही अर्थ है। "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" की भावना हो या "अहिंसापरमो धर्मः" की या फिर "प्रतीत्यसमुत्पाद" को ही धर्म मानने की मान्यता-तीनों ही 'अध्यात्म' के उस प्रस्थान बिन्दु पर टिकी हैं जहां से धर्म की 'भारतीयता' का प्रारम्भ होता है और केवल 'भारतीयता' का।
भारतीय सन्दर्भो में जैन, बौद्ध और वैदिक तीन परम्पराओं ने समान रूप से समानान्तर धाराओं में धर्म के उद्भव और विकास के मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। तीनों धाराओं में तीर्थङ्कर, ऋषि-मुनि आदि धर्मप्रवर्तकों ने जिस किसी भी 'धर्म' की उद्भावना की वे सामान्य चिन्तक न होकर असामान्य 'आप्त' व्यक्ति थे तीनों परम्पराओं का इतिहास यही बताता है कि तपस्या से परिपूत धर्मप्रवर्तक राग-द्वेष-पक्षपात आदि से विरत होकर-दिव्य-ज्ञान से संवलित थे। उन्होंने स्वयं धर्म का साक्षात्कार किया था। जैनदर्शन इसे केवल ज्ञान की स्थिति मान सकता है और बौद्ध धर्म के अनुसार यह 'अर्हत्' की स्थिति संभव है। धर्म का साक्षात्कार करने
१. हिन्द स्वराज्य, अनु० अमृतलाल ठाकोरदास, नाणावटी, १६७३, अहमदाबाद, पृ० २६
जैन प्राच्य विद्याएं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org