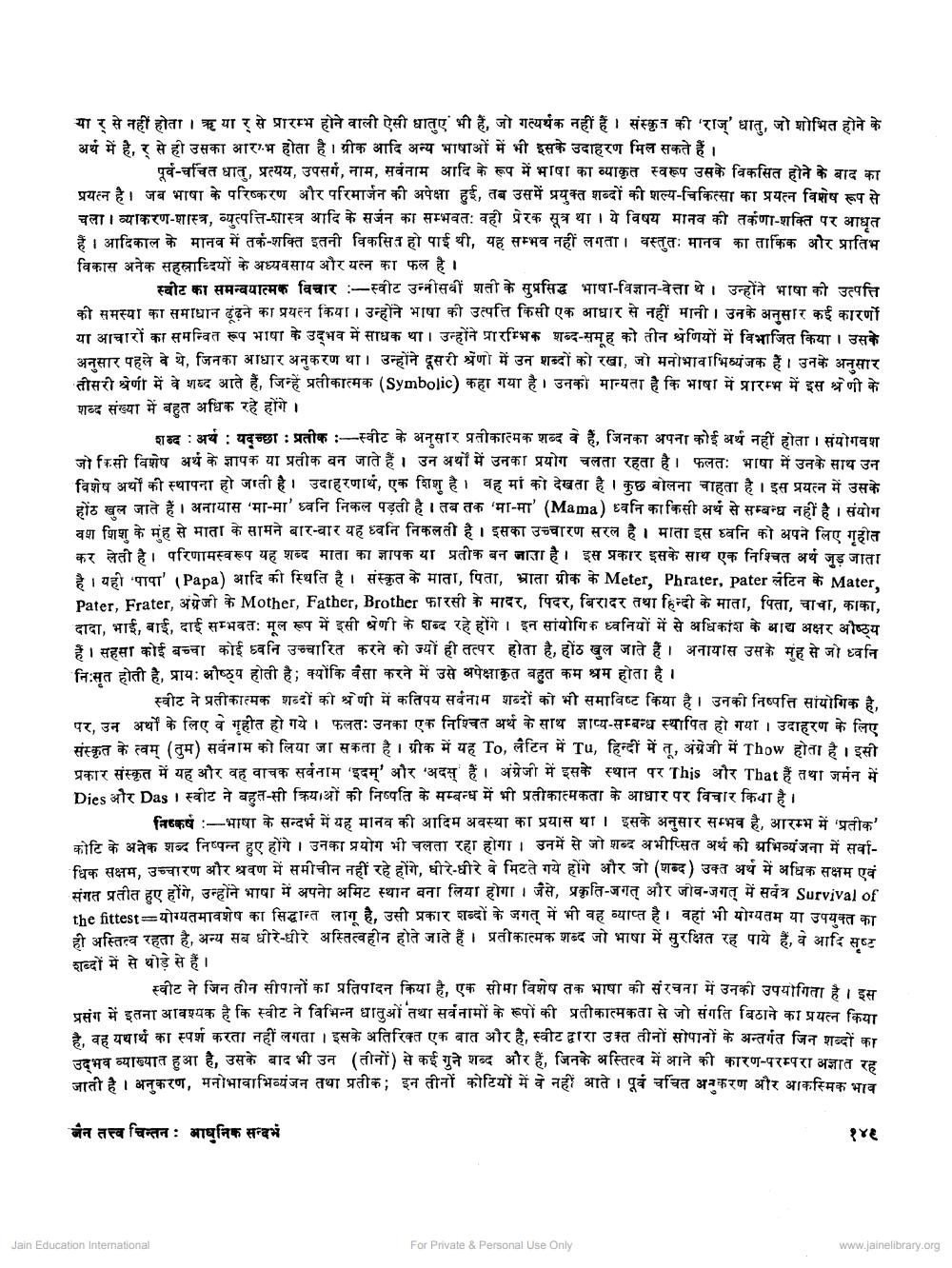________________
या र् से नहीं होता । ऋ या र् से प्रारम्भ होने वाली ऐसी धातुएं भी हैं, जो गत्यर्थक नहीं हैं। संस्कृत की 'राज्' धातु, जो शोभित होने के अर्थ में है, र से ही उसका आरम्भ होता है। ग्रीक आदि अन्य भाषाओं में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं।
पूर्व-चचित धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, नाम, सर्वनाम आदि के रूप में भाषा का व्याकृत स्वरूप उसके विकसित होने के बाद का प्रयत्न है। जब भाषा के परिष्करण और परिमार्जन की अपेक्षा हुई, तब उसमें प्रयुक्त शब्दों की शल्य-चिकित्सा का प्रयत्न विशेष रूप से चला। व्याकरण-शास्त्र, व्युत्पत्ति-शास्त्र आदि के सर्जन का सम्भवत: वही प्रेरक सूत्र था। ये विषय मानव की तकणा-शक्ति पर आधत हैं। आदिकाल के मानव में तर्क-शक्ति इतनी विकसित हो पाई थी, यह सम्भव नहीं लगता। वस्तुतः मानव का तार्किक और प्रातिभ विकास अनेक सहस्राब्दियों के अध्यवसाय और यत्न का फल है।
स्वीट का समन्वयात्मक विचार :-स्वीट उन्नीसवीं शती के सुप्रसिद्ध भाषा-विज्ञान-वेत्ता थे। उन्होंने भाषा को उत्पत्ति की समस्या का समाधान ढंढने का प्रयत्न किया। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति किसी एक आधार से नहीं मानी। उनके अनुसार कई कारणों या आचारों का समन्वित रूप भाषा के उद्भव में साधक था। उन्होंने प्रारम्भिक शब्द-समूह को तीन श्रेणियों में विभाजित किया । उसके अनसार पहले वे थे, जिनका आधार अनुकरण था। उन्होंने दूसरी श्रेणो में उन शब्दों को रखा, जो मनोभावाभिव्यंजक हैं। उनके अनुसार तीसरी श्रेणी में वे शब्द आते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक (Symbolic) कहा गया है। उनको मान्यता है कि भाषा में प्रारम्भ में इस श्रेणी के शब्द संख्या में बहुत अधिक रहे होंगे।
शब्द : अर्थ : यदच्छा : प्रतीक :-स्वीट के अनुसार प्रतीकात्मक शब्द वे हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। संयोगवश जो किसी विशेष अर्थ के ज्ञापक या प्रतीक बन जाते हैं। उन अर्थों में उनका प्रयोग चलता रहता है। फलतः भाषा में उनके साथ उन विशेष अर्थों की स्थापना हो जाती है। उदाहरणार्थ, एक शिशु है। वह मां को देखता है । कुछ बोलना चाहता है । इस प्रयत्न में उसके होंठ खल जाते हैं। अनायास 'मा-मा' ध्वनि निकल पड़ती है। तब तक 'मा-मा' (Mama) ध्वनि का किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं है । संयोग वशिश के मंह से माता के सामने बार-बार यह ध्वनि निकलती है। इसका उच्चारण सरल है। माता इस ध्वनि को अपने लिए गहीत कर लेती है। परिणामस्वरूप यह शब्द माता का ज्ञापक या प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार इसके साथ एक निश्चित अर्थ जुड़ जाता है। यही 'पापा' | Papa) आदि की स्थिति है। संस्कृत के माता, पिता, भ्राता ग्रीक के Meter. Phrater. pater लंटिन के Mater Pater. Frater, अंग्रेजी के Mother, Father, Brother फारसी के मादर, पिदर, बिरादर तथा हिन्दी के माता, पिता, चाचा, काका, दादा भाई, बाई, दाई सम्भवत: मूल रूप में इसी श्रेणी के शब्द रहे होंगे। इन सांयोगिक ध्वनियों में से अधिकांश के माद्य अक्षर औष्ठ्य हैं। सहसा कोई बच्चा कोई ध्वनि उच्चारित करने को ज्यों ही तत्पर होता है, होंठ खुल जाते हैं। अनायास उसके मुह से जो ध्वनि निःसत होती है, प्रायः औष्ठ्य होती है। क्योंकि वैसा करने में उसे अपेक्षाकृत बहुत कम श्रम होता है ।
स्वीट ने प्रतीकात्मक शब्दों की श्रेणी में कतिपय सर्वनाम शब्दों को भी समाविष्ट किया है। उनकी निष्पत्ति सांयोगिक है, पर उन अर्थों के लिए व गहीत हो गये। फलतः उनका एक निश्चित अर्थ के साथ ज्ञाप्य-सम्बन्ध स्थापित हो गया । उदाहरण के लिए संस्कृत के त्वम् (तुम) सर्वनाम को लिया जा सकता है। ग्रीक में यह To, लैटिन में Tu, हिन्दी में तू, अंग्रेजी में Thow होता है। इसी प्रकार संस्कृत में यह और वह वाचक सर्वनाम 'इदम्' और 'अदस् हैं। अंग्रेजी में इसके स्थान पर This और That हैं तथा जर्मन में Dies और Das | स्वीट ने बहुत-सी क्रियाओं की निष्पति के सम्बन्ध में भी प्रतीकात्मकता के आधार पर विचार किया है।
निष्कर्ष :-भाषा के सन्दर्भ में यह मानव की आदिम अवस्था का प्रयास था। इसके अनुसार सम्भव है, आरम्भ में 'प्रतीक' कोटि के अनेक शब्द निष्पन्न हुए होंगे। उनका प्रयोग भी चलता रहा होगा। उनमें से जो शब्द अभीप्सित अर्थ की अभिव्यंजना में सर्वाधिक सक्षम, उच्चारण और श्रवण में समीचीन नहीं रहे होंगे, धीरे-धीरे वे मिटते गये होंगे और जो (शब्द) उक्त अर्थ में अधिक सक्षम एवं संगत प्रतीत हए होंगे, उन्होंने भाषा में अपना अमिट स्थान बना लिया होगा। जैसे, प्रकृति-जगत् और जीव-जगत् में सर्वत्र Survival of the fittest=योग्यतमावशेष का सिद्धान्त लागू है, उसी प्रकार शब्दों के जगत् में भी वह व्याप्त है। वहां भी योग्यतम या उपयक्त का ही अस्तित्व रहता है, अन्य सब धीरे-धीरे अस्तित्वहीन होते जाते हैं। प्रतीकात्मक शब्द जो भाषा में सुरक्षित रह पाये हैं, वे आदि सष्ट शब्दों में से थोड़े से हैं।
स्वीट ने जिन तीन सीपानों का प्रतिपादन किया है, एक सीमा विशेष तक भाषा को संरचना में उनकी उपयोगिता है। इस प्रसंग में इतना आवश्यक है कि स्वीट ने विभिन्न धातुओं तथा सर्वनामों के रूपों की प्रतीकात्मकता से जो संगति बिठाने का प्रयत्न किया है. वह यथार्थ का स्पर्श करता नहीं लगता । इसके अतिरिक्त एक बात और है, स्वीट द्वारा उक्त तीनों सोपानों के अन्तर्गत जिन शब्दों का उदभव व्याख्यात हुआ है, उसके बाद भी उन (तीनों) से कई गुने शब्द और हैं, जिनके अस्तित्व में आने की कारण-परम्परा अज्ञात रख जाती है । अनकरण, मनोभावाभिव्यंजन तथा प्रतीक ; इन तीनों कोटियों में वे नहीं आते । पूर्व चचित अनकरण और आकस्मिक भाव
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
१४६
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org