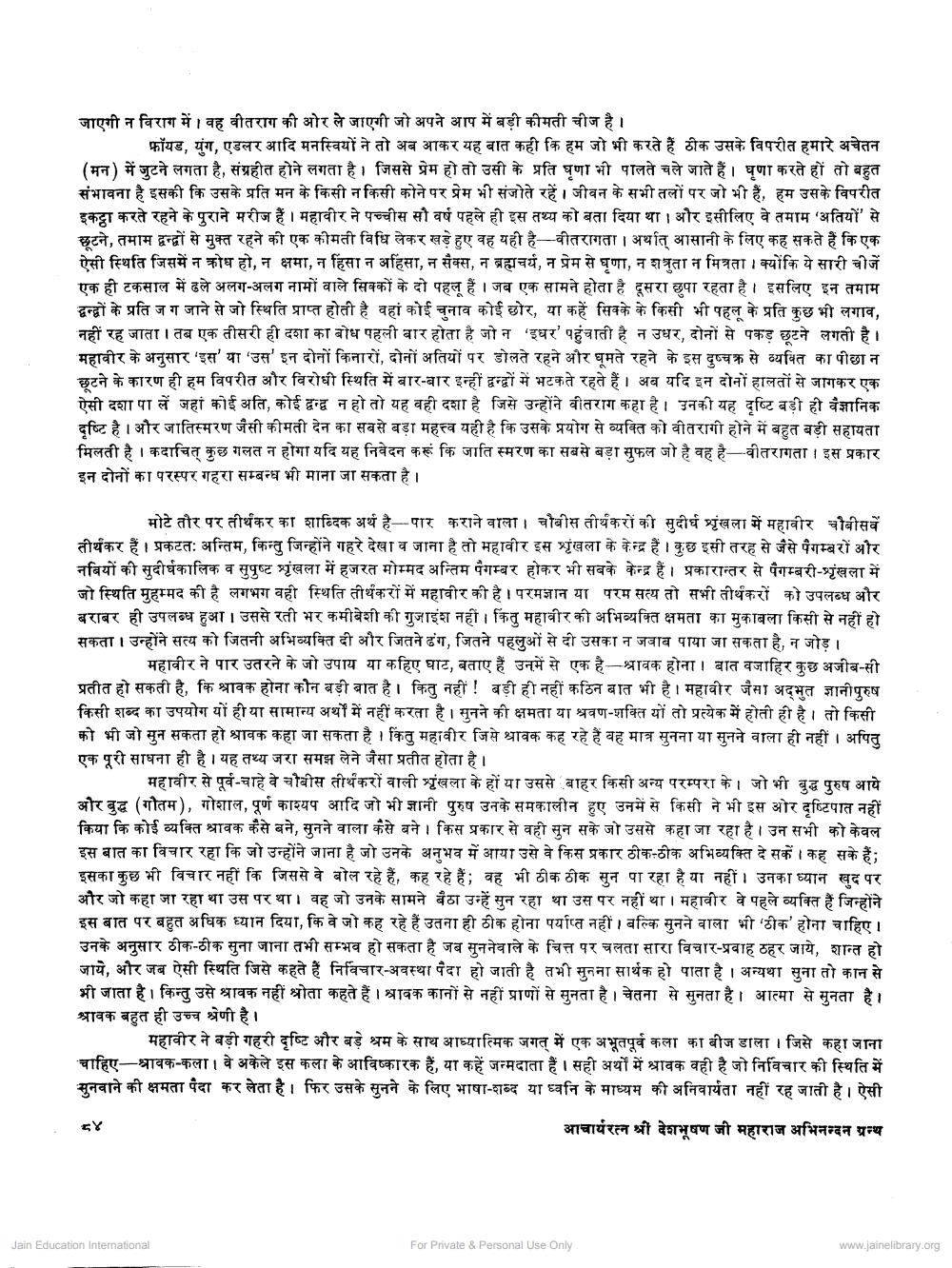________________
जाएगी न विराग में। वह वीतराग की ओर ले जाएगी जो अपने आप में बड़ी कीमती चीज है।
फॉयड, युंग, एडलर आदि मनस्वियों ने तो अब आकर यह बात कही कि हम जो भी करते हैं ठीक उसके विपरीत हमारे अचेतन (मन) में जुटने लगता है, संग्रहीत होने लगता है। जिससे प्रेम हो तो उसी के प्रति घृणा भी पालते चले जाते हैं। घृणा करते हों तो बहुत संभावना है इसकी कि उसके प्रति मन के किसी न किसी कोने पर प्रेम भी संजोते रहें। जीवन के सभी तलों पर जो भी हैं, हम उसके विपरीत इकट्ठा करते रहने के पुराने मरीज हैं। महावीर ने पच्चीस सौ वर्ष पहले ही इस तथ्य को बता दिया था। और इसीलिए वे तमाम 'अतियों' से छूटने, तमाम द्वन्द्वों से मुक्त रहने की एक कीमती विधि लेकर खड़े हुए वह यही है—वीतरागता । अर्थात् आसानी के लिए कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें न क्रोध हो, न क्षमा, न हिंसा न अहिंसा, न सैक्स, न ब्रह्मचर्य, न प्रेम से घृणा, न शत्रुता न मित्रता। क्योंकि ये सारी चीजें एक ही टकसाल में ढले अलग-अलग नामों वाले सिक्कों के दो पहलू हैं । जब एक सामने होता है दूसरा छुपा रहता है। इसलिए इन तमाम द्वन्द्वों के प्रति ज ग जाने से जो स्थिति प्राप्त होती है वहां कोई चुनाव कोई छोर, या कहें सिक्के के किसी भी पहलू के प्रति कुछ भी लगाव, नहीं रह जाता । तब एक तीसरी ही दशा का बोध पहली बार होता है जो न 'इधर' पहुंचाती है न उधर, दोनों से पकड़ छूटने लगती है। महावीर के अनुसार 'इस' या 'उस' इन दोनों किनारों, दोनों अतियों पर डोलते रहने और घूमते रहने के इस दुष्चक्र से व्यक्ति का पीछा न छूटने के कारण ही हम विपरीत और विरोधी स्थिति में बार-बार इन्हीं द्वन्द्वों में भटकते रहते हैं। अब यदि इन दोनों हालतों से जागकर एक ऐसी दशा पा लें जहां कोई अति, कोई द्वन्द्व न हो तो यह वही दशा है जिसे उन्होंने वीतराग कहा है। उनकी यह दृष्टि बड़ी ही वैज्ञानिक दृष्टि है । और जातिस्मरण जैसी कीमती देन का सबसे बड़ा महत्त्व यही है कि उसके प्रयोग से व्यक्ति को वीतरागी होने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है । कदाचित् कुछ गलत न होगा यदि यह निवेदन करूं कि जाति स्मरण का सबसे बड़ा सुफल जो है वह है-वीतरागता । इस प्रकार इन दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध भी माना जा सकता है।
९
.
मोटे तौर पर तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है-पार कराने वाला। चौबीस तीर्थंकरों की सुदीर्घ शृंखला में महावीर चौबीसवें तीर्थकर हैं। प्रकटतः अन्तिम, किन्तु जिन्होंने गहरे देखा व जाना है तो महावीर इस शृंखला के केन्द्र हैं। कुछ इसी तरह से जैसे पैगम्बरों और नबियों की सुदीर्घकालिक व सुपुष्ट शृंखला में हजरत मोम्मद अन्तिम पैगम्बर होकर भी सबके केन्द्र हैं। प्रकारान्तर से पैगम्बरी-शृंखला में जो स्थिति मुहम्मद की है लगभग वही स्थिति तीर्थंकरों में महावीर की है। परमज्ञान या परम सत्य तो सभी तीर्थकरों को उपलब्ध और बराबर ही उपलब्ध हुआ। उससे रती भर कमीबेशी की गुजाइंश नहीं। किंतु महावीर की अभिव्यक्ति क्षमता का मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। उन्होंने सत्य को जितनी अभिव्यक्ति दी और जितने ढंग, जितने पहलुओं से दी उसका न जबाब पाया जा सकता है, न जोड़।
महावीर ने पार उतरने के जो उपाय या कहिए घाट, बताए हैं उनमें से एक है-श्रावक होना। बात वजाहिर कुछ अजीब-सी प्रतीत हो सकती है, कि श्रावक होना कोन बड़ी बात है। कितु नहीं ! बड़ी ही नहीं कठिन बात भी है। महावीर जैसा अद्भुत ज्ञानीपुरुष किसी शब्द का उपयोग यों ही या सामान्य अर्थों में नहीं करता है। सुनने की क्षमता या श्रवण-शक्ति यों तो प्रत्येक में होती ही है। तो किसी को भी जो सुन सकता हो श्रावक कहा जा सकता है। किंतु महावीर जिसे श्रावक कह रहे हैं वह मात्र सुनना या सुनने वाला ही नहीं । अपितु एक पूरी साधना ही है। यह तथ्य जरा समझ लेने जैसा प्रतीत होता है।
महावीर से पूर्व-चाहे वे चौबीस तीर्थंकरों वाली श्रृंखला के हों या उससे बाहर किसी अन्य परम्परा के। जो भी बुद्ध पुरुष आये और बुद्ध (गौतम), गोशाल, पूर्ण काश्यप आदि जो भी ज्ञानी पुरुष उनके समकालीन हुए उनमें से किसी ने भी इस ओर दृष्टिपात नहीं किया कि कोई व्यक्ति श्रावक कैसे बने, सुनने वाला कैसे बने। किस प्रकार से वही सुन सके जो उससे कहा जा रहा है। उन सभी को केवल इस बात का विचार रहा कि जो उन्होंने जाना है जो उनके अनुभव में आया उसे वे किस प्रकार ठीक-ठीक अभिव्यक्ति दे सकें। कह सके हैं; इसका कुछ भी विचार नहीं कि जिससे वे बोल रहे हैं, कह रहे हैं; वह भी ठीक ठीक सुन पा रहा है या नहीं। उनका ध्यान खुद पर
और जो कहा जा रहा था उस पर था। वह जो उनके सामने बैठा उन्हें सुन रहा था उस पर नहीं था। महावीर वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया, कि वे जो कह रहे हैं उतना ही ठीक होना पर्याप्त नहीं। बल्कि सुनने वाला भी ठीक' होना चाहिए। उनके अनुसार ठीक-ठीक सुना जाना तभी सम्भव हो सकता है जब सुननेवाले के चित्त पर चलता सारा विचार-प्रवाह ठहर जाये, शान्त हो जाये, और जब ऐसी स्थिति जिसे कहते हैं निर्विचार-अवस्था पैदा हो जाती है तभी सुनना सार्थक हो पाता है । अन्यथा सुना तो कान से भी जाता है। किन्तु उसे श्रावक नहीं श्रोता कहते हैं। श्रावक कानों से नहीं प्राणों से सुनता है। चेतना से सुनता है। आत्मा से सुनता है। श्रावक बहुत ही उच्च श्रेणी है।
महावीर ने बड़ी गहरी दृष्टि और बड़े श्रम के साथ आध्यात्मिक जगत् में एक अभूतपूर्व कला का बीज डाला । जिसे कहा जाना चाहिए-श्रावक-कला। वे अकेले इस कला के आविष्कारक हैं, या कहें जन्मदाता हैं । सही अर्थों में श्रावक वही है जो निविचार की स्थिति में सुनवाने की क्षमता पैदा कर लेता है। फिर उसके सुनने के लिए भाषा-शब्द या ध्वनि के माध्यम की अनिवार्यता नहीं रह जाती है। ऐसी
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org