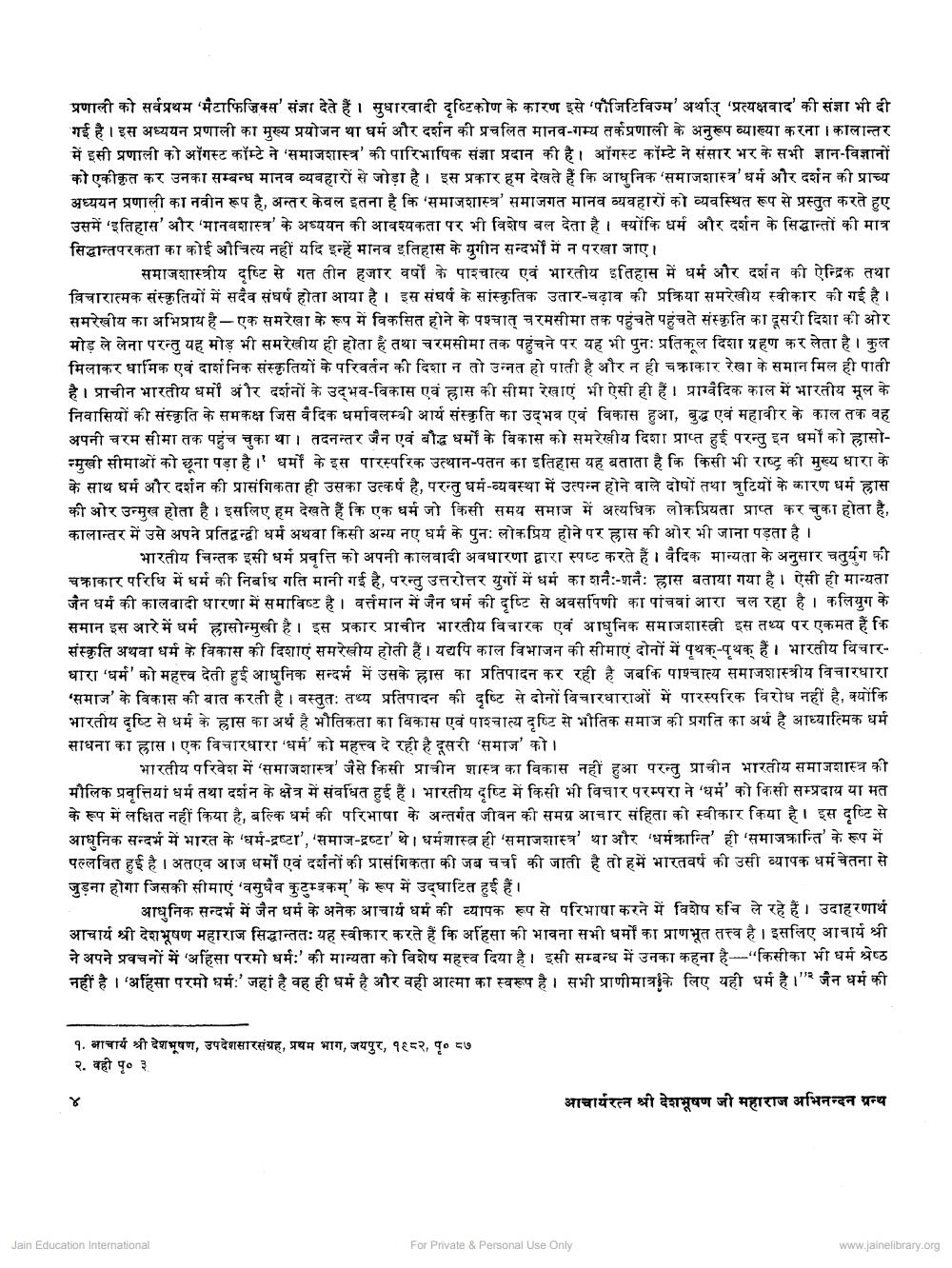________________
प्रणाली को सर्वप्रथम 'मैटाफिजिक्स' संज्ञा देते हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण इसे 'पोजिटिविज्म' अर्थात् 'प्रत्यक्षवाद' की संज्ञा भी दी गई है। इस अध्ययन प्रणाली का मुख्य प्रयोजन था धर्म और दर्शन की प्रचलित मानव-गम्य तर्कप्रणाली के अनुरूप व्याख्या करना । कालान्तर में इसी प्रणाली को ऑगस्ट कॉम्टे ने 'समाजशास्त्र' की पारिभाषिक संज्ञा प्रदान की है। ऑगस्ट कॉम्टे ने संसार भर के सभी ज्ञान-विज्ञानों को एकीकृत कर उनका सम्बन्ध मानव व्यवहारों से जोड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्र' धर्म और दर्शन की प्राच्य अध्ययन प्रणाली का नवीन रूप है, अन्तर केवल इतना है कि 'समाजशास्त्र' समाजगत मानव व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हुए उसमें 'इतिहास' और 'मानवशास्त्र' के अध्ययन की आवश्यकता पर भी विशेष बल देता है। क्योंकि धर्म और दर्शन के सिद्धान्तों की मात्र सिद्धान्तपरकता का कोई औचित्य नहीं यदि इन्हें मानव इतिहास के युगीन सन्दर्भो में न परखा जाए।
समाजशास्त्रीय दृष्टि से गत तीन हजार वर्षों के पाश्चात्य एवं भारतीय इतिहास में धर्म और दर्शन की ऐन्द्रिक तथा विचारात्मक संस्कृतियों में सदैव संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष के सांस्कृतिक उतार-चढ़ाव की प्रक्रिया समरेखीय स्वीकार की गई है। समरेखीय का अभिप्राय है-एक समरेखा के रूप में विकसित होने के पश्चात् चरमसीमा तक पहुंचते पहुंचते संस्कृति का दूसरी दिशा की ओर मोड़ ले लेना परन्तु यह मोड़ भी समरेखीय ही होता है तथा चरमसीमा तक पहुंचने पर यह भी पुनः प्रतिकूल दिशा ग्रहण कर लेता है । कुल मिलाकर धार्मिक एवं दार्शनिक संस्कृतियों के परिवर्तन की दिशा न तो उन्नत हो पाती है और न ही चक्राकार रेखा के समान मिल ही पाती है। प्राचीन भारतीय धर्मों और दर्शनों के उद्भव-विकास एवं ह्रास की सीमा रेखाएं भी ऐसी ही हैं। प्राग्वैदिक काल में भारतीय मूल के निवासियों की संस्कृति के समकक्ष जिस वैदिक धर्मावलम्बी आर्य संस्कृति का उद्भव एवं विकास हुआ, बुद्ध एवं महावीर के काल तक वह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तदनन्तर जैन एवं बौद्ध धर्मों के विकास को समरेखीय दिशा प्राप्त हुई परन्तु इन धर्मों को ह्रासोन्मुखी सीमाओं को छूना पड़ा है।' धर्मों के इस पारस्परिक उत्थान-पतन का इतिहास यह बताता है कि किसी भी राष्ट्र की मुख्य धारा के के साथ धर्म और दर्शन की प्रासंगिकता ही उसका उत्कर्ष है, परन्तु धर्म-व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले दोषों तथा त्रुटियों के कारण धर्म ह्रास की ओर उन्मुख होता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक धर्म जो किसी समय समाज में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर चुका होता है, कालान्तर में उसे अपने प्रतिद्वन्द्वी धर्म अथवा किसी अन्य नए धर्म के पुनः लोकप्रिय होने पर ह्रास की ओर भी जाना पड़ता है।
भारतीय चिन्तक इसी धर्म प्रवृत्ति को अपनी कालवादी अवधारणा द्वारा स्पष्ट करते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार चतुर्युग की चक्राकार परिधि में धर्म की निर्बाध गति मानी गई है, परन्तु उत्तरोत्तर युगों में धर्म का शनैः-शनैः ह्रास बताया गया है। ऐसी ही मान्यता जैन धर्म की कालवादी धारणा में समाविष्ट है। वर्तमान में जैन धर्म की दृष्टि से अवसर्पिणी का पांचवां आरा चल रहा है। कलियुग के समान इस आरे में धर्म ह्रासोन्मुखी है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारक एवं आधुनिक समाजशास्त्री इस तथ्य पर एकमत हैं कि संस्कृति अथवा धर्म के विकास की दिशाएं समरेखीय होती हैं। यद्यपि काल विभाजन की सीमाएं दोनों में पृथक्-पृथक् हैं। भारतीय विचारधारा 'धर्म' को महत्त्व देती हुई आधुनिक सन्दर्भ में उसके ह्रास का प्रतिपादन कर रही है जबकि पाश्चात्य समाजशास्त्रीय विचारधारा 'समाज' के विकास की बात करती है । वस्तुतः तथ्य प्रतिपादन की दृष्टि से दोनों विचारधाराओं में पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योंकि भारतीय दृष्टि से धर्म के ह्रास का अर्थ है भौतिकता का विकास एवं पाश्चात्य दृष्टि से भौतिक समाज की प्रगति का अर्थ है आध्यात्मिक धर्म साधना का ह्रास । एक विचारधारा 'धर्म' को महत्त्व दे रही है दूसरी 'समाज' को।
भारतीय परिवेश में 'समाजशास्त्र' जैसे किसी प्राचीन शास्त्र का विकास नहीं हुआ परन्तु प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र की मौलिक प्रवृत्तियां धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में संवर्धित हुई हैं। भारतीय दृष्टि में किसी भी विचार परम्परा ने 'धर्म' को किसी सम्प्रदाय या मत के रूप में लक्षित नहीं किया है, बल्कि धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत जीवन की समग्र आचार संहिता को स्वीकार किया है। इस दृष्टि से आधुनिक सन्दर्भ में भारत के 'धर्म-द्रष्टा', 'समाज-द्रष्टा' थे। धर्मशास्त्र ही 'समाजशास्त्र' था और 'धर्मक्रान्ति' ही 'समाजक्रान्ति' के रूप में पल्लवित हुई है । अतएव आज धर्मों एवं दर्शनों की प्रासंगिकता की जब चर्चा की जाती है तो हमें भारतवर्ष की उसी व्यापक धर्म चेतना से जुड़ना होगा जिसकी सीमाएं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में उद्घाटित हुई हैं। - आधुनिक सन्दर्भ में जैन धर्म के अनेक आचार्य धर्म की व्यापक रूप से परिभाषा करने में विशेष रुचि ले रहे हैं। उदाहरणार्थ आचार्य श्री देशभूषण महाराज सिद्धान्ततः यह स्वीकार करते हैं कि अहिंसा की भावना सभी धर्मों का प्राणभूत तत्त्व है। इसलिए आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में 'अहिंसा परमो धर्मः' की मान्यता को विशेष महत्त्व दिया है। इसी सम्बन्ध में उनका कहना है.---"किसीका भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है । 'अहिंसा परमो धर्मः' जहां है वह ही धर्म है और वही आत्मा का स्वरूप है। सभी प्राणीमात्र के लिए यही धर्म है।" जैन धर्म की
१. आचार्य श्री देशभूषण, उपदेशसारसंग्रह, प्रथम भाग, जयपुर, १९८२, पृ०८७ २. वही पृ० ३
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org