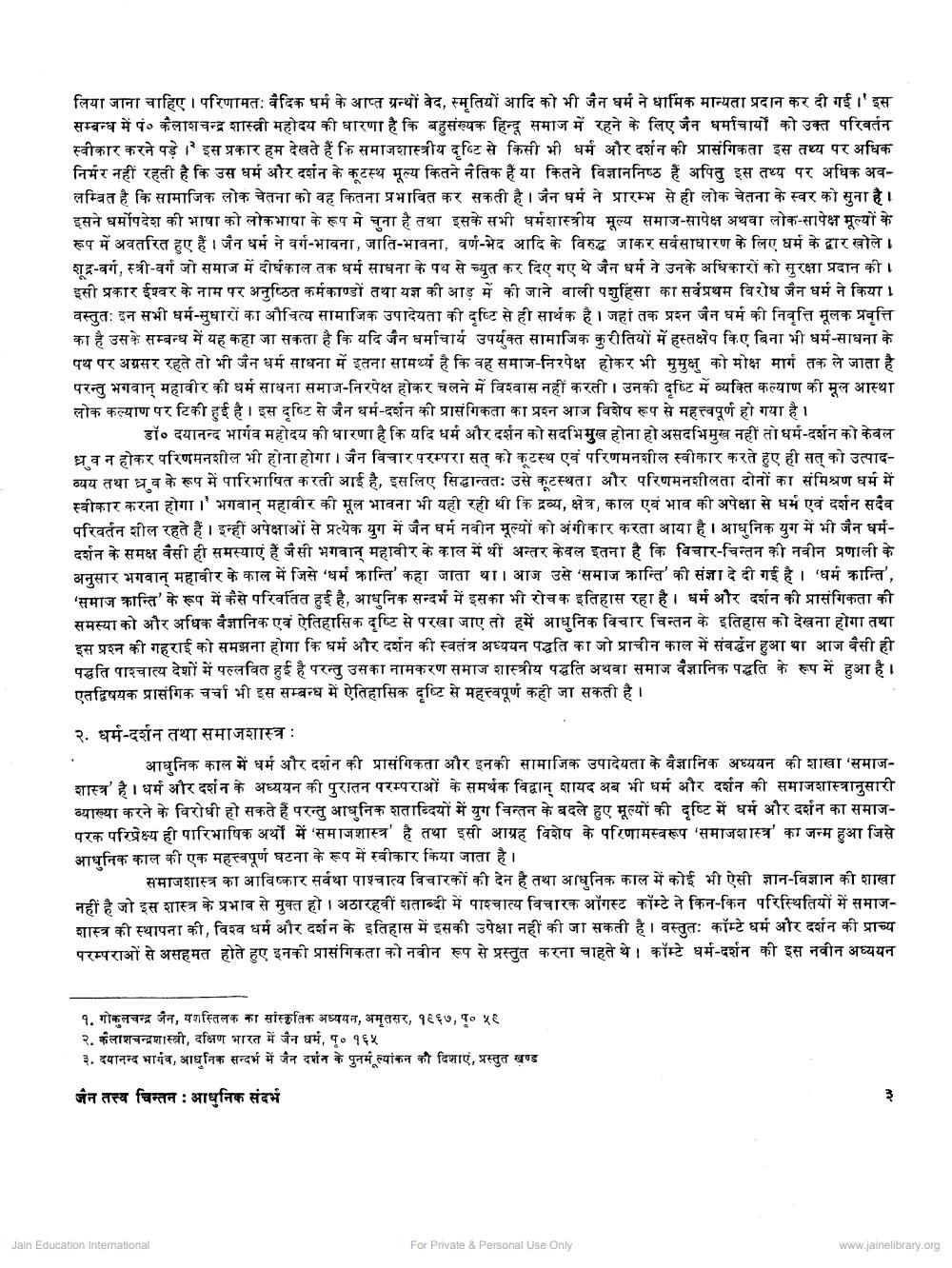________________
लिया जाना चाहिए। परिणामत: वैदिक धर्म के आप्त ग्रन्थों वेद, स्मृतियों आदि को भी जैन धर्म ने धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इस सम्बन्ध में पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री महोदय की धारणा है कि बहुसंख्यक हिन्दू समाज में रहने के लिए जैन धर्माचार्यों को उक्त परिवर्तन स्वीकार करने पड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी भी धर्म और दर्शन की प्रासंगिकता इस तथ्य पर अधिक निर्मर नहीं रहती है कि उस धर्म और दर्शन के कूटस्थ मूल्य कितने नैतिक हैं या कितने विज्ञाननिष्ठ हैं अपितु इस तथ्य पर अधिक अवलम्बित है कि सामाजिक लोक चेतना को वह कितना प्रभावित कर सकती है। जैन धर्म ने प्रारम्भ से ही लोक चेतना के स्वर को सुना है। इसने धर्मोपदेश की भाषा को लोकभाषा के रूप में चुना है तथा इसके सभी धर्मशास्त्रीय मूल्य समाज-सापेक्ष अथवा लोक-सापेक्ष मूल्यों के रूप में अवतरित हुए हैं । जैन धर्म ने वर्ग-भावना, जाति-भावना, वर्ण-भेद आदि के विरुद्ध जाकर सर्वसाधारण के लिए धर्म के द्वार खोले। शूद्र-वर्ग, स्त्री-वर्ग जो समाज में दीर्घकाल तक धर्म साधना के पथ से च्युत कर दिए गए थे जैन धर्म ने उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। इसी प्रकार ईश्वर के नाम पर अनुष्ठित कर्मकाण्डों तथा यज्ञ की आड़ में की जाने वाली पशुहिंसा का सर्वप्रथम विरोध जैन धर्म ने किया। वस्तुतः इन सभी धर्म-सुधारों का औचित्य सामाजिक उपादेयता की दृष्टि से ही सार्थक है। जहां तक प्रश्न जैन धर्म की निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का है उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि जैन धर्माचार्य उपर्युक्त सामाजिक कुरीतियों में हस्तक्षेप किए बिना भी धर्म-साधना के पथ पर अग्रसर रहते तो भी जैन धर्म साधना में इतना सामर्थ्य है कि वह समाज-निरपेक्ष होकर भी मुमुक्षु को मोक्ष मार्ग तक ले जाता है परन्तु भगवान् महावीर की धर्म सावना समाज-निरपेक्ष होकर चलने में विश्वास नहीं करती। उनकी दृष्टि में व्यक्ति कल्याण की मूल आस्था लोक कल्याण पर टिकी हुई है। इस दृष्टि से जैन धर्म-दर्शन की प्रासंगिकता का प्रश्न आज विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गया है।
डॉ. दयानन्द भार्गव महोदय की धारणा है कि यदि धर्म और दर्शन को सदभिमुख होना हो असदभिमुख नहीं तोधर्म-दर्शन को केवल ध्र व न होकर परिणमनशील भी होना होगा। जैन विचार परम्परा सत् को कूटस्थ एवं परिणमनशील स्वीकार करते हुए ही सत् को उत्पादव्यय तथा ध्रुव के रूप में पारिभाषित करती आई है, इसलिए सिद्धान्ततः उसे कूटस्थता और परिणमनशीलता दोनों का संमिश्रण धर्म में स्वीकार करना होगा। भगवान महावीर की मूल भावना भी यही रही थी कि द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा से धर्म एवं दर्शन सदैव परिवर्तन शील रहते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं से प्रत्येक युग में जैन धर्म नवीन मूल्यों को अंगीकार करता आया है । आधुनिक युग में भी जैन धर्मदर्शन के समक्ष वैसी ही समस्याएं हैं जैसी भगवान महावीर के काल में थीं अन्तर केवल इतना है कि विचार-चिन्तन की नवीन प्रणाली के अनुसार भगवान महावीर के काल में जिसे 'धर्म क्रान्ति' कहा जाता था। आज उसे 'समाज क्रान्ति' की संज्ञा दे दी गई है। 'धर्म क्रान्ति', 'समाज क्रान्ति' के रूप में कैसे परिवर्तित हुई है, आधुनिक सन्दर्भ में इसका भी रोचक इतिहास रहा है। धर्म और दर्शन की प्रासंगिकता की समस्या को और अधिक वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से परखा जाए तो हमें आधुनिक विचार चिन्तन के इतिहास को देखना होगा तथा इस प्रश्न की गहराई को समझना होगा कि धर्म और दर्शन की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का जो प्राचीन काल में संवर्द्धन हुआ था आज वैसी ही पद्धति पाश्चात्य देशों में पल्लवित हुई है परन्तु उसका नामकरण समाज शास्त्रीय पद्धति अथवा समाज वैज्ञानिक पद्धति के रूप में हुआ है। एतद्विषयक प्रासंगिक चर्चा भी इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है।
२. धर्म-दर्शन तथा समाजशास्त्र :
आधुनिक काल में धर्म और दर्शन की प्रासंगिकता और इनकी सामाजिक उपादेयता के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा 'समाजशास्त्र' है। धर्म और दर्शन के अध्ययन की पुरातन परम्पराओं के समर्थक विद्वान् शायद अब भी धर्म और दर्शन की समाजशास्त्रानुसारी व्याख्या करने के विरोधी हो सकते हैं परन्तु आधुनिक शताब्दियों में युग चिन्तन के बदले हुए मूल्यों की दृष्टि में धर्म और दर्शन का समाजपरक परिप्रेक्ष्य ही पारिभाषिक अर्थों में समाजशास्त्र' है तथा इसी आग्रह विशेष के परिणामस्वरूप 'समाजशास्त्र' का जन्म हुआ जिसे आधुनिक काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है।
समाजशास्त्र का आविष्कार सर्वथा पाश्चात्य विचारकों की देन है तथा आधुनिक काल में कोई भी ऐसी ज्ञान-विज्ञान की शाखा नहीं है जो इस शास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो । अठारहवीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने किन-किन परिस्थितियों में समाजशास्त्र की स्थापना की, विश्व धर्म और दर्शन के इतिहास में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वस्तुतः कॉम्टे धर्म और दर्शन की प्राच्य परम्पराओं से असहमत होते हुए इनकी प्रासंगिकता को नवीन रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे। कॉम्टे धर्म-दर्शन की इस नवीन अध्ययन
१. गोकुलचन्द्र जैन, यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, अमृतसर, १६६७, पृ० ५६ २. कैलाशचन्द्र शास्त्री, दक्षिण भारत में जैन धर्म, पृ० १६५ ३. दयानन्द भार्गव, आधुनिक सन्दर्भ में जैन दर्शन के पुनर्म ल्यांकन की दिशाएं, प्रस्तुत खण्ड
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक संदर्भ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org