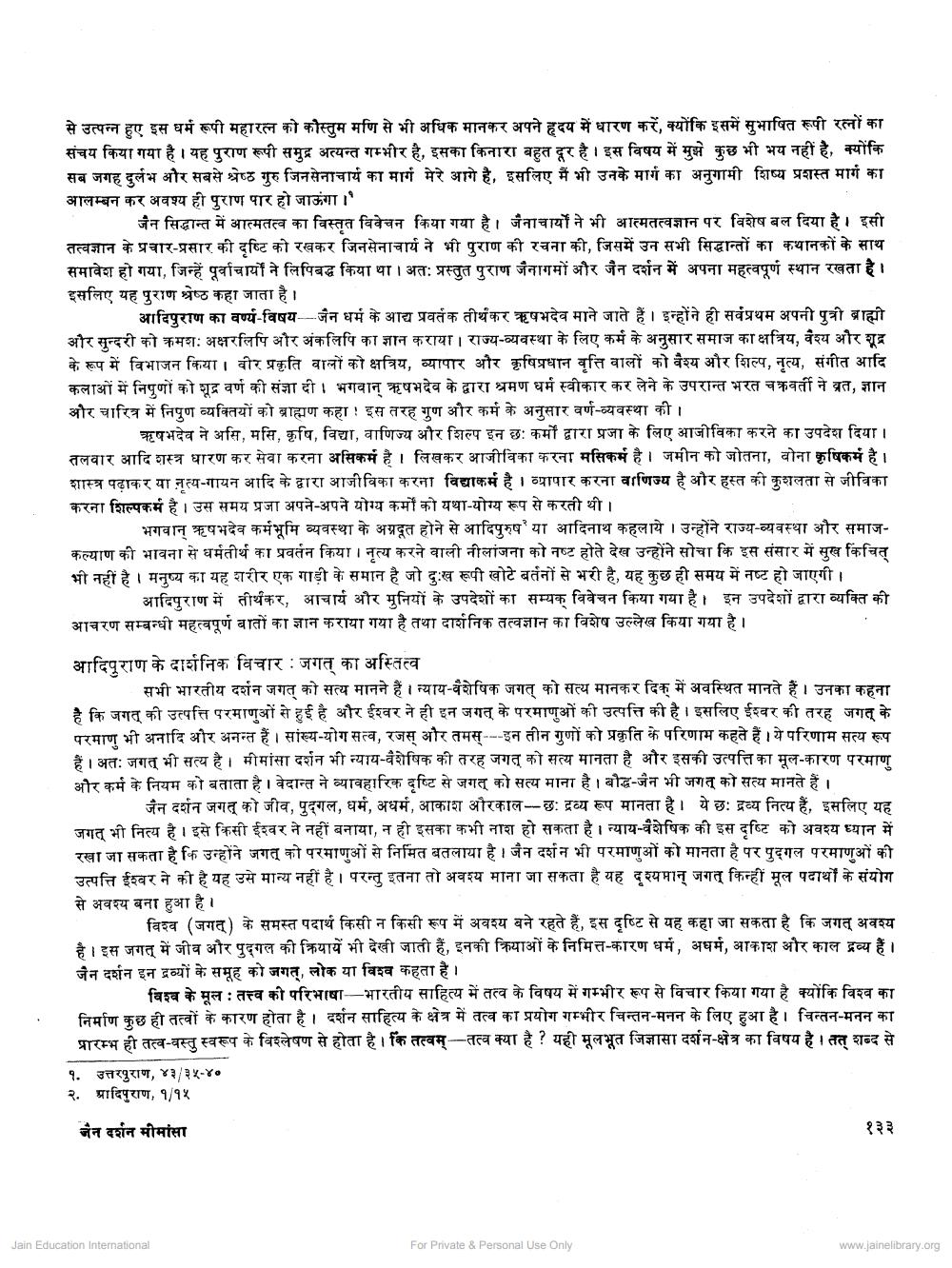________________
से उत्पन्न हुए इस धर्म रूपी महारत्न को कौस्तुम मणि से भी अधिक मानकर अपने हृदय में धारण करें, क्योंकि इसमें सुभाषित रूपी रत्नों का संचय किया गया है । यह पुराण रूपी समुद्र अत्यन्त गम्भीर है, इसका किनारा बहुत दूर है। इस विषय में मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि सब जगह दुर्लभ और सबसे श्रेष्ठ गुरु जिनसेनाचार्य का मार्ग मेरे आगे है, इसलिए मैं भी उनके मार्ग का अनुगामी शिष्य प्रशस्त मार्ग का आलम्बन कर अवश्य ही पुराण पार हो जाऊंगा ।'
जैन सिद्धान्त में आत्मतत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है। जैनाचार्यों ने भी आत्मतत्वज्ञान पर विशेष बल दिया है। इसी तत्वज्ञान के प्रचार-प्रसार की दृष्टि को रखकर जिनसेनाचार्य ने भी पुराण की रचना की, जिसमें उन सभी सिद्धान्तों का कथानकों के साथ समावेश हो गया, जिन्हें पूर्वाचायों ने लिपिबद्ध किया था अतः प्रस्तुत पुराण जैनागमों और जैन दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए यह पुराण श्रेष्ठ कहा जाता है।
आदिपुराण का वर्ण्य विषय- जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को क्रमशः अक्षरलिपि और अंकलिपि का ज्ञान कराया। राज्य व्यवस्था के लिए कर्म के अनुसार समाज का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजन किया। वीर प्रकृति वालों को क्षत्रिय, व्यापार और कृषिप्रधान वृत्ति वालों को वैश्य और शिल्प, नृत्य, संगीत आदि कलाओं में निपुणों को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी। भगवान् ऋषभदेव के द्वारा श्रमण धर्म स्वीकार कर लेने के उपरान्त भरत चक्रवर्ती ने व्रत, ज्ञान और चारित्र में निपुण व्यक्तियों को ब्राह्मण कहा । इस तरह गुण और कर्म के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की ।
ऋषभदेव ने असि मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छः कर्मों द्वारा प्रजा के लिए आजीविका करने का उपदेश दिया । तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना असिकर्म है। लिखकर आजीविका करना मसिकर्म है। जमीन को जोतना, बोना कृषिकर्म है । शास्त्र पढ़ाकर या नृत्य-गायन आदि के द्वारा आजीविका करना विद्याकर्म है । व्यापार करना वाणिज्य है और हस्त की कुशलता से जीविका करना शिल्पकर्म है। उस समय प्रजा अपने-अपने योग्य कर्मों को यथा योग्य रूप से करती थी ।
भगवान् ऋषभदेव कर्मभूमि व्यवस्था के अग्रदूत होने से आदिपुरुष' या आदिनाथ कहलाये । उन्होंने राज्य-व्यवस्था और समाजकल्याण की भावना से धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया । नृत्य करने वाली नीलांजना को नष्ट होते देख उन्होंने सोचा कि इस संसार में सुख किचित् भी नहीं है । मनुष्य का यह शरीर एक गाड़ी के समान है जो दुःख रूपी खोटे बर्तनों से भरी है, यह कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी।
आदिपुराण में तीर्थंकर आचार्य और मुनियों के उपदेशों का सम्यक् विवेचन किया गया है। इन उपदेशों द्वारा व्यक्ति की आचरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान कराया गया है तथा दार्शनिक तत्वज्ञान का विशेष उल्लेख किया गया है ।
आदिपुराण के दार्शनिक विचार जगत् का अस्तित्व
सभी भारतीय दर्शन जगत् को सत्य मानने हैं। न्याय-वैशेषिक जगत् को सत्य मानकर दिक् में अवस्थित मानते हैं। उनका कहना है कि जगत् की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है और ईश्वर ने ही इन जगत् के परमाणुओं की उत्पत्ति की है। इसलिए ईश्वर की तरह जगत् के परमाणु भी अनादि और अनन्त हैं । सांख्य योग सत्व, रजस् और तमस् - इन तीन गुणों को प्रकृति के परिणाम कहते हैं। ये परिणाम सत्य रूप हैं । अतः जगत् भी सत्य है। मीमांसा दर्शन भी न्याय-वैशेषिक की तरह जगत् को सत्य मानता है और इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परमाणु और कर्म के नियम को बताता है । वेदान्त ने व्यावहारिक दृष्टि से जगत् को सत्य माना है । बोद्ध-जैन भी जगत् को सत्य मानते हैं ।
जैन दर्शन जगत् को जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश औरकाल -- छ: द्रव्य रूप मानता है । ये छ: द्रव्य नित्य हैं, इसलिए यह जगत् भी नित्य है । इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, न ही इसका कभी नाश हो सकता है। न्याय-वैशेषिक की इस दृष्टि को अवश्य ध्यान में रखा जा सकता है कि उन्होंने जगत् को परमाणुओं से निर्मित बतलाया है। जैन दर्शन भी परमाणुओं को मानता है पर पुद्गल परमाणुओं की उत्पत्ति ईश्वर ने की है यह उसे मान्य नहीं है । परन्तु इतना तो अवश्य माना जा सकता है यह दृश्यमान् जगत् किन्हीं मूल पदार्थों के संयोग से अवश्य बना हुआ है ।
विश्व (जगत्) के समस्त पदार्थ किसी न किसी रूप में अवश्य बने रहते हैं, इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जगत् अवश्य है । इस जगत् में जीव और पुद्गल की क्रियायें भी देखी जाती हैं, इनकी क्रियाओं के निमित्त कारण धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य हैं । जैन दर्शन इन द्रव्यों के समूह को जगत्, लोक या विश्व कहता है।
विश्व के मूल तत्व की परिभाषा - भारतीय साहित्य में तत्व के विषय में गम्भीर रूप से विचार किया गया है क्योंकि विश्व का निर्माण कुछ ही तत्वों के कारण होता है। दर्शन साहित्य के क्षेत्र में तत्व का प्रयोग गम्भीर चिन्तन-मनन के लिए हुआ है। चिन्तन-मनन का प्रारम्भ ही तत्व-वस्तु स्वरूप के विश्लेषण से होता है। कि तत्वम् -- तत्व क्या है ? यही मूलभूत जिज्ञासा दर्शन क्षेत्र का विषय है । तत् शब्द से १. उत्तरपुराण, ४३ / ३५-४० २. प्रदिपुराण, १/१५
जैन दर्शन मीमांसा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१३३
www.jainelibrary.org