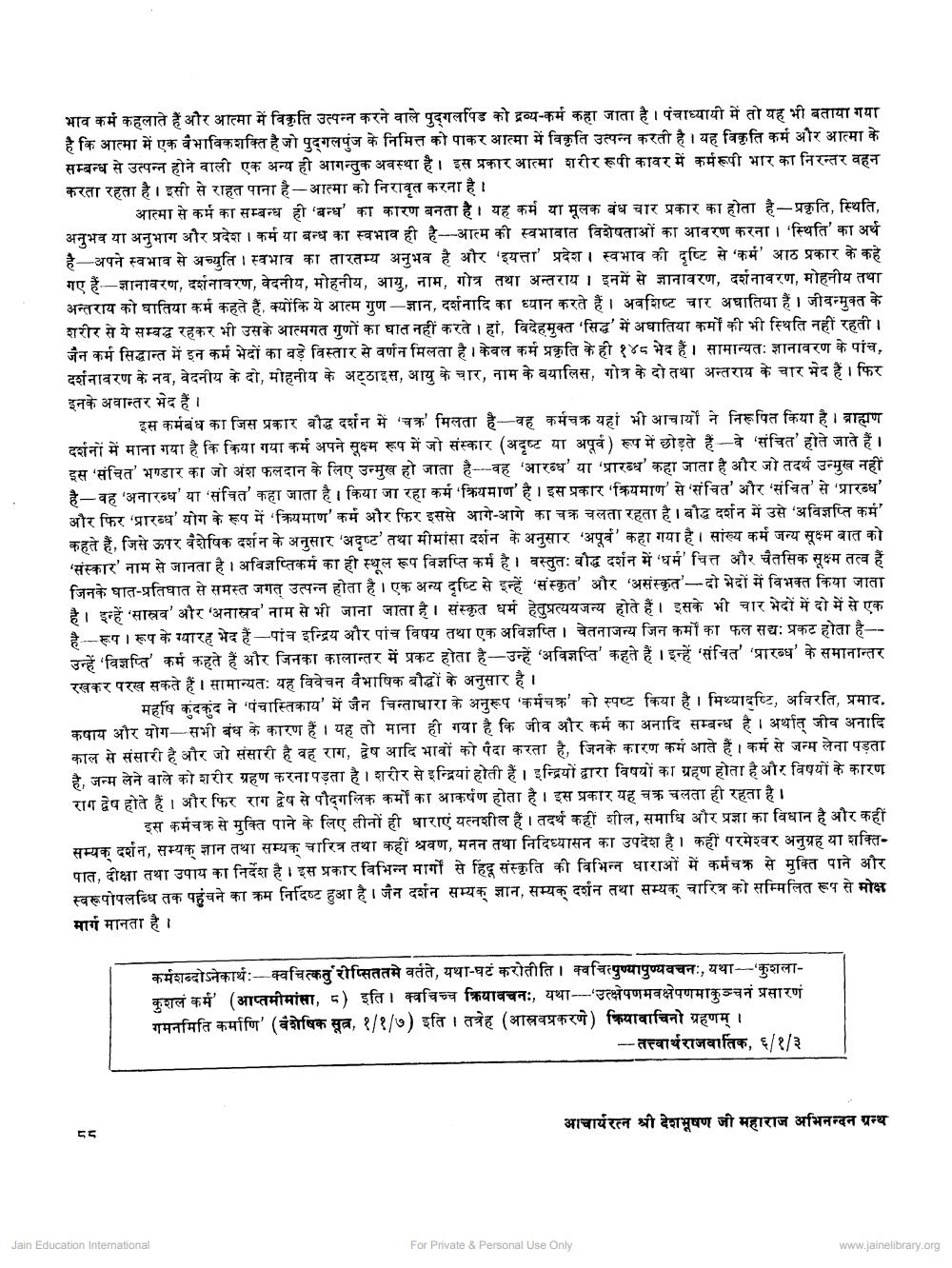________________
भाव कर्म कहलाते हैं और आत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले पुद्गलपिंड को द्रव्य-कर्म कहा जाता है। पंचाध्यायी में तो यह भी बताया गया है कि आत्मा में एक वैभाविकशक्ति है जो पुद्गलपुंज के निमित्त को पाकर आत्मा में विकृति उत्पन्न करती है। यह विकृति कर्म और आत्मा के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली एक अन्य ही आगन्तुक अवस्था है । इस प्रकार आत्मा शरीर रूपी कावर में कर्मरूपी भार का निरन्तर वहन करता रहता है। इसी से राहत पाना है- आत्मा को निरावृत करना है।
आत्मा से कर्म का सम्बन्ध ही 'बन्ध' का कारण बनता है। यह कर्म या मूलक बंध चार प्रकार का होता है- प्रकृति, स्थिति, अनुभव या अनुभाग और प्रदेश । कर्म या बन्ध का स्वभाव ही है-आत्म की स्वभावात विशेषताओं का आवरण करना। 'स्थिति' का अर्थ है - अपने स्वभाव से अच्युति । स्वभाव का तारतम्य अनुभव है और 'इयत्ता' प्रदेश | स्वभाव की दृष्टि से 'कर्म' आठ प्रकार के कहे गए हैं- ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अन्तराय । इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये आत्म गुण- ज्ञान दर्शनादि का ध्यान करते हैं । अवशिष्ट चार अघातिया हैं । जीवन्मुक्त के शरीर से ये सम्बद्ध रहकर भी उसके आत्मगत गुणों का घात नहीं करते। हां, विदेहमुक्त 'सिद्ध' में अघातिया कर्मों की भी स्थिति नहीं रहती । जैन कर्म सिद्धान्त में इन कर्म भेदों का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। केवल कर्म प्रकृति के ही १४८ भेद हैं। सामान्यतः ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावरण के नव, वेदनीय के दो, मोहनीय के अट्ठाइस आयु के चार, नाम के बयालिस, गोत्र के दो तथा अन्तराय के चार भेद हैं। फिर इनके अवान्तर भेद हैं ।
इस कर्मबंध का जिस प्रकार बौद्ध दर्शन में 'चक्र' मिलता है वह कर्मचक्र यहां भी आचार्यों ने निरूपित किया है। ब्राह्मण दर्शनों में माना गया है कि किया गया कर्म अपने सूक्ष्म रूप में जो संस्कार ( अदृष्ट या अपूर्व ) रूप में छोड़ते हैं - वे 'संचित' होते जाते हैं । इस 'संचित' भण्डार का जो अंश फलदान के लिए उन्मुख हो जाता है--- वह 'आरब्ध' या 'प्रारब्ध' कहा जाता है और जो तदर्थ उन्मुख नहीं है - वह 'अनारब्ध' या 'संचित' कहा जाता है। किया जा रहा कर्म 'क्रियमाण' है। इस प्रकार 'क्रियमाण' से 'संचित' और 'संचित' से 'प्रारब्ध' और फिर 'प्रारब्ध' योग के रूप में 'क्रियमाण' कर्म और फिर इससे आगे-आगे का चक्र चलता रहता है। बौद्ध दर्शन में उसे 'अविज्ञप्ति कर्म' कहते हैं, जिसे ऊपर वैशेषिक दर्शन के अनुसार 'अदृष्ट' तथा मीमांसा दर्शन के अनुसार 'अपूर्व कहा गया है। सांख्य कर्म जन्म सूक्ष्म बात को 'संस्कार' नाम से जानता है। अविज्ञप्तिकर्म का ही स्थूल रूप विज्ञप्ति कर्म है। वस्तुतः बौद्ध दर्शन में 'धर्म' चित्त और चैतसिक सूक्ष्म तत्व हैं जिनके घात-प्रतिघात से समस्त जगत् उत्पन्न होता है। एक अन्य दृष्टि से इन्हें 'संस्कृत' और 'असंस्कृत' - दो भेदों में विभक्त किया जाता है इन्हें 'साख' और 'अनान' नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत धर्म हेतुप्रत्ययजन्य होते हैं। इसके भी चार भेदों में दो में से एक है रूप । रूप के ग्यारह भेद हैं-पांच इन्द्रिय और पांच विषय तथा एक अविज्ञप्ति । चेतनाजन्य जिन कर्मों का फल सद्यः प्रकट होता हैउन्हें 'विशति' कर्म कहते हैं और जिनका कालान्तर में प्रकट होता है उन्हें 'अविशन्ति' कहते हैं। इन्हें 'संचित' 'प्रारब्ध' के समानान्तर रखकर परख सकते हैं। सामान्यतः यह विवेचन वैभाषिक बौद्धों के अनुसार है ।
महर्षि कुंदकुंद ने 'पंचास्तिकाय' में जैन चिन्ताधारा के अनुरूप 'कर्मचक्र' को स्पष्ट किया है। मिध्यादृष्टि, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग - सभी बंध के कारण हैं । यह तो माना ही गया है कि जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध है । अर्थात् जीव अनादि काल से संसारी है और जो संसारी है वह राग, द्वेष आदि भावों को पैदा करता है, जिनके कारण कर्म आते हैं। कर्म से जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेने वाले को शरीर ग्रहण करना पड़ता है। शरीर से इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण होता है और विषयों के कारण राग द्वेष होते हैं । और फिर राग द्वेष से पौद्गलिक कर्मों का आकर्षण होता है। इस प्रकार यह चक्र चलता ही रहता है।
इस कर्मचक्र से मुक्ति पाने के लिए तीनों ही धाराएं यत्नशील हैं। तदर्थ कहीं शील, समाधि और प्रज्ञा का विधान है और कहीं सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र तथा कहीं श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन का उपदेश है। कहीं परमेश्वर अनुग्रह या शक्तिपात, दीक्षा तथा उपाय का निर्देश है। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से हिंदू संस्कृति की विभिन्न धाराओं में कर्मचक्र से मुक्ति पाने और स्वरूपोपलब्धि तक पहुंचने का क्रम निर्दिष्ट हुआ है। जैन दर्शन सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् चारित्र को सम्मिलित रूप से मोक्ष मार्ग मानता है ।
८८
1
2
कर्मशब्दोऽकार्यक्वचित्कतु रीप्सिततमे वर्तते यचापटं करोतीति स्ववित्पुण्यापुण्यवचनः यथा कुशलाकुशलं कर्म (आप्तमीमांसा, ६) इति क्वविश्व क्रियावचन:, यथा-उत्पणमनक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं । गमनमिति कर्माणि' (वंशेषिकसूत्र १/१/७ ) इति तह (आयप्रकरणे) क्रियावाचिनो ग्रहणम् ।
- तत्वावराजवातिक ६/१/२
Jain Education International
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org