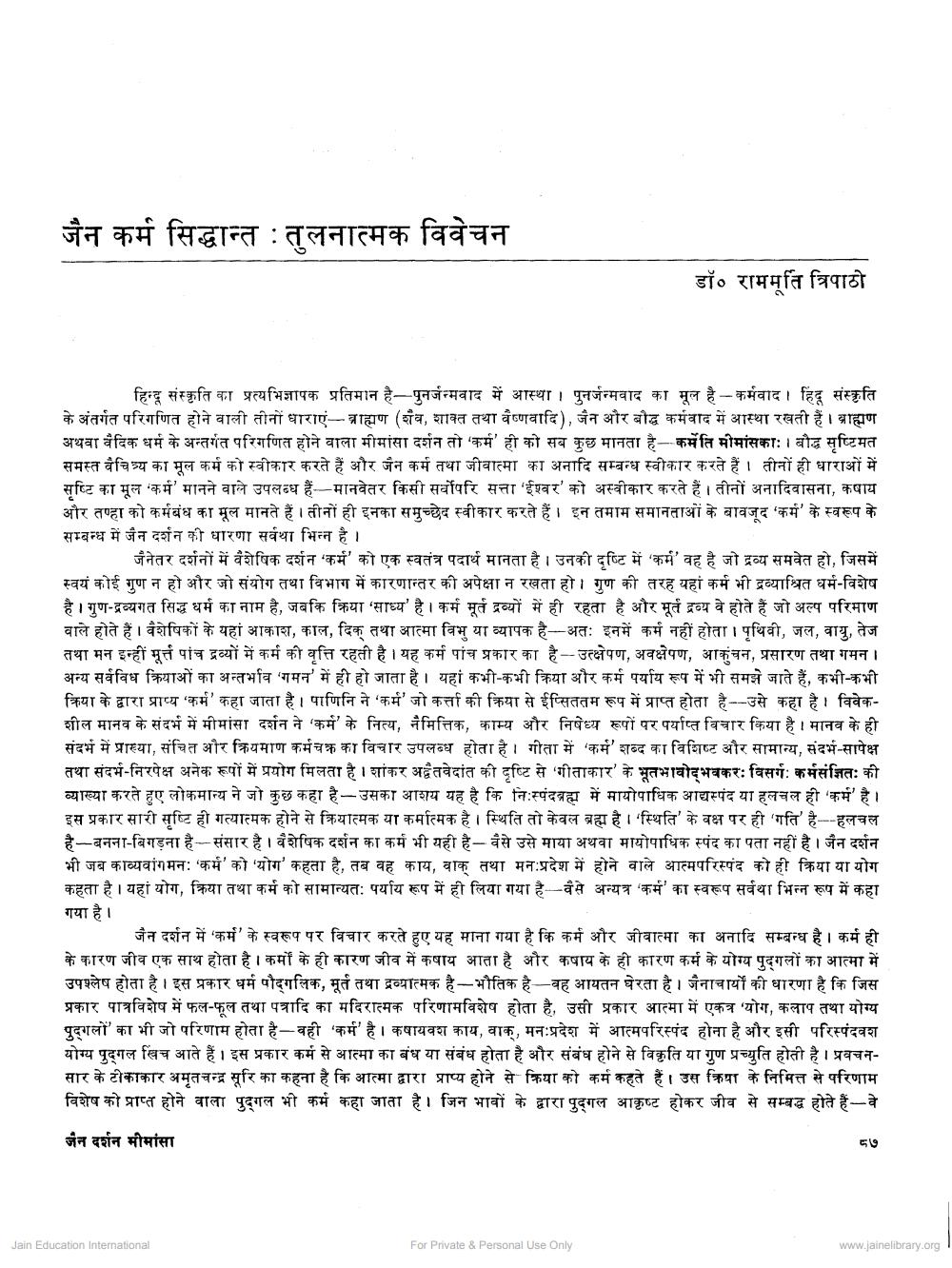________________
जैन कर्म सिद्धान्त : तुलनात्मक विवेचन
डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी
हिन्दू संस्कृति का प्रत्यभिज्ञापक प्रतिमान है-पुनर्जन्मवाद में आस्था। पुनर्जन्मवाद का मूल है- कर्मवाद। हिंदू संस्कृति के अंतर्गत परिगणित होने वाली तीनों धाराएं-ब्राह्मण (शैव, शाक्त तथा वैष्णवादि), जैन और बौद्ध कर्मवाद में आस्था रखती हैं। ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म के अन्तर्गत परिगणित होने वाला मीमांसा दर्शन तो 'कर्म' ही को सब कुछ मानता है-कर्मेति मीमांसकाः । बौद्ध सृष्टिमत समस्त वैचित्र्य का मूल कर्म को स्वीकार करते हैं और जैन कर्म तथा जीवात्मा का अनादि सम्बन्ध स्वीकार करते हैं। तीनों ही धाराओं में सष्टि का मूल 'कर्म' मानने वाले उपलब्ध हैं-मानवेतर किसी सर्वोपरि सत्ता 'ईश्वर' को अस्वीकार करते हैं। तीनों अनादिवासना, कषाय और तण्हा को कर्मबंध का मूल मानते हैं । तीनों ही इनका समुच्छेद स्वीकार करते हैं। इन तमाम समानताओं के बावजूद 'कर्म' के स्वरूप के सम्बन्ध में जैन दर्शन की धारणा सर्वथा भिन्न है।
जैनेतर दर्शनों में वैशेषिक दर्शन 'कर्म' को एक स्वतंत्र पदार्थ मानता है। उनकी दृष्टि में 'कर्म' वह है जो द्रव्य समवेत हो, जिसमें स्वयं कोई गुण न हो और जो संयोग तथा विभाग में कारणान्तर की अपेक्षा न रखता हो। गुण की तरह यहां कर्म भी द्रव्याश्रित धर्म-विशेष है। गुण-द्रव्यगत सिद्ध धर्म का नाम है, जबकि क्रिया 'साध्य' है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही रहता है और मूर्त द्रव्य वे होते हैं जो अल्प परिमाण वाले होते हैं । वैशेषिकों के यहां आकाश, काल, दिक् तथा आत्मा विभु या व्यापक है-अतः इनमें कर्म नहीं होता। पृथिवी, जल, वायु, तेज तथा मन इन्हीं मूर्त पांच द्रव्यों में कर्म की वृत्ति रहती है। यह कर्म पांच प्रकार का है-- उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। अन्य सर्वविध क्रियाओं का अन्तर्भाव ‘गमन' में ही हो जाता है। यहां कभी-कभी क्रिया और कर्म पर्याय रूप में भी समझे जाते हैं, कभी-कभी क्रिया के द्वारा प्राप्य 'कर्म' कहा जाता है। पाणिनि ने 'कर्म' जो कर्त्ता की क्रिया से ईप्सिततम रूप में प्राप्त होता है--उसे कहा है। विवेकशील मानव के संदर्भ में मीमांसा दर्शन ने 'कर्म के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषेध्य रूपों पर पर्याप्त विचार किया है। मानव के ही संदर्भ में प्राख्या, संचित और क्रियमाण कर्मचक्र का विचार उपलब्ध होता है। गीता में 'कर्म' शब्द का विशिष्ट और सामान्य, संदर्भ-सापेक्ष तथा संदर्भ-निरपेक्ष अनेक रूपों में प्रयोग मिलता है । शांकर अद्वैतवेदांत की दृष्टि से 'गीताकार' के भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंजितः की व्याख्या करते हुए लोकमान्य ने जो कुछ कहा है-उसका आशय यह है कि निःस्पंदब्रह्म में मायोपाधिक आद्यस्पंद या हलचल ही 'कर्म' है। इस प्रकार सारी सृष्टि ही गत्यात्मक होने से क्रियात्मक या कर्मात्मक है। स्थिति तो केवल ब्रह्म है । 'स्थिति' के वक्ष पर ही 'गति' है--हलचल है-बनना-बिगड़ना है-संसार है । वैशेषिक दर्शन का कर्म भी यही है- वैसे उसे माया अथवा मायोपाधिक स्पंद का पता नहीं है। जैन दर्शन भी जब काव्यवांगमन: 'कर्म' को 'योग' कहता है, तब वह काय, वाक् तथा मनःप्रदेश में होने वाले आत्मपरिस्पंद को ही क्रिया या योग कहता है । यहां योग, क्रिया तथा कर्म को सामान्यत: पर्याय रूप में ही लिया गया है-वैसे अन्यत्र 'कर्म' का स्वरूप सर्वथा भिन्न रूप में कहा गया है।
जैन दर्शन में 'कर्म' के स्वरूप पर विचार करते हुए यह माना गया है कि कर्म और जीवात्मा का अनादि सम्बन्ध है। कर्म ही के कारण जीव एक साथ होता है । कर्मों के ही कारण जीव में कषाय आता है और कषाय के ही कारण कर्म के योग्य पुद्गलों का आत्मा में उपश्लेष होता है । इस प्रकार धर्म पौद्गलिक, मूर्त तथा द्रव्यात्मक है-भौतिक है-बह आयतन घेरता है। जैनाचार्यों की धारणा है कि जिस प्रकार पात्रविशेष में फल-फूल तथा पत्रादि का मदिरात्मक परिणामविशेष होता है, उसी प्रकार आत्मा में एकत्र 'योग, कलाप तथा योग्य पुद्गलों' का भी जो परिणाम होता है-वही 'कर्म' है । कषायवश काय, वाक्, मनःप्रदेश में आत्मपरिस्पंद होना है और इसी परिस्पंदवश योग्य पुद्गल खिच आते हैं। इस प्रकार कर्म से आत्मा का बंध या संबंध होता है और संबंध होने से विकृति या गुण प्रच्युति होती है। प्रवचनसार के टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि का कहना है कि आत्मा द्वारा प्राप्य होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। उस क्रिया के निमित्त से परिणाम विशेष को प्राप्त होने वाला पुद्गल भी कर्म कहा जाता है। जिन भावों के द्वारा पुद्गल आकृष्ट होकर जीव से सम्बद्ध होते हैं-वे जैन दर्शन मीमांसा
८७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org |