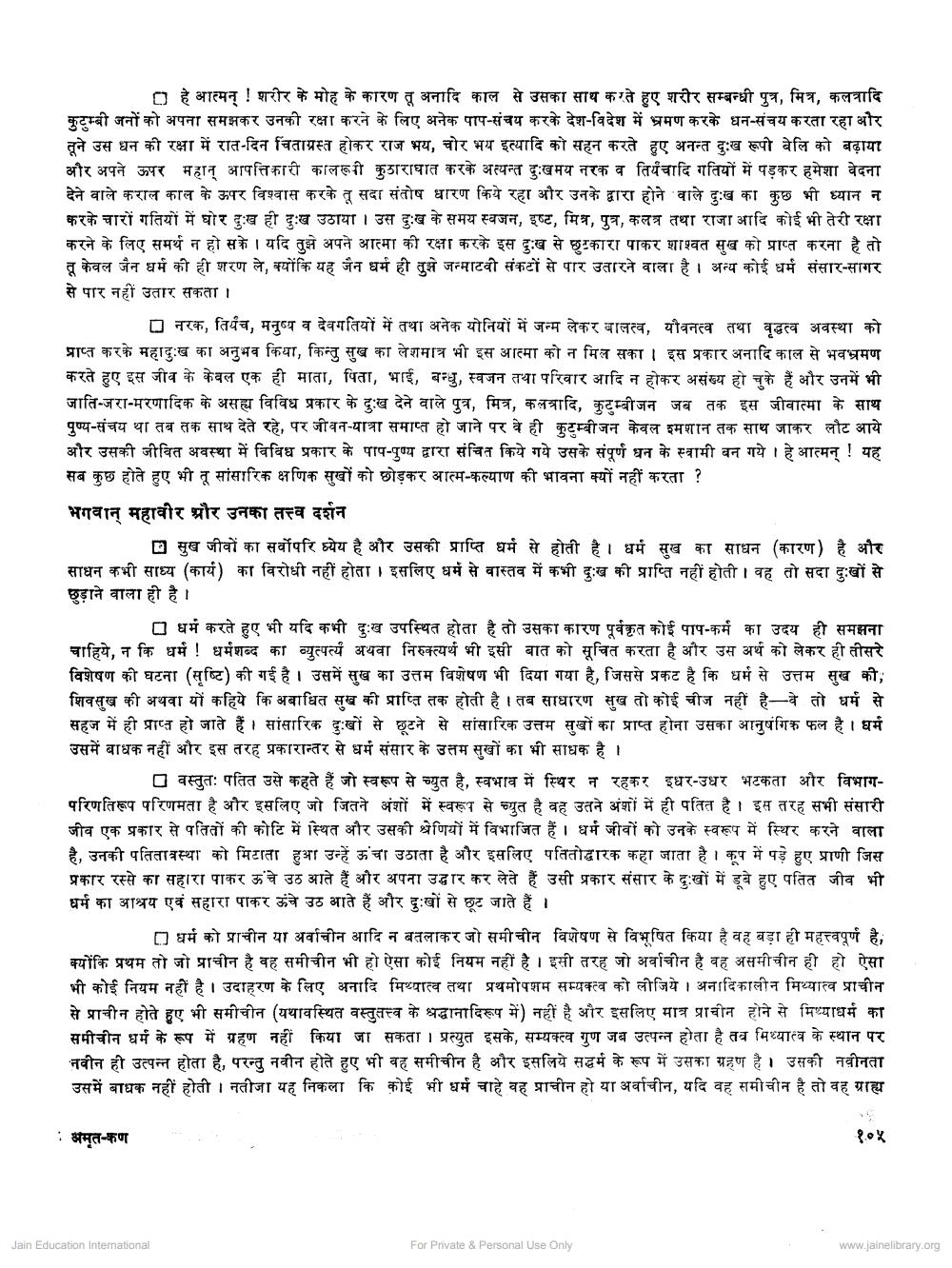________________
[C] हे आत्मन् ! शरीर के मोह के कारण तू अनादि काल से उसका साथ करते हुए शरीर सम्बन्धी पुत्र, मित्र, कलत्रादि कुटुम्बी जनों को अपना समझकर उनकी रक्षा करने के लिए अनेक पाप-संचय करके देश-विदेश में भ्रमण करके धन संचय करता रहा और तूने उस धन की रक्षा में रात-दिन चिंताग्रस्त होकर राज भय, चोर भय इत्यादि को सहन करते हुए अनन्त दुःख रूपी बेलि को बढ़ाया और अपने ऊपर महान् आपत्तिकारी कालरूपी कुठाराघात करके अत्यन्त दुःखमय नरक व तिर्यंचादि गतियों में पड़कर हमेशा वेदना देने वाले कराल काल के ऊपर विश्वास करके तू सदा संतोष धारण किये रहा और उनके द्वारा होने वाले दुःख का कुछ भी ध्यान न करके चारों गतियों में घोर दुःख ही दुःख उठाया । उस दुःख के समय स्वजन, इष्ट, मित्र, पुत्र, कलत्र तथा राजा आदि कोई भी तेरी रक्षा करने के लिए समर्थ न हो सके । यदि तुझे अपने आत्मा की रक्षा करके इस दुःख से छुटकारा पाकर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो तू केवल जैन धर्म की ही शरण ले, क्योंकि यह जैन धर्म ही तुझे जन्माटवी संकटों से पार उतारने वाला है । अन्य कोई धर्म संसार-सागर से पार नहीं उतार सकता ।
नरक, तिथंच मनुष्य व देवगतियों में तथा अनेक योनियों में जन्म लेकर बालत्व, यौवनत्व तथा वृद्धत्व अवस्था को प्राप्त करके महादुःख का अनुभव किया, किन्तु सुख का लेशमात्र भी इस आत्मा को न मिल सका । इस प्रकार अनादि काल से भवभ्रमण करते हुए इस जीव के केवल एक ही माता, पिता, भाई, बन्धु, स्वजन तथा परिवार आदि न होकर असंख्य हो चुके हैं और उनमें भी जाति जरामरणादिक के असह्य विविध प्रकार के दुःख देने वाले पुत्र, मित्र, कलत्रादि, कुटुम्बीजन जब तक इस जीवात्मा के साथ पुण्य-संचय था तब तक साथ देते रहे, पर जीवन-यात्रा समाप्त हो जाने पर वे ही कुटुम्बीजन केवल श्मशान तक साथ जाकर लौट आये और उसकी जीवित अवस्था में विविध प्रकार के पाप-पुण्य द्वारा संचित किये गये उसके संपूर्ण धन के स्वामी बन गये । हे आत्मन् ! यह सब कुछ होते हुए भी तू सांसारिक क्षणिक सुखों को छोड़कर आत्म-कल्याण की भावना क्यों नहीं करता ?
भगवान् महावीर और उनका तत्त्व दर्शन
सुख जीवों का सर्वोपरि ध्येय है और उसकी प्राप्ति धर्म से होती है धर्म सुख का साधन (कारण) है और साधन कभी साध्य ( कार्य ) का विरोधी नहीं होता। इसलिए धर्म से वास्तव में कभी दुःख की प्राप्ति नहीं होती । वह तो सदा दुःखों से छुड़ाने वाला ही है ।
धर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो उसका कारण पूर्वकृत कोई पाप कर्म का उदय ही समझना चाहिये, न कि धर्म धर्मशब्द का व्युत्पत्यें अथवा निरुक्त्यर्थ भी इसी बात को सूचित करता है और उस अर्थ को लेकर ही तीसरे विशेषण को घटना (सृष्टि) की गई है। उसमें सुख का उत्तम विशेषण भी दिया गया है, जिससे प्रकट है कि धर्म से उत्तम सुख की शिवसुख की अथवा यों कहिये कि अबाधित सुख की प्राप्ति तक होती है । तब साधारण सुख तो कोई चीज नहीं है— वे तो धर्म से सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक दुःखों से छूटने से सांसारिक उत्तम सुखों का प्राप्त होना उसका आनुषंगिक फल है । धर्म उसमें बाधक नहीं और इस तरह प्रकारान्तर से धर्म संसार के उत्तम सुखों का भी साधक है ।
वस्तुतः पतित उसे कहते हैं जो स्वरूप से च्युत है, स्वभाव में स्थिर न रहकर इधर-उधर भटकता और विभागपरिणतिरूप परिणमता है और इसलिए जो जितने अंशों में स्वरूप से च्युत है वह उतने अंशों में ही पतित है । इस तरह सभी संसारी जीव एक प्रकार से पतितों की कोटि में स्थित और उसकी श्रेणियों में विभाजित हैं । धर्म जीवों को उनके स्वरूप में स्थिर करने वाला है, उनकी पतितावस्था को मिटाता हुआ उन्हें ऊंचा उठाता है और इसलिए पतितोद्धारक कहा जाता है । कूप में पड़े हुए प्राणी जिस प्रकार रस्से का सहारा पाकर ऊंचे उठ आते हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं उसी प्रकार संसार के दुःखों में डूबे हुए पतित जीव भी धर्म का आश्रय एवं सहारा पाकर ऊंचे उठ आते हैं और दुःखों से छूट जाते हैं ।
[] धर्म को प्राचीन या अर्वाचीन आदि न बतलाकर जो समीचीन विशेषण से विभूषित किया है वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम तो जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी तरह जो अर्वाचीन है वह असमीचीन ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। उदाहरण के लिए अनादि मिध्यात्व तथा प्रथमोपशम सम्यक्त्व को लीजिये। अनादिकालीन मिध्यात्व प्राचीन से प्राचीन होते हुए भी समीचीन ( यथावस्थित वस्तुतत्त्व के श्रद्धानादिरूप में) नहीं है और इसलिए मात्र प्राचीन होने से मिथ्याधर्म का समीचीन धर्म के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रत्युत इसके, सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता है तब मिथ्यात्व के स्थान पर नवीन ही उत्पन्न होता है, परन्तु नवीन होते हुए भी वह समीचीन है और इसलिये सद्धर्म के रूप में उसका ग्रहण है । उसकी नवीनता उसमें बाधक नहीं होती। नतीजा यह निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, यदि वह समीचीन है तो वह ग्राह्य
अमृत-कण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१.०५
www.jainelibrary.org