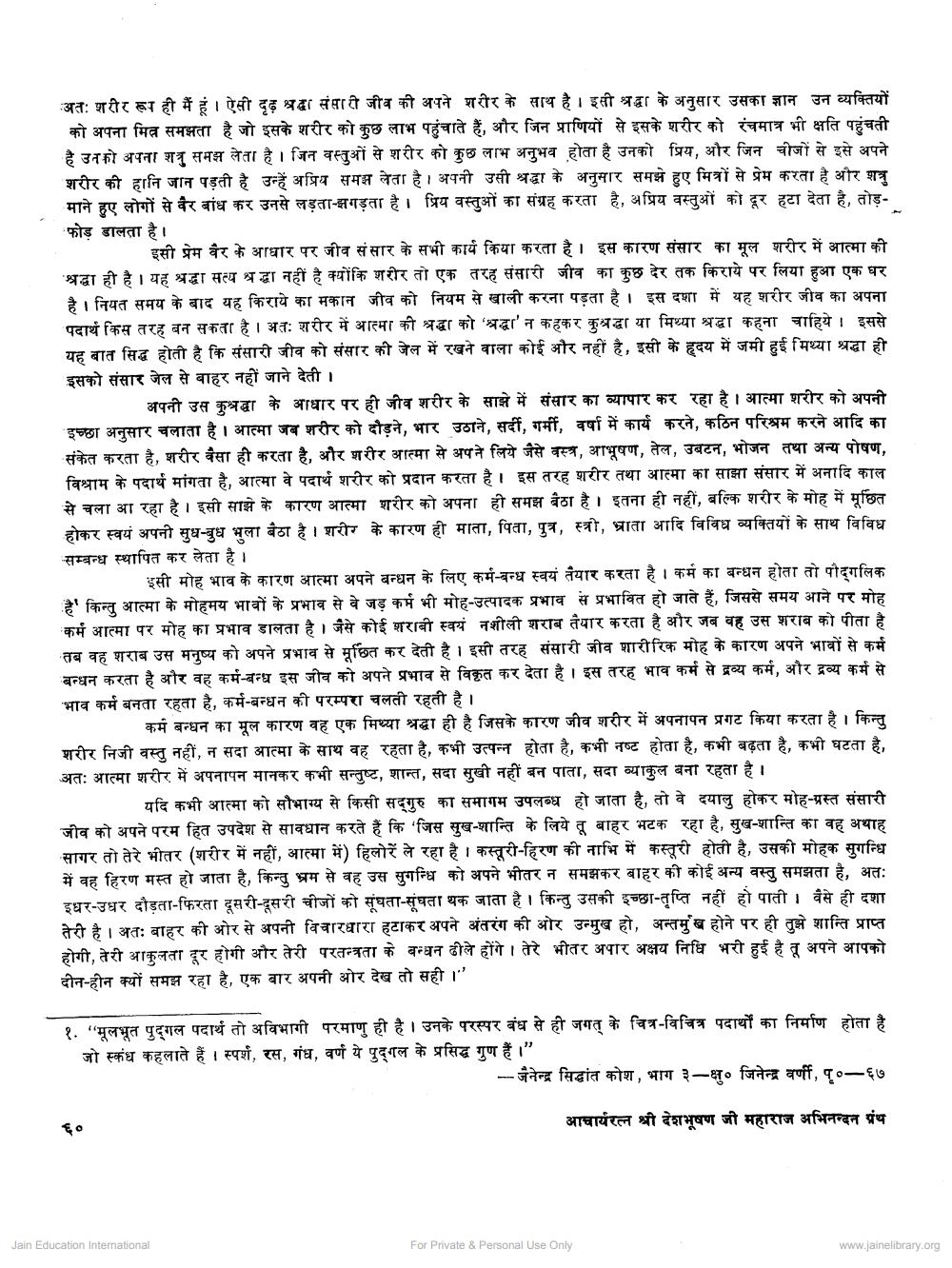________________
अत: शरीर रूप ही मैं हूं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा संसारी जीव की अपने शरीर के साथ है। इसी श्रद्धा के अनुसार उसका ज्ञान उन व्यक्तियों को अपना मित्र समझता है जो इसके शरीर को कुछ लाभ पहुंचाते हैं, और जिन प्राणियों से इसके शरीर को रंचमात्र भी क्षति पहुंचती है उनको अपना शत्रु समझ लेता है। जिन वस्तुओं से शरीर को कुछ लाभ अनुभव होता है उनको प्रिय, और जिन चीजों से इसे अपने शरीर की हानि जान पड़ती है उन्हें अप्रिय समझ लेता है। अपनी उसी श्रद्धा के अनुसार समझे हुए मित्रों से प्रेम करता है और शत्रु माने हुए लोगों से वैर बांध कर उनसे लड़ता-झगड़ता है। प्रिय वस्तुओं का संग्रह करता है, अप्रिय वस्तुओं को दूर हटा देता है, तोड़फोड़ डालता है।
इसी प्रेम वैर के आधार पर जीव संसार के सभी कार्य किया करता है। इस कारण संसार का मूल शरीर में आत्मा की श्रद्धा ही है। यह श्रद्धा सत्य श्रद्धा नहीं है क्योंकि शरीर तो एक तरह संसारी जीव का कुछ देर तक किराये पर लिया हुआ एक घर है। नियत समय के बाद यह किराये का मकान जीव को नियम से खाली करना पड़ता है। इस दशा में यह शरीर जीव का अपना पदार्थ किस तरह बन सकता है । अतः शरीर में आत्मा की श्रद्धा को 'श्रद्धा' न कहकर कुश्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा कहना चाहिये। इससे यह बात सिद्ध होती है कि संसारी जीव को संसार की जेल में रखने वाला कोई और नहीं है, इसी के हृदय में जमी हुई मिथ्या श्रद्धा ही इसको संसार जेल से बाहर नहीं जाने देती।
अपनी उस कुश्रद्धा के आधार पर ही जीव शरीर के साझे में संसार का व्यापार कर रहा है । आत्मा शरीर को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है । आत्मा जब शरीर को दौड़ने, भार उठाने, सर्दी, गर्मी, वर्षा में कार्य करने, कठिन परिश्रम करने आदि का संकेत करता है, शरीर वैसा ही करता है, और शरीर आत्मा से अपने लिये जैसे वस्त्र, आभूषण, तेल, उबटन, भोजन तथा अन्य पोषण, विश्राम के पदार्थ मांगता है, आत्मा वे पदार्थ शरीर को प्रदान करता है। इस तरह शरीर तथा आत्मा का साझा संसार में अनादि काल से चला आ रहा है। इसी साझे के कारण आत्मा शरीर को अपना ही समझ बैठा है। इतना ही नहीं, बल्कि शरीर के मोह में मूछित होकर स्वयं अपनी सुध-बुध भुला बैठा है। शरीर के कारण ही माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भ्राता आदि विविध व्यक्तियों के साथ विविध सम्बन्ध स्थापित कर लेता है।
इसी मोह भाव के कारण आत्मा अपने बन्धन के लिए कर्म-बन्ध स्वयं तैयार करता है । कर्म का बन्धन होता तो पौद्गलिक है किन्तु आत्मा के मोहमय भावों के प्रभाव से वे जड़ कर्म भी मोह-उत्पादक प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे समय आने पर मोह कर्म आत्मा पर मोह का प्रभाव डालता है। जैसे कोई शराबी स्वयं नशीली शराब तैयार करता है और जब वह उस शराब को पीता है तब वह शराब उस मनुष्य को अपने प्रभाव से मूछित कर देती है। इसी तरह संसारी जीव शारीरिक मोह के कारण अपने भावों से कर्म बन्धन करता है और वह कर्म-बन्ध इस जीव को अपने प्रभाव से विकृत कर देता है। इस तरह भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से 'भाव कर्म बनता रहता है, कर्म-बन्धन की परम्परा चलती रहती है।।
कर्म बन्धन का मूल कारण वह एक मिथ्या श्रद्धा ही है जिसके कारण जीव शरीर में अपनापन प्रगट किया करता है। किन्तु शरीर निजी वस्तु नहीं, न सदा आत्मा के साथ वह रहता है, कभी उत्पन्न होता है, कभी नष्ट होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, अतः आत्मा शरीर में अपनापन मानकर कभी सन्तुष्ट, शान्त, सदा सुखी नहीं बन पाता, सदा व्याकुल बना रहता है।
__ यदि कभी आत्मा को सौभाग्य से किसी सद्गुरु का समागम उपलब्ध हो जाता है, तो वे दयालु होकर मोह-ग्रस्त संसारी जीव को अपने परम हित उपदेश से सावधान करते हैं कि 'जिस सुख-शान्ति के लिये तू बाहर भटक रहा है, सुख-शान्ति का वह अथाह सागर तो तेरे भीतर (शरीर में नहीं, आत्मा में) हिलोरें ले रहा है । कस्तूरी-हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी मोहक सुगन्धि में वह हिरण मस्त हो जाता है, किन्तु भ्रम से वह उस सुगन्धि को अपने भीतर न समझकर बाहर की कोई अन्य वस्तु समझता है, अतः इधर-उधर दौड़ता-फिरता दूसरी-दूसरी चीजों को सूंघता-सूंघता थक जाता है। किन्तु उसकी इच्छा-तृप्ति नहीं हो पाती। वैसे ही दशा तेरी है । अतः बाहर की ओर से अपनी विचारधारा हटाकर अपने अंतरंग की ओर उन्मुख हो, अन्तर्मुख होने पर ही तुझे शान्ति प्राप्त होगी, तेरी आकुलता दूर होगी और तेरी परतन्त्रता के बन्धन ढीले होंगे। तेरे भीतर अपार अक्षय निधि भरी हुई है तू अपने आपको दीन-हीन क्यों समझ रहा है, एक बार अपनी ओर देख तो सही।"
१. "मूलभूत पुद्गल पदार्थ तो अविभागी परमाणु ही है। उनके परस्पर बंध से ही जगत् के चित्र-विचित्र पदार्थों का निर्माण होता है जो स्कंध कहलाते हैं । स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के प्रसिद्ध गुण हैं।"
__-जैनेन्द्र सिद्धांत कोश , भाग ३-क्षु० जिनेन्द्र वर्णी, पु०-६७
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रंथ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org