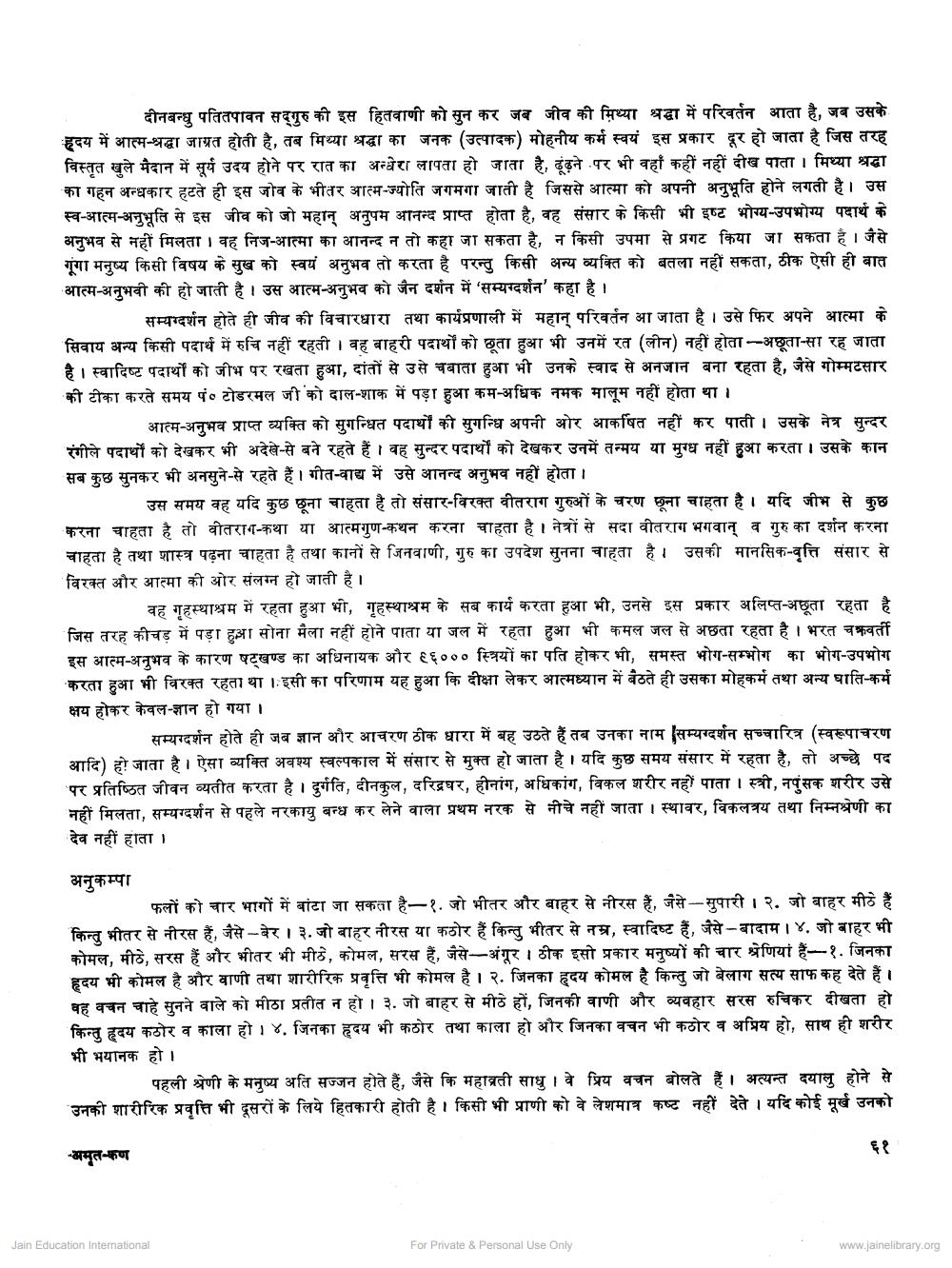________________
दीनबन्धु पतितपावन सद्गुरु की इस हितवाणी को सुन कर जब जीव की मिथ्या श्रद्धा में परिवर्तन आता है, जब उसके हृदय में आत्म-श्रद्धा जाग्रत होती है, तब मिथ्या श्रद्धा का जनक ( उत्पादक) मोहनीय कर्म स्वयं इस प्रकार दूर हो जाता है जिस तरह विस्तृत खुले मैदान में सूर्य उदय होने पर रात का अन्धेरा लापता हो जाता है, ढूंढ़ने पर भी वहाँ कहीं नहीं दीख पाता । मिथ्या श्रद्धा का गहन अन्धकार हटते ही इस जोव के भीतर आत्म-ज्योति जगमगा जाती है जिससे आत्मा को अपनी अनुभूति होने लगती है । उस स्व- आत्म अनुभूति से इस जीव को जो महान् अनुपम आनन्द प्राप्त होता है, वह संसार के किसी भी इष्ट भोग्य उपभोग्य पदार्थ के अनुभव से नहीं मिलता। वह निज आत्मा का आनन्द न तो कहा जा सकता है, न किसी उपमा से प्रगट किया जा सकता है। जैसे गूंगा मनुष्य किसी विषय के सुख को स्वयं अनुभव तो करता है परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को बतला नहीं सकता, ठीक ऐसी ही बात आत्म-अनुभवी की हो जाती है। उस आत्म अनुभव को जैन दर्शन में 'सम्यग्दर्शन' कहा है ।
सम्यग्दर्शन होते ही जीव की विचारधारा तथा कार्यप्रणाली में महान् परिवर्तन आ जाता है । उसे फिर अपने आत्मा के सिवाय अन्य किसी पदार्थ में रुचि नहीं रहती । वह बाहरी पदार्थों को छूता हुआ भी उनमें रत ( लीन) नहीं होता -- अछूता सा रह जाता है । स्वादिष्ट पदार्थों को जीभ पर रखता हुआ, दांतों से उसे चबाता हुआ भी उनके स्वाद से अनजान बना रहता है, जैसे गोम्मटसार की टीका करते समय पं० टोडरमल जी को दाल-शाक में पड़ा हुआ कम अधिक नमक मालूम नहीं होता था ।
आत्म-अनुभव प्राप्त व्यक्ति को सुगन्धित पदार्थों की सुगन्धि अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती । उसके नेत्र सुन्दर रंगीले पदार्थों को देखकर भी अदेखे-से बने रहते हैं। वह सुन्दर पदार्थों को देखकर उनमें तन्मय या मुग्ध नहीं हुआ करता । उसके कान सब कुछ सुनकर भी अनसुने -से रहते हैं । गीत वाद्य में उसे आनन्द अनुभव नहीं होता ।
उस समय वह यदि कुछ छूना चाहता है तो संसार- विरक्त वीतराग गुरुओं के चरण छूना चाहता है। यदि जीभ से कुछ करना चाहता है तो वीतराग-कथा या आत्मगुण-कथन करना चाहता है। नेत्रों से सदा वीतराग भगवान् व गुरु का दर्शन करना चाहता है तथा शास्त्र पढ़ना चाहता है तथा कानों से जिनवाणी, गुरु का उपदेश सुनना चाहता है । उसकी मानसिक वृत्ति संसार से विरक्त और आत्मा की ओर संलग्न हो जाती है ।
वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी गृहस्थाश्रम के सब कार्य करता हुआ भी उनसे इस प्रकार अलिप्त अछूता रहता है जिस तरह कीचड़ में पड़ा हुआ सोना मैला नहीं होने पाता या जल में रहता हुआ भी कमल जल से अछता रहता है। भरत चक्रवर्ती इस आत्म-अनुभव के कारण षट्खण्ड का अधिनायक और ६६००० स्त्रियों का पति होकर भी, समस्त भोग सम्भोग का भोग उपभोग करता हुआ भी विरक्त रहता था। इसी का परिणाम यह हुआ कि दीक्षा लेकर आत्मध्यान में बैठते ही उसका मोहकर्म तथा अन्य घाति-कर्म क्षय होकर केवल ज्ञान हो गया ।
सम्यग्दर्शन होते ही जब ज्ञान और आचरण ठीक धारा में बह उठते हैं तब उनका नाम सम्यग्दर्शन सच्चारित्र ( स्वरूपाचरण आदि) हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य स्वल्पकाल में संसार से मुक्त हो जाता है । यदि कुछ समय संसार में रहता है, तो अच्छे पद पर प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करता है । दुर्गति, दीनकुल, दरिद्रघर, हीनांग, अधिकांग, विकल शरीर नहीं पाता। स्त्री, नपुंसक शरीर उसे नहीं मिलता, सम्यग्दर्शन से पहले नरकायु बन्ध कर लेने वाला प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता। स्थावर, विकलत्रय तथा निम्नश्रेणी का देव नहीं होता ।
अनुकम्पा
फलों को चार भागों में बांटा जा सकता है - १. जो भीतर और बाहर से नीरस हैं, जैसे-सुपारी । २. जो बाहर मीठे हैं। भी किन्तु भीतर से नीरस हैं, जैसे- बेर । ३. जो बाहर नीरस या कठोर हैं किन्तु भीतर से नम्र, स्वादिष्ट हैं, जैसे- बादाम । ४. जो बाहर कोमल, मीठे, सरस हैं और भीतर भी मीठे, कोमल, सरस हैं, जैसे- अंगूर । ठीक इसी प्रकार मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं - १. जिनका हृदय भी कोमल है और वाणी तथा शारीरिक प्रवृति भी कोमल है। २. जिनका हृदय कोमल है किन्तु जो वेलाग सत्य साफ कह देते हैं। वह वचन चाहे सुनने वाले को मीठा प्रतीत न हो। ३. जो बाहर से मीठे हों, जिनकी वाणी और व्यवहार सरस रुचिकर दीखता हो किन्तु हृदय कठोर व काला हो । ४. जिनका हृदय भी कठोर तथा काला हो और जिनका वचन भी कठोर व अप्रिय हो, साथ ही शरीर भी भयानक हो ।
पहली श्रेणी के मनुष्य अति सज्जन होते हैं, जैसे कि महाव्रती साधु । वे प्रिय वचन बोलते हैं । अत्यन्त दयालु होने से उनकी शारीरिक प्रवृत्ति भी दूसरों के लिये हितकारी होती है। किसी भी प्राणी को वे लेशमात्र कष्ट नहीं देते। यदि कोई मूर्ख उनको
६१
अमृत-कण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org