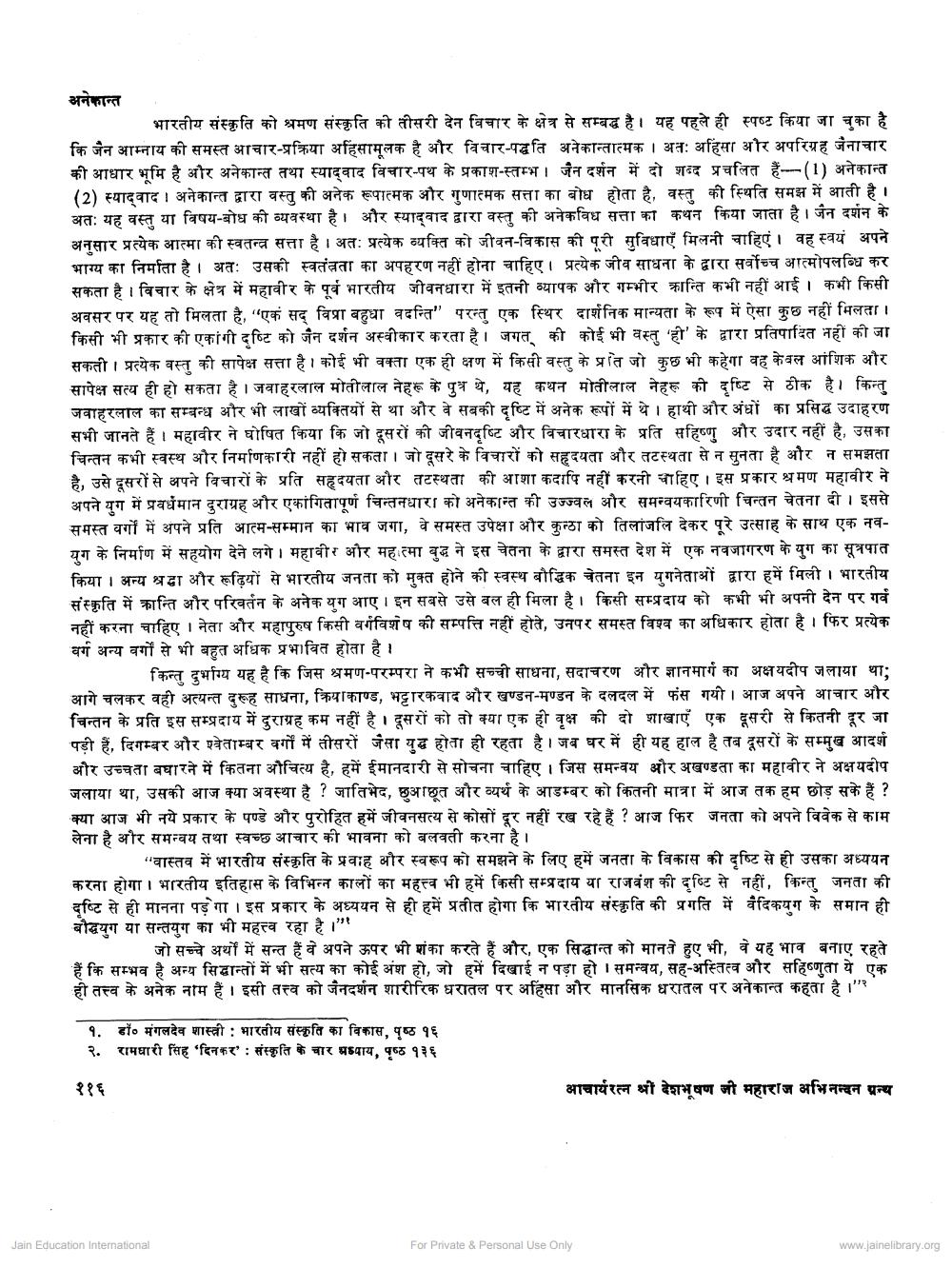________________
भा
अनेकान्त
भारतीय संस्कृति को श्रमण संस्कृति को तीसरी देन विचार के क्षेत्र से सम्बद्ध है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जैन आम्नाय की समस्त आचार-प्रक्रिया अहिंसामूलक है और विचार-पद्धति अनेकान्तात्मक । अतः अहिंसा और अपरिग्रह जैनाचार की आधार भूमि है और अनेकान्त तथा स्याद्वाद विचार-पथ के प्रकाश-स्तम्भ। जैन दर्शन में दो शब्द प्रचलित हैं--(1) अनेकान्त (2) स्याद्वाद । अनेकान्त द्वारा वस्तु की अनेक रूपात्मक और गुणात्मक सत्ता का बोध होता है, वस्तु की स्थिति समझ में आती है। अतः यह वस्तु या विषय-बोध की व्यवस्था है। और स्याद्वाद द्वारा वस्तु की अनेकविध सत्ता का कथन किया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-विकास की पूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिएं। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अतः उसकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव साधना के द्वारा सर्वोच्च आत्मोपलब्धि कर सकता है । विचार के क्षेत्र में महावीर के पूर्व भारतीय जीवनधारा में इतनी व्यापक और गम्भीर क्रान्ति कभी नहीं आई। कभी किसी अवसर पर यह तो मिलता है, “एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" परन्तु एक स्थिर दार्शनिक मान्यता के रूप में ऐसा कुछ नहीं मिलता। किसी भी प्रकार की एकांगी दृष्टि को जैन दर्शन अस्वीकार करता है। जगत की कोई भी वस्तु 'ही' के द्वारा प्रतिपादित नहीं की जा सकती। प्रत्येक वस्तु की सापेक्ष सत्ता है। कोई भी वक्ता एक ही क्षण में किसी वस्तु के प्रति जो कुछ भी कहेगा वह केवल आंशिक और सापेक्ष सत्य ही हो सकता है । जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, यह कथन मोतीलाल नेहरू की दृष्टि से ठीक है। किन्तु जवाहरलाल का सम्बन्ध और भी लाखों व्यक्तियों से था और वे सबकी दृष्टि में अनेक रूपों में थे। हाथी और अंधों का प्रसिद्ध उदाहरण सभी जानते हैं। महावीर ने घोषित किया कि जो दूसरों की जीवनदृष्टि और विचारधारा के प्रति सहिष्णु और उदार नहीं है, उसका चिन्तन कभी स्वस्थ और निर्माणकारी नहीं हो सकता। जो दूसरे के विचारों को सहृदयता और तटस्थता से न सुनता है और न समझता है, उसे दूसरों से अपने विचारों के प्रति सहृदयता और तटस्थता की आशा कदापि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्रमण महावीर ने अपने युग में प्रवर्धमान दुराग्रह और एकांगितापूर्ण चिन्तनधारा को अनेकान्त की उज्ज्वल और समन्वयकारिणी चिन्तन चेतना दी। इससे समस्त वर्गों में अपने प्रति आत्म-सम्मान का भाव जगा, वे समस्त उपेक्षा और कुन्ठा को तिलांजलि देकर पूरे उत्साह के साथ एक नवयुग के निर्माण में सहयोग देने लगे। महावीर और मह त्मा बुद्ध ने इस चेतना के द्वारा समस्त देश में एक नवजागरण के युग का सूत्रपात किया। अन्य श्रद्धा और रूढ़ियों से भारतीय जनता को मुक्त होने की स्वस्थ बौद्धिक चेतना इन युगनेताओं द्वारा हमें मिली । भारतीय संस्कृति में क्रान्ति और परिवर्तन के अनेक युग आए। इन सबसे उसे बल ही मिला है। किसी सम्प्रदाय को कभी भी अपनी देन पर गर्व नहीं करना चाहिए । नेता और महापुरुष किसी वर्गविशेष की सम्पत्ति नहीं होते, उनपर समस्त विश्व का अधिकार होता है। फिर प्रत्येक वर्ग अन्य वर्गों से भी बहुत अधिक प्रभावित होता है।
किन्तु दुर्भाग्य यह है कि जिस श्रमण-परम्परा ने कभी सच्ची साधना, सदाचरण और ज्ञानमार्ग का अक्षयदीप जलाया था; आगे चलकर वही अत्यन्त दुरूह साधना, क्रियाकाण्ड, भट्टारकवाद और खण्डन-मण्डन के दलदल में फंस गयी। आज अपने आचार और चिन्तन के प्रति इस सम्प्रदाय में दुराग्रह कम नहीं है । दूसरों को तो क्या एक ही वृक्ष की दो शाखाएँ एक दूसरी से कितनी दूर जा पड़ी हैं, दिगम्बर और श्वेताम्बर वर्गों में तीसरों जैसा युद्ध होता ही रहता है। जब घर में ही यह हाल है तब दूसरों के सम्मुख आदर्श
और उच्चता बघारने में कितना औचित्य है, हमें ईमानदारी से सोचना चाहिए। जिस समन्वय और अखण्डता का महावीर ने अक्षयदीप जलाया था, उसकी आज क्या अवस्था है ? जातिभेद, छुआछूत और व्यर्थ के आडम्बर को कितनी मात्रा में आज तक हम छोड़ सके हैं ? क्या आज भी नये प्रकार के पण्डे और पुरोहित हमें जीवनसत्य से कोसों दूर नहीं रख रहे हैं ? आज फिर जनता को अपने विवेक से काम लेना है और समन्वय तथा स्वच्छ आचार की भावना को बलवती करना है।
"वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवाह और स्वरूप को समझने के लिए हमें जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका अध्ययन करना होगा। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्त्व भी हमें किसी सम्प्रदाय या राजवंश की दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार के अध्ययन से ही हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति में वैदिकयुग के समान ही बौद्धयुग या सन्तयुग का भी महत्त्व रहा है।"
जो सच्चे अर्थों में सन्त हैं वे अपने ऊपर भी शंका करते हैं और, एक सिद्धान्त को मानते हुए भी, वे यह भाव बनाए रहते हैं कि सम्भव है अन्य सिद्धान्तों में भी सत्य का कोई अंश हो, जो हमें दिखाई न पड़ा हो । समन्वय, सह-अस्तित्व और सहिष्णुता ये एक ही तत्त्व के अनेक नाम हैं। इसी तत्त्व को जैनदर्शन शारीरिक धरातल पर अहिंसा और मानसिक धरातल पर अनेकान्त कहता है।"
१. डॉ० मंगलदेव शास्त्री : भारतीय संस्कृति का विकास, पृष्ठ १६ २. रामधारी सिंह 'दिनकर' : संस्कृति के चार प्रध्याय, पृष्ठ १३६
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन अन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org