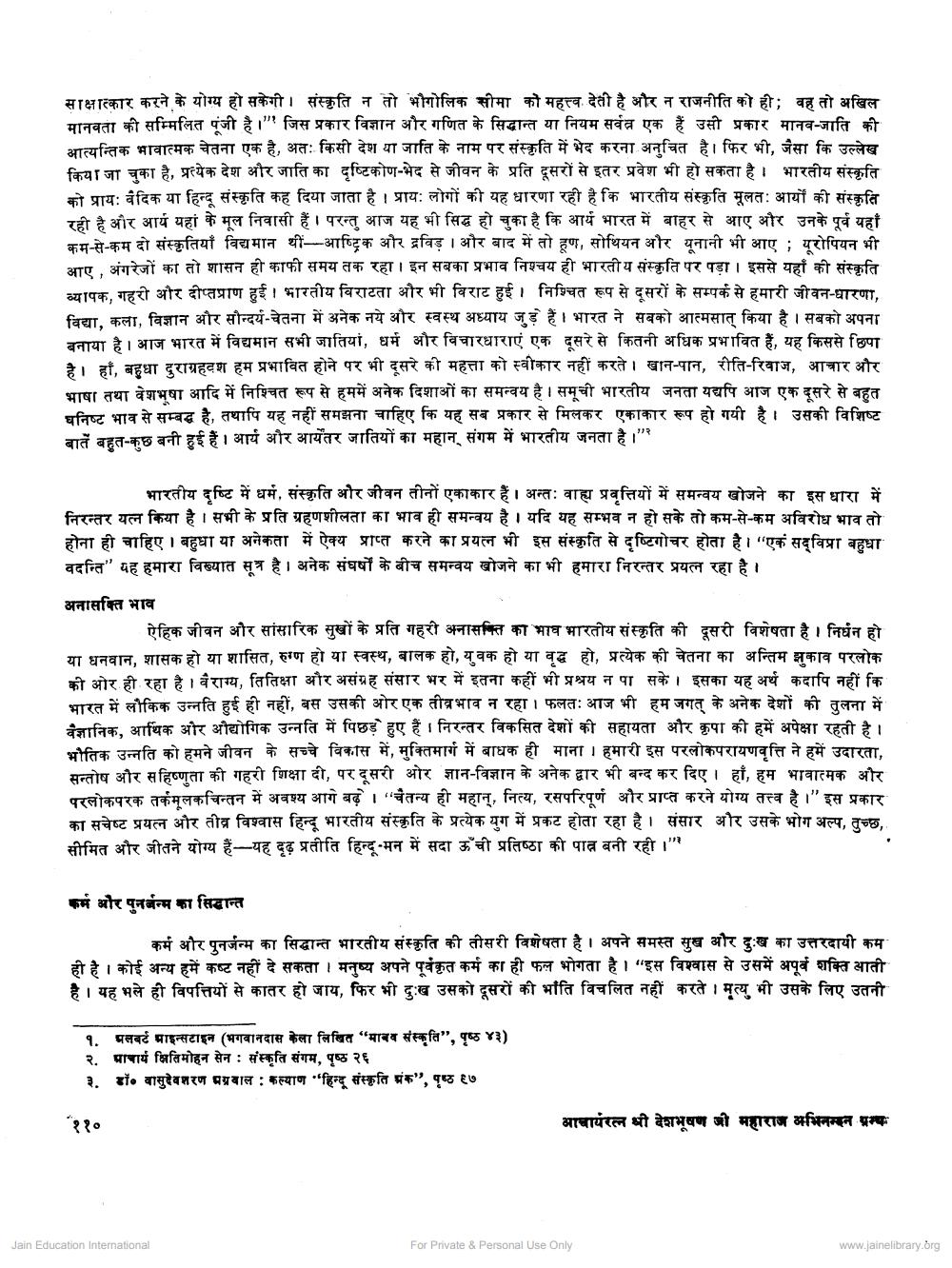________________
साक्षात्कार करने के योग्य हो सकेगी। संस्कृति न तो भौगोलिक सीमा को महत्त्व देती है और न राजनीति को ही; वह तो अखिल मानवता की सम्मिलित पूंजी है। जिस प्रकार विज्ञान और गणित के सिद्धान्त या नियम सर्वत्र एक हैं उसी प्रकार मानव-जाति की आत्यन्तिक भावात्मक चेतना एक है, अतः किसी देश या जाति के नाम पर संस्कृति में भेद करना अनुचित है। फिर भी, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, प्रत्येक देश और जाति का दृष्टिकोण-भेद से जीवन के प्रति दूसरों से इतर प्रवेश भी हो सकता है। भारतीय संस्कृति को प्रायः वैदिक या हिन्दू संस्कृति कह दिया जाता है । प्रायः लोगों की यह धारणा रही है कि भारतीय संस्कृति मूलतः आर्यों की संस्कृति रही है और आर्य यहां के मूल निवासी हैं । परन्तु आज यह भी सिद्ध हो चुका है कि आर्य भारत में बाहर से आए और उनके पूर्व यहाँ कम-से-कम दो संस्कृतियाँ विद्यमान थीं-आष्ट्रिक और द्रविड़ । और बाद में तो हूण, सोथियन और यूनानी भी आए ; यूरोपियन भी आप अंगरेजों का तो शासन ही काफी समय तक रहा। इन सबका प्रभाव निश्चय ही भारतीय संस्कृति पर पड़ा। इससे यहाँ की संस्कृति व्यापक, गहरी और दीप्तप्राण हुई। भारतीय विराटता और भी विराट हुई। निश्चित रूप से दूसरों के सम्पर्क से हमारी जीवन-धारणा, विद्या. कला, विज्ञान और सौन्दर्य-चेतना में अनेक नये और स्वस्थ अध्याय जुड़े हैं। भारत ने सबको आत्मसात् किया है । सबको अपना बनाया है। आज भारत में विद्यमान सभी जातियां, धर्म और विचारधाराएं एक दूसरे से कितनी अधिक प्रभावित हैं, यह किससे छिपा है। हाँ, बहुधा दुराग्रहदश हम प्रभावित होने पर भी दूसरे की महत्ता को स्वीकार नहीं करते। खान-पान, रीति-रिवाज, आचार और भाषा तथा वेशभूषा आदि में निश्चित रूप से हममें अनेक दिशाओं का समन्वय है। समूची भारतीय जनता यद्यपि आज एक दुसरे से बहत घनिष्ट भाव से सम्बद्ध है, तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि यह सब प्रकार से मिलकर एकाकार रूप हो गयी है। उसकी विशिष्ट बातें बहत-कुछ बनी हुई हैं। आर्य और आर्येतर जातियों का महान संगम में भारतीय जनता है।"
भारतीय दृष्टि में धर्म, संस्कृति और जीवन तीनों एकाकार हैं । अन्तः वाह्य प्रवृत्तियों में समन्वय खोजने का इस धारा में निरन्तर यत्न किया है । सभी के प्रति ग्रहणशीलता का भाव ही समन्वय है । यदि यह सम्भव न हो सके तो कम-से-कम अविरोध भाव तो होना ही चाहिए। बहुधा या अनेकता में ऐक्य प्राप्त करने का प्रयत्न भी इस संस्कृति से दृष्टिगोचर होता है। "एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" यह हमारा विख्यात सूत्र है। अनेक संघर्षों के बीच समन्वय खोजने का भी हमारा निरन्तर प्रयत्न रहा है। अनासक्ति भाव
ऐहिक जीवन और सांसारिक सुखों के प्रति गहरी अनासक्ति का भाव भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है । निर्धन हो या धनवान, शासक हो या शासित, रुग्ण हो या स्वस्थ, बालक हो, युवक हो या वृद्ध हो, प्रत्येक की चेतना का अन्तिम झुकाव परलोक की ओर ही रहा है। वैराग्य, तितिक्षा और असंग्रह संसार भर में इतना कहीं भी प्रश्रय न पा सके। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि भारत में लौकिक उन्नति हुई ही नहीं, बस उसकी ओर एक तीव्र भाव न रहा। फलतः आज भी हम जगत् के अनेक देशों की तुलना में वैज्ञानिक, आर्थिक और औद्योगिक उन्नति में पिछड़े हुए हैं । निरन्तर विकसित देशों की सहायता और कृपा की हमें अपेक्षा रहती है। भौतिक उन्नति को हमने जीवन के सच्चे विकास में, मुक्तिमार्ग में बाधक ही माना । हमारी इस परलोकपरायणवृत्ति ने हमें उदारता, सन्तोष और सहिष्णता की गहरी शिक्षा दी, पर दूसरी ओर ज्ञान-विज्ञान के अनेक द्वार भी बन्द कर दिए। हाँ, हम भावात्मक और परलोकपरक तर्कमूलकचिन्तन में अवश्य आगे बढ़ । "चैतन्य ही महान्, नित्य, रसपरिपूर्ण और प्राप्त करने योग्य तत्त्व है।" इस प्रकार का सचेष्ट प्रयत्न और तीव्र विश्वास हिन्दू भारतीय संस्कृति के प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा है। संसार और उसके भोग अल्प, तुच्छ, सीमित और जीतने योग्य हैं-यह दृढ़ प्रतीति हिन्दू-मन में सदा ऊँची प्रतिष्ठा की पात्र बनी रही।"
कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त
कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है। अपने समस्त सुख और दुःख का उत्तरदायी कम ही है । कोई अन्य हमें कष्ट नहीं दे सकता । मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्म का ही फल भोगता है। "इस विश्वास से उसमें अपूर्व शक्ति आती है। यह भले ही विपत्तियों से कातर हो जाय, फिर भी दुःख उसको दूसरों की भांति विचलित नहीं करते । मृत्यु भी उसके लिए उतनी
१. अलबर्ट माइन्सटाइन (भगवानदास केला लिखित “मानव संस्कृति", पृष्ठ ४३) २. प्राचार्य क्षितिमोहन सेन : संस्कृति संगम, पृष्ठ २६ ३. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल : कल्याण "हिन्दू संस्कृति अंक", पृष्ठ १७
आचार्यरत्न श्री वेशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org