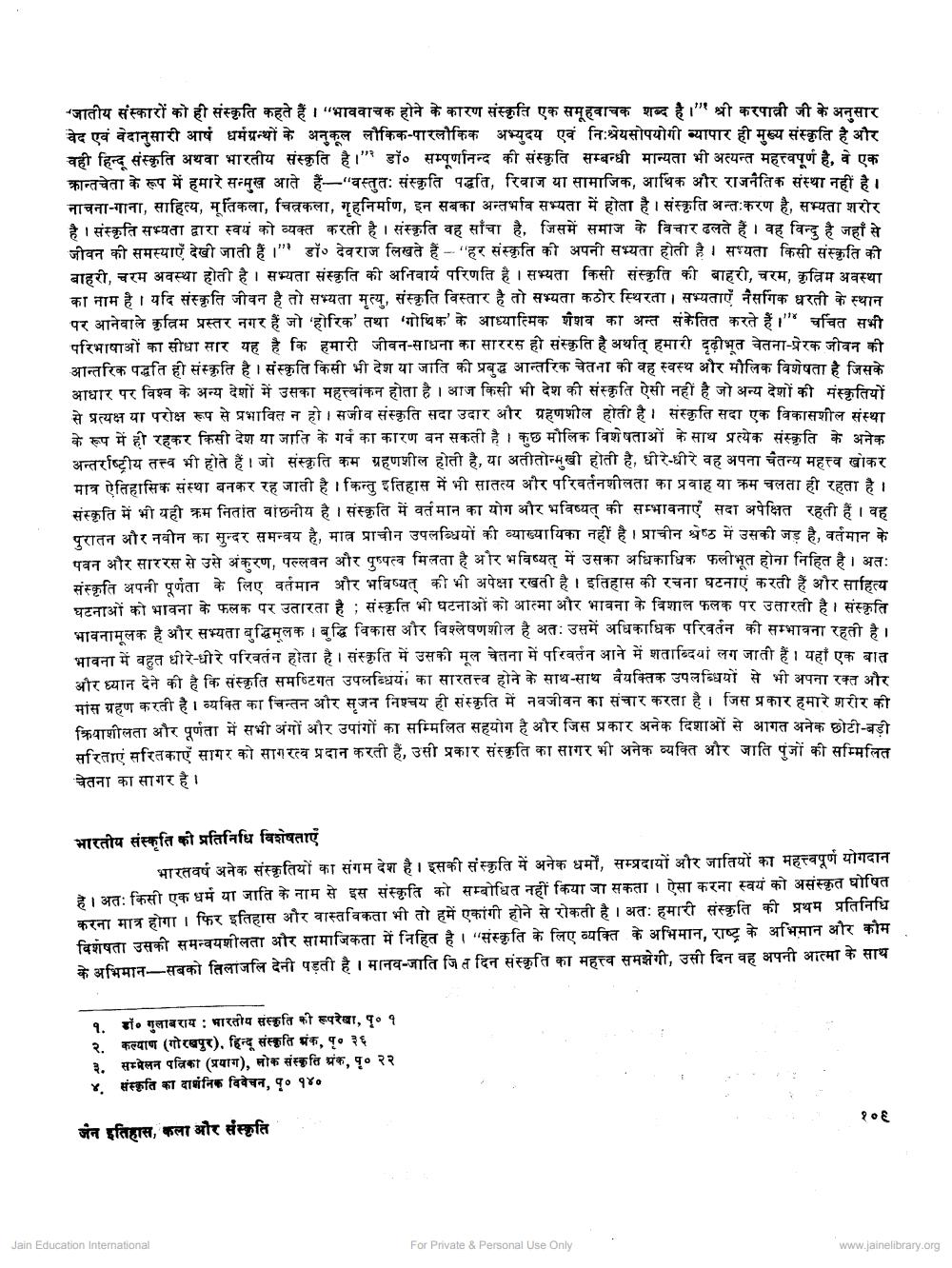________________
११
"जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। "भाववाचक होने के कारण संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। श्री करपात्री जी के अनुसार वेद एवं वेदानुसारी आर्य धर्मग्रन्थों के अनुकूल लौकिक-पारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुख्य संस्कृति है और वही हिन्दू संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति है।"" डॉ० सम्पूर्णानन्द की संस्कृति सम्बन्धी मान्यता भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वे एक क्रान्तचेता के रूप में हमारे सन्मुख आते हैं- “वस्तुतः संस्कृति पद्धति रिवाज या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्था नहीं है । नाचना-गाना, साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला, गृहनिर्माण, इन सबका अन्तर्भाव सभ्यता में होता है । संस्कृति अन्तःकरण है, सभ्यता शरीर है । संस्कृति सभ्यता द्वारा स्वयं को व्यक्त करती है । संस्कृति वह साँचा है, जिसमें समाज के विचार ढलते हैं। वह विन्दु है जहाँ से जीवन की समस्याएँ देखी जाती हैं ।"" डॉ० देवराज लिखते हैं- "हर संस्कृति की अपनी सभ्यता होती है । सभ्यता किसी संस्कृति की बाहरी, चरम अवस्था होती है । सभ्यता संस्कृति की अनिवार्य परिणति है । सभ्यता किसी संस्कृति की बाहरी, चरम, कृत्रिम अवस्था का नाम है । यदि संस्कृति जीवन है तो सभ्यता मृत्यु, संस्कृति विस्तार है तो सभ्यता कठोर स्थिरता । सभ्यताएँ नैसर्गिक धरती के स्थान पर आनेवाले कृत्रिम प्रस्तर नगर हैं जो 'होरिक' तथा 'गोथिक' के आध्यात्मिक शैशव का अन्त संकेतित करते हैं।"" चर्चित सभी परिभाषाओं का सीधा सार यह है कि हमारी जीवन-साधना का साररस ही संस्कृति है अर्थात् हमारी दृढ़ीभूत चेतना - प्रेरक जीवन की आन्तरिक पद्धति ही संस्कृति है । संस्कृति किसी भी देश या जाति की प्रबुद्ध आन्तरिक चेतना की वह स्वस्थ और मौलिक विशेषता है जिसके आधार पर विश्व के अन्य देशों में उसका महत्त्वांकन होता है। आज किसी भी देश की संस्कृति ऐसी नहीं है जो अन्य देशों की संस्कृतियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित न हो। सजीव संस्कृति सदा उदार और ग्रहणशील होती है। संस्कृति सदा एक विकासशील संस्था के रूप में ही रहकर किसी देश या जाति के गर्व का कारण बन सकती है। कुछ मौलिक विशेषताओं के साथ प्रत्येक संस्कृति के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय तत्व भी होते हैं जो संस्कृति कम ग्रहणशील होती है, या अतीतोन्मुखी होती है, धीरे-धीरे वह अपना चैतन्य महत्व खोकर मात्र ऐतिहासिक संस्था बनकर रह जाती है । किन्तु इतिहास में भी सातत्य और परिवर्तनशीलता का प्रवाह या क्रम चलता ही रहता है । संस्कृति में भी यही क्रम नितांत वांछनीय है। संस्कृति में वर्तमान का योग और भविष्यत् की सम्भावनाएँ सवा अपेक्षित रहती है। यह पुरातन और नवीन का सुन्दर समन्वय है, मात्र प्राचीन उपलब्धियों की व्याख्यायिका नहीं है। प्राचीन श्रेष्ठ में उसकी जड़ है, वर्तमान के पवन और सारस से उसे अंकुरण, पल्लवन और पुष्पत्य मिलता है और भविष्य में उसका अधिकाधिक फलीभूत होना निहित है। अतः संस्कृति अपनी पूर्णता के लिए वर्तमान और भविष्यत् की भी अपेक्षा रखती है। इतिहास की रचना घटनाएं करती है और साहित्य घटनाओं को भावना के फलक पर उतारता है; संस्कृति भी घटनाओं को आत्मा और भावना के विशाल फलक पर उतारती है । संस्कृति भावनामूलक है और सभ्यता बुद्धिमुलक । बुद्धि विकास और विश्लेषणशील है अतः उसमें अधिकाधिक परिवर्तन की सम्भावना रहती है । भावना में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। संस्कृति में उसकी मूल वेतना में परिवर्तन आने में शताब्दियां लग जाती हैं । यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि संस्कृति समष्टिगत उपलब्धियों का सारतत्त्व होने के साथ-साथ वैयक्तिक उपलब्धियों से भी अपना रक्त और मांस ग्रहण करती है | व्यक्ति का चिन्तन और सृजन निश्चय ही संस्कृति में नवजीवन का संचार करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की कपाशीलता और पूर्णता में सभी अंगों और उपांगों का सम्मिलित सहयोग है और जिस प्रकार अनेक दिशाओं से आगत अनेक छोटी-बड़ी सरिताएं सरितकाएं सागर को सागरत्य प्रदान करती है, उसी प्रकार संस्कृति का सागर भी अनेक व्यक्ति और जाति पुंजों की सम्मिलित चेतना का सागर है |
भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधि विशेषताएं
भारतवर्ष अनेक संस्कृतियों का संगम देश है। इसकी संस्कृति में अनेक धर्मों, सम्प्रदायों और जातियों का महत्त्वपूर्ण योगदान है । अतः किसी एक धर्म या जाति के नाम से इस संस्कृति को सम्बोधित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना स्वयं को असंस्कृत घोषित करना मात्र होगा। फिर इतिहास और वास्तविकता भी तो हमें एकांगी होने से रोकती है। अतः हमारी संस्कृति की प्रथम प्रतिनिधि विशेषता उसकी समन्वयशीलता और सामाजिकता में निहित है । "संस्कृति के लिए व्यक्ति के अभिमान, राष्ट्र के अभिमान और कोम के अभिमान – सबको तिलांजलि देनी पड़ती है। मानव-जाति जित दिन संस्कृति का महत्त्व समझेगी, उसी दिन वह अपनी आत्मा के साथ
डॉ०
o गुलाबराय : भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, पृ० १ कल्याण (गोरखपुर), हिन्दू संस्कृति शंक, पृ० ३६
२.
३. सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग), लोक संस्कृति अंक, पृ० २२
४. संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० १४०
जंग इतिहास, कला और संस्कृति
१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१०६
www.jainelibrary.org