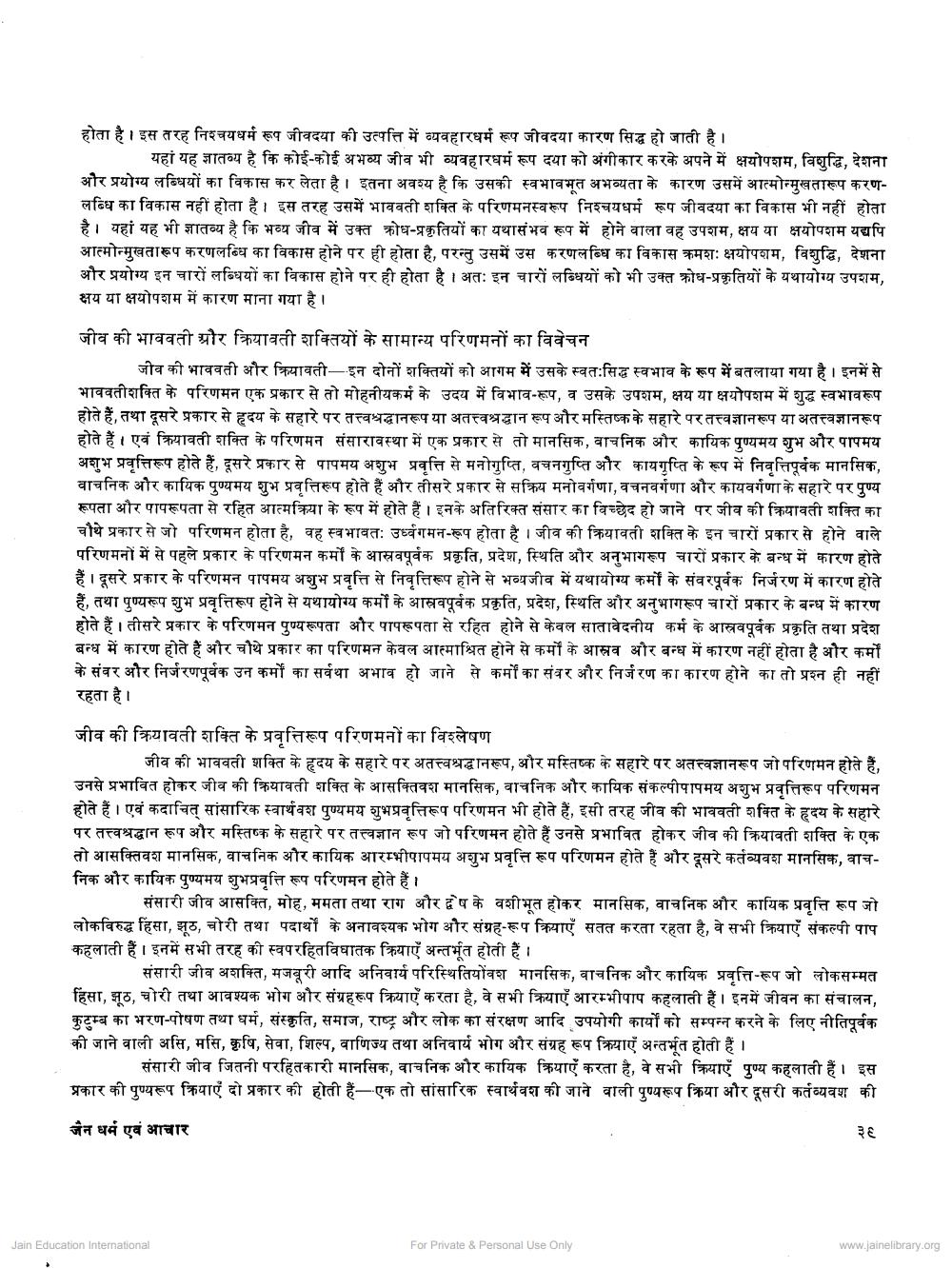________________
होता है। इस तरह निश्चयधर्म रूप जीवदया की उत्पत्ति में व्यवहारधर्म रूप जीवदया कारण सिद्ध हो जाती है।
यहां यह ज्ञातव्य है कि कोई-कोई अभव्य जीव भी व्यवहारधर्म रूप दया को अंगीकार करके अपने में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग्य लब्धियों का विकास कर लेता है। इतना अवश्य है कि उसकी स्वभावभूत अभव्यता के कारण उसमें आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि का विकास नहीं होता है। इस तरह उसमें भाववती शक्ति के परिणमनस्वरूप निश्चयधर्म रूप जीवदया का विकास भी नहीं होता है। यहां यह भी ज्ञातव्य है कि भव्य जीव में उक्त क्रोध-प्रकृतियों का यथासंभव रूप में होने वाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम यद्यपि आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि का विकास होने पर ही होता है, परन्तु उसमें उस करणलब्धि का विकास क्रमशः क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग्य इन चारों लब्धियों का विकास होने पर ही होता है । अतः इन चारों लब्धियों को भी उक्त क्रोध-प्रकृतियों के यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम में कारण माना गया है।
जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियों के सामान्य परिणमनों का विवेचन
जीव की भाववती और क्रियावती-इन दोनों शक्तियों को आगम में उसके स्वतःसिद्ध स्वभाव के रूप में बतलाया गया है। इनमें से भाववतीशक्ति के परिणमन एक प्रकार से तो मोहनीयकर्म के उदय में विभाव-रूप, व उसके उपशम, क्षय या क्षयोपशम में शुद्ध स्वभावरूप होते हैं, तथा दूसरे प्रकार से हृदय के सहारे पर तत्त्वश्रद्धानरूप या अतत्त्वश्रद्धान रूप और मस्तिष्क के सहारे पर तत्त्वज्ञानरूप या अतत्त्वज्ञानरूप होते हैं । एवं क्रियावती शक्ति के परिणमन संसारावस्था में एक प्रकार से तो मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ और पापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं, दूसरे प्रकार से पापमय अशुभ प्रवृत्ति से मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के रूप में निवृत्तिपूर्वक मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं और तीसरे प्रकार से सक्रिय मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणा के सहारे पर पुण्य रूपता और पापरूपता से रहित आत्मक्रिया के रूप में होते हैं। इनके अतिरिक्त संसार का विच्छेद हो जाने पर जीव की क्रियावती शक्ति का चौथे प्रकार से जो परिणमन होता है, वह स्वभावत: उर्ध्वगमन-रूप होता है । जीव की क्रियावती शक्ति के इन चारों प्रकार से होने वाले परिणमनों में से पहले प्रकार के परिणमन कर्मों के आस्रवपूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकार के बन्ध में कारण होते हैं । दूसरे प्रकार के परिणमन पापमय अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्तिरूप होने से भव्यजीव में यथायोग्य कर्मों के संवरपूर्वक निर्जरण में कारण होते हैं, तथा पुण्यरूप शुभ प्रवृत्तिरूप होने से यथायोग्य कर्मों के आस्रवपूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकार के बन्ध में कारण होते हैं। तीसरे प्रकार के परिणमन पुण्यरूपता और पापरूपता से रहित होने से केवल सातावेदनीय कर्म के आस्रवपूर्वक प्रकृति तथा प्रदेश बन्ध में कारण होते हैं और चौथे प्रकार का परिणमन केवल आत्माश्रित होने से कर्मों के आस्रव और बन्ध में कारण नहीं होता है और कर्मों के संवर और निर्जरणपूर्वक उन कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाने से कर्मों का संवर और निर्जरण का कारण होने का तो प्रश्न ही नहीं रहता है। जीव की क्रियावती शक्ति के प्रवत्तिरूप परिणमनों का विश्लेषण
जीव की भाववती शक्ति के हृदय के सहारे पर अतत्त्वश्रद्धानरूप, और मस्तिष्क के सहारे पर अतत्त्वज्ञानरूप जो परिणमन होते हैं, उनसे प्रभावित होकर जीव की क्रियावती शक्ति के आसक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं । एवं कदाचित् सांसारिक स्वार्थवश पुण्यमय शुभप्रवृत्तिरूप परिणमन भी होते हैं, इसी तरह जीव की भाववती शक्ति के हृदय के सहारे पर तत्त्वश्रद्धान रूप और मस्तिष्क के सहारे पर तत्त्वज्ञान रूप जो परिणमन होते हैं उनसे प्रभावित होकर जीव की क्रियावती शक्ति के एक तो आसक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भीपापमय अशुभ प्रवृत्ति रूप परिणमन होते हैं और दूसरे कर्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभप्रवृत्ति रूप परिणमन होते हैं।
संसारी जीव आसक्ति, मोह, ममता तथा राग और द्वेष के वशीभूत होकर मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति रूप जो लोकविरुद्ध हिंसा, झूठ, चोरी तथा पदार्थों के अनावश्यक भोग और संग्रह-रूप क्रियाएँ सतत करता रहता है, वे सभी क्रियाएँ संकल्पी पाप कहलाती हैं । इनमें सभी तरह की स्वपरहितविघातक क्रियाएँ अन्तर्भूत होती हैं।
संसारी जीव अशक्ति, मजबूरी आदि अनिवार्य परिस्थितियोंवश मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति-रूप जो लोकसम्मत हिंसा, झूठ, चोरी तथा आवश्यक भोग और संग्रहरूप क्रियाएँ करता है, वे सभी क्रियाएँ आरम्भीपाप कहलाती हैं। इनमें जीवन का संचालन, कुटुम्ब का भरण-पोषण तथा धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र और लोक का संरक्षण आदि उपयोगी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए नीतिपूर्वक की जाने वाली असि, मसि, कृषि, सेवा, शिल्प, वाणिज्य तथा अनिवार्य भोग और संग्रह रूप क्रियाएँ अन्तर्भूत होती हैं।
संसारी जीव जितनी परहितकारी मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियाएँ करता है, वे सभी क्रियाएँ पुण्य कहलाती हैं। इस प्रकार की पुण्यरूप क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं- एक तो सांसारिक स्वार्थवश की जाने वाली पुण्यरूप क्रिया और दूसरी कर्तव्यवश की
जैन धर्म एवं आचार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org