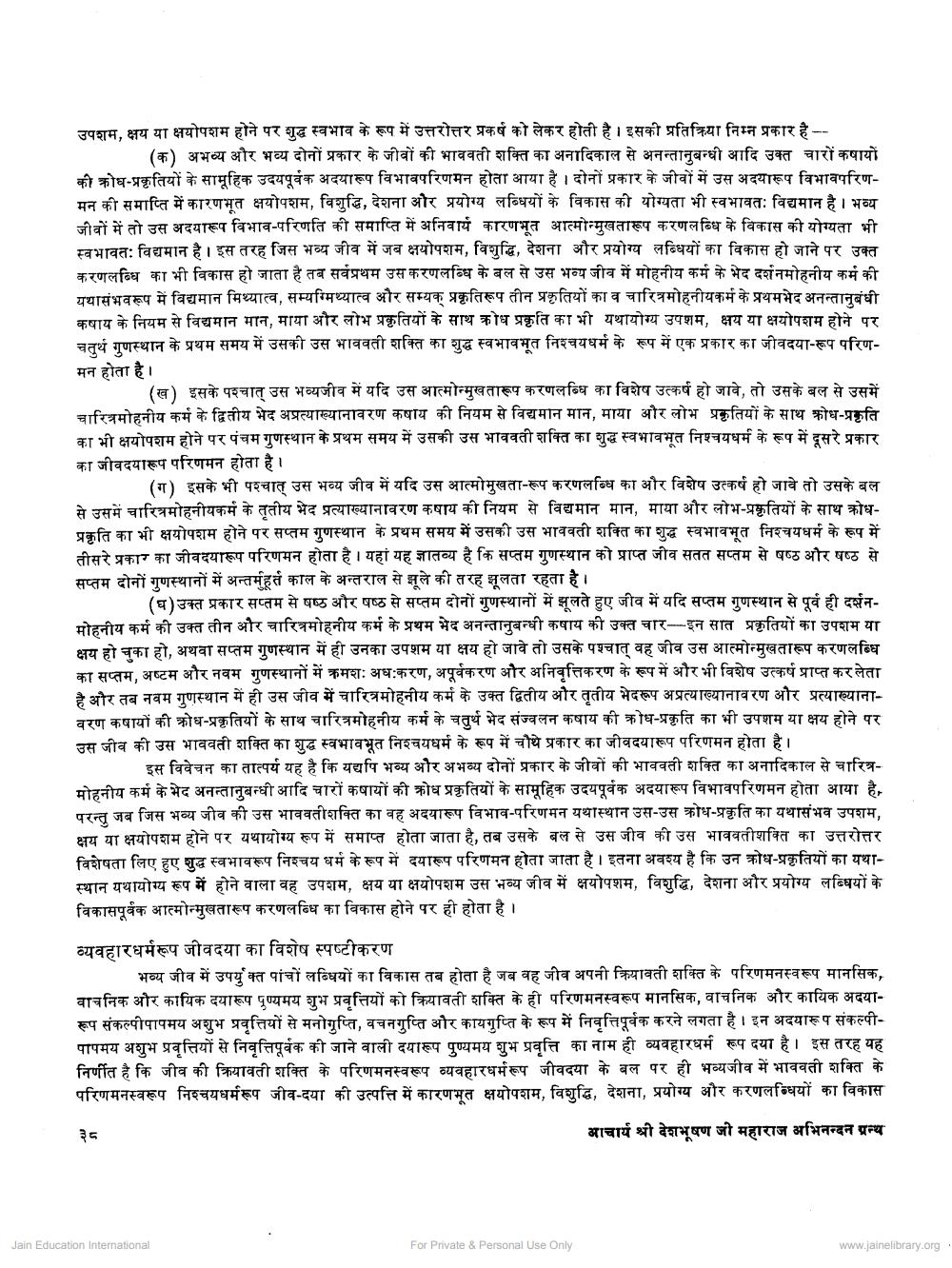________________
उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने पर शुद्ध स्वभाव के रूप में उत्तरोत्तर प्रकर्ष को लेकर होती है। इसकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार है--
(क) अभव्य और भव्य दोनों प्रकार के जीवों की भाववती शक्ति का अनादिकाल से अनन्तानुबन्धी आदि उक्त चारों कषायों की क्रोध-प्रकृतियों के सामूहिक उदयपूर्वक अदयारूप विभावपरिणमन होता आया है। दोनों प्रकार के जीवों में उस अदयारूप विभावपरिणमन की समाप्ति में कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग्य लब्धियों के विकास की योग्यता भी स्वभावतः विद्यमान है। भव्य जीवों में तो उस अदयारूप विभाव-परिणति की समाप्ति में अनिवार्य कारणभूत आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि के विकास की योग्यता भी स्वभावतः विद्यमान है। इस तरह जिस भव्य जीव में जब क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग्य लब्धियों का विकास हो जाने पर उक्त करणलब्धि का भी विकास हो जाता है तब सर्वप्रथम उस करणलब्धि के बल से उस भव्य जीव में मोहनीय कर्म के भेद दर्शनमोहनीय कर्म की यथासंभवरूप में विद्यमान मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिरूप तीन प्रकृतियों का व चारित्रमोहनीयकर्म के प्रथमभेद अनन्तानबंधी कषाय के नियम से विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियों के साथ क्रोध प्रकृति का भी यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने पर चतुर्थ गुणस्थान के प्रथम समय में उसकी उस भाववती शक्ति का शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म के रूप में एक प्रकार का जीवदया-रूप परिणमन होता है।
(ख) इसके पश्चात् उस भव्यजीव में यदि उस आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि का विशेष उत्कर्ष हो जावे, तो उसके बल से उसमें चारित्रमोहनीय कर्म के द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानावरण कषाय की नियम से विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियों के साथ क्रोध-प्रकृति का भी क्षयोपशम होने पर पंचम गुणस्थान के प्रथम समय में उसकी उस भाववती शक्ति का शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म के रूप में दूसरे प्रकार का जीवदयारूप परिणमन होता है।
(ग) इसके भी पश्चात् उस भव्य जीव में यदि उस आत्मोमुखता-रूप करणलब्धि का और विशेष उत्कर्ष हो जावे तो उसके बल से उसमें चारित्रमोहनीयकर्म के तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण कषाय की नियम से विद्यमान मान, माया और लोभ-प्रकृतियों के साथ क्रोधप्रकृति का भी क्षयोपशम होने पर सप्तम गुणस्थान के प्रथम समय में उसकी उस भाववती शक्ति का शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म के रूप में तीसरे प्रकार का जीवदयारूप परिणमन होता है । यहां यह ज्ञातव्य है कि सप्तम गुणस्थान को प्राप्त जीव सतत सप्तम से षष्ठ और षष्ठ से सप्तम दोनों गुणस्थानों में अन्तर्मुहूर्त काल के अन्तराल से झूले की तरह झूलता रहता है।
(घ) उक्त प्रकार सप्तम से षष्ठ और षष्ठ से सप्तम दोनों गुणस्थानों में झूलते हुए जीव में यदि सप्तम गुणस्थान से पूर्व ही दर्शनमोहनीय कर्म की उक्त तीन और चारित्रमोहनीय कर्म के प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषाय की उक्त चार-इन सात प्रकृतियों का उपशम या क्षय होचका हो, अथवा सप्तम गुणस्थान में ही उनका उपशम या क्षय हो जावे तो उसके पश्चात् वह जीव उस आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि का सप्तम, अष्टम और नवम गुणस्थानों में क्रमशः अध:करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के रूप में और भी विशेष उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है और तब नवम गुणस्थान में ही उस जीव में चारित्रमोहनीय कर्म के उक्त द्वितीय और तृतीय भेदरूप अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायों की क्रोध-प्रकृतियों के साथ चारित्रमोहनीय कर्म के चतुर्थ भेद संज्वलन कषाय की क्रोध-प्रकृति का भी उपशम या क्षय होने पर उस जीव की उस भाववती शक्ति का शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म के रूप में चौथे प्रकार का जीवदयारूप परिणमन होता है।
इस विवेचन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों की भाववती शक्ति का अनादिकाल से चारित्रमोहनीय कर्म के भेद अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषायों की क्रोध प्रकृतियों के सामूहिक उदयपूर्वक अदयारूप विभावपरिणमन होता आया है, परन्तु जब जिस भव्य जीव की उस भाववतीशक्ति का वह अदयारूप विभाव-परिणमन यथास्थान उस-उस क्रोध-प्रकृति का यथासंभव उपशम, क्षय या क्षयोपशम होने पर यथायोग्य रूप में समाप्त होता जाता है, तब उसके बल से उस जीव की उस भाववतीशक्ति का उत्तरोत्तर विशेषता लिए हुए शुद्ध स्वभावरूप निश्चय धर्म के रूप में दयारूप परिणमन होता जाता है। इतना अवश्य है कि उन क्रोध-प्रकृतियों का यथास्थान यथायोग्य रूप में होने वाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम उस भव्य जीव में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रयोग्य लब्धियों के विकासपूर्वक आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि का विकास होने पर ही होता है ।
व्यवहारधर्मरूप जीवदया का विशेष स्पष्टीकरण
__ भव्य जीव में उपर्युक्त पांचों लब्धियों का विकास तब होता है जब वह जीव अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तियों को क्रियावती शक्ति के ही परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तियों से मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के रूप में निवृत्तिपूर्वक करने लगता है। इन अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्तिपूर्वक की जाने वाली दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति का नाम ही व्यवहारधर्म रूप दया है। इस तरह यह निर्णीत है कि जीव की क्रियावती शक्ति के परिणमनस्वरूप व्यवहारधर्मरूप जीवदया के बल पर ही भव्यजीव में भाववती शक्ति के परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मरूप जीव-दया की उत्पत्ति में कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रयोग्य और करणलब्धियों का विकास
३८
आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org