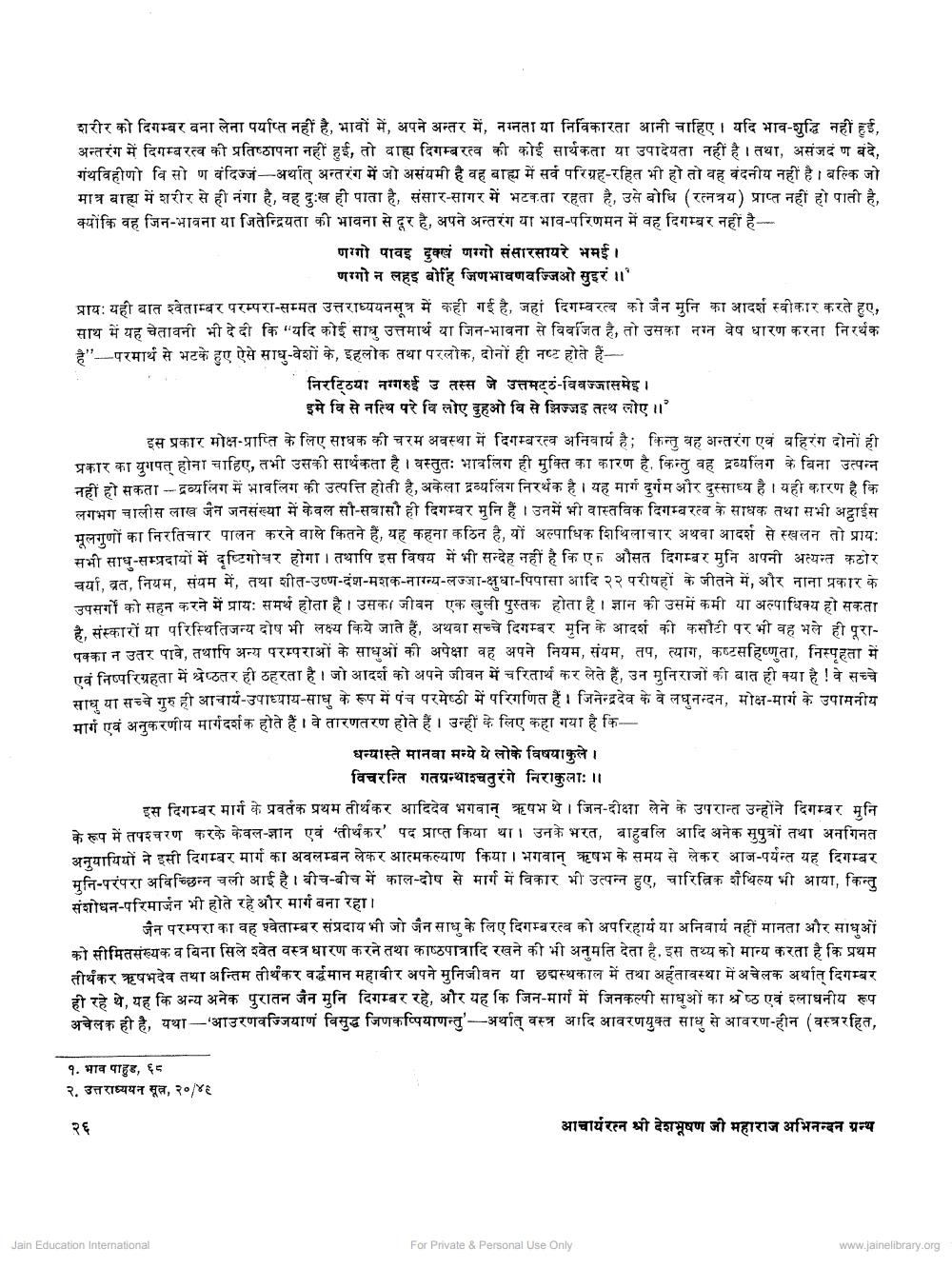________________
शरीर को दिगम्बर बना लेना पर्याप्त नहीं है, भावों में, अपने अन्तर में, नग्नता या निर्विकारता आनी चाहिए। यदि भाव-शुद्धि नहीं हुई, अन्तरंग में दिगम्बरत्व की प्रतिष्ठापना नहीं हुई, तो वाह्य दिगम्बरत्व की कोई सार्थकता या उपादेयता नहीं है । तथा, असंजदं ण बंदे, गंथविहीणो वि सो ण वंदिज्ज-अर्थात् अन्तरंग में जो असंयमी है वह बाह्य में सर्व परिग्रह-रहित भी हो तो वह वंदनीय नहीं है। बल्कि जो मात्र बाह्य में शरीर से ही नंगा है, वह दुःख ही पाता है, संसार-सागर में भटकता रहता है, उसे बोधि (रत्नत्रय) प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जिन-भावना या जितेन्द्रियता की भावना से दूर है, अपने अन्तरंग या भाव-परिणमन में वह दिगम्बर नहीं है--
णग्गो पावइ दुक्खं णग्गो संसारसायरे भमई।
णग्गो न लहइ बोहिं जिणभावणवज्जिओ सुइरं ॥ प्रायः यही बात श्वेताम्बर परम्परा-सम्मत उत्तराध्ययनसूत्र में कही गई है, जहां दिगम्बरत्व को जैन मुनि का आदर्श स्वीकार करते हुए, साथ में यह चेतावनी भी दे दी कि “यदि कोई साधु उत्तमार्थ या जिन-भावना से विजित है, तो उसका नग्न वेष धारण करना निरर्थक है"-परमार्थ से भटके हुए ऐसे साधु-वेशों के, इहलोक तथा परलोक, दोनों ही नष्ट होते हैं---
निरट्ठिया नग्गरुई उ तस्स जे उत्तमठ्ठ-विवज्जासमेइ।
इमे वि से नत्थि परे वि लोए दुहओ वि से झिज्जइ तत्थ लोए॥' इस प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के लिए साधक की चरम अवस्था में दिगम्बरत्व अनिवार्य है; किन्तु वह अन्तरंग एवं बहिरंग दोनों ही प्रकार का युगपत् होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है । वस्तुतः भावलिग ही मुक्ति का कारण है, किन्तु वह द्रव्यलिंग के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता-द्रव्यलिंग में भावलिंग की उत्पत्ति होती है, अकेला द्रव्यलिंग निरर्थक है। यह मार्ग दुर्गम और दुस्साध्य है। यही कारण है कि लगभग चालीस लाख जैन जनसंख्या में केवल सौ-सवासौ ही दिगम्बर मुनि हैं । उनमें भी वास्तविक दिगम्बरत्व के साधक तथा सभी अट्ठाईस मलगुणों का निरतिचार पालन करने वाले कितने हैं, यह कहना कठिन है, यों अल्पाधिक शिथिलाचार अथवा आदर्श से स्खलन तो प्रायः सभी साधु-सम्प्रदायों में दृष्टिगोचर होगा। तथापि इस विषय में भी सन्देह नहीं है कि एक औसत दिगम्बर मुनि अपनी अत्यन्त कठोर जर्या वत. नियम, संयम में, तथा शीत-उष्ण-दंश-मशक-नाग्न्य-लज्जा-क्षधा-पिपासा आदि २२ परीषहों के जीतने में, और नाना प्रकार के उपसर्गों को सहन करने में प्रायः समर्थ होता है। उसका जीवन एक खुली पुस्तक होता है । ज्ञान की उसमें कमी या अल्पाधिक्य हो सकता है. संस्कारों या परिस्थितिजन्य दोष भी लक्ष्य किये जाते हैं, अथवा सच्चे दिगम्बर मुनि के आदर्श की कसौटी पर भी वह भले ही पूरापक्का न उतर पावे, तथापि अन्य परम्पराओं के साधुओं की अपेक्षा वह अपने नियम, संयम, तप, त्याग, कष्टसहिष्णुता, निस्पृहता में एवं निष्परिग्रहता में श्रेष्ठतर ही ठहरता है। जो आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेते हैं, उन मुनिराजों की बात ही क्या है ! वे सच्चे साध या सच्चे गुरु ही आचार्य-उपाध्याय-साधु के रूप में पंच परमेष्ठी में परिगणित हैं। जिनेन्द्रदेव के वे लघुनन्दन, मोक्ष-मार्ग के उपासनीय मार्ग एवं अनुकरणीय मार्गदर्शक होते हैं । वे तारणतरण होते हैं। उन्हीं के लिए कहा गया है कि
धन्यास्ते मानवा मन्ये ये लोके विषयाकुले।
विचरन्ति गतग्रन्थाश्चतुरंगे निराकुलाः ।। इस दिगम्बर मार्ग के प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर आदिदेव भगवान् ऋषभ थे। जिन-दीक्षा लेने के उपरान्त उन्होंने दिगम्बर मुनि के रूप में तपश्चरण करके केवल-ज्ञान एवं 'तीर्थकर' पद प्राप्त किया था। उनके भरत, बाहुबलि आदि अनेक सुपुत्रों तथा अनगिनत अनयायियों ने इसी दिगम्बर मार्ग का अवलम्बन लेकर आत्मकल्याण किया । भगवान् ऋषभ के समय से लेकर आज-पर्यन्त यह दिगम्बर मनि-परंपरा अविच्छिन्न चली आई है। बीच-बीच में काल-दोष से मार्ग में विकार भी उत्पन्न हुए, चारित्रिक शैथिल्य भी आया, किन्तु संशोधन-परिमार्जन भी होते रहे और मार्ग बना रहा।
जैन परम्परा का वह श्वेताम्बर संप्रदाय भी जो जैन साधु के लिए दिगम्ब रत्व को अपरिहार्य या अनिवार्य नहीं मानता और साधुओं कोसीमितसंख्यक ब बिना सिले श्वेत वस्त्र धारण करने तथा काष्ठपात्रादि रखने की भी अनुमति देता है. इस तथ्य को मान्य करता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अन्तिम तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर अपने मुनिजीवन या छद्मस्थकाल में तथा अर्हतावस्था में अचेलक अर्थात दिगम्बर दी रहे थे. यह कि अन्य अनेक पुरातन जैन मुनि दिगम्बर रहे, और यह कि जिन-मार्ग में जिनकल्पी साधुओं का श्रेष्ठ एवं श्लाघनीय रूप अचेलक ही है, यथा-'आउरणवज्जियाणं विसुद्ध जिणकप्पियाणन्तु'-अर्थात् वस्त्र आदि आवरणयुक्त साधु से आवरण-हीन (वस्त्ररहित,
१. भाव पाहुड, ६८ २. उत्तराध्ययन सूत्र, २०/४६
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org