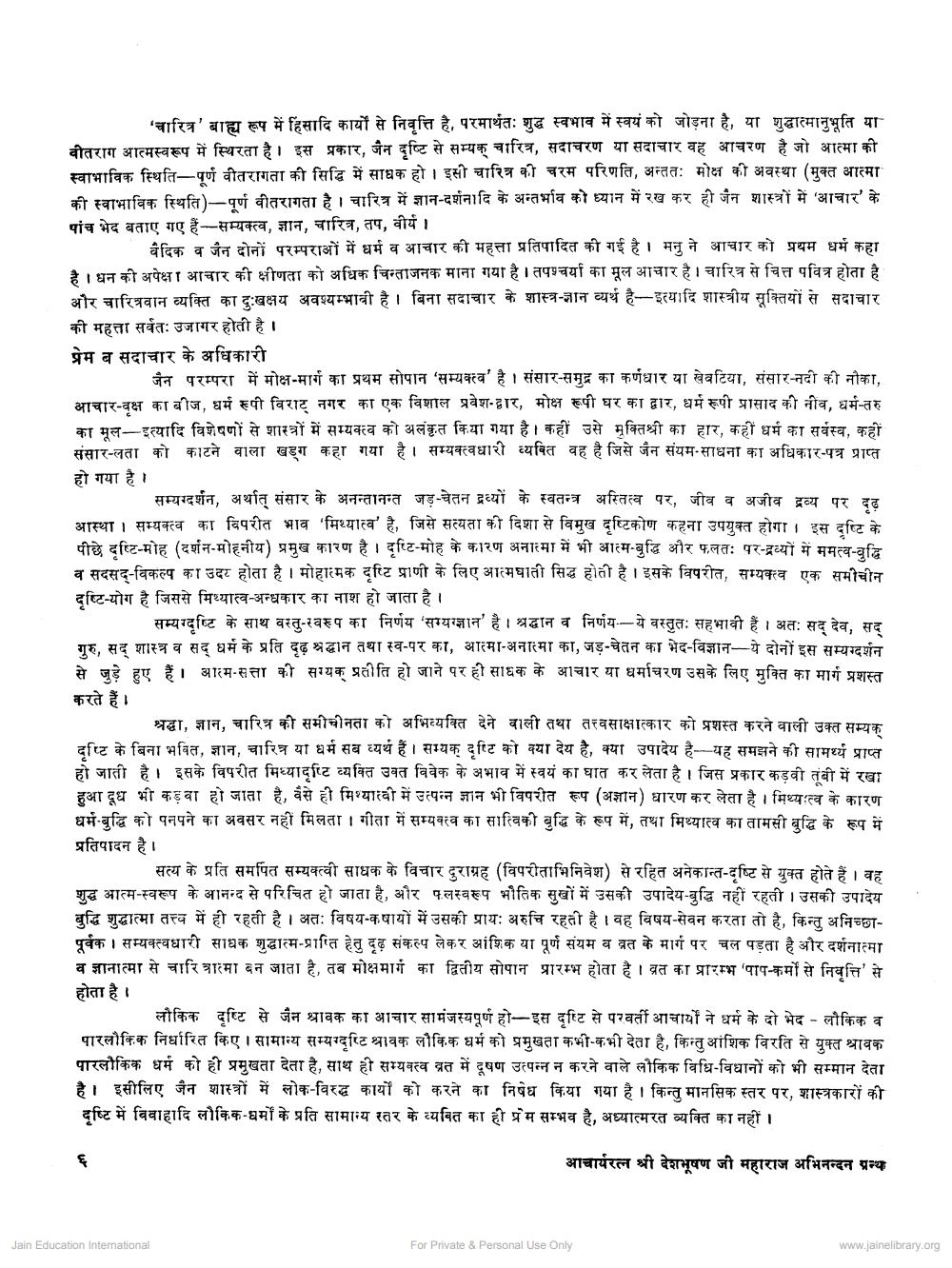________________
'चारिष' बाह्य रूप में हिंसादि कार्यों से निवृत्ति है, परमार्थतः शुद्ध स्वभाव में स्वयं को जोड़ना है, या शुद्धात्मानुभूति या वीतराग आत्मस्वरूप में स्थिरता है। इस प्रकार, जैन दृष्टि से सम्यक् चारित्र, सदाचरण या सदाचार वह आचरण है जो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति - पूर्ण वीतरागता की सिद्धि में साधक हो। इसी चारित्र की चरम परिणति, अन्ततः मोक्ष की अवस्था ( मुक्त आत्मा की स्वाभाविक स्थिति ) - पूर्ण वीतरागता है । चारित्र में ज्ञान दर्शनादि के अन्तर्भाव को ध्यान में रख कर ही जैन शास्त्रों में 'आचार' के पांच भेद बताए गए हैं सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य ।
वैदिक व जैन दोनों परम्पराओं में धर्म व आचार की महत्ता प्रतिपादित की गई है । मनु ने आचार को प्रथम धर्म कहा है। धन की अपेक्षा आचार की क्षीणता को अधिक चिन्ताजनक माना गया है। तपश्चर्या का मूल आचार है। चारित्र से चित्त पवित्र होता है। और चारित्रवान व्यक्ति का दुःखक्षय अवश्यम्भावी है। बिना सदाचार के शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है-- इत्यादि शास्त्रीय सूक्तियों से सदाचार की महत्ता 'सर्वतः उजागर होती है ।
प्रेम व सदाचार के अधिकारी
जैन परम्परा में मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान 'सम्यक्त्व' है। संसार समुद्र का कर्णधार या खेवटिया, संसार-नदी की नौका, आचार-वृक्ष का बीज, धर्म रूपी विराट् नगर का एक विशाल प्रवेश द्वार, मोक्ष रूपी घर का द्वार, धर्म रूपी प्रासाद की नींव, धर्म-तरु का मूल इत्यादि विशेषणों से शास्त्रों में सम्यक्त्व को अलंकृत किया गया है। कहीं उसे मुक्तिधी का हार, कहीं धर्म का सर्वस्य कहीं संसार-लता को काटने वाला खड्ग कहा गया है । सम्यक्त्वधारी व्यक्ति वह है जिसे जैन संयम साधना का अधिकार-पत्र प्राप्त हो गया है।
सम्यग्दर्शन, अर्थात् संसार के अनन्तानन्त जड़-चेतन द्रव्यों के स्वतन्त्र अस्तित्व पर जीव व अजीव द्रव्य पर दृढ़ आस्था । सम्यक्त्व का विपरीत भाव 'मिथ्यात्व' है, जिसे सत्यता की दिशा से विमुख दृष्टिकोण कहना उपयुक्त होगा । इस दृष्टि के पीछे दृष्टि-मोह (दर्शन-मोहनीय) प्रमुख कारण है दृष्टि-मोह के कारण अनात्मा में भी आत्म-वृद्धि और फलतः परद्रव्यों में ममत्व वृद्धि व सदसद्-विकल्प का उदय होता है । मोहात्मक दृष्टि प्राणी के लिए आत्मघाती सिद्ध होती है। इसके विपरीत, सम्यक्त्व एक समीचीन दृष्टि-योग है जिससे मिथ्यात्व - अन्धकार का नाश हो जाता है ।
सम्यग्दृष्टि के साथ वस्तु-स्वरूप का निर्णय 'सम्यग्ज्ञान' है। श्रद्धान व निर्णय - ये वस्तुतः सहभावी हैं । अतः सद् देव, सद् गुरु, सद् शास्त्र व सद् धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धान तथा स्व-पर का, आत्मा-अनात्मा का जड़-चेतन का भेद - विज्ञान - ये दोनों इस सम्यग्दर्शन से जुड़े हुए हैं। आत्म-सत्ता की सम्यक् प्रतीति हो जाने पर ही साधक के आचार या धर्माचरण उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की समीचीनता को अभिव्यक्ति देने वाली तथा तत्त्वसाक्षात्कार को प्रशस्त करने वाली उक्त सम्यक् दृष्टि के बिना भक्ति, ज्ञान, चारित्र या धर्म सब व्यर्थ हैं। सम्यक दृष्टि को क्या देय है, क्या उपादेय है—यह समझने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत मिध्यादृष्टि व्यक्ति उक्त विवेक के अभाव में स्वयं का घात कर लेता है। जिस प्रकार कड़वी तूंबी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है, वैसे ही मिथ्यात्वी में उत्पन्न ज्ञान भी विपरीत रूप ( अज्ञान) धारण कर लेता है। मिथ्यात्व के कारण धर्म- बुद्धि को पनपने का अवसर नहीं मिलता। गीता में सम्यक्त्व का सात्विकी बुद्धि के रूप में, तथा मिथ्यात्व का तामसी बुद्धि के रूप में प्रतिपादन है।
सत्य के प्रति समर्पित सम्यक्त्वी साधक के विचार दुराग्रह ( विपरीताभिनिवेश) से रहित अनेकान्त दृष्टि से युक्त होते हैं। वह शुद्ध आत्म-स्वरूप के आनन्द से परिचित हो जाता है, और फलस्वरूप भौतिक सुखों में उसकी उपादेय बुद्धि नहीं रहती । उसकी उपादेय बुद्धि शुद्धात्मा तत्त्व में ही रहती है । अतः विषय कषायों में उसकी प्राय: अरुचि रहती है । वह विषय सेवन करता तो है, किन्तु अनिच्छापूर्वक । सम्यक्त्वधारी साधक शुद्धात्म-प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प लेकर आंशिक या पूर्ण संयम व व्रत के मार्ग पर चल पड़ता है और दर्शनात्मा व ज्ञानात्मा से चारित्रात्मा बन जाता है, तब मोक्षमार्ग का द्वितीय सोपान प्रारम्भ होता है । व्रत का प्रारम्भ पाप कर्मों से निवृत्ति' से होता है ।
लौकिक दृष्टि से जैन श्रावक का आचार सामंजस्यपूर्ण हो - इस दृष्टि से परवर्ती आचार्यों ने धर्म के दो भेद - लौकिक व पारलौकिक निर्धारित किए। सामान्य सम्यग्दृष्टि श्रावक लौकिक धर्म को प्रमुखता कभी-कभी देता है, किन्तु आंशिक विरति से युक्त श्रावक पारलौकिक धर्म को ही प्रमुखता देता है, साथ ही सम्यवत्व व्रत में दूषण उत्पन्न न करने वाले लौकिक विधि-विधानों को भी सम्मान देता है इसीलिए जैन शास्त्रों में लोक-विरुद्ध कार्यों को करने का निषेध किया गया है किन्तु मानसिक स्तर पर शास्त्रकारों की दृष्टि में विवाहादि लौकिक धर्मों के प्रति सामान्य स्तर के व्यक्ति का ही प्रेम सम्भव है, अध्यात्मरत व्यक्ति का नहीं ।
Jain Education International
आचार्यरल भी देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन
श्री
For Private & Personal Use Only
ग्रन्थ
www.jainelibrary.org