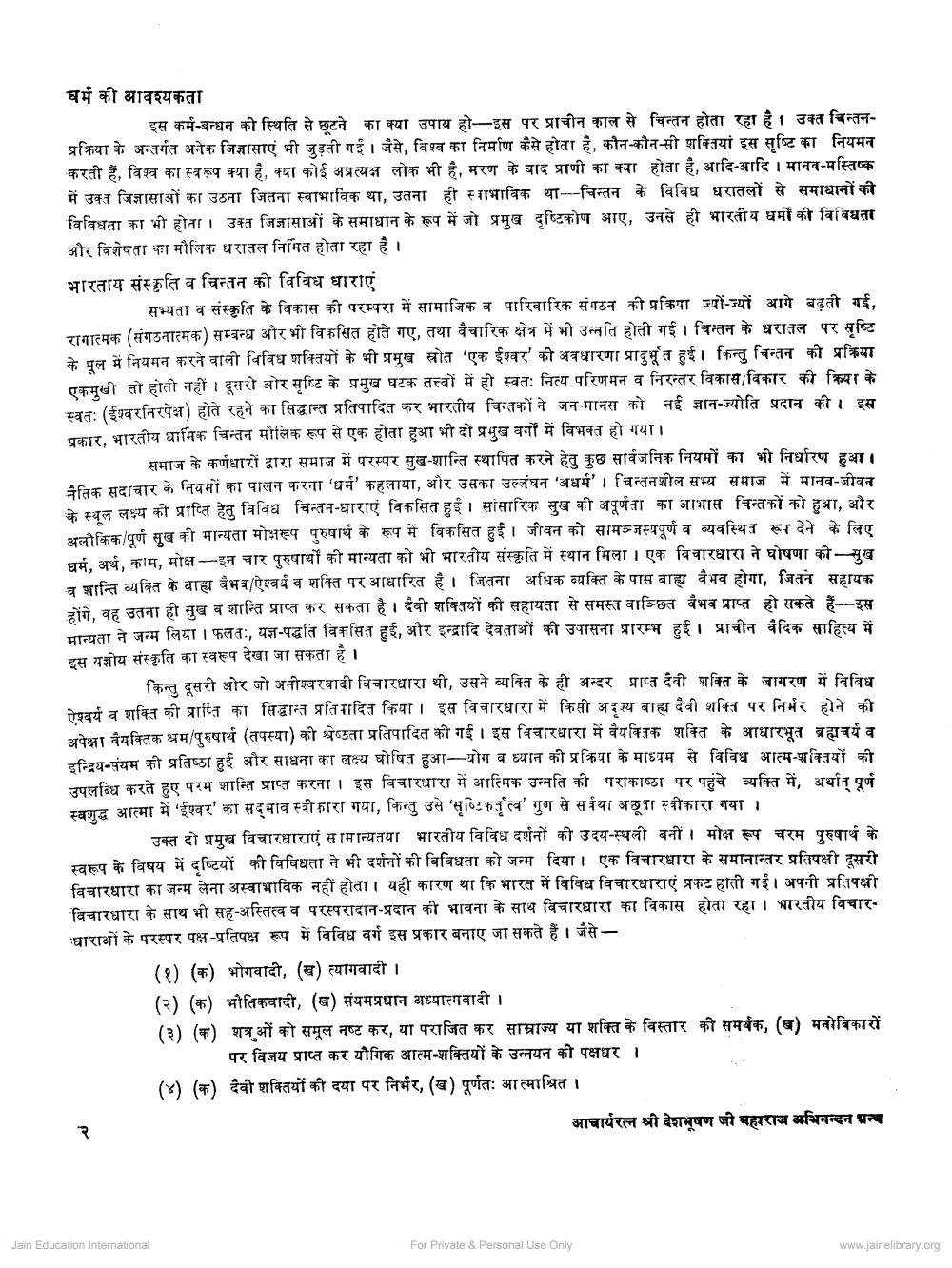________________
धर्म की आवश्यकता
इस कर्म बन्धन की स्थिति से छूटने का क्या उपाय हो—इस पर प्राचीन काल से चिन्तन होता रहा है। उक्त चिन्तनप्रक्रिया के अन्तर्गत अनेक जिज्ञासाएं भी जुड़ती गई। जैसे विश्व का निर्माण कैसे होता है, कौन-कौन-सी शक्तियां इस सृष्टि का नियमन करती हैं, विश्व का स्वरूप क्या है, क्या कोई अप्रत्यक्ष लोक भी हैं, मरण के बाद प्राणी का क्या होता है, आदि-आदि। मानव मस्तिष्क में उक्त जिज्ञासाओं का उठना जितना स्वाभाविक था, उतना ही स्वाभाविक था--- चिन्तन के विविध धरातलों से समाधानों की विविधता का भी होता । उक्त जिज्ञासाओं के समाधान के रूप में जो प्रमुख दृष्टिकोण आए, उनसे ही भारतीय धर्मों की विविधता और विशेषता मौलिक धरातल निर्मित होता रहा है।
भारताय संस्कृति व चिन्तन की विविध धाराएं
सभ्यता व संस्कृति के विकास की परम्परा में सामाजिक व पारिवारिक संगठन की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गई, रागात्मक (संगठनात्मक ) सम्बन्ध और भी विकसित होते गए, तथा वैचारिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई । चिन्तन के धरातल पर सृष्टि के ' में नियमन करने वाली विविध शक्तियों के भी प्रमुख स्रोत 'एक ईश्वर' की अवधारणा प्रादुर्भूत हुई। किन्तु चिन्तन की प्रक्रिया एकमुखी तो होती नहीं दूसरी ओर सृष्टि के प्रमुख घटक तत्वों में ही स्वतः नित्य परिणमन व निरन्तर विकास विकार की किया के स्वतः (ईश्वरनिरपेक्ष) होते रहने का सिद्धान्त प्रतिपादित कर भारतीय चिन्तकों ने जन-मानस को नई ज्ञान ज्योति प्रदान की । इस प्रकार, भारतीय धार्मिक चिन्तन मौलिक रूप से एक होता हुआ भी दो प्रमुख वर्गों में विभक्त हो गया ।
मूल
समाज के कर्णधारों द्वारा समाज में परस्पर सुख-शान्ति स्थापित करने हेतु कुछ सार्वजनिक नियमों का भी निर्धारण हुआ । नैतिक सदाचार के नियमों का पालन करना 'धर्म' कहलाया, और उसका उल्लंघन 'अधर्म' । चिन्तनशील सभ्य समाज में मानव जीवन के स्कूल लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विविध चिन्तनधाराएं विकसित हुई सांसारिक सुख की अपूर्णता का आभास चिन्तकों को हुआ और अलौकिक पूर्ण सुख की मान्यता मोजरूप पुरुषार्थ के रूप में विकसित हुई जीवनको सामजस्यपूर्ण व व्यवस्थित रूप देने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष -- इन चार पुरुषार्थों की मान्यता को भी भारतीय संस्कृति में स्थान मिला। एक विचारधारा ने घोषणा की सुख व शान्ति व्यक्ति के बाह्य वैभव / ऐश्वर्य व शक्ति पर आधारित है। जितना अधिक व्यक्ति के पास बाह्य वैभव होगा, जितने सहायक होंगे, वह उतना ही सुख व शान्ति प्राप्त कर सकता है। देवी शक्तियों की सहायता से समस्त वाञ्छित वैभव प्राप्त हो सकते हैं - इस मान्यता ने जन्म लिया । फलतः, यज्ञ-पद्धति विकसित हुई, और इन्द्रादि देवताओं की उपासना प्रारम्भ हुई। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस यज्ञीय संस्कृति का स्वरूप देखा जा सकता है ।
किन्तु दूसरी ओर जो अनीश्वरवादी विचारधारा थी, उसने व्यक्ति के ही अन्दर प्राप्त देवी शक्ति के जागरण में ऐश्वर्य व शक्ति की प्राप्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इस विचारधारा में किसी अदृश्य बाह्य दैवी शक्ति पर निर्भर होने की अपेक्षा वैयक्तिक श्रम / पुरुषार्थ (तपस्या) की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई। इस विचारधारा में वैयक्तिक शक्ति के आधारभूत ब्रह्मचर्य व इन्द्रियसंयम की प्रतिष्ठा हुई और साधना का लक्ष्य घोषित हुआ योग ध्यान की प्रकिया के माध्यम से विविध आत्मयों की उपलब्धि करते हुए परम शान्ति प्राप्त करना । इस विचारधारा में आत्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचे व्यक्ति में, अर्थात् पूर्ण स्वशुद्ध आत्मा में 'ईश्वर' का सद्भाव स्वीकारा गया, किन्तु उसे 'सृष्टिकर्तृत्व' गुण से सर्वथा अछूता स्वीकारा गया ।
उक्त दो प्रमुख विचारधाराएं सामान्यतया भारतीय विविध दर्शनों की उदय स्थली बनीं। मोक्ष रूप चरम पुरुषार्थ के स्वरूप के विषय में दृष्टियों की विविधता ने भी दर्शनों की विविधता को जन्म दिया। एक विचारधारा के समानान्तर प्रतिपक्षी दूसरी विचारधारा का जन्म लेना अस्वाभाविक नहीं होता। यही कारण था कि भारत में विविध विचारधाराएं प्रकट होती गईं। अपनी प्रतिपक्षी विचारधारा के साथ भी सह-अस्तित्व व परस्परादान-प्रदान की भावना के साथ विचारधारा का विकास होता रहा। भारतीय विचारधाराओं के परस्पर पक्ष प्रतिपक्ष रूप में विविध वर्ग इस प्रकार बनाए जा सकते हैं। जैसे
Jain Education International
(१) (क) भोगवादी, (ख) त्यागवादी ।
(२) (क) भौतिकवादी (ख) संयमप्रधान अध्यात्मवादी ।
(३) (क) शत्रुओं को समूल नष्ट कर, या पराजित कर साम्राज्य या शक्ति के विस्तार की समर्थक, (ख) मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर यौगिक आत्म-शक्तियों के उन्नयन की पक्षधर ।
(४) (क) दैवी शक्तियों की दया पर निर्भर, (ख) पूर्णतः आत्माश्रित ।
"
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org