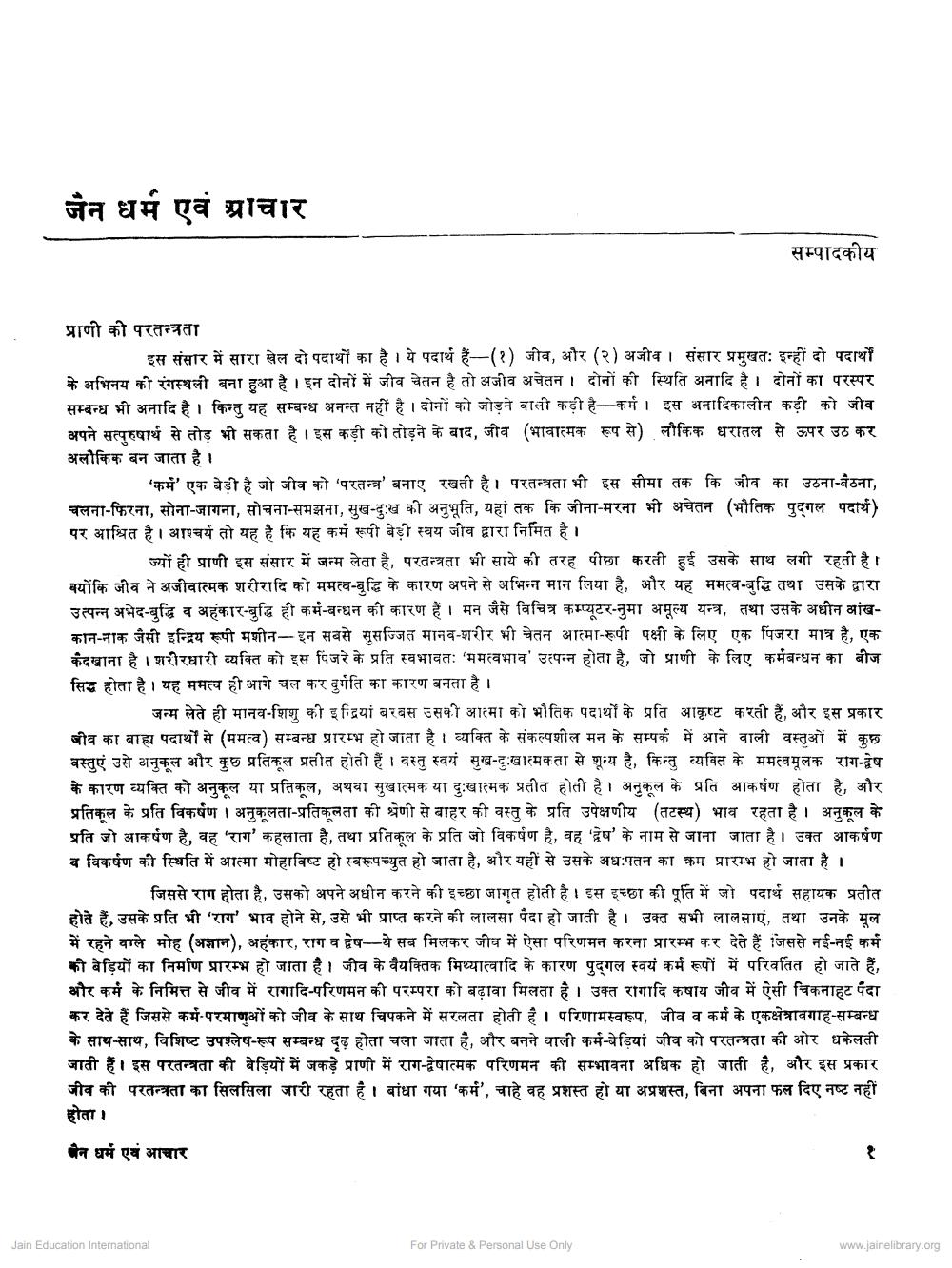________________
जैन धर्म एवं प्राचार
प्राणी की परतन्त्रता
इस संसार में सारा खेल दो पदार्थों का है। ये पदार्थ हैं - ( १ ) जीव, और (२) अजीव । संसार प्रमुखतः इन्हीं दो पदार्थों के अभिनय की रंगस्थली बना हुआ है। इन दोनों में जीव चेतन है तो अजीव अचेतन । दोनों की स्थिति अनादि है। दोनों का परस्पर सम्बन्ध भी अनादि है । किन्तु यह सम्बन्ध अनन्त नहीं है। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है-कर्म । इस अनादिकालीन कड़ी को जीव अपने सत्पुरुषार्थ से तोड़ भी सकता है। इस कड़ी को तोड़ने के बाद, जीव (भावात्मक रूप से) लौकिक धरातल से ऊपर उठ कर अलौकिक बन जाता है ।
सम्पादकीय
'कर्म' एक बेड़ी है जो जीव को 'परतन्त्र' बनाए रखती है। परतन्त्रता भी इस सीमा तक कि जीव का उठना-बैठना, चलना-फिरना, सोना-जागना, सोचना-समझना, सुख-दुःख की अनुभूति, यहां तक कि जीना मरना भी अचेतन (भौतिक पुद्गल पदार्थ ) पर आश्रित है । आश्चर्य तो यह है कि यह कर्म रूपी बेड़ी स्वय जीव द्वारा निर्मित है ।
1
ज्यों हो प्राणी इस संसार में जन्म लेता है, परतन्त्रता भी साये की तरह पीछा करती हुई उसके साथ लगी रहती है । क्योंकि जीव ने अजीवात्मक शरीरादि को ममत्व-बुद्धि के कारण अपने से अभिन्न मान लिया है, और यह ममत्व बुद्धि तथा उसके द्वारा उत्पन्न अभेद-बुद्धि व अहंकार बुद्धि ही कर्म-बन्धन की कारण हैं। मन जैसे विचित्र कम्प्यूटर-नुमा अमूल्य यन्त्र तथा उसके अधीन आंखकान-नाक जैसी इन्द्रिय रूपी मशीन - इन सबसे सुसज्जित मानव शरीर भी चेतन आत्मा रूपी पक्षी के लिए एक पिंजरा मात्र है, एक कैदखाना है | शरीरधारी व्यक्ति को इस पिंजरे के प्रति स्वभावतः 'ममत्वभाव' उत्पन्न होता है, जो प्राणी के लिए कर्मबन्धन का बीज सिद्ध होता है। यह ममत्व ही आगे चल कर दुर्गति का कारण बनता है ।
जन्म लेते ही मानव-शिशु की इन्द्रियां बरबस उसकी आत्मा को भौतिक पदार्थों के प्रति आकृष्ट करती हैं, और इस प्रकार जीव का बाह्य पदार्थों से (ममत्व) सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाता है । व्यक्ति के संकल्पशील मन के सम्पर्क में आने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुएं उसे अनुकूल और कुछ प्रतिकूल प्रतीत होती हैं वस्तु स्वयं सुख-दुःखात्मकता से शून्य है, किन्तु व्यक्ति के ममत्वमूलक राग-द्वेष के कारण व्यक्ति को अनुकूल या प्रतिकूल अथवा सुखात्मक या दुःखात्मक प्रतीत होती है। अनुकूल के प्रति आकर्षण होता है, और प्रतिकूल के प्रति विकर्षण । अनुकूलता-प्रतिकूलता की श्रेणी से बाहर की वस्तु के प्रति उपेक्षणीय ( तटस्थ ) भाव रहता है। अनुकूल के प्रति जो आकर्षण है, वह 'राग' कहलाता है, तथा प्रतिकूल के प्रति जो विकर्षण है, वह 'द्वेष' के नाम से जाना जाता है । उक्त आकर्षण व विकर्षण की स्थिति में आत्मा मोहाविष्ट हो स्वरूपच्युत हो जाता है, और यहीं से उसके अधःपतन का क्रम प्रारम्भ हो जाता है ।
जिससे राग होता है, उसको अपने अधीन करने की इच्छा जागृत होती है। इस इच्छा की पूर्ति में जो पदार्थ सहायक प्रतीत होते हैं, उसके प्रति भी 'राग' भाव होने से, उसे भी प्राप्त करने की लालसा पैदा हो जाती है। उक्त सभी लालसाएं, तथा उनके मूल में रहने वाले मोह (अज्ञान), अहंकार, राग व द्वेष—ये सब मिलकर जीव में ऐसा परिणमन करना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे नई-नई कर्म की बेड़ियों का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है । जीव के वैयक्तिक मिथ्यात्वादि के कारण पुद्गल स्वयं कर्म रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, और कर्म के निमित्त से जीव में रागादि-परिणमन की परम्परा को बढ़ावा मिलता है। उक्त रागादि कषाय जीव में ऐसी चिकनाहट पैदा कर देते हैं जिससे कर्म परमाणुओं को जीव के साथ चिपकने में सरलता होती है। परिणामस्वरूप जीव व कर्म के एकक्षेषावगाह सम्बन्ध के साथ-साथ, विशिष्ट उपश्लेष- रूप सम्बन्ध दृढ़ होता चला जाता है, और बनने वाली कर्म-बेड़ियां जीव को परतन्त्रता की ओर धकेल जाती हैं। इस परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े प्राणी में राग-द्वेषात्मक परिणमन की सम्भावना अधिक हो जाती है, और इस प्रकार जीव की परतन्त्रता का सिलसिला जारी रहता है। बांधा गया 'कर्म', चाहे वह प्रशस्त हो या अप्रशस्त, बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता ।
जैन धर्म एवं आचार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१
www.jainelibrary.org