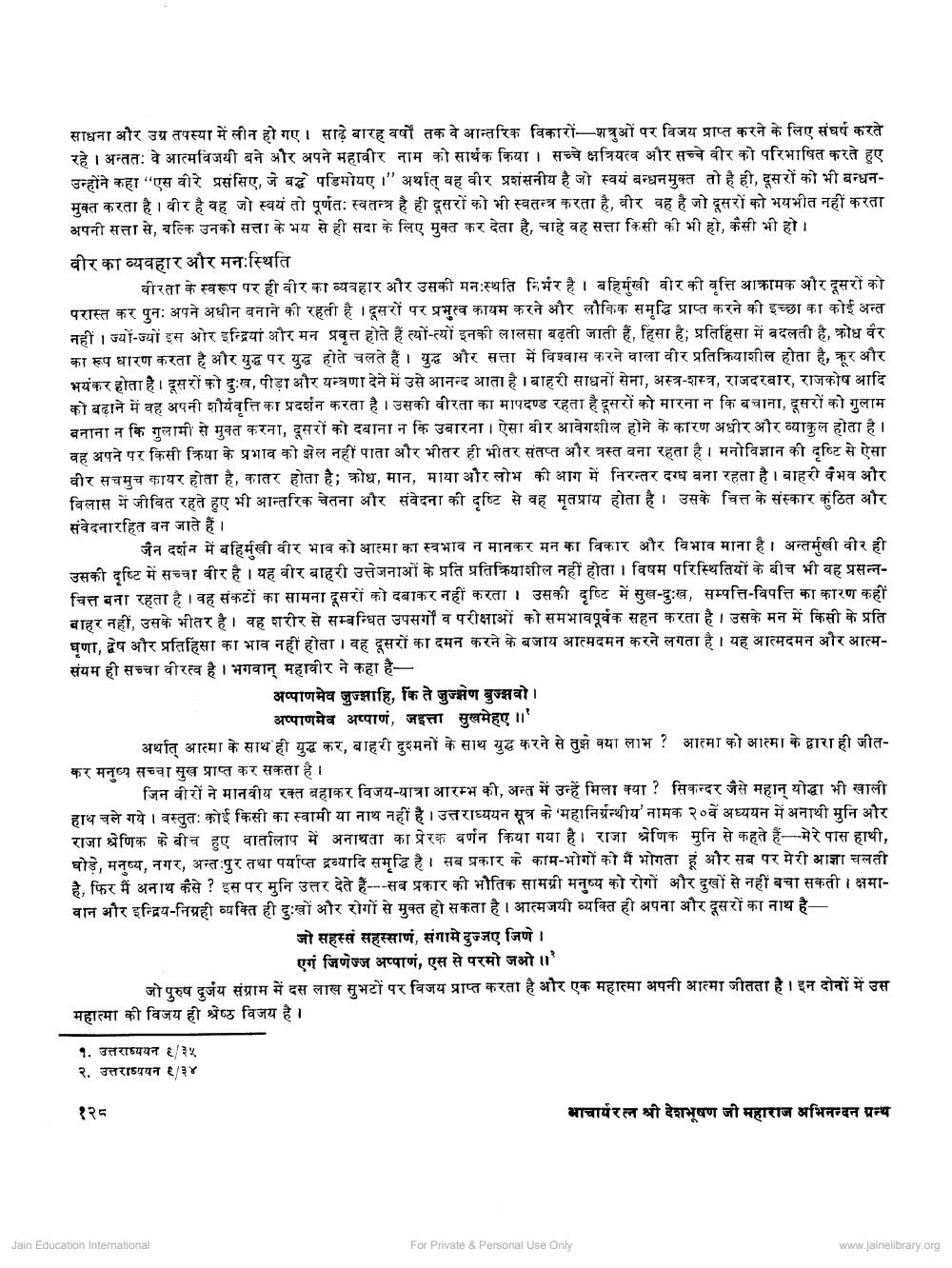________________
साधना और उग्र तपस्या में लीन हो गए। साढ़े बारह वर्षों तक वे आन्तरिक विकारों-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे । अन्ततः वे आत्मविजयी बने और अपने महावीर नाम को सार्थक किया। सच्चे क्षत्रियत्व और सच्चे वीर को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा “एस वीरे प्रसंसिए, जे बद्ध पडिमोयए।" अर्थात् वह वीर प्रशंसनीय है जो स्वयं बन्धन मुक्त तो है ही, दूसरों को भी बन्धनमुक्त करता है। वीर है वह जो स्वयं तो पूर्णतः स्वतन्त्र है ही दूसरों को भी स्वतन्त्र करता है, वीर वह है जो दूसरों को भयभीत नहीं करता अपनी सत्ता से, बल्कि उनको सत्ता के भय से ही सदा के लिए मुक्त कर देता है, चाहे वह सत्ता किसी की भी हो, कैसी भी हो। वीर का व्यवहार और मनःस्थिति
वीरता के स्वरूप पर ही वीर का व्यवहार और उसकी मनःस्थति निर्भर है। बहिर्मुखी बीर की वृत्ति आक्रामक और दूसरों को परास्त कर पुनः अपने अधीन बनाने की रहती है । दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और लौकिक समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा का कोई अन्त नहीं । ज्यों-ज्यों इस ओर इन्द्रियां और मन प्रवृत्त होते हैं त्यों-त्यों इनकी लालसा बढ़ती जाती हैं, हिंसा है। प्रतिहिंसा में बदलती है, क्रोध वैर का रूप धारण करता है और युद्ध पर युद्ध होते चलते हैं। युद्ध और सत्ता में विश्वास करने वाला वीर प्रतिक्रियाशील होता है, क्रूर और भयंकर होता है। दूसरों को दुःख, पीड़ा और यन्त्रणा देने में उसे आनन्द आता है । बाहरी साधनों सेना, अस्त्र-शस्त्र, राजदरबार, राजकोष आदि को बढ़ाने में वह अपनी शौर्यवृत्ति का प्रदर्शन करता है । उसकी वीरता का मापदण्ड रहता है दूसरों को मारना न कि बचाना, दूसरों को गुलाम बनाना न कि गुलामी से मुक्त करना, दूसरों को दबाना न कि उबारना । ऐसा वीर आवेगशील होने के कारण अधीर और व्याकुल होता है। वह अपने पर किसी क्रिया के प्रभाव को झेल नहीं पाता और भीतर ही भीतर संतप्त और त्रस्त बना रहता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐसा वीर सचमुच कायर होता है, कातर होता है; क्रोध, मान, माया और लोभ की आग में निरन्तर दग्ध बना रहता है। बाहरी वैभव और विलास में जीवित रहते हुए भी आन्तरिक चेतना और संवेदना की दृष्टि से वह मृतप्राय होता है। उसके चित्त के संस्कार कुंठित और संवेदनारहित बन जाते हैं।
जैन दर्शन में बहिर्मुखी वीर भाव को आत्मा का स्वभाव न मानकर मन का विकार और विभाव माना है। अन्तर्मुखी वीर ही उसकी दृष्टि में सच्चा वीर है । यह वीर बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होता। विषम परिस्थितियों के बीच भी वह प्रसन्नचित्त बना रहता है । वह संकटों का सामना दूसरों को दबाकर नहीं करता। उसकी दृष्टि में सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति का कारण कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर है। वह शरीर से सम्बन्धित उपसर्गों व परीक्षाओं को समभावपूर्वक सहन करता है । उसके मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष और प्रतिहिंसा का भाव नहीं होता । वह दूसरों का दमन करने के बजाय आत्मदमन करने लगता है। यह आत्मदमन और आत्मसंयम ही सच्चा वीरत्व है । भगवान् महावीर ने कहा है
अप्पाणमेव जुज्झाहि, कि ते जुज्झण बुज्झवो।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुखमेहए।' अर्थात् आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी दुश्मनों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ ? आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जीतकर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है।
जिन वीरों ने मानवीय रक्त बहाकर विजय-यात्रा आरम्भ की, अन्त में उन्हें मिला क्या ? सिकन्दर जैसे महान योद्धा भी खाली हाथ चले गये । वस्तुतः कोई किसी का स्वामी या नाथ नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र के 'महानिर्ग्रन्थीय' नामक २०वें अध्ययन में अनाथी मुनि और राजा श्रेणिक के बीच हुए वार्तालाप में अनाथता का प्रेरक वर्णन किया गया है। राजा श्रेणिक मुनि से कहते हैं---मेरे पास हाथी, घोड़े, मनुष्य, नगर, अन्तःपुर तथा पर्याप्त द्रव्यादि समृद्धि है। सब प्रकार के काम-भोगों को मैं भोगता हूं और सब पर मेरी आज्ञा चलती है, फिर मैं अनाथ कैसे? इस पर मुनि उत्तर देते हैं----सब प्रकार की भौतिक सामग्री मनुष्य को रोगों और दुखों से नहीं बचा सकती। क्षमावान और इन्द्रिय-निग्रही व्यक्ति ही दुःखों और रोगों से मुक्त हो सकता है । आत्मजयी व्यक्ति ही अपना और दूसरों का नाथ है
जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ।' जो पुरुष दुर्जय संग्राम में दस लाख सुभटों पर विजय प्राप्त करता है और एक महात्मा अपनी आत्मा जीतता है। इन दोनों में उस महात्मा की विजय ही श्रेष्ठ विजय है।
१. उत्तराध्ययन ६/३५ २. उत्तराध्ययन ६/३४
१२८
भाचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org