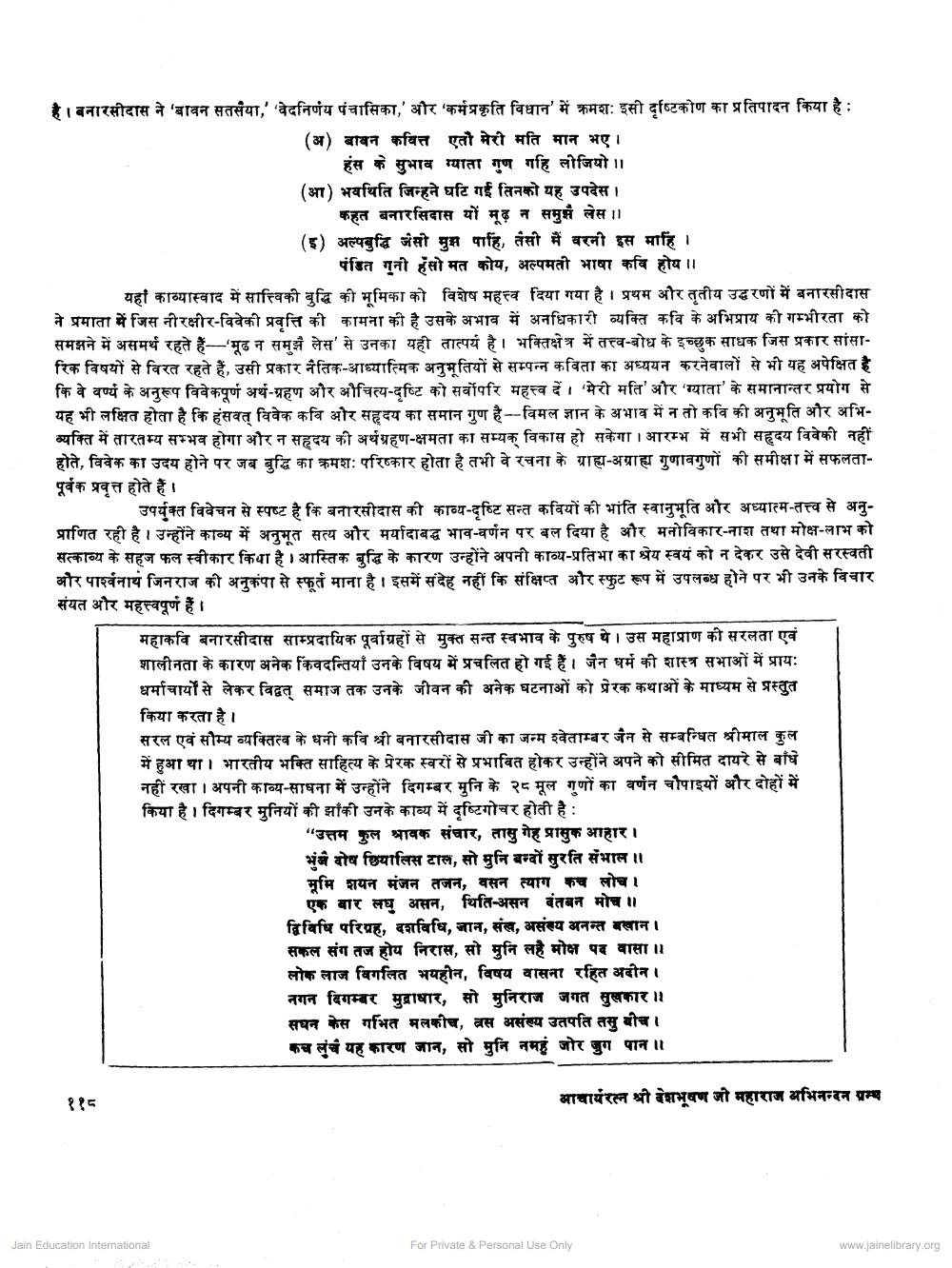________________
है। बनारसीदास ने 'बावन सतसया, 'वेदनिर्णय पंचासिका,' और 'कर्मप्रकृति विधान' में क्रमशः इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है:
(अ) बावन कवित्त एतो मेरी मति मान भए।
हंस के सुभाव ग्याता गुण गहि लीजियो। (आ) भवयिति जिन्हने घटि गई तिनको यह उपदेस ।
कहत बनारसिदास यों मूढ़ न समुझ लेस। (इ) अल्पबुद्धि जैसी मुझ पाहि, तैसी मैं वरनी इस माहि ।
पंडित गुनी हंसो मत कोय, अल्पमती भाषा कवि होय ।। यहाँ काव्यास्वाद में सात्त्विकी बुद्धि की भूमिका को विशेष महत्त्व दिया गया है । प्रथम और तृतीय उद्धरणों में बनारसीदास ने प्रमाता में जिस नीरक्षीर-विवेकी प्रवृत्ति की कामना की है उसके अभाव में अनधिकारी व्यक्ति कवि के अभिप्राय की गम्भीरता को समझने में असमर्थ रहते हैं—'मूढ न समुझे लेस' से उनका यही तात्पर्य है। भक्तिक्षेत्र में तत्त्व-बोध के इच्छुक साधक जिस प्रकार सांसारिक विषयों से विरत रहते हैं, उसी प्रकार नैतिक-आध्यात्मिक अनुभूतियों से सम्पन्न कविता का अध्ययन करनेवालों से भी यह अपेक्षित है कि वे वर्ण्य के अनुरूप विवेकपूर्ण अर्थ-ग्रहण और औचित्य-दृष्टि को सर्वोपरि महत्त्व दें। 'मेरी मति' और 'ग्याता' के समानान्तर प्रयोग से यह भी लक्षित होता है कि हंसवत् विवेक कवि और सहृदय का समान गुण है-विमल ज्ञान के अभाव में न तो कवि की अनुभूति और अभिव्यक्ति में तारतम्य सम्भव होगा और न सहृदय की अर्थग्रहण-क्षमता का सम्यक विकास हो सकेगा। आरम्भ में सभी सहृदय विवेकी नहीं होते, विवेक का उदय होने पर जब बुद्धि का क्रमशः परिष्कार होता है तभी वे रचना के ग्राह्य-अग्राह्य गुणावगुणों की समीक्षा में सफलतापूर्वक प्रवृत्त होते हैं।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बनारसीदास की काव्य-दृष्टि सन्त कवियों की भांति स्वानुभूति और अध्यात्म-तत्त्व से अनुप्राणित रही है । उन्होंने काव्य में अनुभूत सत्य और मर्यादाबद्ध भाव-वर्णन पर बल दिया है और मनोविकार-नाश तथा मोक्ष-लाभ को सत्काव्य के सहज फल स्वीकार किया है। आस्तिक बुद्धि के कारण उन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा का श्रेय स्वयं को न देकर उसे देवी सरस्वती और पार्श्वनाथ जिनराज की अनुकंपा से स्फूर्त माना है। इसमें संदेह नहीं कि संक्षिप्त और स्फुट रूप में उपलब्ध होने पर भी उनके विचार संयत और महत्त्वपूर्ण हैं।
महाकवि बनारसीदास साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त सन्त स्वभाव के पुरुष थे। उस महाप्राण की सरलता एवं शालीनता के कारण अनेक किंवदन्तियाँ उनके विषय में प्रचलित हो गई हैं। जैन धर्म की शास्त्र सभाओं में प्रायः धर्माचार्यों से लेकर विद्वत् समाज तक उनके जीवन की अनेक घटनाओं को प्रेरक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया करता है। सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी कवि श्री बनारसीदास जी का जन्म श्वेताम्बर जैन से सम्बन्धित श्रीमाल कुल में हुआ था। भारतीय भक्ति साहित्य के प्रेरक स्वरों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने को सीमित दायरे से बाँधे नहीं रखा । अपनी काव्य-साधना में उन्होंने दिगम्बर मुनि के २८ मूल गुणों का वर्णन चौपाइयों और दोहों में किया है। दिगम्बर मुनियों की झांकी उनके काव्य में दृष्टिगोचर होती है :
"उत्तम कुल श्रावक संचार, तासु गेह प्रासुक आहार। भुंजै दोष छियालिस टाल, सो मुनि बन्दों सुरति संभाल । भूमि शयन मंजन तजन, वसन त्याग कच लोच ।
एक बार लघु असन, थिति-असन बंतबन मोच ॥ विविधि परिग्रह, बशविधि, जान, संख, असंख्य अनन्त बखान । सकल संग तज होय निरास, सो मुनि लहै मोक्ष पद वासा॥ लोक लाज विगलित भयहीन, विषय वासना रहित अदीन । नगन दिगम्बर मुद्राधार, सो मुनिराज जगत सुखकार ॥ सघन केस गभित मलकीच, बस असंख्य उतपति तसु बीच । कच लुच यह कारण जान, सो मुनि नमहं जोर जुग पान ।
आचार्यरत्न श्री वेशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org