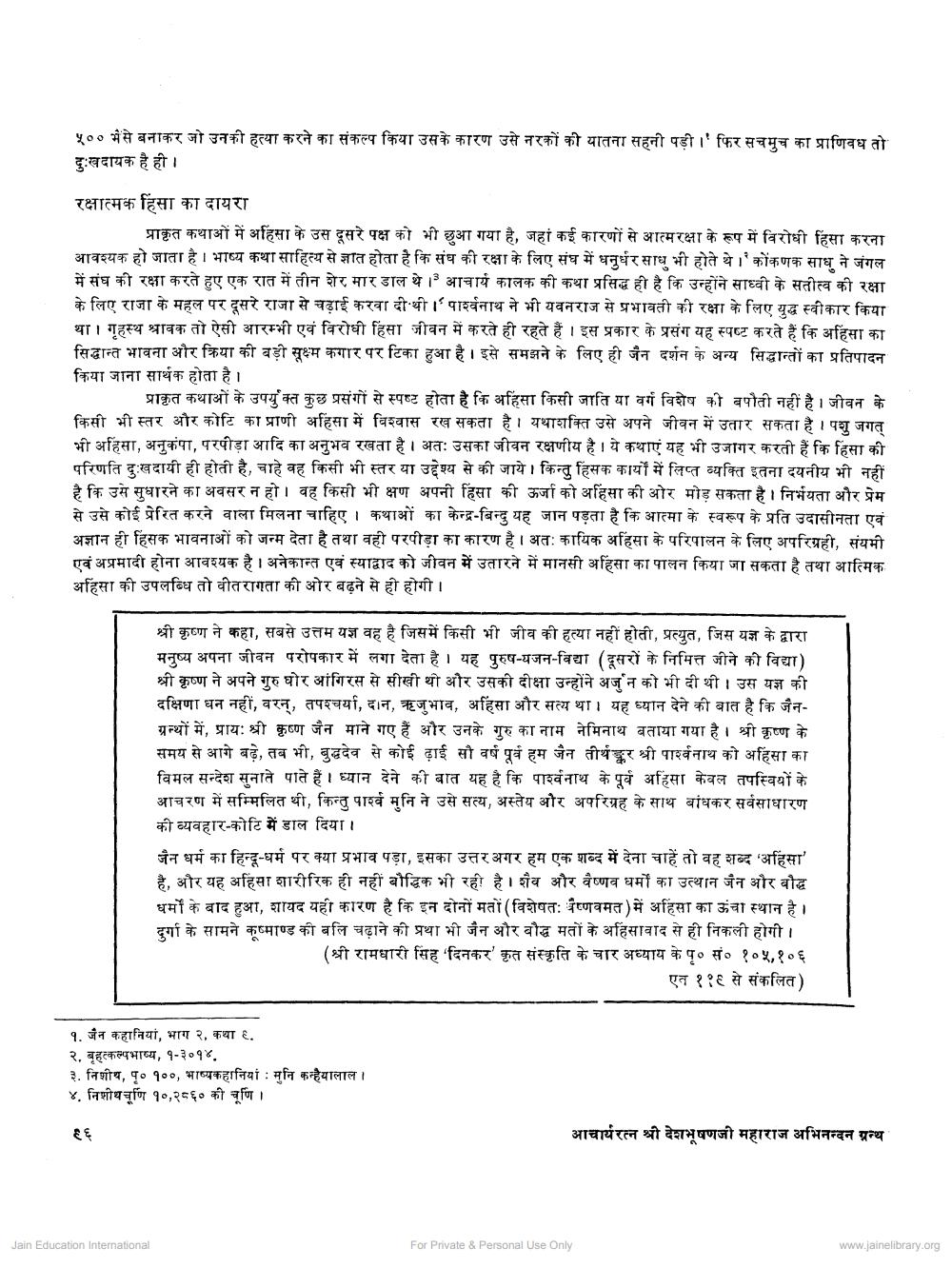________________
५०० भैसे बनाकर जो उनकी हत्या करने का संकल्प किया उसके कारण उसे नरकों की यातना सहनी पड़ी।' फिर सचमुच का प्राणिवध तो दुःखदायक है ही।
रक्षात्मक हिंसा का दायरा
प्राकृत कथाओं में अहिंसा के उस दूसरे पक्ष को भी छुआ गया है, जहां कई कारणों से आत्मरक्षा के रूप में विरोधी हिंसा करना आवश्यक हो जाता है । भाष्य कथा साहित्य से ज्ञात होता है कि संघ की रक्षा के लिए संघ में धनुर्धर साधु भी होते थे। कोंकणक साधु ने जंगल में संघ की रक्षा करते हुए एक रात में तीन शेर मार डाल थे। आचार्य कालक की कथा प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने साध्वी के सतीत्व की रक्षा के लिए राजा के महल पर दूसरे राजा से चढ़ाई करवा दी थी।' पार्श्वनाथ ने भी यवनराज से प्रभावती की रक्षा के लिए युद्ध स्वीकार किया था। गृहस्थ श्रावक तो ऐसी आरम्भी एवं विरोधी हिंसा जीवन में करते ही रहते हैं । इस प्रकार के प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि अहिंसा का सिद्धान्त भावना और क्रिया की बड़ी सूक्ष्म कगार पर टिका हुआ है । इसे समझने के लिए ही जैन दर्शन के अन्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाना सार्थक होता है।
प्राकृत कथाओं के उपर्युक्त कुछ प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि अहिंसा किसी जाति या वर्ग विशेष की बपौती नहीं है। जीवन के किसी भी स्तर और कोटि का प्राणी अहिंसा में विश्वास रख सकता है। यथाशक्ति उसे अपने जीवन में उतार सकता है । पशु जगत् भी अहिंसा, अनुकंपा, परपीड़ा आदि का अनुभव रखता है। अतः उसका जीवन रक्षणीय है । ये कथाएं यह भी उजागर करती हैं कि हिंसा की परिणति दुःखदायी ही होती है, चाहे वह किसी भी स्तर या उद्देश्य से की जाये। किन्तु हिंसक कार्यों में लिप्त व्यक्ति इतना दयनीय भी नहीं है कि उसे सुधारने का अवसर न हो। वह किसी भी क्षण अपनी हिंसा की ऊर्जा को अहिंसा की ओर मोड़ सकता है। निर्भयता और प्रेम से उसे कोई प्रेरित करने वाला मिलना चाहिए। कथाओं का केन्द्र-बिन्दु यह जान पड़ता है कि आत्मा के स्वरूप के प्रति उदासीनता एवं अज्ञान ही हिंसक भावनाओं को जन्म देता है तथा वही परपीड़ा का कारण है । अतः कायिक अहिंसा के परिपालन के लिए अपरिग्रही, संयमी एवं अप्रमादी होना आवश्यक है। अनेकान्त एवं स्याद्वाद को जीवन में उतारने में मानसी अहिंसा का पालन किया जा सकता है तथा आत्मिक अहिंसा की उपलब्धि तो वीतरागता की ओर बढ़ने से ही होगी।
श्री कृष्ण ने कहा, सबसे उत्तम यज्ञ वह है जिसमें किसी भी जीव की हत्या नहीं होती, प्रत्युत, जिस यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपना जीवन परोपकार में लगा देता है। यह पुरुष-यजन-विद्या (दूसरों के निमित्त जीने की विद्या) श्री कृष्ण ने अपने गुरु घोर आंगिरस से सीखी थी और उसकी दीक्षा उन्होंने अर्जुन को भी दी थी। उस यज्ञ की दक्षिणा धन नहीं, वरन्, तपश्चर्या, दान, ऋजुभाव, अहिंसा और सत्य था। यह ध्यान देने की बात है कि जैनग्रन्थों में, प्रायः श्री कृष्ण जैन माने गए हैं और उनके गुरु का नाम नेमिनाथ बताया गया है। श्री कृष्ण के समय से आगे बढ़े, तब भी, बुद्धदेव से कोई ढाई सौ वर्ष पूर्व हम जैन तीर्थङ्कर श्री पार्श्वनाथ को अहिंसा का विमल सन्देश सुनाते पाते हैं । ध्यान देने की बात यह है कि पार्श्वनाथ के पूर्व अहिंसा केवल तपस्वियों के आचरण में सम्मिलित थी, किन्तु पार्श्व मुनि ने उसे सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के साथ बांधकर सर्वसाधारण की व्यवहार-कोटि में डाल दिया। जैन धर्म का हिन्दू-धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर अगर हम एक शब्द में देना चाहें तो वह शब्द 'अहिंसा' है, और यह अहिंसा शारीरिक ही नहीं बौद्धिक भी रही है। शैव और वैष्णव धर्मों का उत्थान जैन और बौद्ध धर्मों के बाद हुआ, शायद यही कारण है कि इन दोनों मतों (विशेषत: वैष्णवमत) में अहिंसा का ऊंचा स्थान है। दुर्गा के सामने कूष्माण्ड की बलि चढ़ाने की प्रथा भी जैन और बौद्ध मतों के अहिंसावाद से ही निकली होगी। (श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' कृत संस्कृति के चार अध्याय के पृ० सं० १०५,१०६
एत ११६ से संकलित)
१. जैन कहानियां, भाग २, कथा ६. २. बृहत्कल्पभाष्य, १-३०१४. ३. निशीथ, पृ० १००, भाष्यकहानियां : मुनि कन्हैयालाल। ४. निशीथचूणि १०,२८६० की चूणि ।
आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org