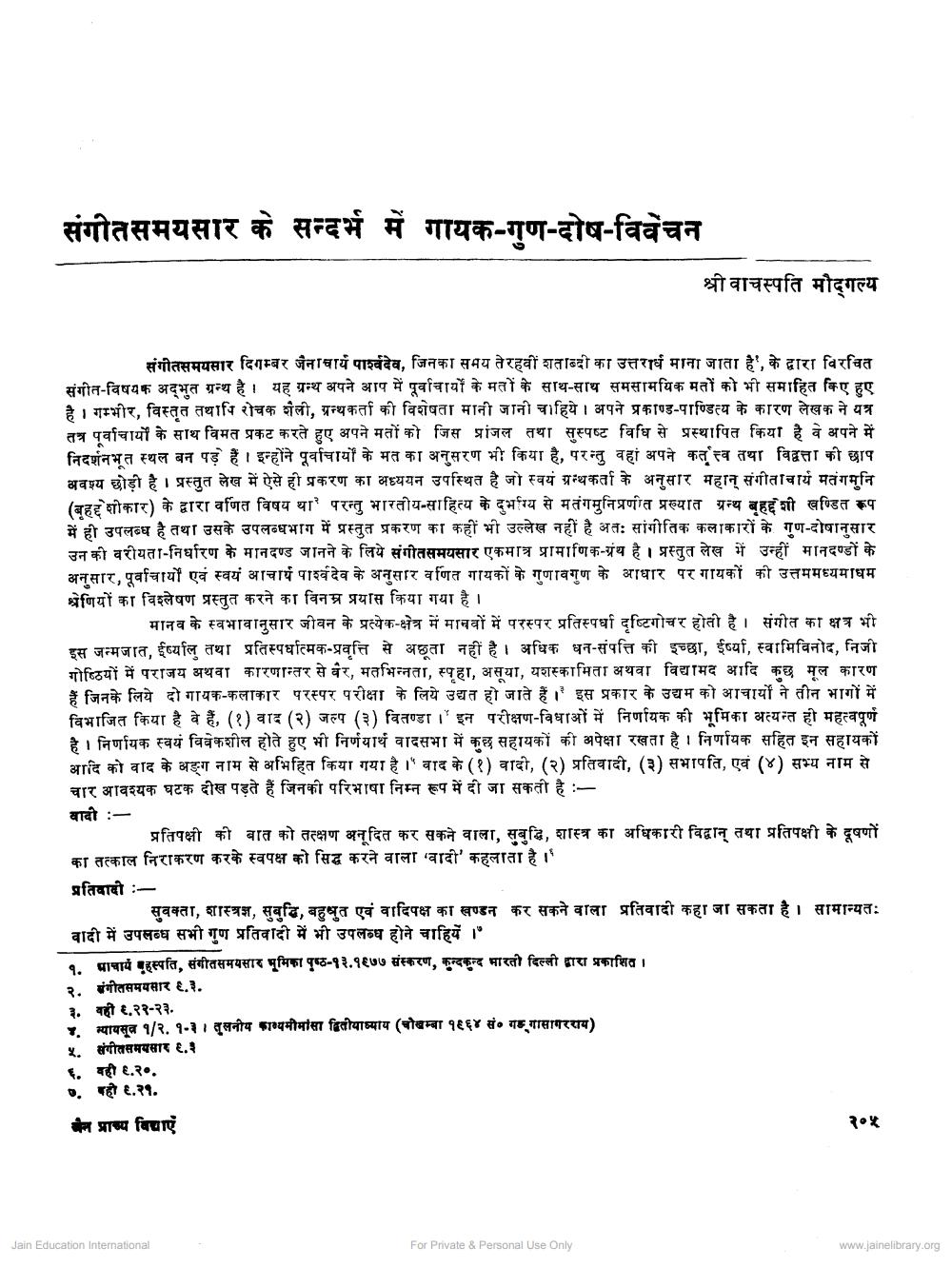________________
संगीतसमयसार के सन्दर्भ में गायक-गुण-दोष-विवेचन
श्री वाचस्पति मौदगल्य
संगीतसमयसार दिगम्बर जैनाचार्य पार्श्वदेव, जिनका समय तेरहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है', के द्वारा विरचित संगीत-विषयक अद्भुत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अपने आप में पूर्वाचार्यों के मतों के साथ-साथ समसामयिक मतों को भी समाहित किए हए है। गम्भीर, विस्तृत तथापि रोचक शैली, ग्रन्थकर्ता की विशेषता मानी जानी चाहिये । अपने प्रकाण्ड-पाण्डित्य के कारण लेखक ने यत्र तत्र पर्वाचार्यों के साथ विमत प्रकट करते हुए अपने मतों को जिस प्रांजल तथा सुस्पष्ट विधि से प्रस्थापित किया है वे अपने में निदर्शनभूत स्थल बन पड़े हैं। इन्होंने पूर्वाचार्यों के मत का अनुसरण भी किया है, परन्तु वहां अपने कर्तृत्त्व तथा विद्वत्ता की छाप अवश्य छोड़ी है । प्रस्तुत लेख में ऐसे ही प्रकरण का अध्ययन उपस्थित है जो स्वयं ग्रन्थकर्ता के अनुसार महान् संगीताचार्य मतंगमुनि (बह शोकार) के द्वारा वणित विषय था परन्तु भारतीय-साहित्य के दुर्भाग्य से मतंगमुनिप्रणीत प्रख्यात ग्रन्थ बहुद्देशी खण्डित रूप में ही उपलब्ध है तथा उसके उपलब्धभाग में प्रस्तुत प्रकरण का कहीं भी उल्लेख नहीं है अतः सांगीतिक कलाकारों के गुण-दोषानुसार उन की वरीयता-निर्धारण के मानदण्ड जानने के लिये संगीतसमयसार एकमात्र प्रामाणिक-ग्रंथ है। प्रस्तुत लेख में उन्हीं मानदण्डों के अनुसार, पूर्वाचार्यों एवं स्वयं आचार्य पार्श्वदेव के अनुसार वणित गायकों के गुणावगुण के आधार पर गायकों की उत्तममध्यमाधम श्रेणियों का विश्लेषण प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया गया है।
मानव के स्वभावानुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा दृष्टिगोचर होती है। संगीत का क्षत्र भी इस जन्मजात, ईर्ष्यालु तथा प्रतिस्पर्धात्मक-प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। अधिक धन-संपत्ति की इच्छा, ईर्ष्या, स्वामिविनोद, निजी गोष्ठियों में पराजय अथवा कारणान्तर से वैर, मतभिन्नता, स्पहा, असूया, यशस्कामिता अथवा विद्यामद आदि कुछ मूल कारण हैं जिनके लिये दो गायक-कलाकार परस्पर परीक्षा के लिये उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार के उद्यम को आचार्यों ने तीन भागों में विभाजित किया है वे हैं, (१) वाद (२) जल्प (३) वितण्डा । इन परीक्षण-विधाओं में निर्णायक की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । निर्णायक स्वयं विवेकशील होते हुए भी निर्णयार्थ वादसभा में कुछ सहायकों की अपेक्षा रखता है । निर्णायक सहित इन सहायकों आदि को वाद के अङ्ग नाम से अभिहित किया गया है। वाद के (१) वादी, (२) प्रतिवादी, (३) सभापति, एवं (४) सभ्य नाम से चार आवश्यक घटक दीख पड़ते हैं जिनकी परिभाषा निम्न रूप में दी जा सकती है :वादी :
प्रतिपक्षी की बात को तत्क्षण अनूदित कर सकने वाला, सुबुद्धि, शास्त्र का अधिकारी विद्वान् तथा प्रतिपक्षी के दूषणों का तत्काल निराकरण करके स्वपक्ष को सिद्ध करने वाला 'वादी' कहलाता है। प्रतिवादी :
सुवक्ता, शास्त्रज्ञ, सुबुद्धि, बहुश्रुत एवं वादिपक्ष का खण्डन कर सकने वाला प्रतिवादी कहा जा सकता है। सामान्यतः वादी में उपलब्ध सभी गुण प्रतिवादी में भी उपलब्ध होने चाहिये ।' १. प्राचार्य एहस्पति, संगीतसमयसार भूमिका पृष्ठ-१३.१९७७ संस्करण, कुन्दकुन्द भारती दिल्ली द्वारा प्रकाशित । २. संगीतसमयसार ६.३. ३. वही १.२२-२३. 1. न्यायसूत्र १/२. १.11 तुलनीय काव्यमीमांसा द्वितीयाध्याय (चौखम्बा १९६४ सं० गगासागरराय) ५. संगीतसमयसार . ६. वही ६.२.. .. बही ६.२१. बैन प्राच्य विद्याएं
२०५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org