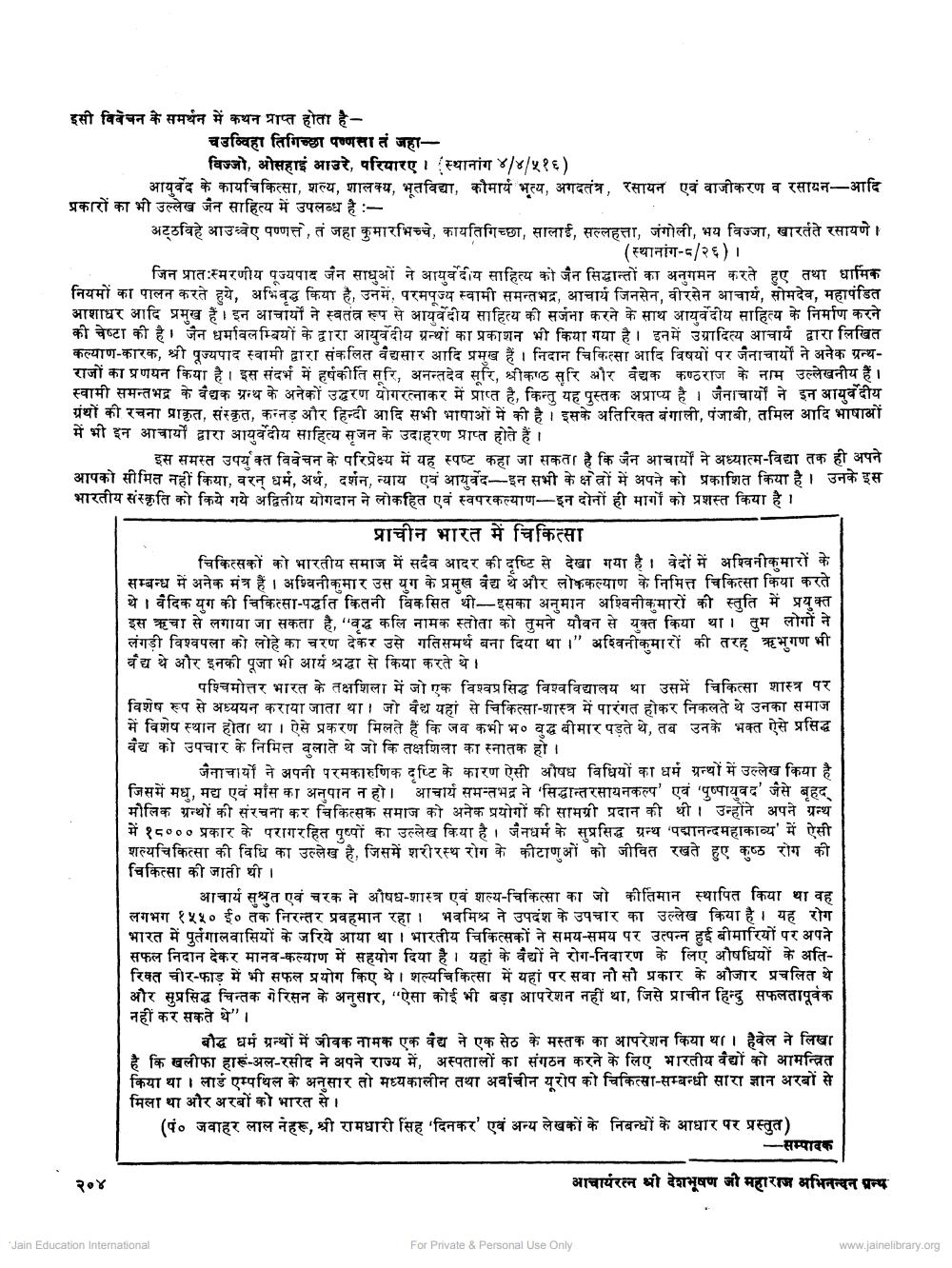________________
इसी विवेचन के समर्थन में कथन प्राप्त होता है
चउब्विहा तिगिच्छा पण्णता तं जहा
विज्जो, ओसहाई आउरे, परियारए। स्थानांग ४/४/५१६)
आयुर्वेद के कायचिकित्सा, शल्य, शालक्य, भूतविद्या, कौमार्य भत्य, अगदतंत्र, रसायन एवं वाजीकरण व रसायन-आदि प्रकारों का भी उल्लेख जैन साहित्य में उपलब्ध है :अट्ठविहे आउध्वेए पण्णत्ते, तं जहा कुमारभिच्चे, कायतिगिच्छा, सालाई, सल्लहत्ता, जंगोली, भय विज्जा, खारर्तते रसायणे।
(स्थानांग-८/२६) । जिन प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद जैन साधुओं ने आयुर्वेदीय साहित्य को जैन सिद्धान्तों का अनुगमन करते हुए तथा धार्मिक नियमों का पालन करते हुये, अभिवृद्ध किया है, उनमें, परमपूज्य स्वामी समन्तभद्र, आचार्य जिनसेन, वीरसेन आचार्य, सोमदेव, महापंडित आशाधर आदि प्रमुख हैं। इन आचार्यों ने स्वतंत्र रूप से आयर्वेदीय साहित्य की सर्जना करने के साथ आयर्वेदीय साहित्य के निर्माण करने की चेष्टा की है। जैन धर्मावलम्बियों के द्वारा आयुर्वेदीय ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया गया है। इनमें उग्रादित्य आचार्य द्वारा लिखित कल्याण-कारक, श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा संकलित वैद्यसार आदि प्रमुख हैं। निदान चिकित्सा आदि विषयों पर जैनाचार्यों ने अनेक ग्रन्थराजों का प्रणयन किया है। इस संदर्भ में हर्षकीति सरि, अनन्तदेव सरि, श्रीकण्ठ सरि और वैद्यक कण्ठराज के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वामी समन्तभद्र के वैद्यक ग्रन्थ के अनेकों उद्धरण योगरत्नाकर में प्राप्त है, किन्तु यह पुस्तक अप्राप्य है । जैनाचार्यों ने इन आयुर्वेदीय ग्रंथों की रचना प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ और हिन्दी आदि सभी भाषाओं में की है। इसके अतिरिक्त बंगाली, पंजाबी, तमिल आदि भाषाओं में भी इन आचार्यों द्वारा आयुर्वेदीय साहित्य सृजन के उदाहरण प्राप्त होते हैं।
इस समस्त उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जैन आचार्यों ने अध्यात्म-विद्या तक ही अपने आपको सीमित नहीं किया, वरन धर्म, अर्थ, दर्शन, न्याय एवं आयर्वेद--इन सभी के क्षेत्रों में अपने को प्रकाशित किया है। उनके इस भारतीय संस्कृति को किये गये अद्वितीय योगदान ने लोकहित एवं स्वपरकल्याण-इन दोनों ही मार्गों को प्रशस्त किया है।
प्राचीन भारत में चिकित्सा चिकित्सकों को भारतीय समाज में सदैव आदर की दृष्टि से देखा गया है। वेदों में अश्विनीकुमारों के सम्बन्ध में अनेक मंत्र हैं। अश्विनीकुमार उस युग के प्रमुख वैद्य थे और लोककल्याण के निमित्त चिकित्सा किया करते थे। वैदिक युग की चिकित्सा-पद्धति कितनी विकसित थी-इसका अनुमान अश्विनीकुमारों की स्तुति में प्रयुक्त इस ऋचा से लगाया जा सकता है, "वृद्ध कलि नामक स्तोता को तुमने यौवन से युक्त किया था। तुम लोगों ने लंगड़ी विश्वपला को लोहे का चरण देकर उसे गतिसमर्थ बना दिया था।" अश्विनीकुमारों की तरह ऋभुगण भी वंद्य थे और इनकी पूजा भी आर्य श्रद्धा से किया करते थे।
पश्चिमोत्तर भारत के तक्षशिला में जो एक विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय था उसमें चिकित्सा शास्त्र पर विशेष रूप से अध्ययन कराया जाता था। जो वैध यहां से चिकित्सा-शास्त्र में पारंगत होकर निकलते थे उनका समाज में विशेष स्थान होता था। ऐसे प्रकरण मिलते हैं कि जब कभी भ० बुद्ध बीमार पड़ते थे, तब उनके भक्त ऐसे प्रसिद्ध वैद्य को उपचार के निमित्त बुलाते थे जो कि तक्षशिला का स्नातक हो ।
जैनाचार्यों ने अपनी परमकारुणिक दष्टि के कारण ऐसी औषध विधियों का धर्म ग्रन्थों में उल्लेख किया है जिसमें मधु, मद्य एवं मांस का अनुपान न हो। आचार्य समन्तभद्र ने 'सिद्धान्तरसायनकल्प' एवं 'पुष्पायुवद' जैसे बृहद मौलिक ग्रन्थों की संरचना कर चिकित्सक समाज को अनेक प्रयोगों की सामग्री प्रदान की थी। उन्होंने अपने ग्रन्थ में १८००० प्रकार के परागरहित पूष्पों का उल्लेख किया है। जैनधर्म के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'पद्मानन्दमहाकाव्य' में ऐसी शल्यचिकित्सा की विधि का उल्लेख है, जिसमें शरीरस्थ रोग के कीटाणुओं को जीवित रखते हुए कुष्ठ रोग की चिकित्सा की जाती थी।
आचार्य सुश्रुत एवं चरक ने औषध-शास्त्र एवं शल्य-चिकित्सा का जो कीर्तिमान स्थापित किया था वह लगभग १५५० ई० तक निरन्तर प्रवहमान रहा। भवमिश्र ने उपदंश के उपचार का उल्लेख किया है। यह रोग भारत में पुर्तगालवासियों के जरिये आया था। भारतीय चिकित्सकों ने समय-समय पर उत्पन्न हुई बीमारियों पर अपने सफल निदान देकर मानव-कल्याण में सहयोग दिया है। यहां के वैद्यों ने रोग-निवारण के लिए औषधियों के अतिरिक्त चीर-फाड़ में भी सफल प्रयोग किए थे। शल्यचिकित्सा में यहां पर सवा नौ सौ प्रकार के औजार प्रचलित थे और सुप्रसिद्ध चिन्तक गेरिसन के अनुसार, "ऐसा कोई भी बड़ा आपरेशन नहीं था, जिसे प्राचीन हिन्दु सफलतापूर्वक नहीं कर सकते थे"।
बौद्ध धर्म ग्रन्थों में जीवक नामक एक वैद्य ने एक सेठ के मस्तक का आपरेशन किया था। हैवेल ने लिखा है कि खलीफा हारूं-अल-रसीद ने अपने राज्य में, अस्पतालों का संगठन करने के लिए भारतीय वैद्यों को आमन्त्रित किया था। लार्ड एम्पथिल के अनुसार तो मध्यकालीन तथा अर्वाचीन यूरोप को चिकित्सा-सम्बन्धी सारा ज्ञान अरबों से मिला था और अरबों को भारत से। (पं. जवाहर लाल नेहरू, श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' एवं अन्य लेखकों के निबन्धों के आधार पर प्रस्तुत)
-सम्पादक
२०४
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन अन्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org