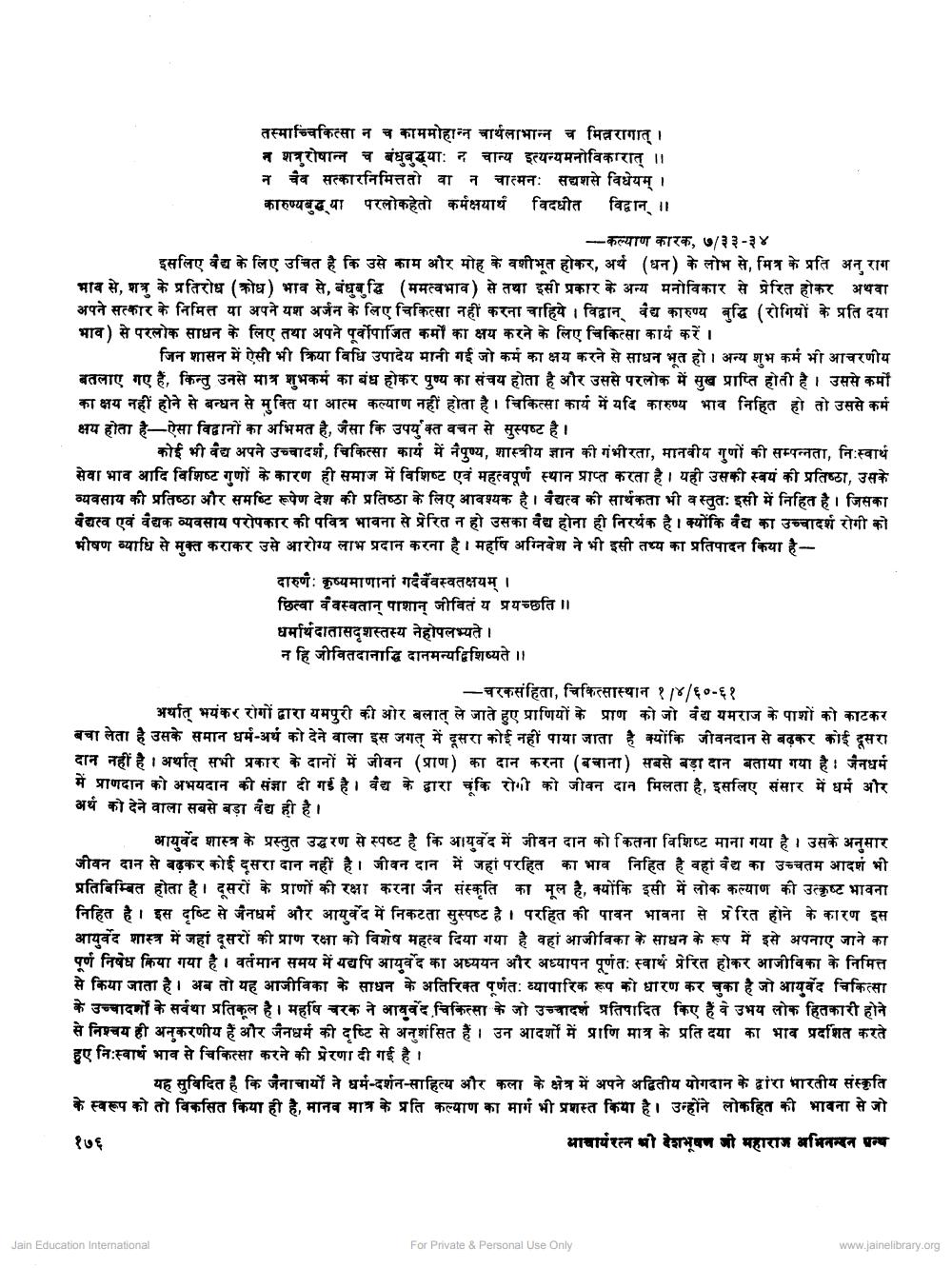________________
तस्माच्चकित्सा न च काममोहान्न पार्यलाभान्न च मित्ररागात् ।
न शत्रुरोषान्न च न चान्य इत्यन्यमनोविकारात् ॥ न चैव सत्कारनिमित्ततो वा न चात्मनः सद्यशसे विधेयम् । कारुण्यबुद्धया परलोकहेतो कर्मक्षयार्थं विदधीत विद्वान् ॥
- कल्याण कारक, ७/३३-३४
इसलिए बंध के लिए उचित है कि उसे काम और मोह के वशीभूत होकर अर्थ (धन) के लोभ से मित्र के प्रति अनुराग भाव से, शत्रु के प्रतिरोध (क्रोध) भाव से, बंधुबुद्धि ( ममत्वभाव) से तथा इसी प्रकार के अन्य मनोविकार से प्रेरित होकर अथवा अपने सत्कार के निमित्त या अपने यश अर्जन के लिए चिकित्सा नहीं करना चाहिये। विद्वान वैद्य कारुण्य बुद्धि ( रोगियों के प्रति दया भाव) से परलोक साधन के लिए तथा अपने पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए चिकित्सा कार्य करें ।
जिन शासन में ऐसी भी क्रिया विधि उपादेय मानी गई जो कर्म का क्षय करने से साधन भूत हो । अन्य शुभ कर्म भी आचरणीय बतलाए गए हैं, किन्तु उनसे मात्र शुभकर्म का बंध होकर पुण्य का संचय होता है और उससे परलोक में सुख प्राप्ति होती है। उससे कर्मों का क्षय नहीं होने से बन्धन से मुक्ति या आत्म कल्याण नहीं होता है। चिकित्सा कार्य में यदि कारुण्य भाव निहित हो तो उससे कर्म अप होता है—ऐसा विद्वानों का अभिमत है, जैसा कि उपर्युक्त वचन से सुस्पष्ट है।
कोई भी वंद्य अपने उच्चादर्श, चिकित्सा कार्य में नैपुण्य, शास्त्रीय ज्ञान की गंभीरता, मानवीय गुणों की सम्पन्नता, निःस्वार्थ सेवा भाव आदि विशिष्ट गुणों के कारण ही समाज में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है । यही उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा, उसके व्यवसाय की प्रतिष्ठा और समष्टि रूपेण देश की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है । वैद्यत्व की सार्थकता भी वस्तुतः इसी में निहित है। जिसका वैद्यस्व एवं वैद्यक व्यवसाय परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित न हो उसका वैद्य होना ही निरर्थक है। क्योंकि वैद्य का उच्चादर्श रोगी को भीषण व्याधि से मुक्त कराकर उसे आरोग्य लाभ प्रदान करना है। महर्षि अग्निवेश ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है
दारुणः कृष्यमाणानां गर्दैवस्वतक्षयम् । छित्वा वैवस्वतान् पाशान् जीवित व प्रयच्छति ।। धर्माविंदातासदृशस्तस्य नेहोपलभ्यते । न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यते ॥
परकसंहिता चिकित्सास्थान १/४/६०-६१
अर्थात् भयंकर रोगों द्वारा यमपुरी की ओर बलात् ले जाते हुए प्राणियों के प्राण को जो वंद्य यमराज के पाशों को काटकर बचा लेता है उसके समान धर्म-अर्थ को देने वाला इस जगत् में दूसरा कोई नहीं पाया जाता है क्योंकि जीवनदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है । अर्थात् सभी प्रकार के दानों में जीवन (प्राण) का दान करना ( बचाना) सबसे बड़ा दान बताया गया है। जैनधर्म में प्राणदान को अभयदान की संज्ञा दी गई है । वैद्य के द्वारा चूंकि रोगी को जीवन दान मिलता है, इसलिए संसार में धर्म और अर्थ को देने वाला सबसे बड़ा वैद्य ही है।
आयुर्वेद शास्त्र के प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि आयुर्वेद में जीवन दान को कितना विशिष्ट माना गया है। उसके अनुसार जीवन दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है । जीवन दान में जहां परहित का भाव निहित है वहां वैद्य का उच्चतम आदर्श भी प्रतिबिम्बित होता है। दूसरों के प्राणों की रक्षा करना जैन संस्कृति का मूल है, क्योंकि इसी में लोक कल्याण की उत्कृष्ट भावना निहित है । इस दृष्टि से जैनधर्म और आयुर्वेद में निकटता सुस्पष्ट है । परहित की पावन भावना से प्रेरित होने के कारण इस आयुर्वेद शास्त्र में जहां दूसरों की प्राण रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है वहां आजीविका के साधन के रूप में इसे अपनाए जाने का पूर्ण निषेध किया गया है। वर्तमान समय में यद्यपि आयुर्वेद का अध्ययन और अध्यापन पूर्णतः स्वायं प्रेरित होकर आजीविका के निमित्त से किया जाता है। अब तो यह आजीविका के साधन के अतिरिक्त पूर्णतः व्यापारिक रूप को धारण कर चुका है जो आयुर्वेद चिकित्सा के उच्चादर्शो के सर्वथा प्रतिकूल है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा के जो उच्चादर्श प्रतिपादित किए हैं वे उभय लोक हितकारी होने से निश्चय ही अनुकरणीय है और जैनधर्म की दृष्टि से अनुशंसित हैं। उन आदशों में प्राणि मात्र के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करते हुए निःस्वार्थ भाव से चिकित्सा करने की प्रेरणा दी गई है।
Jain Education International
यह सुविदित है कि जैनाचार्यों ने धर्म-दर्शन-साहित्य और कला के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के द्वारा भारतीय संस्कृति के स्वरूप को तो विकसित किया ही है, मानव मात्र के प्रति कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने लोकहित की भावना से जो
१७६
आचार्य रत्न को देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org