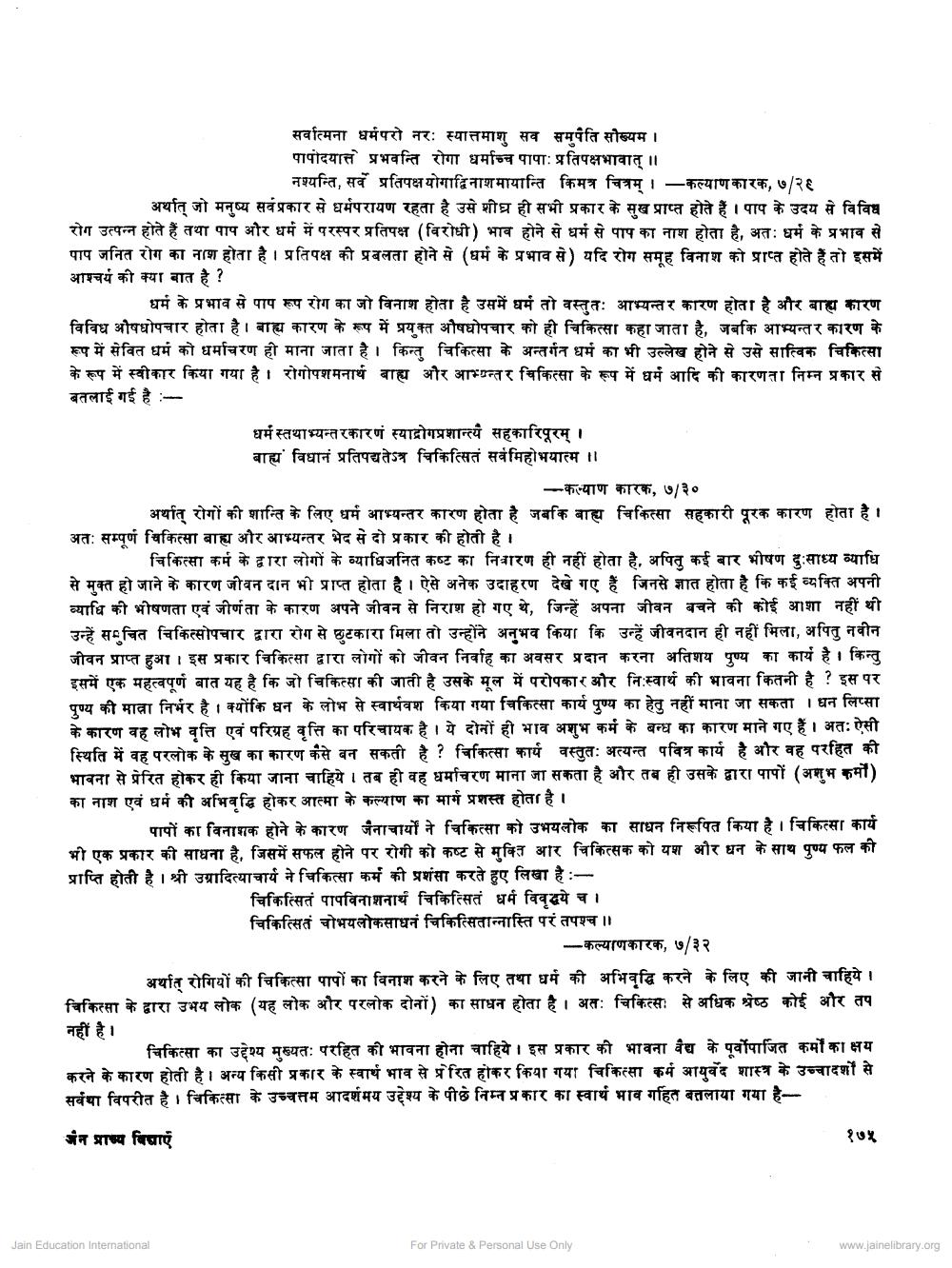________________
सर्वात्मना धर्मपरो नरः स्यात्तमाशु सव समुपैति सौख्यम। पापोदयात प्रभवन्ति रोगा धर्माच्च पापाः प्रतिपक्षभावात् ।।
नश्यन्ति, सर्व प्रतिपक्ष योगाद्विनाशमायान्ति किमत्र चित्रम् । -कल्याण कारक, ७/२६ अर्थात् जो मनुष्य सर्वप्रकार से धर्मपरायण रहता है उसे शीघ्र ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । पाप के उदय से विविध रोग उत्पन्न होते हैं तथा पाप और धर्म में परस्पर प्रतिपक्ष (विरोधी) भाव होने से धर्म से पाप का नाश होता है, अतः धर्म के प्रभाव से पाप जनित रोग का नाश होता है । प्रतिपक्ष की प्रबलता होने से (धर्म के प्रभाव से) यदि रोग समूह विनाश को प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?
धर्म के प्रभाव से पाप रूप रोग का जो विनाश होता है उसमें धर्म तो वस्तुतः आभ्यन्तर कारण होता है और बाह्य कारण विविध औषधोपचार होता है। बाह्य कारण के रूप में प्रयुक्त औषधोपचार को ही चिकित्सा कहा जाता है, जबकि आभ्यन्तर कारण के रूप में सेवित धर्म को धर्माचरण ही माना जाता है। किन्तु चिकित्सा के अन्तर्गत धर्म का भी उल्लेख होने से उसे सात्विक चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया गया है। रोगोपशमनार्थ बाह्य और आभ्यन्तर चिकित्सा के रूप में धर्म आदि की कारणता निम्न प्रकार से बतलाई गई है :
धर्म स्तथाभ्यन्तरकारणं स्याद्रोगप्रशान्त्य सहकारिपूरम् । बाह्य विधानं प्रतिपद्यतेऽत्र चिकित्सितं सर्वमिहोभयात्म ।।
-कल्याण कारक, ७/३० अर्थात् रोगों की शान्ति के लिए धर्म आभ्यन्तर कारण होता है जबकि बाह्य चिकित्सा सहकारी पूरक कारण होता है। अतः सम्पूर्ण चिकित्सा बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार की होती है।
चिकित्सा कर्म के द्वारा लोगों के व्याधिजनित कष्ट का निवारण ही नहीं होता है, अपितु कई बार भीषण दुःसाध्य व्याधि से मुक्त हो जाने के कारण जीवन दान भी प्राप्त होता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कई व्यक्ति अपनी व्याधि की भीषणता एवं जीर्णता के कारण अपने जीवन से निराश हो गए थे, जिन्हें अपना जीवन बचने की कोई आशा नहीं थी उन्हें समुचित चिकित्सोपचार द्वारा रोग से छुटकारा मिला तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें जीवनदान ही नहीं मिला, अपितु नवीन जीवन प्राप्त हुआ। इस प्रकार चिकित्सा द्वारा लोगों को जीवन निर्वाह का अवसर प्रदान करना अतिशय पुण्य का कार्य है। किन्तु इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिकित्सा की जाती है उसके मूल में परोपकार और निःस्वार्थ की भावना कितनी है ? इस पर पूण्य की मात्रा निर्भर है। क्योंकि धन के लोभ से स्वार्थवश किया गया चिकित्सा कार्य पुण्य का हेतु नहीं माना जा सकता । धन लिप्सा के कारण वह लोभ वृत्ति एवं परिग्रह वृत्ति का परिचायक है। ये दोनों ही भाव अशुभ कर्म के बन्ध का कारण माने गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में वह परलोक के सुख का कारण कैसे बन सकती है ? चिकित्सा कार्य वस्तुतः अत्यन्त पवित्र कार्य है और वह परहित की भावना से प्रेरित होकर ही किया जाना चाहिये । तब ही वह धर्माचरण माना जा सकता है और तब ही उसके द्वारा पापों (अशुभ कर्मों) का नाश एवं धर्म की अभिवृद्धि होकर आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।
पापों का विनाशक होने के कारण जैनाचार्यों ने चिकित्सा को उभयलोक का साधन निरूपित किया है । चिकित्सा कार्य भी एक प्रकार की साधना है, जिसमें सफल होने पर रोगी को कष्ट से मुक्ति आर चिकित्सक को यश और धन के साथ पुण्य फल की प्राप्ति होती है । श्री उग्रादित्याचार्य ने चिकित्सा कर्म की प्रशंसा करते हुए लिखा है :
चिकित्सितं पापविनाशनार्थ चिकित्सितं धर्म विवृद्धये च । चिकित्सितं चोभयलोकसाधनं चिकित्सितान्नास्ति परं तपश्च ।।
-कल्याणकारक, ७/३२ अर्थात् रोगियों की चिकित्सा पापों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए की जानी चाहिये । चिकित्सा के द्वारा उभय लोक (यह लोक और परलोक दोनों) का साधन होता है। अत: चिकित्सः से अधिक श्रेष्ठ कोई और तप नहीं है।
चिकित्सा का उद्देश्य मुख्यतः परहित की भावना होना चाहिये । इस प्रकार की भावना वैद्य के पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय करने के कारण होती है। अन्य किसी प्रकार के स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर किया गया चिकित्सा कर्म आयुर्वेद शास्त्र के उच्चादों से सर्वथा विपरीत है। चिकित्सा के उच्चत्तम आदर्शमय उद्देश्य के पीछे निम्न प्रकार का स्वार्थ भाव गहित बतलाया गया है
जन प्राच्य विधाएं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org