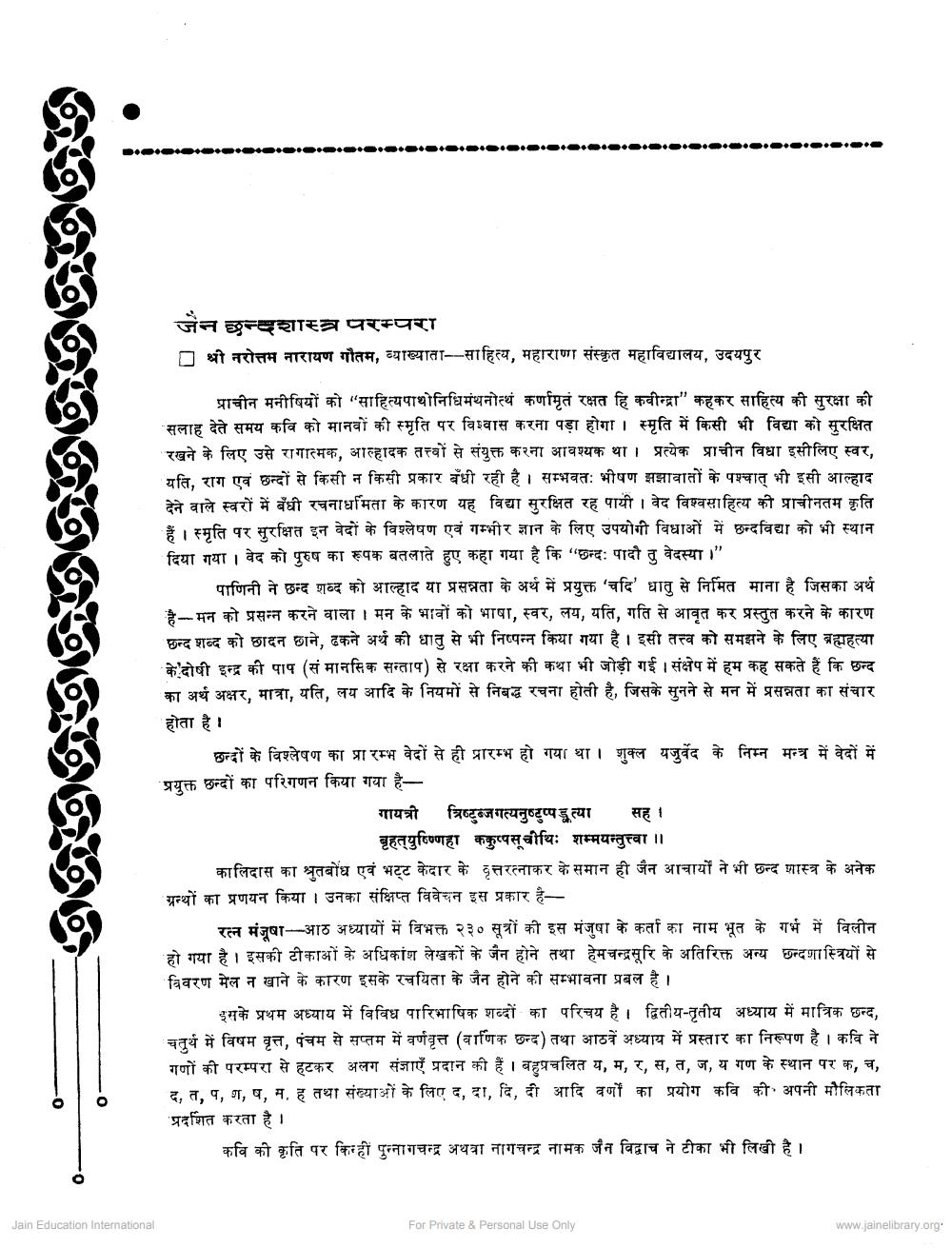________________
..
-
.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-.
-
.
-.
जैन छन्दशास्त्र परम्परा 0 श्री नरोत्तम नारायण गौतम, व्याख्याता-साहित्य, महाराणा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर
प्राचीन मनीषियों को “साहित्यपाथोनिधिमंथनोत्थं कर्णामृतं रक्षत हि कवीन्द्रा" कहकर साहित्य की सुरक्षा की सलाह देते समय कवि को मानवों की स्मृति पर विश्वास करना पड़ा होगा। स्मृति में किसी भी विद्या को सुरक्षित रखने के लिए उसे रागात्मक, आल्हादक तत्त्वों से संयुक्त करना आवश्यक था। प्रत्येक प्राचीन विधा इसीलिए स्वर, यति, राग एवं छन्दों से किसी न किसी प्रकार बँधी रही है। सम्भवत: भीषण झझावातों के पश्चात् भी इसी आल्हाद देने वाले स्वरों में बँधी रचनाधर्मिता के कारण यह विद्या सुरक्षित रह पायी । वेद विश्वसाहित्य की प्राचीनतम कृति हैं। स्मृति पर सुरक्षित इन वेदों के विश्लेषण एवं गम्भीर ज्ञान के लिए उपयोगी विधाओं में छन्दविद्या को भी स्थान दिया गया । वेद को पुरुष का रूपक बतलाते हुए कहा गया है कि "छन्दः पादौ तु वेदस्या।"
पाणिनी ने छन्द शब्द को आल्हाद या प्रसन्नता के अर्थ में प्रयुक्त 'चदि' धातु से निर्मित माना है जिसका अर्थ है-मन को प्रसन्न करने वाला । मन के भावों को भाषा, स्वर, लय, यति, गति से आवृत कर प्रस्तुत करने के कारण छन्द शब्द को छादन छाने, ढकने अर्थ की धातु से भी निष्पन्न किया गया है। इसी तत्त्व को समझने के लिए ब्रह्महत्या के दोषी इन्द्र की पाप (सं मानसिक सन्ताप) से रक्षा करने की कथा भी जोड़ी गई । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छन्द का अर्थ अक्षर, मात्रा, यति, लय आदि के नियमों से निबद्ध रचना होती है, जिसके सुनने से मन में प्रसन्नता का संचार होता है।
छन्दों के विश्लेषण का प्रारम्भ वेदों से ही प्रारम्भ हो गया था। शुक्ल यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में वेदों में प्रयुक्त छन्दों का परिगणन किया गया है
गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप्पङ्कत्या सह ।
बृहत्युष्ण्णिहा ककुप्पसूचीथिः शम्मयन्तुत्त्वा ॥ कालिदास का श्रुतबोध एवं भट्ट केदार के वृत्तरत्नाकर के समान ही जैन आचार्यों ने भी छन्द शास्त्र के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया। उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है
रत्न मंजूषा-आठ अध्यायों में विभक्त २३० सूत्रों की इस मंजुषा के कर्ता का नाम भूत के गर्भ में विलीन हो गया है। इसकी टीकाओं के अधिकांश लेखकों के जैन होने तथा हेमचन्द्रसूरि के अतिरिक्त अन्य छन्दशास्त्रियों से विवरण मेल न खाने के कारण इसके रचयिता के जैन होने की सम्भावना प्रबल है।
इसके प्रथम अध्याय में विविध पारिभाषिक शब्दों का परिचय है। द्वितीय-तृतीय अध्याय में मात्रिक छन्द, चतुर्थ में विषम वृत्त, पंचम से सप्तम में वर्णवृत्त (वाणिक छन्द) तथा आठवें अध्याय में प्रस्तार का निरूपण है। कवि ने गणों की परम्परा से हटकर अलग संज्ञाएँ प्रदान की हैं । बहुप्रचलित य, म, र, स, त, ज, य गण के स्थान पर क, च, द, त, प, श, ष, म, ह तथा संख्याओं के लिए द, दा, दि, दी आदि वर्गों का प्रयोग कवि की अपनी मौलिकता प्रदर्शित करता है।
कवि की कृति पर किन्हीं पुन्नागचन्द्र अथवा नागचन्द्र नामक जैन विद्वाच ने टीका भी लिखी है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org: