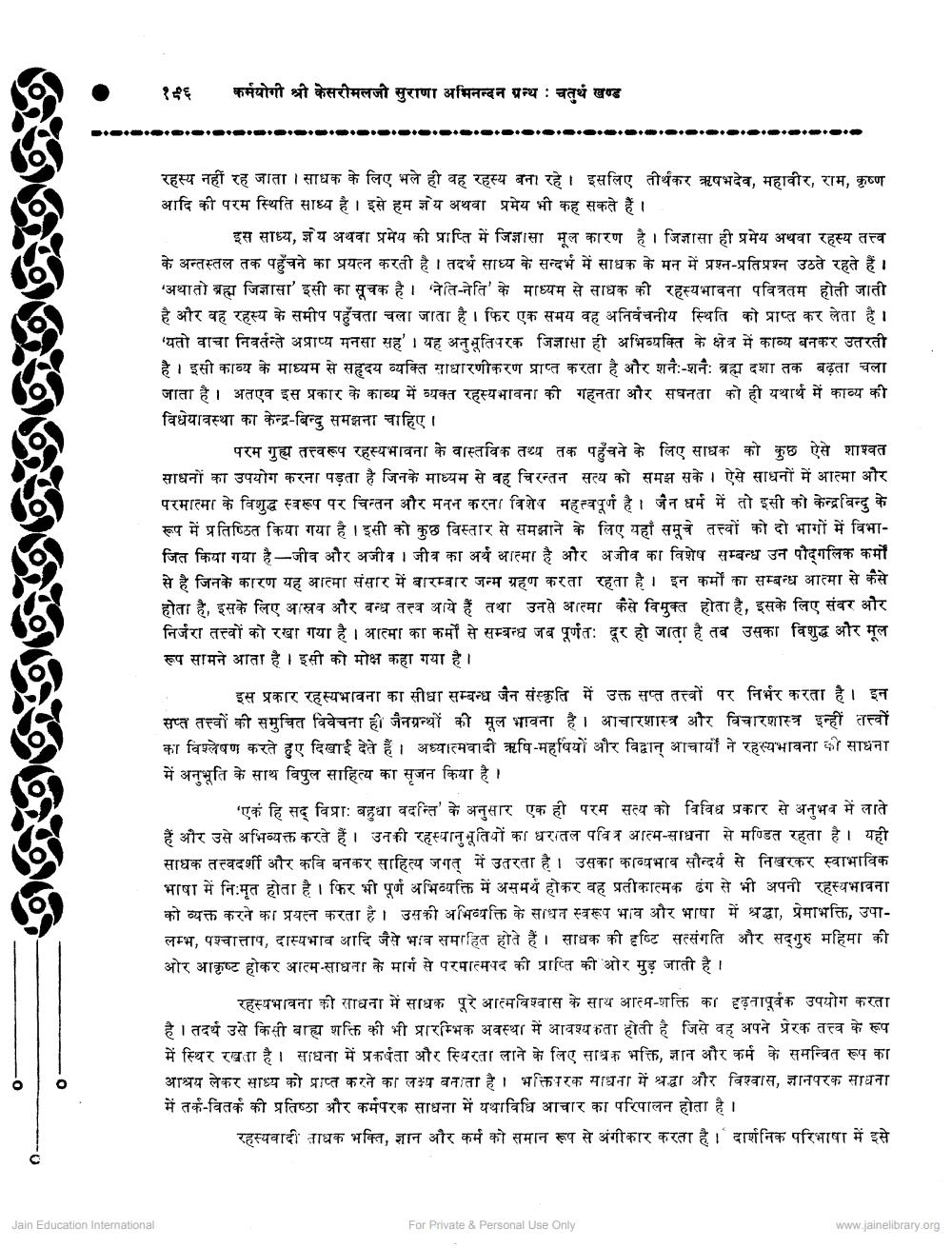________________
१९६
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
रहस्य नहीं रह जाता । साधक के लिए भले ही वह रहस्य बना रहे। इसलिए तीर्थकर ऋषभदेव, महावीर, राम, कृष्ण आदि की परम स्थिति साध्य है। इसे हम ज्ञेय अथवा प्रमेय भी कह सकते हैं।
इस साध्य, ज्ञेय अथवा प्रमेय की प्राप्ति में जिज्ञासा मूल कारण है। जिज्ञासा ही प्रमेय अथवा रहस्य तत्त्व के अन्तस्तल तक पहुँचने का प्रयत्न करती है । तदर्थ साध्य के सन्दर्भ में साधक के मन में प्रश्न-प्रतिप्रश्न उठते रहते हैं। 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' इसी का सूचक है। 'नेति-नेति' के माध्यम से साधक की रहस्यभावना पवित्रतम होती जाती है और वह रहस्य के समीप पहुँचता चला जाता है । फिर एक समय वह अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। 'यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' । यह अनुभूतिपरक जिज्ञासा ही अभिव्यक्ति के क्षेत्र में काव्य बनकर उतरती है। इसी काव्य के माध्यम से सहृदय व्यक्ति साधारणीकरण प्राप्त करता है और शनै:-शनैः ब्रह्म दशा तक बढ़ता चला जाता है। अतएव इस प्रकार के काव्य में व्यक्त रहस्यभावना की गहनता और सघनता को ही यथार्थ में काव्य की विधेयावस्था का केन्द्र-बिन्दु समझना चाहिए।
परम गुह्य तत्त्वरूप रहस्यभावना के वास्तविक तथ्य तक पहुँचने के लिए साधक को कुछ ऐसे शाश्वत साधनों का उपयोग करना पड़ता है जिनके माध्यम से वह चिरन्तन सत्य को समझ सके । ऐसे साधनों में आत्मा और परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप पर चिन्तन और मनन करना विशेष महत्त्वपूर्ण है। जैन धर्म में तो इसी को केन्द्रबिन्दु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । इसी को कुछ विस्तार से समझाने के लिए यहाँ समूचे तत्त्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है-जीव और अजीव । जीव का अर्थ आत्मा है और अजीव का विशेष सम्बन्ध उन पौद्गलिक कर्मों से है जिनके कारण यह आत्मा संसार में बारम्बार जन्म ग्रहण करता रहता है। इन कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से कैसे होता है, इसके लिए आस्रव और बन्ध तत्त्व आये हैं तथा उनसे आत्मा कैसे विमुक्त होता है, इसके लिए संवर और निर्जरा तत्त्वों को रखा गया है । आत्मा का कर्मों से सम्बन्ध जब पूर्णत: दूर हो जाता है तब उसका विशुद्ध और मूल रूप सामने आता है। इसी को मोक्ष कहा गया है। . इस प्रकार रहस्यभावना का सीधा सम्बन्ध जैन संस्कृति में उक्त सप्त तत्त्वों पर निर्भर करता है। इन सप्त तत्त्वों की समुचित विवेचना ही जैनग्रन्थों की मूल भावना है। आचारशास्त्र और विचारशास्त्र इन्हीं तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए दिखाई देते हैं। अध्यात्मवादी ऋषि-महर्षियों और विद्वान् आचार्यों ने रहस्यभावना की साधना में अनुभूति के साथ विपुल साहित्य का सृजन किया है।
'एक हि सद् विप्राः बहुधा वदन्ति' के अनुसार एक ही परम सत्य को विविध प्रकार से अनुभव में लाते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं। उनकी रहस्यानुभूतियों का धरातल पवित्र आत्म-साधना से मण्डित रहता है। यही साधक तत्त्वदर्शी और कवि बनकर साहित्य जगत् में उतरता है। उसका काव्यभाव सौन्दर्य से निखरकर स्वाभाविक भाषा में नि:मृत होता है। फिर भी पूर्ण अभिव्यक्ति में असमर्थ होकर वह प्रतीकात्मक ढंग से भी अपनी रहस्यभावना को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। उसकी अभिव्यक्ति के साधन स्वरूप भाव और भाषा में श्रद्धा, प्रेमाभक्ति, उपालम्भ, पश्चात्ताप, दास्यभाव आदि जैसे भाव समाहित होते हैं। साधक की दृष्टि सत्संगति और सद्गुरु महिमा की ओर आकृष्ट होकर आत्म-साधना के मार्ग से परमात्मपद की प्राप्ति की ओर मुड़ जाती है ।
रहस्यभावना की साधना में साधक पूरे आत्मविश्वास के साथ आत्म-शक्ति का दृढ़तापूर्वक उपयोग करता है । तदर्थ उसे किसी बाह्य शक्ति की भी प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता होती है जिसे वह अपने प्रेरक तत्त्व के रूप में स्थिर रखता है। साधना में प्रकर्षता और स्थिरता लाने के लिए साधक भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वित रूप का आश्रय लेकर साध्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है। भक्तिपरक साधना में श्रद्धा और विश्वास, ज्ञानपरक साधना में तर्क-वितर्क की प्रतिष्ठा और कर्मपरक साधना में यथाविधि आचार का परिपालन होता है।
रहस्यवादी ताधक भक्ति, ज्ञान और कर्म को समान रूप से अंगीकार करता है। दार्शनिक परिभाषा में इसे
-
००
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org