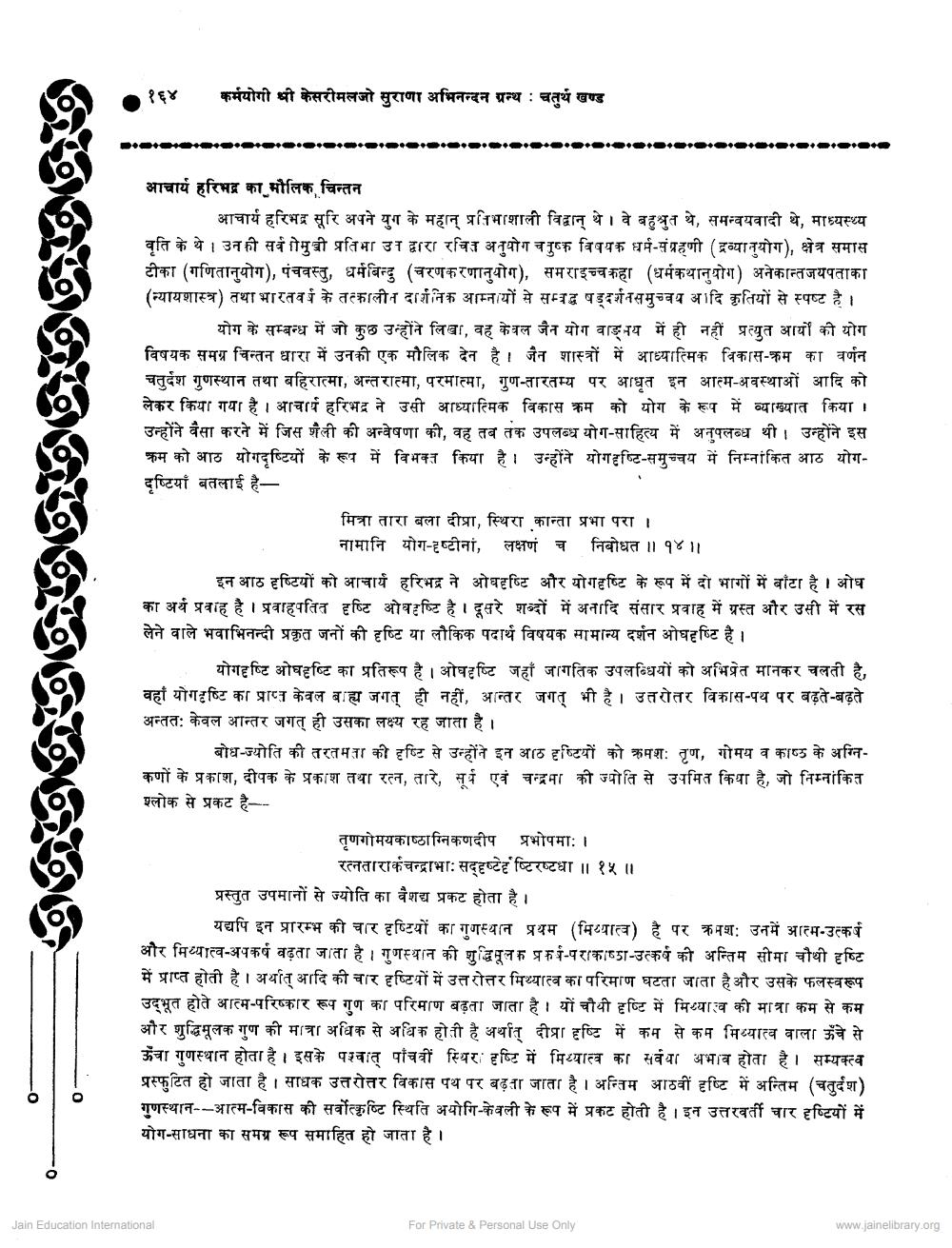________________
.१६४
कर्मयोगी श्री केसरीमलजो सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
..
..
.
....
..
..
..
......
....
..........
..
.....................
..
..
..
..
.......
आचार्य हरिभद्र का मौलिक चिन्तन
आचार्य हरिभद्र सूरि अपने युग के महान् प्रतिभाशाली विद्वान् थे। वे बहुश्रुत थे, समन्वयवादी थे, माध्यस्थ्य वृति के थे। उनकी सर्व गोमुखी प्रतिभा उस द्वारा रचित अनुयोग चतुष्क विषयक धर्म-संग्रहणी (द्रव्यानुयोग), क्षेत्र समास टीका (गणितानुयोग), पंचवस्तु, धर्मबिन्दु (चरणकरणानुयोग), समराइच्चकहा (धर्मकथानुयोग) अनेकान्तजयपताका (न्यायशास्त्र) तथा भारतवर्ष के तत्कालीन दार्शनिक आम्नायों से सम्बद्ध षड्दर्शनसमुच्चय आदि कृतियों से स्पष्ट है।
योग के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने लिखा, वह केवल जैन योग वाङ्मय में ही नहीं प्रत्युत आर्यों की योग विषयक समग्र चिन्तन धारा में उनकी एक मौलिक देन है। जैन शास्त्रों में आध्यात्मिक विकास-क्रम का वर्णन चतुर्दश गुणस्थान तथा बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, गुण-तारतम्य पर आधृत इन आत्म-अवस्थाओं आदि को लेकर किया गया है । आचार्य हरिभद्र ने उसी आध्यात्मिक विकास क्रम को योग के रूप में व्याख्यात किया । उन्होंने वैसा करने में जिस शैली की अन्वेषणा की, वह तब तक उपलब्ध योग-साहित्य में अनुपलब्ध थी। उन्होंने इस क्रम को आठ योगदृष्टियों के रूप में विभक्त किया है। उन्होंने योगदृष्टि-समुच्चय में निम्नांकित आठ योगदृष्टियाँ बतलाई है
मित्रा तारा बला दीप्रा, स्थिरा कान्ता प्रभा परा ।
नामानि योग-दृष्टीना, लक्षणं च निबोधत ॥ १४ ।। इन आठ दृष्टियों को आचार्य हरिभद्र ने ओघदृष्टि और योगदृष्टि के रूप में दो भागों में बाँटा है । ओघ का अर्थ प्रवाह है । प्रवाहपतित दृष्टि ओषदृष्टि है । दूसरे शब्दों में अनादि संसार प्रवाह में ग्रस्त और उसी में रस लेने वाले भवाभिनन्दी प्रकृत जनों की दृष्टि या लौकिक पदार्थ विषयक सामान्य दर्शन ओघदृष्टि है।
योगदृष्टि ओघदृष्टि का प्रतिरूप है । ओघदृष्टि जहाँ जागतिक उपलब्धियों को अभिप्रेत मानकर चलती है, वहाँ योगदष्टि का प्राप्त केवल बाह्य जगत् ही नहीं, आन्तर जगत् भी है। उत्तरोतर विकास-पथ पर बढ़ते-बढ़ते अन्तत: केवल आन्तर जगत् ही उसका लक्ष्य रह जाता है।
बोध-ज्योति की तरतमता की दृष्टि से उन्होंने इन आठ दृष्टियों को क्रमश: तृण, गोमय व काष्ठ के अग्निकणों के प्रकाश, दीपक के प्रकाश तथा रत्न, तारे, सूर्य एवं चन्द्रमा की ज्योति से उपमित किया है, जो निम्नांकित श्लोक से प्रकट है--
तृणगोमयकाष्ठाग्निकणदीप प्रभोपमाः ।
रत्नतारार्कचन्द्राभा: सदृष्टेदृष्टिरष्टधा ।। १५ ।। प्रस्तुत उपमानों से ज्योति का वैशद्य प्रकट होता है।
यद्यपि इन प्रारम्भ की चार दृष्टियों का गुणस्थान प्रथम (मिथ्यात्व) है पर क्रमश: उनमें आत्म-उत्कर्ष और मिथ्यात्व-अपकर्ष बढ़ता जाता है। गुणस्थान की शुद्धिमूलक प्रकर्ष-पराकाष्ठा-उत्कर्ष की अन्तिम सीमा चौथी दृष्टि में प्राप्त होती है । अर्थात् आदि की चार दृष्टियों में उत्तरोत्तर मिथ्यात्व का परिमाण घटता जाता है और उसके फलस्वरूप उद्भूत होते आत्म-परिष्कार रूप गुण का परिमाण बढ़ता जाता है। यों चौथी दृष्टि में मिथ्यात्व की मात्रा कम से कम और शुद्धिमूलक गुण की मात्रा अधिक से अधिक होती है अर्थात् दीपा दृष्टि में कम से कम मिथ्यात्व वाला ऊँचे से ऊँचा गुणस्थान होता है। इसके पश्चात् पाँचवीं स्थिर दृष्टि में मिथ्यात्व का सर्वथा अभाव होता है। सम्यक्त्व प्रस्फुटित हो जाता है। साधक उत्तरोत्तर विकास पथ पर बढ़ता जाता है । अन्तिम आठवीं दृष्टि में अन्तिम (चतुर्दश) गुणस्थान---आत्म-विकास की सर्वोत्कृष्टि स्थिति अयोगि-केवली के रूप में प्रकट होती है। इन उत्तरवर्ती चार दृष्टियों में योग-साधना का समग्र रूप समाहित हो जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org